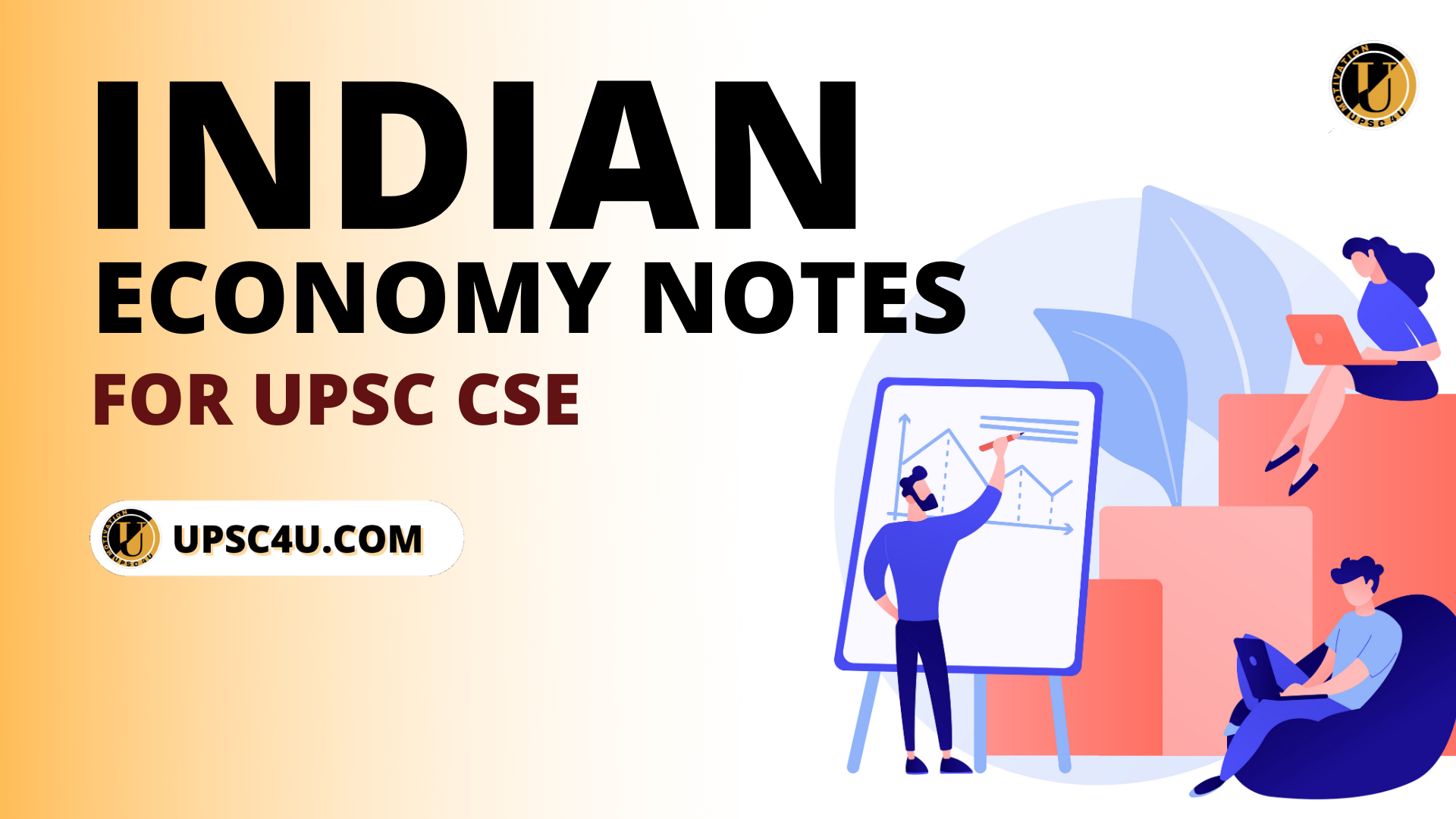RBI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली
- भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी विनियमित इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिये एकल खिड़की के रूप में RBI की वेबसाइट पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) की शुरुआत की है।
- इस प्रणाली को शुरू करने का उद्देश्य शिकायतों का समय से समाधान कर ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है।
- RBI के अनुसार, इस प्रणाली को शुरू करने से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- इस प्रणाली की सहायता से ग्राहक सार्वजनिक/पब्लिक इंटरफेस वाली किसी भी विनियमित इकाई जैसे- वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- CMS के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शिकायत को उपयुक्त लोकपाल कार्यालय या रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय ऑफिस को भेज दिया जाएगा।
- CMS को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के ज़रिये एक्सेस किया जा सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक CMS के डेटा को विश्लेषण के लिये उपयोग कर सकता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर विनियामक और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के लिये किया जा सकता है।
- ग्राहकों द्वारा दर्ज शिकायतों के स्टेटस को ट्रैक करने के लिये रिज़र्व बैंक एक डेडीकेटेड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (IVR) सिस्टम भी लागू करने की योजना बना रहा है।
क्या होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- यह भारत में सरकार द्वारा प्रबंधित एक प्रणाली हैजिसमे समाज के गरीब वर्गों को भोजन, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करते हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित ‘उचित मूल्य की दुकानों’ (FPS) या राशन की दुकानों की एक शृंखला के माध्यम से खाद्य और कुछ गैर-खाद्य पदार्थ रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस प्रणाली का प्रबंधन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- राज्य और केंद्र सरकारें गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे ऊपर के समुदायों के लिये कम कीमत पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने हेतु काम करती हैं।
- केंद्र सरकार संसाधनों की खरीद, संरक्षण, परिवहन और आवंटन हेतु उत्तरदायी है।
- राज्य सरकार कार्ड और दुकानों के माध्यम से इन राशनकार्ड धारकों की पहचान और उपलब्धता का एक नेटवर्क स्थापित करना सुनिश्चित करती है।
- केंद्र सरकार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में वितरण के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है।कुछ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ आउटलेट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुओं जैसे- दालें, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले आदि का वितरण भी करते हैं।
- ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013’ कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
क्या है अति महत्वपूर्ण UNFCCC, IPCC तथा PCA?
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)
- UNFCCC का का अर्थ ‘जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क’ से है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
- UNFCCC सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है।
- UNFCCC जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है।
- यह समझौता जून, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था।
- विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।
- वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) के नाम से जाना जाता है।
- UNFCCC के तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ और विकसित देशों (एनेक्स-1 में शामिल देश) द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया।
- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।
- यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है।
- UNFCCC का सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। जिसमें 195 सदस्य देश हैं।
- इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोिखमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है।
- IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका मुख्यालय ज़िनेवा में स्थित है।
पेरिस जलवायु समझौता
- यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP 21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों द्वारा अपनाया गया था।
- औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिमानतः इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना।
- वर्ष 2050 से 2100 के बीच मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों और मृदा द्वारा इसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।