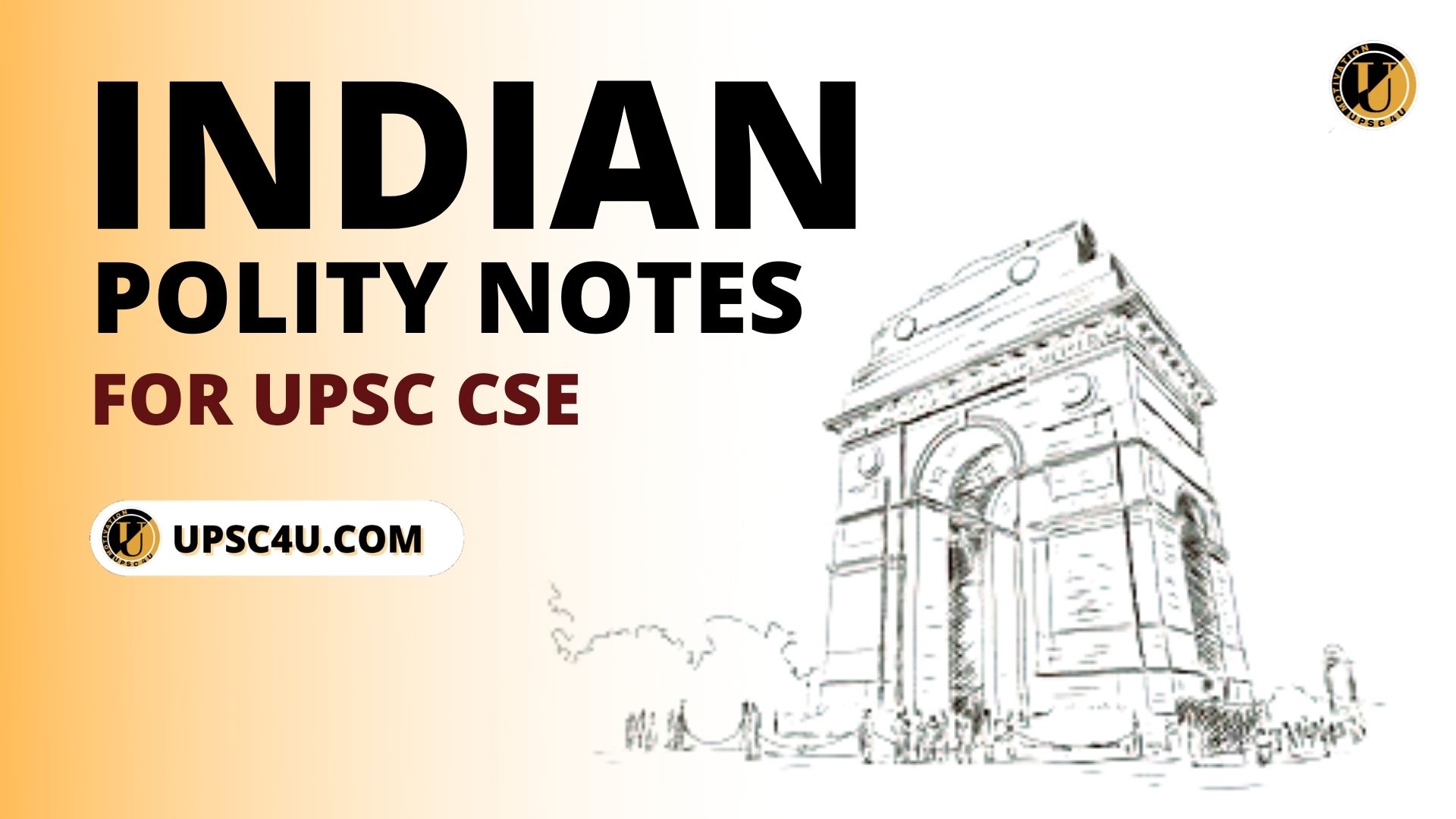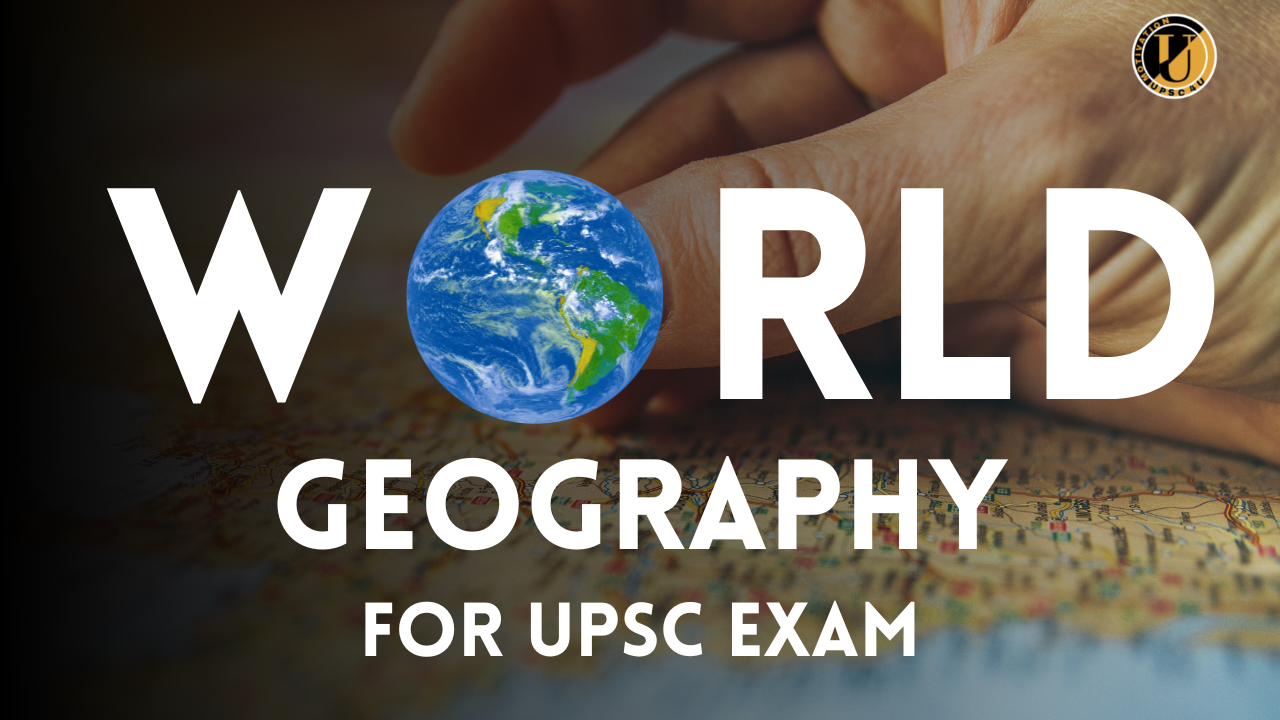अभ्रक Mica
अभ्रक एक बहुपयोगी गैर-धात्विक खनिज है। यह लचीला, चमकदार, हल्का, ताप निरोधक व विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग विद्युत-उद्योग, रेडियो तथा वायुयान निर्माण में होता है। उद्योगों में अभ्रक के छोटे-छोटे टुकड़ों का उपयोग माइकेनाइट के रूप में होता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी तन्यता है जिसके कारण इसे किसी भी वस्तु परत के रूप में चढ़ाया जा सकता है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे नेत्ररक्षक चश्मों, मकानों आदि के सजावट के सुन्दर कागज, लालटेन की चिमनियों और खपरैलों के निर्माण कार्य में किया जाता है।
सफेद अभ्रक के टुकड़े धारियों के रूप में बनी हुई पैग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में ही मिलते हैं। इसको मस्कोवाइट अभ्रक, सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन लिए अभ्रक की वायोटाइप अभ्रक कहते हैं।
अभ्रक का एक प्रमुख गुण उसका पूर्ण आधार विदलन है। किसी भी वस्तु पर इसकी पतली से पतली परत चढ़ायी जा सकती है।
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (United Nations Framework Classification -UNFC) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 तक देश में अभ्रक का कुल भंडार 393855 अनुमानित है, जिसमें से केवल 68570 टन संरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है। शेष संसाधन में 325285 टन है। राजस्थान में 51 प्रतिशत अभ्रक है।
वितरण: भारत विश्व में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक उत्पादक देश है और यहीं से विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अभ्रक प्राप्त होता है। यह झारखंड में कोडरमा अभ्रक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र और राजस्थान अभ्रक क्षेत्र में पाया जाता है।
कोडरमा अभ्रक क्षेत्र झारखंड में स्थित है। यह क्षेत्र गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर जिले तक फैला हुआ है। यहाँ का अभ्रक सफ़ेद है, जिसकी परत गुलाबी रंग की होती है। इसे बंगाल रूबी कहा जाता है।
नेल्लौर अभ्रक क्षेत्र गुंटूर और संगम के मध्य फैला हुआ है। इस क्षेत्र का अभ्रक निम्न कोटि का है, जिससे हरे रंग की झलक मिलती है।
राजस्थान अभ्रक क्षेत्र जयपुर एवं उदयपुर जिले के मध्य फैला हुआ है। यहां सर्वाधिक अभ्रक भीलवाड़ा से प्राप्त होता है।
कर्नाटक में मैसूर और हसन जिले में मुख्य खानें हैं। यहां अभ्रक निम्न कोटि का पाया जाता है।
तमिलनाडु में अभ्रक तिरुनेलवैली जिले में, कोयम्बटूर जिले में, तिरुचिरापल्ली जिले में, मदुराई जिले में और कन्याकुमारी जिले में मिलता है।
केरल में अलप्पी और क्विलोन जिले में भी कुछ अभ्रक प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में भी अभ्रक पाया जाता है।
चूना-पत्थर Limestone
चूना-पत्थर का काफी प्रयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जो कि निर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग कोयला खदानों में सफाई के लिए, अयस्क से सिलिका और एलुमिना को पृथक् करने में तथा ब्लीचिंग पाउडर और सोडा ऐश जैसे रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। इसका प्रयोग चीनी के परिष्करण में तथा चीनी उद्योग में अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। कांच, रबड़ एवं कागज उद्योग में यह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चूना-पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट्स अथवा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स से बना है। यह अवसादी शैल है। यह गोंडवाना को छोड़कर प्रायः सभी भूवैज्ञानिक संरचना में पाया जाता है।
वितरण: मध्य प्रदेश में, चूना-पत्थर निक्षेप कटनी, जबलपुर, अलकतारा बिलासपुर जिले में, और छत्तीसगढ़ में, रायपुर, राजगढ़, बस्तर, दुर्ग, बैतूल और सागर जिलों में मिलती हैं। रीवा में सीमेंट-वर्गीय चूना-पत्थर मिलता है।
आंध्र प्रदेश में, गुंटूर, कृष्णा, कुडप्पा, खम्माम, कुर्नूल, नालगोंडा, और गोदावरी जिले में चूना-पत्थर मिलता है। तमिलनाडु में मुख्य रूप से सीमेंट वर्गीय चूना-पत्थर तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मदुरई, रामनाथपुरम् आदि जिलों में मिलता है। सलेम में प्रवाही चूना-पत्थर मिलता है। चूना की प्राप्ति तिरुनेलवेल्ली, दक्षिणी अर्काट और तंजावुर जिले के सुरक्षित भण्डार से भी होती है।
कर्नाटक में शिमोगा, बेलगांव और बीजापुर जिलों में प्रवाही चूना-पत्थर मिलता है। मैसूर, गुलबर्ग, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में भी चूना-पत्थर का भण्डार है।
गुजरात में, जूनागढ़, बनासकंथा, साबरकथा और खेड़ा जिलों में उच्च स्तर का चूना-पत्थर पाया जाता है।
राजस्थान में वर्गीय चुना-पत्थर जयपुर, सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, सिरोही, बूंदी और बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है।
मेघालय में खासी और जयंतियां पहाड़ियों में; असम में नौगांव और सिबसागर जिले; बिहार में आरा जिला; झारखंड में पलामू, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिले; महाराष्ट्र में अहमदनगर, यवतमाल, चंद्रपुर और नांदेड़ जिले आदि में भी चूना-पत्थर मिलता है।
डोलोमाइट Dolomite
यह रंगहीन, सफेद तथा कभी-कभी गुलाबी रंग में पाया जाता है। इससे मैग्नीशियम व कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है।
वितरण: डोलोमाइट झारखंड के सिंहभूम और बिहार के शाहाबाद जिले; तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली, सलेम जिले और तूतीकोरिन के समीप समुद्रतटीय क्षेत्र; ओडीशा में बीरमित्रपुर, बिल्डीह, खतेपुर, हाथीबारी (संबलपुर जिला) और कोरापुट जिले; छत्तीसगढ़ में बिलासपुर व दुर्ग जिले; हिमाचल प्रदेश की हिमालयीय पहाड़ी के कुछ क्षेत्र और गुजरात के भावनगर तथा वड़ोदरा जिलों में मिलता है।
घीया-पत्थर Steatite

घीया-पत्थर टॉल्क नामक खनिज की एक अच्छी किस्म है। टॉल्क अभ्रक के समान परतदार और सफेद होता है। यह खनिज विशेषतः मैग्नेशिया, सिलिका और जल का सम्मिश्रण होता है। इसका संबंध आग्नेय अथवा डोलोमाइट और चूने के पत्थर से है।
वितरण: राजस्थान में घीया-पत्थर के सर्वाधिक भंडार हैं। भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर जिलों में राज्य के कुल उत्पाद का ⅘ भाग पैदा होता है। अलवर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर जिलों में भी घीया पत्थर मिलता है।
आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कर्नूल, नेल्लौर, वारंगल, कडुप्पा और चितूर जिले में यह प्राप्त किया जाता है।
झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और रांची जिले में घीया-पत्थर पाया जाता है।
घीया-पत्थर के भण्डार अन्य राज्यों में इस प्रकार हैं- मध्य प्रदेश (मुख्यतया जबलपुर और झाबुआ जिले में); कर्नाटक (बेल्लारी, शिमोगा, हासन, बीजापुर, तुमकुर, मैसूर और दक्षिण कनारा जिलों में); ओडीशा (तिरिंग के पास, केंदूमुंडी और मयूरभंज में खारीदमक जिला, बालसोर जिला, सुंदरगढ़ जिला और कटक जिला); तमिलनाडु (सलेम, कोयम्बटूर, उत्तरी और दक्षिणी अरकाट तथा तिरुचिरापल्ली जिलों में); गुजरात (वरथा, घण्टा और धूरवास); महाराष्ट्र (रत्नागिरि का भाग, बांद्रा और चन्द्रपुर जिलों में) तथा पश्चिम बंगाल (पुरुलिया दार्जिलिंग और मिदनापुर जिले)।
मैग्नेसाइट Magnesite
मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण खनिज है। यह ऊष्मसह खनिज है। मैग्नेसाइट का फोटोग्राफी और आतिशबाजी के लिए पाउडर बनाने में, हवाई जहाज में मिश्रधातु के लिए, अग्नि और धूल प्रतिरोधक होने के कारण अस्पतालों, आदि में प्रयोग किया जाता है।
यहां प्राकृतिक मैग्नेसाइट की दो प्रमुख किस्म हैं-
क्रिस्टलाइन या स्पथिक तथा एमॉरफॉस या मेसिब। एमॉरफॉस किस्म, हालांकि क्रिस्टलीय किस्म की शुद्धता की अपेक्षा थोड़ी कम प्राप्त होती है। मैग्नेसाइट सर्पिल पुंज में अनियमित नसों और विभंजन क्षेत्रों में पाया जाता है।
वितरण: भारत में मैग्नेसाइट के बड़े भण्डार हैं। भारत में कुल मैग्नेसाइट का लगभग दो-तिहाई भाग तमिलनाडु के सलेम जिले में मिलता है और चौथाई भाग से अधिक उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले से प्राप्त होता है। कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में छोटे-स्तर पर इसका उत्पादन होता है।
क्यानाइट Kyanite
क्यानाइट एल्युमिनियम सिलिकेट वर्ग का एक खनिज है। इसकी प्राप्ति आग्नेय एवं कायान्तरित चट्टानों से होती है। विश्व के सभी क्यानाइट उत्पादक देशों में भारत का सर्वोच्च स्थान है। भारत में झारखंड के सिंहभूम जिले में 80 मील लंबी पट्टी में सर्वाधिक क्यानाइट मिलता है। बिहार का लाप्साबुरू का क्यानाइट भण्डार विश्व का सबसे बड़ा क्यानाइट का भण्डार है। क्यानाइट का कुछ उत्पादन अभ्रक-क्षेत्र में भी होता है।
वितरण: विश्व के सभी क्यानाइट उत्पादक देशों में भारत का सर्वोच्च स्थान है। भारत में झारखंड के सिंहभूम जिले में 80 मील लंबी पट्टी में सर्वाधिक क्यानाइट मिलता है। बिहार का लाप्साबुरू का क्यानाइट भण्डार विश्व का सबसे बड़ा क्यानाइट का भण्डार है। क्यानाइट का कुछ उत्पादन अभ्रक-क्षेत्र में भी होता है।
महाराष्ट्र में बांद्रा जिला प्रमुख क्यानाइट उत्पादक है। कर्नाटक में हासन, मैसूर और चित्रदुर्ग जिले प्रमुख क्यानाइट उत्पादक हैं।
राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और पुरुलिया जिले, हिमाचल प्रदेश में महासू जिला, तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिला और हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिला क्यानाइट के अन्य उत्पादक हैं।
सिलिमेनाइट Sillimanite
यह एल्युमिनियम का सिलिकेट है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। यह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है।
वितरण: कुल उत्पादन का चौथा या पांचवां भाग मेघालय की खासी पहाड़ियों में उत्पादित होता है। इसके अलावा सिलिमेनाइट के अन्य उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले महत्वपूर्ण हैं। इसके भंडार केरल की समुद्री बालू में और बिहार के गया और झारखंड के हजारीबाग जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली जिले तथा महाराष्ट्र के नागपुर और बांद्रा जिले में भी मिलते हैं।
ग्रेफाइट Graphite
ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जिसे काला सीसा भी कहा जाता है। इसके अयस्क के साथ सिलिका और सिलिकेट भी मिलता है।
वितरण: आध्र प्रदेश में पडानकोंडा में ग्रेफाइट का भण्डार है, जिसमें 40 से 65 प्रतिशत तक कार्बन की मात्रा मिलती है। पश्चिमी गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिले मुख्य ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। कृष्णा, खम्माम, विशाखापत्तनम, गुंटूर, बुदेरू और श्रीकाकुलम अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं।
ओडिशा में कालाहांडी, बोलंगिरी, संबलपुर, कोरापुट और फुलबानी जिले प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। यहां 55-60 प्रतिशत तक कार्बन की मात्रा वाला ग्रेफाइट मिलता है।
बिहार में रजहारा और खानडीह में 50 प्रतिशत की कार्बन की मात्रा वाला ग्रेफाइट मिलता है।
तमिलनाडु में तिरुनेलवेल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम् जिले में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में ग्रेफाइट मिलता है।
एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट Apatite and Rock Phosphate
एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट को खनिजों के समूह में शामिल किया जाता है, यह प्राकृतिक तौर पर मूल फॉस्फेट के रूप में, ऐपेटाइट या रॉक फास्फेट, या फास्फोराइट के रूप में पाया जाता है। यह सामान्यतः आग्नेय और अवसादी शैलों में मिलता है। ऐपेटाइट सफेद, भूरा-स्लेटी, हरा या गहरा हरा रंग का हो सकता है।
ऐपेटाइट कच्चा माल के तौर पर बेहद उपयोगी है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उपचार के बाद सुपरफास्फेट फास्फेरिक उर्वरकों के निर्माण में काम आता है। इसकी थोड़ी मात्रा का स्पन पाइप के लिए उच्च फास्फोरस पिग आयरन के निर्माण में किया जाता है।
जिप्सम Gypsum
जिप्सम एक हाइड्रेट कैल्सियम सल्फेट है, जो साधारणतया अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जैसे-चूना-पत्थर, बालू-पत्थर तथा शेल के रूप में। यह खनिज दो रासायनिक तत्वों के संयोजन से यथा CasO4 . 2H2O तथा CaSO4 से मिलकर बना है, जिनमें संघटकों की मात्रा लगभग 79.1 प्रतिशत तथा जल की मात्रा 20.9 प्रतिशत है। उस प्रकार के खनिज को कभी जिप्सम नहीं कहा जाना चाहिए, जिसमें CaSO4 .2H2O का मिश्रण 64.5 प्रतिशत से कम वजन का हो। जिप्सम पांच प्रकार का होता है-
- शुद्ध जिप्सम की प्रकृति क्रिस्टलीय और पारदर्शी होती है।
- एलबास्टर, सघन, ठोस, खादार और पारभासी होता है।
- चमकीला, रेशेदार प्रकार होता है।
- जिप्साइट, धरातलीय, मुलायम और अशुद्ध प्रकार है, जिसमें कठोर जिप्सम चिकनी एवं बलुई मिट्टी से प्राप्त होता है।
- चट्टानीय जिप्सम एक रवादार, युग्मित एवं ठोस प्रकार का जिप्सम अयस्क है, जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। यह अशुद्ध माना जाता है।
इसके उत्पादन का उपयोग भवन निर्माण के लिए प्रयुक्त सीमेंट के निर्माण में होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के प्लास्टर के कार्य होते हैं। जिप्सम का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण में तथा अन्य संरचनात्मक उद्योगों में होता है। इसका उपयोग उर्वरक तथा पेंट निर्माण, रबड़ तथा कागज उद्योग में तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में भी होता है।
वितरण: जिप्सम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भण्डार राजस्थान राज्य में पाया जाता है। यहां ज्प्सम की आधे से दो मीटर तक की मोटी चादरें न्हार्तीय मरुस्थल में यहाँ-वहां चरों ओर फैली हुई मिलती है, विशेष रूप से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चुरू, नागौर, पाली, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों में।
जिप्सम का एक महत्वपूर्ण भण्डार तमिलनाडु स्थित कोयम्बटूर के निकट अन्नुप्पापट्टी, अण्डियूर, वेंकटापुरम तथा पुसरीपट्टी क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिलनाडु में रामानाथपुरम तथा कोयम्बटूर में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है।
उत्तराखण्ड में जिप्सम का उत्पादन विभिन्न स्थलों पर, जैसे- लक्ष्मण झूला, खरारी छट्टी के चारों ओर, सीरा, नरेन्द्रनगर और गुघथानी (गढ़वाल जिला में) और इसके समीप धपीला, भट्टा, खलगांव, सहस्रधारा, नैनीताल, खुरपतल और देहरादून जिलों में स्थित मंझरिया क्षेत्रों में होता है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिप्सम उत्पादन क्षेत्रों के विषय में पता चला है, जिसमें झांसी जिले में स्थित गोन्ती तथा परसुआ और हमीरपुर जिले के समीप स्थित पुरूने स्थल प्रमुख हैं।
जम्मू-कश्मीर में स्थित बारमूला और डोडा जिलों में भी जिप्सम का उत्पादन किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश में जिप्सम का संग्रह क्रॉन चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट के साथ चम्बा, महासू और सिरमौर जिले में पाया गया है।
गुजरात में जिप्सम का उत्पादन सौराष्ट्र क्षेत्र में, विशेष रूप से हलार और भावनगर जिले में गुहिलवाड, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ क्षेत्रों में होता है। जामनगर जिले में सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र रन, वीरपुर और भाटीस है।
सुरक्षित भंडार: भारत में जिप्सम का प्रतिलक्ष्य अनुमानित भंडार 383 मिलियन टन का है। इसमें से 2 मिलियन टन सर्जिकल प्लास्टर श्रेणी का है, 92 मिलियन टन उर्वरक या चीनी मिट्टी स्तर का है, 76 मिलियन लाख टन सीमेंट या पेंट स्तर का है, 13 मिलियन टन भूमि सुधार स्तर का है और शेष अवर्गीकृत किस्म का है।
एस्बेस्टस Asbestos
एस्बेस्टस का व्यापारिक मूल्य काफी है क्योंकि इसका उपयोग अग्नि प्रतिरोधक वस्तु (तख्ते, कपड़े, कागज, परदे आदि) बनाने के लिए किया जाता है। हाल ही में, हालांकि, इसकी विषाक्तता सामने आई है।
वितरण: भारत में एस्बेस्ट्स का लगभग 95 प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त किया जाता है।
राजस्थान के अजमेर अलवर, डूंगरपुर, पाली और उदयपुर जिलों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश (कड्डप्पा जिला), कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड और नागालैंड एस्बेस्टस के अन्य उत्पादक राज्य हैं।
नमक Salt
नमक सोडियम क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस से बना होता है। यह प्रमुखतः समुद्र तथा खारी झीलों से प्राप्त किया जाता है। नमक को अनेक तरह से उपयोग में लाया जाता है। यह रासायनिक पदार्थों, रंग, कांच, खाद, स्टॉर्च आदि उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, नमक का तेजाब, सोडियम व क्लोरीन बनाने तथा चमड़ा रंगने, मछलियां सुखाने तथा ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में भी होता है।
नमक प्राप्ति के स्रोत:
- समुद्र: नमक उत्पादन हेतु समुद्र सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में 70 प्रतिशत नमक का उत्पादन समुद्रतटीय क्षेत्रों में होता है।
- खनिज लवण: यह विशेष चट्टानों में उपलब्ध होता है। हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में सर्वाधिक क्षेत्र मिलते हैं।
- आंतरिक झीलें: राजस्थान की सांभर भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है।
- अधोभूमि लवण: भारत में भूमि के नीचे मिलने वाला नमक राजस्थान के भरतपुर तथा तमिलनाडु जिलों में पाया जाता है। कच्छ का रन इसका सबसे बड़ा स्रोत है।
समुद्री नमक प्राप्ति के क्षेत्र: भारत में नमक का निर्माण सर्वाधिक समुद्रतटीय क्षेत्रों में किया जाता है। कुल नमक उत्पादन का ⅓ भाग समुद्र से प्राप्त किया जाता है। नमक निर्माण के सर्वाधिक कारखाने मुम्बई क्षेत्र में स्थित हैं। सूरत से मंगलुरु तक नमक उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। ये तटीय क्षेत्र अपने उत्पादन का केवल ¼ भाग ही उपयोग करते हैं शेष मध्य भारत तथा उत्तर भारत को सम्पूरित कर दिया जाता है। नमक निर्माण के प्रमुख क्षेत्र निम्नांकित हैं-
सौराष्ट्र तथा कच्छ तट: इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है। सौराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर चौड़ाई के औसतन 7-8 मीटर गहरे कुओं से खारा जल निकाल कर नमक निर्माण किया जाता है। सौराष्ट्र के मुख्य नमक उत्पादन केंद्र हैं-मीठापुर, मोरवी में लखनपुर, जामनगर में बेदी, धारंगध्रा में कुटू व पोरबंदर, जूनागढ़ में भैरई, क्रीक तथा बेरावल, जंजीरा में जाफराबाद, भावनगर व कच्छ में कांडला, जसदान, दहीगाम, बजाना, खारगोधा और खम्बात की खाड़ी में मंडप, भीमन्दर, ऊरन, धरसाणा और छरवादा।
धारगंध्रा, द्वारका व पोरबंदर में क्षार प्राप्त किया जाता है और खारगोधा में मैग्नीशियम प्राप्त करने के कारखाने भी हैं।
महाराष्ट्र: यहां नमक निर्माण प्रमुखतः सामुद्रिक जल से किया जाता है। कोलाबा, रत्नागिरि व ठाणे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
केरल: यहां एक दर्जन से अधिक स्थानों पर नमक बनाया जाता है। इनमें प्रमुख हैं एलॉन, पुपालम, पालकुलम, वरीयूर, मालीपुरम तथा थामरकुलम इत्यादि।
तमिलनाडु: आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों के तटीय क्षेत्रों पर नमक निर्माण होता है। तमिलनाडु के निम्न जिले प्रमुख नमक उत्पादक क्षेत्र हैं: चिंगलपेट- थिलाई, बोयालूर, अट्टीपुट, वलूर, चेमूर और चूनमपेट।
दक्षिणी अर्काट– मरकनम, कडूडालोर, मनमबाड़ी।
तंजावुर- नेदवसाल, कत्तमबाड़ी, वेदनारयणम ट्रक्वींनार, नागापाट्टिपम।
रामनाथपुरम– थीथान्दथरम, बन्तानम, मोरेकुलम, मनाकुडी।
तिरूनेलवैली- अरसादी, कारानौरा, कुलासैकरपटनम।
कन्याकुमारी- कोलम्बेल, करापद, कल्याणपटनम।
आन्ध्र प्रदेश: यहाँ नामक की प्राप्ति श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और नैल्लौर जिलों के तटीय भागों से की जाती है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख केंद्र नानापदा व पेनूगुडूरू हैं।
आोडीशा: यहां नमक-निर्माण बालासोर व गंजाम जिलों में किया जाता है। यहां चिल्का झील से भी नमक प्राप्त किया जाता है।
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल की तटीय परिस्थितियों के नामक निर्माण के प्रतिकूल होते हुए भी नमक निर्माण के प्रयास किये गये हैं। यहां परिस्थितियां विपरीत होने के कारण हैं- नदियों के मीठे जल का खारे जल में भारी मात्रा में मिलना व अधिक वर्षा इत्यादि। मिदनापुर के निकट सूर्यताप से नमकीन जल को सुखाकर नमक बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं। यहां कौण्टाई तट पर नमक बनाया जाता है।
खारी झीलों से नमक प्राप्ति: कच्छ के तट से लेकर राजस्थान तक फैली विस्तृत मरुभूमि की खारी झीलों से नमक निर्माण किया जाता है। यहां पर जयपुर जिले में सांभर व जोधपुर जिले में डीडवाणा, फलौदी और डिगाणा और बीकानेर में लूनकर्णसागर नामक खारी झीलें हैं।
सांभर झील उत्तर भारत के लिए नमक की लगभग संपूर्ण पूर्ति करती है।
सोडियम नमक: मिट्टी के ऊपर जमी नमकीन परतों से सोडियम नामक की प्राप्ति की जाती है। इन परतों को रेह, कलर, ऊसर थूर या खारी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सोडियम नमक की पतें मेरठ, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, कानपुर, गढ़मुक्तेश्वर, हाथरस, मथुरा व शाहजहांपुर के निकट मिलती हैं। उत्तम किस्म की रेह गढ़मुक्तेश्वर में पायी जाती है तथा गाजियाबाद के बहुत बड़े क्षेत्र में रेह मौजूद है। बिहार में मुजफ्फरपुर, सारण और चम्पारण जिलों तथा शेखूपुरा व नवादा क्षेत्र में रेह पायी जाती है। इसके अतिरिक्त निम्न स्थानों पर भी रेह पायी जाती है-
- गुजरात में प्रतिज कस्बे के निकट खारी नदी के किनारे।
- महाराष्ट्र में बुलढाना जिले की लोनार झील।
- कर्नाटक में मैसूर, मंड्या, तुमकुर, गुलबर्ग व चित्रदुर्ग।
- तमिलनाडु में उत्तरी-दक्षिणी अर्काट व रामनाथपुरम में।
सेंधा नमक: यह नमक गहरा आसमानी रंग का होता है। यह नमक हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में अवसादी शैलों से ध्रांग और गूमा की खानों से मिलता है। ध्रांग में नमकीन जल के अनेक झरने है। नमक के इन घोलों के वाष्पीकरण से उत्तम श्रेणी का नमक प्राप्त किया जाता है।
हीरा Diamond
हीरा के भंडार तीन प्रकार के भू-गर्भीय संरचना में पाये जाते हैं- किंबरलाइट पाइप, संपीडित बेड एवं कछारी कंकड़ के रूप में।
वितरण: भारत में हीरा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश के पन्ना में है। भारत में यह कुर्नूल जिले के मुनीयाडुगू-बंगनपल्ली, अनंतपुर जिले के बजराकरूर, आंध्र प्रदेश की कृष्णाघाटी, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर और रायगढ़ जिलों में भी मिलता है। हीरे को रत्न-आभूषण बनाने के लिए काटा और तराशा जाता है। हीरे के कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र मुख्यतः गुजरात में (सूरत, जयपुर, त्रिशूर (केरल) और गोवा। केवल पन्ना पेटी और कृष्णा घाटी में अनुमानित भण्डार हैं। ये लगभग 45 लाख कैरेट के हैं। हीरे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है।
अन्य खनिज Other Minerals
बैरीलियम Beryllium: यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है। बैरीलियम से निऑन, सिग्नल, वायुयानों के कार्बोरेटर, साइक्लोट्रान और विस्फोटक बनाये जाते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय शक्ति उत्पादन में मंदक के रूप में किया जाता है। राजस्थान (उदयपुर, डूंगरपुर एवं अजमेर जिले), तमिलनाडु, बिहार (गया जिले), झारखंड (हजारीबाग व कोड़रमा जिले), उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश (नेल्लौर जिले) तथा जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों से बैरीलियम प्राप्त होता है।
जिरकोनियम Zirconium: इसे जिरकन अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यह सामान्यतः आग्नेय शैल के साथ सम्बद्ध होती है तथा इल्मेनाइट और मोनाजाइट के साथ बालू पुलिन (बीच) पर पाई जाती है। जिरकोनियम कोलम तथा कन्याकुमारी के बीच बालू पुलिन में, तथा रामानाथपुरम, विशाखापट्नम, तंजावुर और तिरुनेलवेली जिलों के तटीय मार्ग पर पाई जाती है।
इल्मेनाइट Ilmenite: यह मुख्यतः रत्नागिरि (महाराष्ट्र) से लेकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं ओडीशा के तटों तक बालू के किनारों में पाए जाते हैं। भारत में इल्मेनाइट का भंडार 461.37 मिलियन टन है। यह खनिज बिहार एवं पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है।
यूरेनियम Uranium: इसके भण्डार झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम जिले, बिहार में गया जिला और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। कुछ यूरेनियम भण्डार राजस्थान में उदयपुर की कॉपर और जस्ता खान में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यूरेनियम के निक्षेप हैं।
थोरियम Thorium: इसमें मोनाजाइट, एलैनाइट और थोरियेनाइट खनिजों को शामिल किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। यह केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा बिहार और राजस्थान इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं।
टंगस्टन Tungsten: टंगस्टन कठोर, भारी और ऊंचे द्रवणांक वाली धातु है जिसका उपयोग इस्पात के मिश्रण, विद्युत यंत्रों, उच्च गति इस्पातों को काटने में, पारा संशोधकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य भंडार देगना नागपुर जिला तथा राजस्थान में रावत पहाड़ियों में, पश्चिम बंगाल में बांकुरा, महाराष्ट्र में सकोली बेसिन, कर्नाटक में कोलार, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, झारखंड में सिंहभूम और गुजरात में अहमदाबाद जिले में पाया जाता है।
संगमरमर की खानें राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हैं। संगमरमर का सजावटी पत्थर बनाने में अधिक योगदान रहता है।