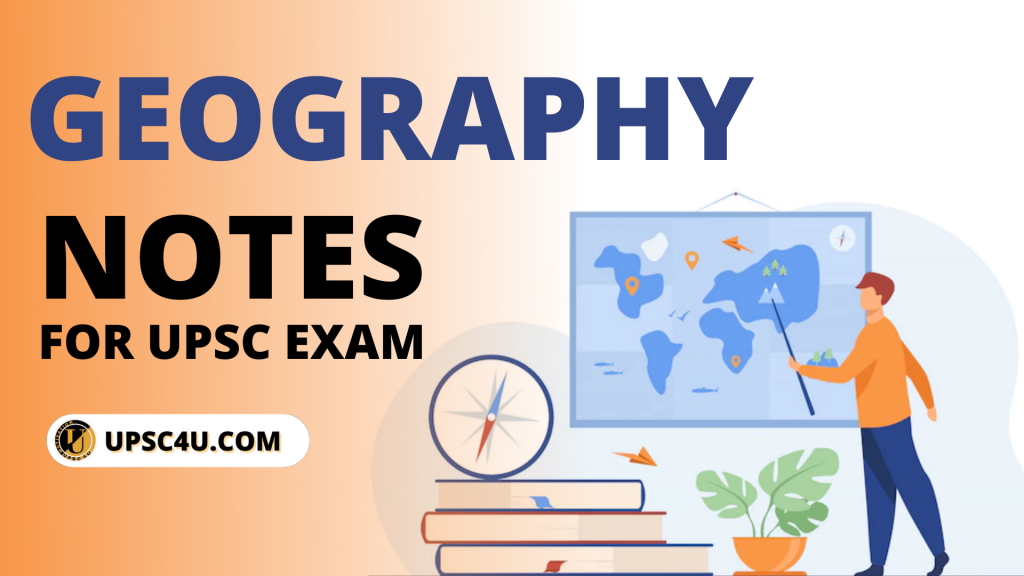पर्यावरणीय संकट
परिवर्तन प्रकृति की मूलभूत प्रक्रिया है। परिवर्तन शनैः-शनैः भी हो सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों का उद्गम; यह तीव्र एवं अचानक भी हो सकते हैं जैसाकि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, सुनामी, चक्रवात और टॉरनेडो में होता है। हम उन्हें प्राकृतिक या पर्यावरणीय संकट के तौर पर मान सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में वे तत्व और परिस्थितियां जिनमें लोगों या संपति को नष्ट करने की क्षमता होती है। महासागरों में जलधाराएं या विपरीत जलवायु दशाएं संकट/आपद होते हैं। थार की गर्म मरुस्थलीय जलवायु और कश्मीर में शीतल मरुस्थलीय जलवायु प्राकृतिक आपद हो सकते हैं।
पर्यावरणीय संकट ऐसे भूभौतिक घटनाक्रम हैं, जो बड़े स्तर पर आर्थिक परिसम्पतियों के विनाश, भौतिक क्षति एवं मानव जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इन घटनाओं का प्रभाव भी समय-समय पर भिन्न होता है और उनके विस्तार की मात्रा एवं संबद्ध पर्यावरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विनाश, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। कुछ सामान्य पर्यावरण संकटों या प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सूखा और चक्रवात शामिल हैं। पी. मे (P.May) द्वारा, 1996 में ओजोन परत के क्षरण तथा समुद्री जलस्तर में वृद्धि को भी पर्यावरण संकट के अंतर्गत शामिल किया गया।
पर्यावरणीय संकट की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- यह प्रत्यक्ष रूप से मानवजनित नहीं होते।
- ये मानवों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।
- ये प्रायः ऊर्जा की प्रचंड निर्मुक्ति से सम्बद्ध होते हैं।
- माध्यम के प्रकार के संबंधों में ये भविष्यवाणियों से परे होते हैं।
मानवीय कारक पर्यावरण संकटों को प्रायः नियति या ईश्वरीय कृत्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। किंतु इस मामले में मानवीय अभिकरण का योगदान भी, विशेषतः प्रभाव के संबंध में, महत्वपूर्ण होता है। जैसे-मानवीय बस्तियों से रहित क्षेत्र में बाढ़ों का आना मात्र एक प्राकृतिक परिघटना है। इसके अलावा वृक्षों की कटाई, प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करने वाला मानव जनित प्रदूषण तथा दलदली भूमियों का अपवाहन जैसे मानवीय कारक भी बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि कटे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के कारण भूस्खलन की घटनाएं होती हैं।
बड़े नगरों और तट के साथ पत्तन-कस्बों का विकास जैसे मुम्बई, चेन्नई, विशाखापट्टनम् ने, सुनामी, हरिकेन और चक्रवातों के प्रति अपनी भेद्यता में वृद्धि कर ली है। विनिर्माण शैली और विशेष क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त भवन सामग्री के प्रयोग ने आवासों के भूकंप और भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि की है।
मानव निर्मित संकट एवं पर्यावरण संकट में भेद करना आज कठिन हो गया है। आज की भौतिक घटनाओं पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, जो आगे चलकर भावी भौतिक घटनाओं की प्रकृति पर भी प्रभाव डालेगा।
भूस्खलन
भूस्खलन से संपत्ति, जीवन तथा संचारतंत्र को भारी क्षति पहुंचती है। यद्यपि, व्यापक वैज्ञानिक समझ एवं जन-जागरूकता के कारण विश्व में भूस्खलन की घटनाओं में कमी आयी है, तथापि, ढालू आधारों, कैनियनों तथा पठारों की अस्थिर सीमाओं में बढ़ते जनसंख्या दबाव के फलस्वरूप भूस्खलन के खतरों में वृद्धि होती जा रही है।

भूस्खलन एक सार्वभौमिक तत्व है, लेकिन प्राकृतिक आपद होने से अधिक, इसे मानव गतिविधियों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है।
1972 में एम.ए. कार्सन और एम.जे. किरबी ने पहाड़ी ढालों को दो भागों में बांटा-
- सीमित-अपक्षय ढाल और
- सीमित परिवहन ढाल।
पहले मामले में, चट्टान का अपक्षय होता है, जबकि बाद वाली स्थिति में, ढाल मोटी मृदा परत से ढके होते हैं या टूटी हुई चट्टान होती हैं, जिन्हें रिगोलिथ के तौर पर जाना जाता है। रिगोलिथ की उपस्थिति के कारण सीमित परिवहन वाले ढाल तीव्र भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
भूस्खलन शब्द गुरुत्वीय एवं अन्य कारकों के मजबूत प्रभाव के फलस्वरूप मृदा या शैल पदार्थ के घंसाव, स्खलन, प्रवाह एवं पातन का सूचक है। कुछ भू-आकृति वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन की जगह वृहत् संचलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृहत् संचलन के परिणामस्वरूप निर्मित स्थतरूपों को वृहत् क्षरण कहते हैं। वृहत् संचलन तब घटित होता है जब ढाल प्रवणता अपनी स्थिरता के कोण की प्रभाव सीमा को पार कर जाती है।
भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक
नदी अपरदन, सड़क कटाव, भ्रंशन विवर्तनिक संचलन तथा कृत्रिम ढाल निर्माण द्वारा पाश्विक या अंतर्निहित समर्थन को समाप्त कर देने के कारण ढाल अस्थिरता का जन्म होता है।
अपक्षय द्वारा शैल विखंडन होने के कारण मृदा कमजोर हो जाती है। भूस्खलन का एक महत्वपूर्ण कारण बढ़ते हुए जल अंतःस्रवण से संबंधित है, जो मृदा को संतृप्त कर देता है। यह ढालों पर जुताई या अपवाह के कुसंगठन के कारण जन्म लेता है। छिद्र जल दबाव में मृदा संतृप्तिकरण द्वारा वृद्धि होती है, जिसके कारण ढाल पर एक प्रत्यक्ष बल पड़ता है।
जंगलों में इमारती लकड़ी की कटाई, ढाल स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ट्रैक्टरों का प्रयोग भी मृदा संरचना को अस्थिर करता है। इन कारकों के अलावा भूकंप, भारी वर्षण, हिम द्रवण तथा ढल के दीर्घकालिक कटाव के फलस्वरूप भी भूस्खलन की घटनाएं जन्म लेती हैं।
उपरिलिखित बलों या शक्तियों के अतिरिक्त, ढाल के दरकने के कारणों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है-
- आकस्मिक कारणों में कंपन, भूकंप के झटके, भारी वर्षण तथा जमना और पिघलना आते हैं,
- दीर्घावधिक कारण जिसमें ढाल का धीमा और लगातार कटाव होना है।
भारत में भूस्खलन
हिमालय में स्थित अस्थायी वलित पर्वत, पश्चिमी घाट में तीव्र या खड़े ढालों के साथ भारी वर्षा क्षेत्र\, उत्तर-पूर्व क्षेत्र और वह क्षेत्र जहां लगातार भूकंप के झटके आते हैं, ऐसे क्षेत्र है जो भूस्खलन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।
जनसंख्या दबाव तथा पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक दोहन ने भूस्खलन के प्रमुख कारणों को जन्म दिया है। वन भूमिका बागानों में रूपांतरण, सड़क एवं भवन निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी तथा पशुओं की चराई इत्यादि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, जो भूस्खलन के अवसरों को बढ़ाती हैं। झूम खेती तथा इमारती लकड़ी हेतु वृक्षों की कटाई ने भी मूल्यवान वानस्पतिक आवरण को नुकसान पहुंचाया है, जो मृदा अपरदन और अंततः भूस्खलन की ओर ले जाता है।
झारखंड, ओडीशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु जहां खनन उद्योग प्रमुख हैं, खनन गतिविधियों के कारण भूस्खलन आमतौर पर होता है।
प्रभाव एवं शमन
भूस्खलन का प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय और कम होता है; हालांकि यह सड़क अवरोध, नहर अवरुद्धता और चट्टानों के गिरने से रेलमार्ग को नष्ट करने के रूप में व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। भूस्खलन नदियों का मार्ग परिवर्तित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आ सकती है।
भूस्खलन से निपटने के लिए क्षेत्र विशेष के अनुसार उपाय अपनाने होंगे। भूमि प्रयोग को तकनीकी-आर्थिक सुसाध्यता पर, बांधों की भौगोलिक अवस्थिति, पुलों का निर्माण और आवासीय परिसरों, सड़क निर्माण के तहत् निर्णय लेने की आवश्यकता है, और आपदा से निपटने के लिए और क्षेत्र के पारितंत्र को बचाने के लिए उपयुक्त उपाय करने होंगे। भूमिगत कुओं और सुरंगों का निर्माण तथा भूमिगत जल को पम्पिंग द्वारा बाहर निकाल कर सतही नगर बनाने जैसी अभियांत्रिकी पद्धतियां भू-स्खलन को रोकने में बेहद कारगर होती हैं।
बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों और जलप्रवाह को कम करने के लिए पुश्तों का निर्माण किया जाना चाहिए। उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, झूम कृषि की जगह स्थायी कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समग्र रूप से, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में, विकासपरक गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है।
ज्वालामुखी विस्फोट
ज्वालामुखी क्रिया का तात्पर्य किसी ज्वालामुखी की गतिविधि तथा उत गतिविधि के परिणाम से होता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी में स्थित एक छिद्र या दरार है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद पिघले चट्टानी पदार्थ, गर्म जल वाष्प, धूल तथा गैसों का पृथ्वी की सतह पर उद्गार होता है।

उद्गारों की आवृति के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं-
- जाग्रत ज्वालामुखी जो निरंतर लावा का उद्गार करते रहते हैं। हालांकि कुछ ज्वालामुखी ही कम या अधिक रूप से लंबे समय तक निरंतर उद्गारशील रहते हैं किंतु जाग्रत ज्वालामुखी की आवर्तक गतिविधियां सामान्यतया अधिक होती हैं,
- सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे नियमित व निरंतर उद्गार नहीं होता। ऐसे ज्वालामुखी के उद्गारों के बीच बहुत लम्बा समयांतराल होता है। इस समयांतराल में ज्वालामुखी गतिविधियों के सभी बाहरी लक्ष्य अदृश्य होते हैं, तथा
- शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं, जिनमें भूगर्भिक इतिहास के अनुसार लम्बे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है। भविष्य में भी इनके उद्गार की संभावनाएं नहीं रहती क्योंकि ये शांत होने से पहले एक ह्रासोन्मुखी चरण से गुजर चुके होते हैं, जिसके दौरान समस्त वाष्प एवं गैसें धुंआरे के रूप में निकल जाती है तथा ज्वालामुखी के मुख (क्रेटर) पर पानी की झील का निर्माण हो जाता है।
कभी-कभी कोई शांत मान लिया गया ज्वालामुखी भी सक्रिय हो जाता है। अंडमान व निकोबार स्थित बैरेन द्वीप (भारत), क्राकाटाओ (इंडोनेशिया) इसके उदाहरण हैं।
हिमालय क्षेत्र या भारतीय प्रायद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। बैरन द्वीप, जो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में 135 किमी. पर स्थित है, को 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उद्गार के समय से सक्रिय ज्वालामुखी समझा जाता था। यह मार्च 1991 में अचानक, फिर से सक्रिय हो गया। इसके प्रस्फुटित होने का दूसरा चरण जनवरी 1995 में प्रारंभ हुआ। इस द्वीप का आधार समुद्र स्तर से 2000 मीटर नीचे है और इसका क्रेटर समुद्र स्तर से लगभग 350 मीटर ऊपर है। 19वीं शताब्दी में इसकी क्रियाशीलता के बाद, इसके क्रेटर की दीवारों के ऊपर सल्फर के इकट्ठा होने से यह मंदक स्थिति में पहुंच गया। भारतीय क्षेत्र में एक अन्य ज्वालामुखीय द्वीप नारकोंदम है, जो वैरन द्वीप के उत्तर-पूर्व के लगभग 150 किमी. पर अवस्थित है; यह शायद विलुप्त हो गया है। इसकी क्रेटर भित्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है।
मानवीय गतिविधियों पर ज्वालामुखीय क्रिया के प्रभाव
विनाशात्मक प्रभाव
ज्वालामुखी उद्गारों को पृथ्वी का सबसे प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किया जाता है। इतिहास प्रमाण है कि सक्रिय ज्वालामुखी के निकट रहने वाले लोगों को अनगिनत जीवनक्षतियों तथा कस्बों एवं शहरों के विनाश चक्र में पिसना पड़ा हैं। लावा का प्रवाह, लैपिली व बमों की वर्षा, गैस मिश्रित उदीप्त ज्वालामुखी राख के दालों, खिसकते टीले, उद्गार से जुड़े भूकंप तथा वर्षा जल से संतृप्त ज्वालामुखी राख का पंक प्रवाह आदि व्यापक नुकसान के कारण बनते हैं। तटीय क्षेत्रों में भूकपीय समुद्रीय तरंगें (सुनामिस) एक अतिरिक्त खतरा होती हैं। 1948 में मैक्सिको के एक ज्वालामुखी ने अपने पहले वर्ष एक दिन में 4 लाख टन लावा विस्तृत किया जिससे 750 वर्ग कि.मी. क्षेत्र जनसंख्या विहीन हो गया तथा भारी नुकसान हुआ।
सकारात्मक प्रभाव: ज्वालामुखी राख तथा धुल कृषि एवं बागवानी हेतु अत्यंत उपयोगी होती है।ज्वालामुखी चट्टानों के वियोजन तथा अपक्षय द्वारा बहुत उपजाऊ मिट्टी निर्मित होती है। हालांकि तीव्र ज्वालामुखी ढाल व्यापक कृषि में बाधक होते हैं, किंतु उन पर वनारोपण करके कीमती लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। ज्वालामुखी क्रिया से पृथ्वी पर विस्तृत पठारों तथा ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है।
ज्वालामुखी व लावा प्रवाह में खनिज सामग्री का अभाव होता है, किंतु बाद की भूगर्भिक घटनाओं के परिणामस्वरूप ज्वालामुखीय चट्टानों में खनिज अयस्कों का जमाव हो जाता है। कभी-कभी कॉपर एवं अन्य दूसरे अयस्क गैस बुलबुलों के विवरों को भर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध किम्बरलाइट चट्टानें एक प्राचीन ज्वालामुखी की नली का अंग हैं तथा हीरों का प्रमुख स्रोत हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों के निकट का भूमिगत जल गर्म मैग्मा के सम्पर्क से ऊष्माशील हो जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित क्षेत्रों के आंतरिक भूभाग में मौजूद ऊष्मा का उपयोग भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।
भूकंप
भूकंप, प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को नहीं मारते; जीवन एवं सम्पति का विनाश मुख्यतः भवनों एवं अन्य निर्माणों के दहने के कारण होता है।
भूकंप का सबसे मुख्य कारण भूपर्पटी के भ्रंशों या जोड़ों का चट्टानों के साथ अचानक खिसकना है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद सघन दाब तथा तापमान के फलस्वरूप चट्टानों के आयतन तथा सघनता में निरंतर परिवर्तन होने के कारण होता है। कुछ कंपन सैकड़ों किमी. नीचे गहराई में जन्म लेते हैं तथा ऐसी स्थिति में पैदा होने वाली भूकंप तरंगें भूसतह तक पहुंचते-पहुंचते क्षीण हो जाती हैं और अधिक नुकसान का कारक नहीं बनती। भूकंप के समय भूमि का वास्तविक विचलन भ्रंश रेखा के दोनों ओर निकटस्थ क्षेत्रों में होता है। भूकपीय झटकों का मुख्य क्षेत्र तया उसके परिणामस्वरूप होने वाला विनाश क्षेत्र रेखाबद्ध होते हैं, क्योंकि कंपन भ्रंश रेखा में ही पैदा होता है। 80 से कई सौ किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा के किनारे 10-15 मी. की दूरी पर होने वाला कोई भी स्खलन एक बड़े भूकंप का कारण बन सकता है। ज्वालामुखीय क्रिया को भी भूकंप का कारण माना जाता है किंतु ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा जनति भूकंप कम शक्तिशाली तथा विस्तार क्षेत्र में सीमित होते हैं। कुछ छोटे-छोटे भूकंप गुफाओं, सुरंगों या भवनों की छतों के ढहने के परिणामस्वरूप भी पैदा हो जाते हैं।

भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान भूकंप अधिकेंद्र (epicentre) कहलाता है, भूकंप तरंगों का अनुभव यहां सबसे पहले किया जाता है। अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के ठीक लम्बवत होती है।
आवृति: विश्व में एक वर्ष के दौरान लगभग 8 से 10 हजार भूकंप (अर्थात् प्रत्येक एक घंटे में एक भूकप) आते हैं। वास्तव में अधिकांश भूकंपों का पता नहीं लगता क्योंकि आज भी भूतल के बहुत बड़े भाग में विस्तृत महासागरों में होने वाली भूकंपीय गतिविधियों को मापने हेतु अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
अवधि: मनुष्यों द्वारा महसूस किये जाने वाले भूकपीय झटकों की अवधि कुछ सैकेंड से लेकर कई मिनटों तक होती है। सामान्यतः कंपन की गहनता से ही उनकी समयावधि निर्धारित होती है। पर्याप्त नुकसान पहुंचाने में सक्षम भूकंप की औसत अवधि संभवतः 1 से दो मिनट तक हो सकती है।
तरंग वेग: भूकंप तरंगों की औसत गति भूपर्पटी के बाहरी भाग में लगभग 5 से 8 किमी. प्रति सेकंड होती है। गहराई में इनकी गति और अधिक तीव्र होती है
भूकंप समाघात रेखा: यह भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है।
भूकंप के प्रभाव Effects of the Earthquake
नगरों का नष्ट होना, भूस्खलन, दरारों का निर्माण, स्थलभाग में उभार तथा धंसाव, जलतरंगों का आविर्भाव, भूमिगत जल प्रवाह में बदलाव, नदी मार्ग में बाधा आना तथा जल स्रोतों का उद्भव आदि भूकंप के सम्मिश्रित प्रभाव हैं।
भारत वैश्विक भूकंप पेटी के ठीक ऊपर स्थित है, जो पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली है तथा अल्पाइन-हिमालय पेटी कहलाती है। मुख्य भूकंप क्षेत्र मुख्य सीमा भ्रंश के साथ फैला हुआ है, जो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में सादिया तक जाता है तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से दक्षिण दिशा में मुड़कर इंडोनेशिया द्वीप समूह तक व्याप्त होता है।
गोंडवानालैंड एवं लरिशियन प्लेट के बीच स्थित हिमालयी पेटी भारतीय महाद्वीप को अस्थिर भूगर्भिक प्रकृति प्रदान करती है। हिमालय भूगर्भ विज्ञान के वाडिया संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का कारण है- पिछले 8 करोड़ वर्षों से भारतीय स्थलखंड का उत्तर की ओर खिसकना। यह उत्तरोन्मुखी प्लेट संचलन दबाव का निर्माण करता है तथा ऊर्जा के रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग से निर्मुक्त होता है। कुछ समय पूर्व में जबलपुर एवं किलारी में आये भूकंपों से यह पता चलता है कि भूकंप की आवृत्ति भूकंपग्रस्त क्षेत्रों से तथाकथित स्थिर भूखंडों की ओर विस्थापित हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिक इन भूकंपों का कारण कृत्रिम जलाशयों को मानते हैं, जबकि कुछ इसे देश की विशिष्ट भूगर्भिक संरचना का परिणाम मानते हैं।
भूगर्भिक रूप से भारतीय स्थलखंड की रचना शैल इकाइयों के अनेक अनुक्रमों से हुई है। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक प्राचीन आकियन चट्टानें पायी जाती हैं क्योंकि आर्कियन स्तर 2.5 अरब वर्ष पुराना है, अतः यह आधारशैल के रूप में कार्य करता है, जिस पर अन्य शैल परतें बिछी हुई हैं। आधार शैल स्तर की अदृश्यमानता के कारण उसके रासायनिक व भौतिक गुणों का विश्लेषण संभव नहीं है। निरंतर अनाच्छादन के कारण हिमालय क्षेत्र भी संतुलन को कायम रखने के लिए ऊपर उठता जा रहा है। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में निरंतर जमा हो रहे अवसाद समुद्री नितल पर एक वृहत् भार डाल रहे हैं। इस परिघटना को मुख्य स्थल खंड पर दबाव डालने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। महासागरीय कटक तथा हिंद महासागर की अन्य जटिल संरचनात्मक विशेषताएं भी निकटवर्ती स्थलखंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।
भारत में भूकंपीय क्षेत्र Seismic Zone in India
भूकंपन संबंधी आंकड़ों तथा विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिक मापदंडों के आधार पर भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पांचों क्षेत्रों में पांचवां क्षेत्र सर्वाधिक सक्रिय तथा पहला क्षेत्र न्यूनतम भूकंपीय सक्रियता दर्शाता है।
पंचम क्षेत्र में संपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों के दौरान 7.0 से अधिक तीव्रता वाले पांच प्रमुख भूकंप घटित हुए हैं। जुलाई 1918, जुलाई 1930 एवं अक्टूबर 1949 में असम में, अगस्त 1950 में अरुणाचल प्रदेश-चीन सीमा क्षेत्र में, अगस्त 1988 में मणिपुर-म्यांमार सीमा क्षेत्र में तथा 2011 में सिक्किम-नेपाल सीमा क्षेत्र में प्रमुख भूकंपीय घटनाएं हुई।
इस क्षेत्र की उच्चस्तरीय भूकंप आवृत्ति का कारण इस पेटी का उस रेखा के साथ-साथ चलना है, जहां भारतीय प्लेट (पुरातन गोंडवानालैंड) यूरेशियन प्लेट से मिलती है।
अभिसारी कोर होने के कारण भारतीय प्लेट 5 सेमी. प्रतिवर्ष की गति से यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है। यह संचलन एक तीव्र दबाव को जन्म देता है, जो चट्टानों में संचित होता रहता है तथा समय-समय पर भूकंपों के रूप में बाहर आता है। इन भूकपीय झटकों से अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होने के कारण भूकंप व्यापक विनाश एवं धन-जन की हानि का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार अपेक्षाकृत युवा हिमालय क्षेत्र, जो अभी तक स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाया है, पिछली कुछ शताब्दियों में कई बड़े भूकंपों का साक्षी रहा है।
विभिन्न भू-गर्भिक तथा भू-भौतिक मापदण्डों व भूकंप विज्ञान से संबद्ध आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर भारत को पांच भूकंप संभावित क्षेत्रों में विभाजित किया गया। किंतु वर्ष 2003 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्षेत्र I व II को मिलाकर एक कर दिया तथा शेष भागों को यथावत् रखा गया। इस तरह अब ये क्षेत्र हैं- II, III, IV तथा V। ।
- क्षेत्र-II (I और II): इस क्षेत्र में भूकंप की सामान्य तरंगें उठती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र को कम भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र माना गया है।
- क्षेत्र-III: इस क्षेत्र के अंतर्गत केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश एब्वं कर्नाटक को शामिल कर चिन्हित किया गया है। इन राज्यों में मध्यस्तरीय भूकंप की तीव्रता आंकी गयी है।
- क्षेत्र-IV: इसके अंतर्गत दिल्ली, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा, महाराष्ट्र का तटीय भाग तथा गुजरात का कुछ हिस्सा आता है। यह द्वितीय स्तर की भूकम्पीय तीव्रता वाला क्षेत्र है।
- क्षेत्र-V: इस क्षेत्र में भूकम्पों की सर्वाधिक आशंका रहती है। पूर्वोत्तर भारत के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, कच्छ का रन, उत्तरी बिहार, अंडमान तया निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख भूकपीय घटनाएं हुई हैं- उत्तरकाशी (अक्टूबर 1991), लातूर (सितंबर 1993), जबलपुर (मई 1997) तथा चमोली (मार्च 1999)। इन सभी की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 से अधिक आंकी गयी। तृतीय क्षेत्र प्रदेश तथा कर्नाटक शामिल हैं। शेष निम्नतम सक्रियता वाले राज्य प्रथम एवं द्वितीय क्षेत्रों में शामिल हैं।
प्रभाव
भूकंप के मुख्य प्रभावों को तालिका में देखा जा सकता है।
[table id=66 /]
नगरों का नष्ट होना, भूस्खलन, दरारों का निर्माण, स्थलभाग में उभार तथा धंसाव, जलतरंगों का आविर्भाव, भूमिगत जल प्रवाह में बदलाव, नदी मार्ग में बाधा आना तथा जल स्रोतों का उद्भव आदि भूकंप के सम्मिश्रित प्रभाव हैं।
भूकम्प के धक्के के प्रभाव से स्थल का अथवा समुद्री पेटी का कुछ भाग नीचे चला जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। सागरीय भूकम्प से उत्पन्न सुनामिस लहरों द्वारा महाद्वीपीय मग्नतट (shelves) तथा महाद्वीपीय ढाल के पदार्थ काफी कमजोर हो जाते हैं तथा नीचे की तरफ अर्थात् सागरतली की तरफ सरकने लगते हैं।
भूकम्प के आवेग से टूटे हुये विशालखण्ड के नदियों के मार्ग में आ जाने से नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है\, जिस कारण या तो उनमें बाढ़ आ जाती है अथवा उनका मार्ग परिवर्तित हो जाता है।
सागर तटवर्ती स्थलीय भागों में भूकम्प के आवेग से सागर में उत्ताल ज्वार तरंगें उठने लगती हैं, जिससे समीपवर्ती भागों में पर्याप्त क्षति होती है।
भूकम्प के प्रभाव से भूमिगत जल की व्यवस्था में बाधा उपस्थित हो जाती है। चूने की चट्टान वाले भाग में कन्दराओं की छतें टूट कर नीचे गिरने लगती हैं।
लोयस मिट्टी के क्षेत्रों में भूमिस्खलन (landslide) होने लगता है, जिसकारण अपार धन-जन की हानि होती है।
निवारण
भूकंप को रोकना संभव नहीं है, सबसे अच्छी बात जिसे किया जा सकता है कि भूकंप के प्रभावों को कम करने के उपायों की तैयारी के साथ विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहा जाए। निरंतर निगरानी के लिए भूकंप अधिकेंद्रों की स्थापना और संवेदनशीलता क्षेत्रों तक सूचना को तेजी से पहुंचाने की आवश्यकता है। भौगोलिक स्थिति तंत्र (जीपीएस) के इस्तेमाल द्वारा टेक्टोनिक प्लेट के संचलन की निगरानी की जा सकती है।
सभी भूकंपीय संभावना वाले क्षेत्रों में आपदा के वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग, निर्माण गतिविधियों तथा आधार संरचना नियोजन से जुड़े नियामक उपायों को लागू किया जाना चाहिए। अग्रिम या पूर्व योजना द्वारा भेद्यनीय सामुदायिक संपत्ति, समर्थन प्रणालियों तथा लागत-प्रभावी नैदानिक उपायों की पहचान में सहायता मिलती है। जन जागरूकता तथा शैक्षिक अभियानों द्वारा भूकंप के खतरों के प्रति जनता को सचेत बनाया जाना भी जरूरी है। अग्रिम चेतावनी द्वारा सघन क्षेत्रों को खाली कराया जा सकता है तथा यातायात, संचार एवं शक्ति प्रणालियों को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा क्षति के भौगोलिक विस्तार का त्वरित मूल्यांकन होना चाहिए ताकि सीधी बचाव एवं राहत कार्यवाही की जा सके।
भूम्कंप विज्ञान में सेंसर डिजाइन, टेलीमेट्री, ऑनलाइन कंप्यूटिंग, तथा बेहतर संचार जैसे नवीन विकासों ने जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों की प्रभाविता को बढ़ा दिया है। भारत के भूकंप आपदा मानचित्रों को भी तैयार कर लिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भवन निर्माण हेतु कई मापदंडों का विकास किया गया है।
अब तक हिमालय विवर्तनिकी के संबंध में पर्याप्त जानकारी हासिल की जा चुकी है तथा सीएसआईआर द्वारा इन प्रक्रियाओं की दर एवं शैली को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। मृदा एवं स्थलाकृतिक मानचित्रों तथा उपग्रह सर्वेक्षणों द्वारा भी जोखिम के मूल्यांकन में सहायता दी जा सकती है। जोखिम मानचित्र तैयार करने के लिए पर्याप्त विषय सामग्री एवं तकनीकी उपकरणों का उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि देश के विशिष्ट समाजार्थिक वातावरण के अनुकूल डिजायन तैयार किया जा सके। एक राष्ट्रीय आपदा शमन कानून के माध्यम से सभी स्तरों पर जोखिम को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
संवेदनशील क्षेत्रों में आवासीय प्रकारों और भवन-निर्माण को भूकंपरोधी बनाकर तथा हल्की भवन-निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके सुधारा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में, ऊची इमारतें, वृहद् औद्योगिक परिसर और शहरी केन्द्रों के निर्माण एवं विस्तार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतिम रूप से, प्रत्यक्ष बचाव एवं राहत अभियानों के लिए क्षति के भौगोलिक विस्तार का तीव्र आकलन किया जाना चाहिए।
सुनामी
सुनामी वे अनुक्रमिक समुद्री प्रगामी तरंगें हैं, जो धारा की दिशा में प्रतितुलन के रूप में समुद्र के तल पर भूगर्भीय विक्षोभ पैदा करती हैं। ये तरंगें वेगपूर्वक ऊपर तक उठती हैं और देखते ही देखते समुद्र के चारों ओर प्रबल आवेग से कई हजार किलोमीटर तक फैल जाती हैं। कुछ सुनामी ज्वार की तरह प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में वह ज्वार नहीं है। ज्वारभाटा जहां चंद्रमा, सूर्य तथा ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटित होता है, वहीं सुनामी समुद्र में आने वाले भूकम्प के कारण उठने वाली समुद्री तरंगें हैं। इस प्रकार, सुनामी तरंगें भूकम्प सम्बन्धी तंत्र से उत्पन्न होती हैं। सुनामी तरंगें या लहरें अधिकांशतः भूकम्प का परिणाम होती हैं, लेकिन समय-समय पर ये भूस्खलन या ज्वालामुखी उद्गारों या दुर्लभ रूप से आकाशीय उल्कापिण्ड के समुद्री प्रभाव के कारण भी घटित हो जाती हैं। सुनामी को आधारभूत स्तर पर संकेंद्रित अनुक्रमित उर्मिका (छोटी लहरों), जो एक तालाब पर पत्थर फेंकने पर बनती हों, के रूप में जाना जा सकता है। सुनामी तरंगें ऐसे ही बनती हैं, लेकिन विक्षोभ के कारण उनकी प्रबलता अत्यधिक हो जाती है।

सुनामी दीर्घ तरंगदैर्ध्य युक्त अनुक्रमिक समुद्री तरंगें हैं, जो समुद्र में विक्षोभीय आवेग के कारण समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं। सुनामी छिछले-जल में उठने वाली तरंगें हैं, जो वायविक-जल तरंगों से भिन्न होती हैं तथा जो 4 से 20 सेकण्ड के अंतर में अनुक्रमिक तरंगों के रूप में 100 से 200 मीटर तक जाती हैं। सुनामी उथले जत की तरंगें हैं, जिसके कारण इनका तरंगदैर्ध्य हुत अधिक होता है। यह एक समय में 10 मिनट से 2 घंटे तक रहती हैं तथा इनका तरंगदैर्घ्य 500 किमी. तक बढ़ जाता है। तरंगों की ऊर्जा का क्षरण तरंगदैर्ध्य के व्युक्रमानुपाती होता है, इसलिए सुनामी तरंगों की ऊर्जा का क्षरण बहुत कम होता है। इससे तरंगें तीव्र गति से गहरे पानी में चलती हैं और बहुत लम्बी दूरी तय करती हैं। इसमें ऊर्जा क्षरण बहुत कम होता है। सुनामी 365 किमी. प्रति घंटे की चाल से 1000 मीटर गहरे पानी में चल सकती हैं तथा 873 किमी. प्रति घंटे की चाल से ये 6000 मीटर गहरे पानी में दौड़ सकती हैं। छिछले जल में इनकी गति बहुत कम होती है, जबकि गहरे जल में अत्यधिक होती है। औसत समुद्री गहराई 5000 मी. मानी जाती है तथा सुनामी का औसत वेग 750 किमी. प्रति घंटा माना जाता है।
दीर्घ गुरुत्व वाली सुनामी तरंगें दो अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। समुद्र तल के ढाल द्वारा क्षैतिज दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण समुद्र तल न्यूनतम स्तर तक आ जाता है तथा उस समय वह परिवर्तित गति से तरंगों की दिशा में तेजी से बढ़ता है। इस प्रक्रिया के साथ-साथ होने से समुद्री तरंगों को प्रसरण शुरू हो जाता है। सुनामी गहरे पानी में किसी भी विक्षोभ के कारण पानी के साम्य अवस्था से हट जाने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। समुद्री भूकम्प के कारण, समुद्री तल सिकुड़ जाता है, इस कारण दो प्लेटें एक-दूसरे के ऊपर अनुप्रस्थीय रूप से अवलम्बित हो जाती हैं, जिसे सबडक्शन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें समुद्री भारी प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे रह जाती है। प्लेटें अचानक ऊपर नीचे होने लगती हैं, जो महाद्वीपीय प्लेट के किनारों से चिपक जाती हैं, उसमें तनाव के कारण बंद क्षेत्र से धाराओं को रास्ता मिल जाता है। महासागर तल का कुछ भाग तेजी से उठता है तथा समुद्र का अन्य भाग नीचे की ओर तेजी से सिकुड़ता जाता है। भूकम्प के बाद अति शीघ्र समुद्र की सतह पुनः संचयन वाली मूल रूप रेखा में आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उच्च गुरुत्व बल के कारण यह पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण सुनामी का कहर टूटता है। सुनामी तरंगें मुख्य सबडक्शन क्षेत्रों (Subduction zones), जैसे- चिली, निकारागुआ, मैक्सिको तया इण्डोनेशिया में अपना कहर बरपा चुकी है। प्रशांत महासागर में 17 बार सुनामी (1992-1996) आ चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 1,700 जानें गई।
अंतःसागरीय भूस्खलन के दौरान, अवसादों के समुद्र तट के साथ जमा होने के कारण समुद्री तल में परिवर्तन होता है। पुनः सागरीय ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आवेग बल उत्पन्न होता है, जो जल स्तर को विस्थापित कर देता है, जिससे सुनामी का जन्म होता है। जल के ऊपरी स्तर पर होने वाले भूस्खलन के कारण जल विस्थापित होता है, उदाहरणार्थ आकाशीय उल्कापात, जो सुनामी का कारण बनते हैं।
सुनामी तरंगें गहरे जल में उत्पन्न होती हैं, बाद में रूपांतरित होकर यह उथले जल तक फैल जाती हैं क्योंकि गहराई की तरफ जल घटता जाता है, सुनामी की गति भी कम हो जाती है, लेकिन उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। गति के घटने के साथ ही सुनामी तरंगें बहुत ऊचाई तक उठने लगती हैं। सुनामी, जो अति-सूक्ष्म रूप में गहरे जल में होती है, वह कई बार बहुत ऊंचाई तक उठ सकती हैं। इसे शोलिंग प्रभाव (shoaling-धीरे-धीरे उथला या जल का झुण्ड या गोला बनना) कहते हैं।
सुनामी का कहर विभिन्न रूपों में व्याप्त हो सकता है, यह समुद्र तलीय तरंगों के ज्यामितीय संबलन पर निर्भर करता है। कभी-कभी महासागर ऐसे दिखाई देता है जैसे झोंके से पानी को नीचे खींच रहा है, अगले ही पल वह पानी सुनामी श्रृंगित तरंगों के रूप में निवर्तित होती है। तटवर्ती क्षेत्रों पर समुद्र जल स्तर कई मीटर उठ जाता है, भूकम्प अधिकेंद्र से 30 मीटर ऊपर तया ऊपर उठने के बाद लगभग 15 मीटर ऊपर तक सुनामी लहरें उठती हैं। ये तरंगें तटीय क्षेत्रों पर हिंसात्मक हो जाती हैं, जबकि अन्य जगहों पर इनका प्रभाव बहुत कम होता है। 305 मीटर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है, सुनामी के कारण जान-माल की अत्यधिक क्षति होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी तरंगें लगभग तीस मीटर तक उठ सकती हैं।
सुनामी तरंगों का आकार महासागर तट के विरूपण प्रमात्रा के द्वारा सुनिश्चित होता है। उर्ध्वाधर स्थानांतरण से तरंगों की लम्बाई बढ़ जाती है। समुद्री भूकम्प के कारण ही सुनामी तरंगें अधिकांशतः समुद्री नितल पर घटित होती है। भूकम्प की प्रबलता, गहराई, अवसादों के अचानक जमाव आदि के आधार पर सुनामी का आकार निश्चित किया जा सकता है।
एशिया में 26 दिसंबर, 2005 को भयानक सुनामियों में से एक आई। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और सोमालिया इस प्राकृतिक आपदा एवं विध्वंस से प्रभावित हुए जिसमें 55,000 से अधिक लोगों की जानें गई।
विगत चार दशकों में यह बेहद शक्तिशाली भूकंप था, जिसका रिक्टर पैमाने पर मैग्निट्यूड 8.9 था।
हिंद महासागर सुनामी संभावित क्षेत्र नहीं है। 26 दिसंबर, 2004 की सुनामी को शामिल करते हुए, इसमें बेहद कम सुनामी आई हैं।
प्रभाव
सुनामी तथा भूकम्प आदि घटनाएं भौगोलिक परिवर्तन के कारण होती हैं। 26 दिसंबर को आए भूकम्प तथा सुनामी के कारण पृथ्वी का उत्तरी धुव 145 डिग्री पूर्वी अक्षांश की ओर खिसक गया तया दिन की अवधि में 2.68 माइक्रो सेकण्ड की कमी आ गई। इसका प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन एवं कोरियॉलिस बल पर भी पड़ा, जो जलवायु प्रतिरूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूकम्प तथा सुनामी के प्रभाव से अण्डमान तथा निकोबार द्वीप लगभग 1.25 मीटर तक स्थानांतरित हो गए थे।
चेतावनी प्रणालियां
सुनामी की आगामी चेतावनी उसी समुद्र के अन्दर भूकम्प की केवल जांच करके ही प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें कई छोटी-छोटी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। अंतरराष्ट्रीय चेतावनी पद्धति की शुरुआत 1965 में शुरू की गई थी। इसका संचालन राष्ट्रीय महासागरीय और वातावरणीय प्रशासन (National ocenic and Atmospheric Administration—NOAA) द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रशासन सत्ता महासागर के किनारे वाले देश, उत्तर अमेरिका, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड हैं। नोवा (NOAA) के अंतर्गत फ्रांस तथा रूस भी शामिल हैं, जिनका प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर आधिपत्य है।
हवाई स्थित प्रशांत स्नामी चेतावनी केंद्र (Pacific Tsunami warning centre– PTWC) कम्प्यूटर डाटा पद्धति से अमेरिका स्थित में स्टेशन से संचालित होता है तथा अन्यत्र भी भूकम्प के समय सूचना पहुंचाता है। इसकी अवस्थिति समुद्र के अंदर है तथा इसकी तीव्रता पूर्व-निश्चित अवसीमा में सूचना पहुंचा देती है।
नोवा द्वारा गहन महासागरीय सुनामी मूल्यांकन एवं सूचना (Deep ocean Assessment and Reportry of Tsunami–DART) gएज का विकास किया गया है। प्रत्येक गेज पर संवेदनशील रिकॉर्डर लगे हुए हुए हैं, जो समुद्र के जल स्तर के परिवर्तन को (यदि 1 सेमी. भी उठता है) माप सकते हैं। डाटा को ध्वनि रूप में तरणशील तल पर प्रेषित किया जाता है, जो सेटेलाइट के माध्यम से चेतावनी केंद्र तक पहुंचाया जाता है।
समुद्री संसूचना प्रणाली विकसित करने में भारत अग्रणी हैं। इसलिए पूर्णतः परिष्कृत सूचना प्रणाली तंत्र हिन्द महासागर के बीच में सूनामी की पूर्व सूचना के लिए विकसित करने का निर्णय लिया गया। गहन महासागर मूल्यांकन एवं सुचना व्यवस्था (The Deep Ocean Assessment and Reporting system-DOARS) को 6 किलोमीटर गहरे महासागर में स्थित किया जायेगा। इसके साथ दबावयुक्त संवेदक सूचक लगा होगा, जो जल के स्थानांतरण की जांच करेगा। इस सेंसर को सेटेलाइट से जोड़ा जायेगा, जो सीधे प्रसारित सूचना पृथ्वी स्टेशन तक पहुंचायेगा। 6-12 अन्य सेंसर भी प्रणाली के साथ बाद में जोड़े जायेंगे, जो जल स्तर में हो रहे परिवर्तन को रिकॉर्ड कर सकेंगे।
6 से अधिक प्रबलता वाले भूकम्पों की पहचान की क्षमता वाला एक राष्ट्रीय राज्य-कला सुनामी पूर्व चतावनी केंद्र (State-of-the art National Tsunami Early Warning centre) 2007 में हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र में स्थापित किया गया। भू-विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय संसूचना केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services—INCOIS) में 125 करोड़ की लागत से स्थापित यह प्रणाली 30 मिनट में भूकम्पीय तरंगों को आकलित कर सूचना पहुंचा सकती है। इस प्रणाली में, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर (BPRS) 30 ज्वारीय गेज, सुनामी उत्पन्न करने वाली भूकम्पीय तरंगों की पहचानने की जांच करने की क्षमता वाला सुनामी मॉनिटर समाविष्ट हैं।
उष्णकटिबन्धीय चक्रवात Tropical Cyclone
उष्णकटिबन्धीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनों भूमध्यरेखीय पछुआ पवनों की आधारभूत धाराओं के साथ गति करते हैं। ये तूफान जैसे ही भूमध्यरेखा से गति करते हैं, वे क्रमिक रूप से गति प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव कुछ प्राथमिकता प्राप्त मागों के साथ गति करते हैं। सम्भवतः, उष्ण सागरीय धाराएं चक्रवातों के मार्गों को विशाल मात्रा में प्रभावित करती हैं। उष्णकटिबंधीय सागर के पश्चिमी भाग तक पहुंचने के बाद, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुव की ओर घूम जाते हैं।
इनकी उत्पत्ति तापीय होती है तथा ये सुनिश्चित मौसमों के दौरान उष्णकटिबंधीय सागरों के ऊपर विकसित होते हैं। इन अवस्थितियों पर स्थानीय संवहनीय धाराएं करिऑलिस बल के कारण एक चक्रीय गति हासिल कर लेती हैं। विकसित

होने के बाद ये चक्रवात तब तक आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक व्यापारिक पवन पेटी में एक कमजोर बिंदु या स्थान नहीं ढूंढ़ लेते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास हेतु आदर्श स्थितियां हैं- (i) उच्च तापमान, (ii) शांत वायु, एवं, (iii) अतिसंतृप्त वायुमंडलीय स्थितियां।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
ये सममित अंडाकार आकृति के होते हैं, जिनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। इनकी दाब प्रवणता अत्यंत खड़ी या सीधी होती है। इनका आकार केंद्र के निकट 50 किमी. होता है, जो 300 से लेकर 1500 किमी. तक विकसित हो सकता है।
इनमें पवन वेग केंद्र की तुलना में ध्रुवोन्मुखी सीमांतों पर अधिक होता है। महासागरों के ऊपर भी इनका पवन वेग महाद्वीपीय भागों से अधिक होता है। पवन वेग की सीमा शून्य से लेकर 1200 किमी. प्रति घंटा तक हो सकती है।
ये चक्रवात एक पश्चिमोन्मुखी संचलन के साथ आरंभ होते हैं किंतु 20° अंक्षाश के निकट जाकर उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं। 25° अक्षांश के निकट वे उत्तर-पूर्व में तथा 30° अक्षांश के आस-पास जाकर पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। वे तब ऊर्जा एव धंसन की प्रवृत्ति का क्षय कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक परवलयिक पथ का अनुसरण करते हैं, अतः उनका अक्ष समदाब रेखाओं के समांतर बना रहता है।
केंद्र की पहचान साफ आकाश के एक टुकड़े से की जाती है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। यहां अवरोही शुष्क वायु के कारण शांत दशाएं मौजूद रहती हैं। केंद्र के बाहर, पक्षाभ मेघ तथा उससे भी बाहर की ओर गहरे वर्षा मेघ होते हैं, जो अनियमित मूसलागर वर्षा एवं तड़ित झंझाओं को जन्म देते हैं। इन चक्रवातों के दायीं ओर का पिछला कोना भारी वर्षा एवं बौछार करता है, जबकि दायीं ओर के पिछले भाग में साफ मौसम रहता है। विशेषतः चक्रवात के वाताग्र पर ये चक्रवात विनाशकारी मौसम दशाओं से सम्बद्ध होते हैं। साथ ही, इनकी भविष्यवाणी करना भी अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि महासागरों एवं तटीय क्षेत्रों के ऊपर तापीय प्रभाव बहुत तेजी के साथ बदलता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आगमन की पहचान पर चक्रवात की आंख के पक्षाभ मेघों तथा आकाश को आवृत्त किये हुए गहन वर्षा मेघों एवं भारी वर्षा की शुरूआत से की जाती है। यह केंद्र के आस-पास समान रूप से वितरित होती है तथा सहिम वृष्टि एवं साफ मौसम के साथ पुच्छ के आने तक जारी रहती है। किंतु, पुच्छ के आगमन से ठीक पहले शांत एवं प्रघाती मौसम के साथ मेघों का गर्जन तथा बिजली का चमकाव होता है। पवन ऊपर की ओर गतिशील एक सर्पिल का निर्माण करती है, जिससे पवन विस्थापन की पहचान कर पाना संभव नहीं होता। बाद के प्रभावों को तापमान की गिरावट एवं दाब वृद्धि के रूप में अनुभव किया जा सकता है।
हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात
चक्रवातों की आवृति, सघनता और तटीय प्रभाव क्षेत्रवार बदलता रहता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के साथ भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, इन दो अवस्थितियों पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मजेदार बात है कि, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृति बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में सर्वाधिक कम है। इनकी सघनता भी संयत है। लेकिन ये खतरनाक हो जाते हैं जब ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी की सीमा को लांघ देते हैं (ओडीशा के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश) इसका मुख्य कारण ज्वारीय तरंगों का आना है जो इस क्षेत्र के तटीय प्रदेश में आती रहती हैं।
बंगाल की खाड़ी के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात दो भिन्न मौसमों में आते हैं। यह मौसम अप्रैल-मई का मानसून-पूर्व माह है और अक्टूबर-नवम्बर का मानसून पश्चात् माह है। औसत तौर पर, वास्तव में, लगभग आधा दर्जन उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं, जिनमें से दो या तीन शक्तिशाली हो सकते हैं। इनमें से मई, जून, अक्टूबर और नवम्बर बेहद झंझावत वाले महीने होते हैं। मई-जून के मानसून-पूर्व मौसम की तुलना में, शक्तिशाली तूफान दुर्लभ होते हैं, अक्टूबर और नवम्बर के महीने बेहद शक्तिशाली चक्रवातों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में।
अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में बेहद अधिक और जल्दी-जल्दी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इसके लिए तीन कारण हो सकते हैं- (i) बंगाल की खाड़ी में जल का तुलनात्मक रूप से उथला होना; (ii) बंगाल की खाड़ी तटरेखा बेहद जटिल है; और (iii) अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक संख्या में नदी अपवाह का होना।
प्रभाव
बलशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों में जीवन, संपदा और कृषि फसल की बेहद क्षति का कारण हैं।
मुख्य खतरे-
(a) प्रचंड पवन, (b) भीषण वर्षा और बाढ़, और (c) विशाल तूफानी ज्वार-भाटा।
आंधी और कठोर पवन और साथ ही भीषण वर्षा संपति, कृषि, मानव जीवनै की क्षति का पर्याप्त विध्वंसक कारण है। उच्च ज्वार और तूफानी आंधी के समन्वय के कारण बाढ़ (जल प्रलय) बेहद विनाशकारी कारक हो सकती है।
बाढ़ Flood
बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है- विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। सामान्यतः यह समझा जाता है कि बाढ़ की स्थिति उस समय होती है जब जल नदी के किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर उस नदी के समीपस्थ भागों को, जलमग्न कर देता है। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक पर्यावरण का एक गुण है तथा अपवाह बेसिन के जलीय चक्र का एक संघटक है। उल्लेखनीय है कि, बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है तथा अति जल वर्षा का परिणाम है। यह मात्र उस समय प्रकोप बन जाती है जब इसके द्वारा अपार धन-जन की क्षति होती है।
भारतीय जलवायु की विशिष्ट प्रकृति, जो मानसून द्वारा प्रभावित होती है, के कारण देश में अलग-अलग क्षेत्र एक ही समय में सूखा एवं बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं।
बाढ़ के कारण
भारत में बाढ़ के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण निम्न हैं-
भारी संकेन्द्रित वर्षा
भारत अपने आकार के हिसाब से औसत रूप में उच्च वर्षा प्राप्त करता है। कभी-कभी मात्र एक दिन के अंदर किसी स्थान पर 15 सेमी. तक वर्षा हो जाती है। रोचक तथ्य यह है कि मानसूनी वर्षा उस समय आरंभ होती है जब ग्रीष्म ऋतु अपने उभार पर होती है तथा हिमालय की नदियां भी पहाड़ों की बर्फ पिघलने के कारण जल की प्रचुरता से ग्रस्त होती हैं। ऐसी स्थिति में इन नदियों की वर्षा जल के ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। परिणामतः उत्तर के मैदान, जहां नदी का वेग पहले से ही कम होता है, बाढ़ों का शिकार बन जाता है। भारी वर्षा नदी भार की मात्रा को अचानक बढ़ा देती है, जिसके कारण नदी का प्रवाह मार्ग परिवर्तित हो जाता है और नदी का जल संलग्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जो इस जल को अपवाहित करने में असमर्थ होते हैं। उत्तरी भारत की दामोदर, कोसी व ब्रह्मपुत्र नदियां अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र का मध्य एवं निचला प्रवाह मार्ग विशेष रूप से बाढ़ प्रवण रहता है, क्योंकि इसकी अत्यंत क्रमिक प्रवणता मानसून के दौरान बढ़े नदी भार को ग्रहण करने में असमर्थ रहती है।
प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ अलग कारणों से बाढ़ें आती हैं, ये कारण उन स्थलरूपों की प्रकृति से जुड़े हैं, जिन पर ये नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां परिपक्व हैं तथा अत्यंत कठोर संस्तरों पर प्रवाहित होती हैं। अपने संस्तरों की गहराई तक अपरदित करने में असमर्थ रहने के कारण इन नदियों के बेसिन या घाटियां छिछली होती हैं। यह स्थिति भारी संकेन्द्रित वर्षा के दौरान इन नदियों में बाढ़ लाने के लिए उत्तरदायी होती है।
चक्रवात एवं शक्तिशाली पवनें
भारत के पूर्वी तट के क्षेत्र अक्टूबर-नवंबर के दौरान चक्रवातों के विशेष शिकार बनते हैं। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब वाताग्रों के रूप में विकसित होते हैं तथा पूर्वी तट पर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये चक्रवात शक्तिशाली हवाओं तथा भारी वर्षा के साथ आक्रमण करते हैं, जो अल्प समय में ही व्यापक विनाश का कारण बन जाती हैं।
कु-अपवाह तंत्र
पंजाब एवं हरियाणा के सघन कृषि क्षेत्र कु-अपवाह के कारण आसानी से बाढ़ प्रवण हो जाते हैं।
मानवीय कारक
बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तीन कारक बाढ़ की संभावना को मजबूत बनाते हैं- (i) नदी अपवाह क्षेत्र एवं ऊपरी भूभागों में वनों की अंधाधुंध कटाई, जो मृदा अपरदन को जन्म देती है, जिससे आगे चलकर नदियों में गाद जमा हो जाती है। गाद जमा होने से नदियों की अधिक जलग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। हिमालयी नदियों में आने वाली बाढ़ों के सम्बंध में यह कारक सबसे मुख्य माना जाता है। ब्रह्मपुत्र अपनी सहायक दिहांग एवं लोहित द्वारा जमा की जाने वाली गादों से प्रभावित होती है। (ii) अत्यधिक चराई, विशेषतः गिरिपाद क्षेत्रों, मिट्टी को आवरण रहित बना देती है। इसके परिणामस्वरूप भारी वर्षा के समय मिट्टी आसानी से सतह से अलग हो जाती है और नदियों के तल पर निक्षेपित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब व उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली अतिचराई से हिमालयी नदियों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। (iii) झूम कृषि जैसी अवैज्ञानिक खेती के परिणामस्वरूप भी वनस्पति आवरण का क्षय होता है, जिसका परिणाम पुनः मृदा अपक्षय के रूप में सामने आता है। उत्तर-पूर्वी भारत में इस प्रकार के मृदाक्षय के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ का मुख्य स्रोत बन गयी है।
बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का वितरण
ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बिहार तथा निचला प. बंगाल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसके अलावा बाढ़ से ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों की कुछ पेटियां इस प्रकार हैं-
- नदियों के निचले प्रवाह मार्ग में गाद जमा होने से ये अपने प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार व प.बंगाल में बाढ़े आती हैं।
- झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, रावी आदि सिंधु की सहायक नदियां जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में आने वाली बाढ़ों का कारण बनती हैं।
- मध्य भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में नर्मदा, ताप्ती, चंबल, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं पेन्नार नदियों द्वारा बाढ़ लायी जाती है।
- पूर्वी तट के कुछ सुनिश्चित क्षेत्र चक्रवाती तूफानों के कारण बाढ़ प्रवण हो जाते हैं। भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्र 75 लाख से 1 करोड़ हेक्टेयर के बीच आंका गया है।
बाढ़ के परिणाम
बाढ़ का सबसे विनाशक पक्ष व्यापक मानवीय क्षति होना है। प्रतिवर्ष औसतन 100 व्यक्ति बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं। आर्थिक रूप से, बाढ़ों द्वारा अस्थायी रूप से उपजाऊ भूमि का क्षरण किया जाता है, क्योंकि बाढ़ से प्रभावित आधिकांश क्षेत्र मुख्यतः सर्वाधिक कृषित क्षेत्र माने जाते हैं। बुआई के समय ही भारत में मानसून का आगमन होता है। यद्यपि बाढ़ें अपने साथ उपजाऊ गाद लाती हैं, किंतु ये व्यापक मृदा अपक्षय का कारण बनती हैं, जिससे मूल्य मृदा आवरण का नाश होता है। ब्रह्मपुत्र द्वारा मानसून के दौरान अपने किनारों पर व्यापक मृदा अपरदन किया जाता है। पंजाब व हरियाणा गहन कृषि क्षेत्र में, जहां नहर सिंचाई, रासायनिक उवरंकों एवं कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग होता है, बाढ़ के जल के वाष्पित हो जाने के उपरांत भूमि क्षारीयता का शिकार हो जाती है। ये क्षारीयता भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती है।
कभी-कभी बाढ़ों के कारण नदियों का प्रवाह मार्ग स्थायी रूप से विस्थापित हो जाता है। यह प्रवाह मागों के साथ लगी भूमि के उपयोग पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। बाढ़ का अप्रत्यक्ष प्रभाव रेल, सड़क एवं अन्य आवश्यक संचार सेवाओं के सुचारू संचालन में आयी बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है।
बाढ़ नियंत्रण के उपाय
बाढ़ में कमी लाने के कुछ उपाय निम्न हैं-
- बाढ़ पूर्वानुमान में स्थान विशेष को बाढ़ आने संबंधी सूचना समय पूर्व प्रदान करनी चाहिए ताकि बाढ़ से होने वाले विध्वंस को समय पर कार्यवाही करके कम किया जा सके। बाढ़ पूर्वानुमान को केंद्रीय जल आयोग ने नवम्बर 1958 में शुरू किया। वर्तमान में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। दैनंदिन बाढ़ पूर्वानुमान प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के दौरान पूरे बाढ़ मौसम में जारी किए जाते हैं।
- जल संग्रहण क्षेत्र में सतही जल के भूमि में अंतःस्पंदन द्वारा जल बहाव को कम करना जो बाढ़ रोकने का एक प्रभावी तरीका है। नदियों के ऊपरी अपवाह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनरोपण करके बाढ़ को कम किया जा सकता है।
- बाढ़ संभावित नदियों की पहचान की जाए और बाढ़ कम करने के लिए इनके रास्तों को चौड़ा और गहरा किया जाए। वर्षा के कारण नदी जल की मात्रा में हुई अत्यधिक वृद्धि का विचलन करने के लिए नहरों का निर्माण किया जाए।
- नदियों पर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट और बांध बनाए जाएं तो अधिशेष जल का भंडारण करेंगे और नदी जल के बहाव में कमी लाएंगे।
- बाढ़ के विध्वंस को प्रभावी रूप से रोकने के लिए नदियों के साथ-साथ पुश्ता निर्माण किया जाना चाहिए।
- एक क्षेत्र में बाढ़ चक्र का परीक्षण करने के पश्चात् बाढ़ संभावित क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए।
- बाढ़ संभावित नदियों में बड़ी निर्माण गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- बाढ़ के मैदानों को आबादी से मुक्त किया जाना चाहिए और नदी मागों से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए।
खास दीर्घावधिक उपायोग में जल संबंधी आंकड़ों और बाढ़ चेतावनी तंत्र की स्थापना को शामिल किया जाना चाहिए।
भारत सरकार द्वारा बाधों की रोकथाम एवं उनके विनाशकारी परिणामों को न्यूनतम करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के अंतर्गत अनेक बाढ़ प्रवण नदियों पर संचित जलाशयों का निर्माण किया गया है। कोनार, पंचेत, माइयान, तिलैया (सभी दामोदर नदी पर), हीराकुंड (महानदी), भाकड़ा (सतलज), पोंग (व्यास), उकाई (ताप्ती) तथा नागार्जुन सागर (कृष्णा) आदि ऐसे ही विशाल जलाशय हैं।
कुछ दीर्घकालिक उपायों में जल-विज्ञान सम्बंधी आंकड़ों का संग्रहण तथा बाढ़-चेतावनी प्रणालियों की स्थापना शामिल है।
किंतु इन उपायों के बावजूद बाढ़ के संकट का कोई व्यापक निदान सामने नहीं आ सका है।
भंडार जलाशयों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं
भंडार जलाशयों में जमा होने वाली गाद को रोकने के लिए व्यापक मृदा संरक्षण उपायों को भंडार जलाशय के उर्ध्व प्रवाह एवं आसपास के क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। गाद के जमा होने से जलाशयों की जल संचय की क्षमता घट जाती है। इस प्रकार ये बाढ़ के पानी को अवशोषित कर पाने में असमर्थ होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में जलाशयों के अवसादीकरण की दर आकलित दर से तीन गुना अधिक है। इससे भारत में जलाशयों की जीवनावधि में एक-तिहाई की कमी आई है।
भारी वर्षा के कारण निचले प्रवाह क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ों को रोकने में भी जलाशय अप्रभावी साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में पंजाब में स्थित भाखड़ा एवं पोंग जलाशय में शायद ही कभी उनकी क्षमतानुसार जल संचित हुआ है, जबकि भारी वर्षा के कारण निचले प्रवाह क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ों से पंजाब की लगभग आधी जनसंख्या प्रभावित रही है।
तटबंध-एक वैज्ञानिक समाघान नहीं
तटबंध जल प्रवाह को नियंत्रित करने वाले अप्राकृतिक साधन हैं। प्रायः एक तटबंधित नदी का जलस्तर आसपास की सतह से ऊपर होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में गाद बाढ़कृत मैदान पर बिछने की बजाय नदी संस्तर पर जमा हो जाती है। परिणामस्वरूप बाढ़कृत मैदान की उपजाऊ गाद से वर्ष दर वर्ष वंचित रहना पड़ता है। साथ ही तटबंध में कोई दरार आने की स्थिति में पानी अत्यधिक वेग के साथ आसपास के क्षेत्र में फैल सकता है और गंभीर हानि पहुंचा सकता है, जो सम्भवतः गैर-तटबंधित नदी में आयी धीमी बाढ़ की तुलना में अधिक हो। तटबंधित नदी में होने वाला अवसादीकरण अपवाह क्षेत्रों में हल्की-सी वर्षा होने पर बाढ़ को जन्म दे सकता है। इस प्रकार तटबंधों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अस्थायी होती है।
बाढ़ मैदान मंडलीकरण-एक टिकाऊ एवं वैज्ञानिक पद्धति
जलाशयों एवं तटबंधों की तुलना में यह एक गैर-संरचनात्मक उपाय है। यह नदी के प्रवाह मार्ग चयन के अधिकार पर बल देता है। बाढ़ मैदान, नदी प्रवाह मार्ग के विस्थापन का विस्तार या सीमारेखा है। स्थलाकृतिक रूप से बाढ़ मैदान आसपास के क्षेत्र से नीचे होते हैं तथा इसीलिए बाढ़ प्रवण हो जाते हैं।
बाढ़ मैदान मंडलीकरण का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा इन क्षेत्रों में विकास एवं मानवीय अधिवास गतिविधियों को रोकना है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1957 में बाढ़ मैदान मंडलीकरण के विचार को स्वीकार किया गया। 1975 में केंद्र सरकार द्वारा इस सम्बंध में एक प्रारूप विधेयक जारी किया गया। यह सभी राज्यों में बाढ़ मंडलन प्राधिकरणों के गठन का भी प्रावधान करता था। इन प्राधिकरणों से बाढ़ मैदानों या मंडलों के सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण का दायित्व निभाने की अपेक्षा की गयी। उक्त विधेयक में बाढ़ मैदानों के उपयोग को निषेधित करने तथा अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु विधायी समर्थन की अनुशंसा भी की गयी थी। हालांकि मणिपुर ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां इस सम्बंध में कानून बनाया है। अन्य राज्य प्रभावशाली भवन निर्माताओं, उद्योगपतियों एवं अन्य निहित स्वार्थों के दबाव में अपेक्षित कदम उठा पाने में असफल रहे हैं। ये राज्य राहत कार्यों के लिए अधिकाधिक अनुदानों की मांग तो करते हैं, किंतु बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की दीर्घावधि सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने के बारे में कोई पहल करना नहीं चाहते।
सूखा
सूखा शुष्कता की एक दशा है, जो एक दीर्घकाल तक जल की कमी होने के कारण पैदा होती है। मौसम विज्ञान के अर्थों में, सूखा वर्षण में होने वाली निरंतर एवं क्षेत्रीय रूप से विस्तृत कमी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार, सूखा एक ऐसी स्थिति है जब एक मौसम वैज्ञानिक उप-विभाग स्तर पर वर्षापात की कमी, एक दिए गए समय में उस उप-विभाग के दीर्घकालिक औसत से 25 प्रतिशत अधिक हो जाती है। यदि उक्त कमी 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच होती है तो सूखा को मृदु माना जाता है जबकि 50 प्रतिशत से अधिक होने पर यह कठोर हो जाता है।

भारत में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून द्वारा 70 से 80 प्रतिशत वर्षापात किया जाता है। सामान्य मात्रा से 19 प्रतिशत अधिक मानसूनी वर्षापात को अतिरेक वर्षा कहा जाता है। उन्नीस प्रतिशत होने पर सामान्य वर्षा तथा 19 प्रतिशत से कम की स्थिति में न्यून वर्षा होती है। उनसठ प्रतिशत से कम होने पर विरत वर्षापात की स्थिति पैदा होती है। मौसम वैज्ञानिक सूखा सांख्यिकी तथा वर्षापात वितरण प्रतिरूप का प्रदर्शन मात्र है। जलवैज्ञानिक सूखा निम्न जलस्तर तथा नदी व छोटी धाराओं के घटते हुए प्रवाह का प्रकटीकरण है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं एवं मनुष्यों की जरूरतों के लिए पानी की भारी कमी हो जाती है।
मौसम संबंधी सूखा वर्षण वितरण पैटर्न और सांख्यिकी का एक प्रतिनिधित्व मात्र है।
जलीय सूखा संकटकारी रूप से भूमिगत जल क्षेत्र में कमी आना, और नदी जल एवं धाराप्रवाह में कमी को चिन्हित करता है, जिस कारण पशुओं और मानव जरूरतों के लिए जल की भारी कमी हो जाती है।
कृषि सूखा तब होता है जब फसल वृद्धि के दौरान मृदा नमी और वर्षण में अपर्याप्तता होती है।
पारिस्थितिकीय सूखे की स्थिति तब आती है जब पानी की कमी के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता खत्म हो जाती है, और पारितंत्र को बेहद क्षति होती है।
सूखे की गहनता कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे, वर्षा अल्पता की मात्रा, शुष्ककाल की लम्बाई, प्रभावित क्षेत्र का आकार, तथा सिंचाई सहित विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि। सूखे की गहनता को व्यक्त करने के लिए सामान्यतः पामर सूखा कठोरता सूची का उपयोग किया जाता है। यह सूची +6 (नम स्थिति) से लेकर -6 (कठोर सूखा) तक की सीमा को शामिल करती है। इस सूचिका द्वारा उत्तरोत्तर काल अंतरालों में स्थानीय मौसम की सापेक्षिक शुष्कता को मापा जाता है। यह सामान्य दशाओं में एक जलवायु क्षेत्र के भीतर वाष्पोत्सर्जन, वाह तथा नमी भंडारण हेतु जरूरी वर्षण की न्यूनतम मात्रा तथा वास्तविक वर्षण के बीच विभेदों पर विचार करती है।
भारत में विशाल जनसंसाधनों के बावजूद सूखे की स्थिति बार-बार घटित होती रही है। वाष्पोत्सर्जन एवं अन्य हानियों के बाद भी लगभग 1870 क्यूबिक किमी. जल अधिशेष रह जाता है। किंतु, यथार्थ में मात्र 700 क्यूबिक किमी. सतही जलभंडार उपयोग के लायक रहता है क्योंकि कई प्रकार की स्थलाकृतिक एवं जलवैज्ञानिक बाधाएं मौजूद रहती हैं।
बेबाक रूप से कहा जाए तो, केवल गुजरात का कच्छ क्षेत्र और राजस्थान में मौसम संबंधी कारक गंभीर सूखे के लिए जिम्मेदार रहे हैं। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्र मौसम संबंधी सूखे की अपेक्षा जलीय सूखे से पीड़ित रहे हैं।
यह तथ्य चिंता का कारण है कि जलीय सूखा मौसम संबंधी सूखे का प्राकृतिक परिणाम नहीं है। अपेक्षतया, यह जल प्रबंधन कार्यों का अभाव या कमी और परम्परागत जल की कमी वाले क्षेत्रों में नियोजन के अभाव का परिणाम है।
अधिकतर विश्लेषकों ने वर्ष 2000 के पूर्वार्द्ध में उत्पन्न स्थिति को अकाल की अपेक्षा जलाभाव शब्द से विवेचित किए जाने का समर्थन किया। अकाल या सूखा एक प्राकृतिक विशेषता है, जबकि जलाभाव या कमी जनसंख्या वृद्धि और कमजोर शासन के माध्यम से मानवीय कुप्रबंधन है और जब तक प्रबंधन को सुधारा नहीं जाता इसकी स्थिति बदतर होती रहेगी।
सूखा संभावित क्षेत्रों में शामिल हैं-
- दक्षिण सौराष्ट्र तट से कानपुर और तब जालंधर तक जाने वाली लाइन का आयताकार आकृति बनाना, जिसमें राजस्थान का अधिकतर हिस्सा, विशेष रूप से अरावली पहाड़ियों का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात का मरुस्थलीय और कच्छ प्रदेश शामिल हैं;
- एक द्वितीय सूखा क्षेत्र जिसमें सहयाद्रि का अधिकतर हिस्सा जो पूर्व की ओर पश्चिम तट के 100 किमी. तक और दक्षिण की ओर टुककुर (कर्नाटक) और चितूर (आंध्र प्रदेश) को जोड़ने वाली लाइन तक
- कुछ खास पृथक् क्षेत्रों तक (तमिलनाडु के कोयम्बटूर और त्रिनेलवेली जिले; उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा और मिर्जापुर जिले; पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, झारखंड का पलामू जिला और ओडीशा का कालाहांडी जिला शामिल हैं)।
प्रभाव
सामान्यतः सूखा फसलों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, जिसके फलस्वरूप कुपोषण, महामारी, बाध्यकारी प्रवासन, आर्थिक अस्थिरता, जीवन क्षति तथा सामाजिक संघर्ष जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। भाग्यवश वर्तमान सूखे की स्थिति अकाल की ओर नहीं ले जाती। भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का भारी भंडार होता है। खाद्यान्नों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। एक मत के अनुसार नकदी फसलों पर सूखा द्वारा डाले गये प्रभाव के फलस्वरूप ग्रामीण आय स्तर में कमी आ जाती है। गुजरात एवं राजस्थान जैसे राज्यों में यह प्रभाव अधिक स्थानीयकृत एवं सीमित होता है। दूसरी ओर, एक अन्य मत के अनुसार सूखा प्रभावित क्षेत्र खपत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं ला पाते, भले ही खाद्यान्न एवं नकदी फसलों पर हानिकारी प्रभाव पड़ा हो।
सूखे के दीर्घकालिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूखे द्वारा होने वाली सामाजिक, परितंत्रीय पर्यावरणीय क्षति मापनीय नहीं होती। बस्ती प्रतिरूप तथा सामाजिक व रहन-सहन शैलियों में भी सूखे के फलस्वरूप बदलाव आ जाते हैं।
यहां तक कि फसल की त्वरित सिंचाई की आशिक असफलता शहरी अवसंरचना पर दबाव का कारण बनती है।
झाड़ियों की वृद्धि में कमी, मृदा अपरदन में वृद्धि और मरुस्थलीकरण का विस्तार जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रभाव हैं।
सूखे से निपटना
विगत् अनुभवों से, देश में सूखे के हानिकारक प्रभावों का प्रशमन करने के लिए कुछ दिशा-निर्देशों को रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम में शामिल होगा-
- वर्षा जल, सतही जल और भूमिगत जल क्षमता का समुच्चयपरक प्रयोग,
- उचित पक्तिबद्धता (बड़े पत्थरों या ककड़ों जैसे कठोर पदार्थों के साथ नहर की ढलवां दिशा का संरक्षण करना) ताकि आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले रिसाव द्वारा जल की क्षति से बचा जा सके;
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और लवणीय भूमि की पुनप्राप्ति के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर का विकास एवं प्रोत्साहन;
- सूखे से संरक्षा के लिए उचित पौधा किस्मों और फसल प्रतिरूप का प्रयोग करना।