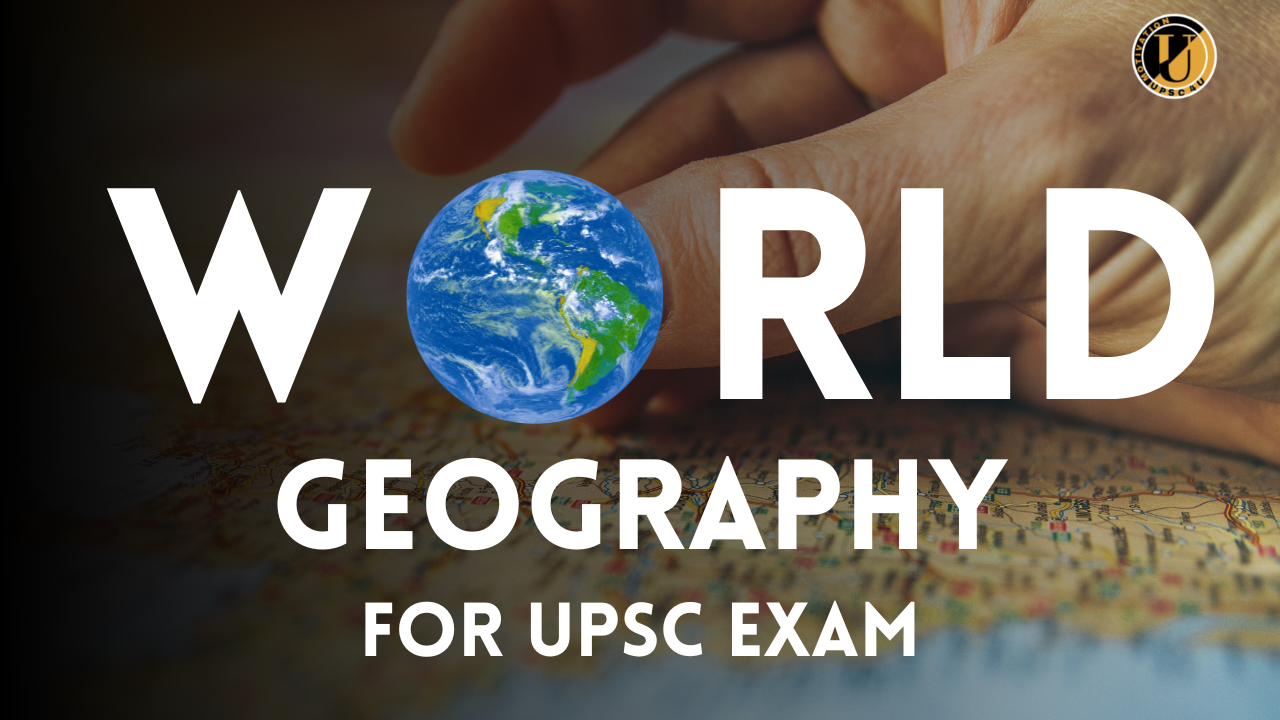मानव की आर्थिक क्रियाएँ एवं सम्पन्नता स्पष्टतः उसके चारों ओर मिलने वाले प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित रहे हैं। मानव पृथ्वी के धरातल (पर्यावरण) की उपज है” (Man is a Product of earth’s surface.)भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण से हमारा अभिप्राय उन अवस्थाओं से है जिनका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतन्त्र है, जो मानवरचित नहीं हैं और जो बिना मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों से प्रभावित हुए स्वतः परिवर्तित होती रहती हैं।
भूगोलवेत्ता डॉ. डेविस के अनुसार, “मनुष्य के सम्बन्ध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों और फैले उन सभी धरातलीय तथा अन्य प्राकृतिक स्वरूपों से है, जिनमें वह रहता है, जिनका उसकी आदतों और क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है।”
पर्यावरण के प्रकार Types of Environment
भौगोलिक पर्यावरण दो प्रकार का होता है :
- भौतिक अथवा प्राकृतिक
- सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित
प्राकृतिक पर्यावरण
प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन सम्पूर्ण भौतिक शक्तियों (forces), प्रक्रियाओं (processes), और तत्वों (Elements) से लिया जाता है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। इन शक्तियों के अन्तर्गत सूर्यताप, पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक परिभ्रमण की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वालामुखी क्रियाएँ, भू-पटल की गति तथा जीवन सम्बन्धी दृश्य सम्मिलित किए गए हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, जिनसे पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं और इन सबका प्रभाव मानव की क्रियाओं पर पड़ता है।
प्रक्रियाओं में भूमि का अपक्षय, अवसादीकरण, ताप विकिरण एवं चालन, ताप संवहन, वायु एवं जल में गति का पैदा होना, जीव की जातियों का जन्म, मरण और विकास, आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण से अनेक क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं जो मानव के क्रियाकलापों पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों के अन्तर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो शक्तियों और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होते हैंi इन तत्वों में
- भावात्मक तत्व, जैसे क्षेत्रीय विस्तार और आकार, प्रादेशिक स्वरूप और आकार, प्राकृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और ज्यामितीय स्थिति,
- प्राकृतिक तत्व, और तटीय क्षेत्र और
- जैविक तत्व, जैसे प्राकृतिक, वनस्पति, जीवजन्तु और अणु जीव सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त सभी तथ्य व तत्व मिलकर मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी मनुष्य के जीवन एवं उसके क्रियाकलापों तथा विकास के स्वरूप पर प्रभाव डालते हैं। इन्हें प्राथमिक , प्राकृतिक (Natural) या भौतिक (Physical) पर्यावरण कहा जाता है। इन सबका अस्तित्व मनुष्यों के कार्यो से स्वतन्त्र है, क्योंकि उनका मनुष्य ने सृजन नहीं किया है, वरन् ये प्रकृति की मानव को देन है। वैसे स्वयं मानव भी प्रकृति की ही उपज है। इसी कारण मानव के सभी क्रियाकलाप एवं स्वयं मानव अनेक प्रकार व विधियों से इनसे न्यूनाधिक प्रकार से प्रभावित होता रहा है।
सांस्कृतिक पर्यावरण
उपर्युक्त प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य प्रविधि या तकनीकी विकास की सहायता से संशोधन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वनाता रहा है। उदाहरण के लिए, वह घास के मैदानों में भूमि को जोतकर खेती पशुपालन करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग, आदि बनाता है, पर्वतों को काटकर सुरंग आदि निकालता है, नयी बस्तियाँ बसाता है तथा भूगर्भ से खनिज सम्पति निकालकर अनेक उपकरण एवं अन्य अस्त्रशस्त्र, यन्त्र, आदि बनाता है और प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से शोषण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन सबके फलस्वरूप वह एक नए पर्यावरण को जन्म देता है। इसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं।
इस मानव निर्मित या सांस्कृतिक पर्यावरण में भी शक्तियाँ, प्रक्रियाएँ एवं तत्व कार्य करते हैं। सामाजिक पर्यावरण मानव का नियामक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्देशक माना जाता है। इनमें-
शक्तियों के अन्तर्गत मानव स्वयं एक भौगोलिक घटक के रूप में क्षेत्र की जनसंख्या, उसका वितरण जनसंख्या में वृद्धि और उसके कारण सम्मिलित किए जाते हैं।
सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में वे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनके द्वारा मानव और मानव समूह वातावरण से सामंजस्य स्थापित करते हैं तथा पोषण, समूहीकरण, पुनः उत्पादन, प्रभुत्व स्थापना, प्रवास, पृथक्करण, अनुकूलन, विशिष्टीकरण और अनुक्रम को प्रभावित करते हैं एवं इनसे प्रभावित होते हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व
इन तत्वों के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है-
भौगोलिक स्थिति
भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोगों की आकृति, डीलडौल, रहनसहन, वेशभूषा, आचार विचार, कार्य करने की शक्ति, आदि में अन्तर भौगोलिक स्थिति के कारण पाया जाता है। प्रो. हंटिंगटन तथा कुशिंग के अनुसार, पृथ्वी के गोले की स्थिति ही भूगोल की वास्तविक कुंजी है।” किसी भी देश की स्थिति तभी अनुकूल मानी जाती है जबकि वहाँ की सीमा रेखाएँ प्राकृतिक हो, जलवायु सम हो, विश्व के व्यापारिक देशों के निकट हो और आवागमन के लिए मार्ग की सुविधाएँ पायी जाती हों। अनुकूल स्थिति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं-

सागरीय स्थिति- समुद्र के निकट स्थिति होने से उस देश का सम्बन्ध अन्य देशों से आसानी से जुड़ जाता है जिससे व्यापार में सुविधा होती है। जो देश समुद्र के निकट होते हैं वहाँ (विशेषतः तट के किनारे के) लोगों का मुख्य उद्योग व्यापार एवं मछली पकड़ना होता है।
तटीय स्थिति द्वीपीय, प्रायद्वीपीय अथवा तट के निकट कहीं भी हो सकती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जहाँ का तट कटाफटा हो, आदर्श स्थिति मानी जाती है। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड, जापान, आदि श्रीलंका, सिंगापुर, हाँगकाँग प्रधान मार्गों पर स्थित होने से भी श्रेष्ठ स्थिति में हैं। प्राकृतिक पोताश्रयों का निर्माण भी उत्तम व कटेफटे तटों पर ही सम्भव है।
जिन देशों की स्थिति तट से दूर महाद्वीपीय है। उन्हें अनेक प्रकार की प्रतिकूलता उठानी पड़ती है। नेपाल, अफगानिस्तान, बोलीविया, चेक गणराज्य व् स्लोवाक आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। इनकी नीति हमेशा ही तटीय पड़ोसी देशों से प्रभावित रहती है।
व्यापारिक मागों के समीप स्थिति- यदि किसी देश की स्थिति व्यापारिक मार्गों पर है तो उस देश का विदेशी व्यापार भी विकसित होने लगता है। सिंगापुर अदन, कोलम्बो व मुम्बई पूर्व-पश्चिम के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण ही विकसित हो सके हैं।
उन्नतशील एवं समृद्ध देशों के समीप स्थिति- जो देश उन्नतशील और समृद्ध देशों के समीप स्थित होते हैं उनका व्यापार भी काफी विकसित हो जाता है। जैसे यूरोप के निकट टर्की की स्थिति।
समुद्र से दूरी या तटीय रेखीय स्थिति
तट रेखा का किसी देश के व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तट रेखा कई प्रकार की हो सकती है- सपाट या कटीफटी, ऊँची या नीची, व्यापारिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से तट का कटाफटा होना आवश्यक है जिससे समुद्र देश के भीतर तक प्रविष्ट हो सके।
जापान एवं ब्रिटेन का समुद्री तट अधिक कटाफटा होने से ही वहाँ के आन्तरिक भाग भी सामुद्रिक मार्ग के निकट हैं जिससे आयात निर्यात एवं व्यापारिक व औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है।
सीमा रेखाएं Boundaries
सीमा रेखाएँ प्राकृतिक एवं कृत्रिम हो सकती हैं। प्राकृतिक सीमा (Natural Boundary) सागर, पर्वत, मरुभूमि, दलदल और नदियों द्वारा बनायी जाती है। इनस शत्रु से आक्रमण के प्रति निश्चिन्तता एवं स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न होती है। समुद्रों से घिरे होने के कारण ब्रिटेन की सीमा रेखाओं में युद्ध अथवा राजनीतिक क्रान्तियों द्वारा होने वाले परिवर्तनों की आशंका नहीं है और इसलिए यहाँ की आर्थिक दशा सीमा-परिवर्तन द्वारा होने वाले प्रभावों से मुक्त है। यूरोप में जहाँ मरुस्थलीय सीमाओं का अभाव पाया जाता है, वहाँ नदियों को अधिकांश यूरोपीय देशों की सीमा निर्धारण में काम में लाया गया है। मध्य राइन फ्रांस की जर्मनीसे और मध्य ड्रेन्यूब हंगरी और चैकव स्लोवाक गणराज्य के बीच सीमा बनाती है, परन्तु जिन नदियों को आसानी से पार किया जा सकता है, वे अच्छी सीमाएँ नहीं बनातीं।
मानवनिर्मित सीमा रेखाएँ प्रायः स्थलीय होती हैं। इनमें पर्वतों, मरुभूमियों, आदि प्राकृतिक व स्पष्ट विभाजन रेखाओं का अभाव होता है। ये ऐतिहासिक परिस्थितियों, सन्धियों, युद्धों अथूवा स्वीकृति पुत्रों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पोलैण्ड, चैक व स्लोवाक गणराज्य, रोमानिया, आदि की ऐसी ही सीमाएँ हैं। भारत व बांग्लादेश एवं भारत व पाकिस्तान के मध्य अधिकाँशत: ऐसी ही सीमाएँ हैं। अत: इन पर राजनीतिक परिवर्तनों, आदि का असर पड़ता रहता है। सन् 1938 से 1992 तक जर्मनी, पोलैण्ड, रूस और इटली, आदि कितने ही यूरोपीय देशों की सीमा रेखाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा भी मानव निर्मित है, अत: आपसी साधारण मतभेदों को लेकर ही यहाँ भी भारत पाक के मध्य अब तक तीन बड़े युद्ध हो चुके हैं।
देशों का आकार Size and Extention of Countries
किसी भी देश के आर्थिक साधनों में उसके आकार व विस्तार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो देश 26 लाख वर्ग किमी (10 लाख वर्गमील) या अधिक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उन्हें दानवाकार (Giant) देश कहते हैं। जिन देशों का क्षेत्रफल 2.6 लाख वर्ग किमी एक लाख वर्गमील) से अधिक, परन्तु 26 लाख वर्ग किमी (10 लाख वर्गमील) से कम होता है उन्हें बड़े देश कहते हैं और जो देश 2,60,000 वर्ग किमी (1 लाख वर्गमील) से कम, परन्तु 1,04,000 वर्ग किमी (40,000 वर्ग मील) से अधिक क्षेत्रफल वाले देशों को मध्यम विस्तार का देश कहते हैं। इससे कम क्षेत्रफल के अन्य सभी देश छोटे देशों में गिने जाते हैं।
देश का आकार कई प्रकार का होता है सघनाकार, छिन्नाकार और लम्बाकार। रूस, ब्राजील, भारत, संयुक्त राज्य, आदि देशों का सघनाकार (Compact) स्वरूप उस देश की यातायात की सुविधा और राजनीतिक एकता में सहायक होता है। इसके विपरीत, इण्डोनेशिया, यूनान जैसे देशों का छिन्नाकार स्वरूप माल वितरण और विचार-विमर्श में कठिनाई उत्पन्न करता है। चिली के समान लम्बाकार देश भी खेती के कायों में बाधक रहते हैं, क्योंकि अधिक लम्बाई के कारण जलवायु विषम एवं विविध हो जाती है।
देशों के आकार व विस्तार का प्रभाव जनसंख्या से सीधा सम्बन्धित होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या वाले छोटे देशों के निवासी केवल भूमि या कृषि पर ही निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि भूमि सीमित होती है। इन प्रदेशों में उत्पादन स्तर को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। चाहे गहरी खेती की जाए अथवा रासायनिक खाद दिया जाए और चाहे भूमि सम्बन्धी सुधार किए जाएँ। अतः ऐसे देशों में लोग अन्य विकसित उद्योग प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और जापान इसी प्रकार के देशों के मुख्य उदाहरण हैं, जहाँ कृषि की अपेक्षा उद्योगों और वैदेशिक व्यापार की विशेष उन्नति हुई है। सत्रहवीं से उन्नीसवीं सदी के मध्य सघन आबाद यूरोपीय देशों से बड़े पैमाने पर नई दुनिया एवं आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड की ओर आबादी के निरन्तर प्रवास से भी इन देशों की जन समस्याएँ कभी उग्र नहीं बन सकीं।
स्थल स्वरूप या धरातल Land Forms or Relief
इसके अन्तर्गत पर्वत पठार और मैदान सम्मिलित किए जाते हैं।
पर्वत पृथ्वी के धरातल पर उन भू-भागों को कहा जाता है जो समुद्रतल से 600 मी. से ऊँचे होते हैं। इनका क्षेत्रफल पृथ्वी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का केवल 1/10 है। पर्वत मानवजीवन को विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जैसा कि निम्न तथ्यों से स्पष्ट होगा-
पर्वतों का मानव जीवन पर प्रभाव Effects of Mountains On human Life
पर्वत अनेक प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं-
- पर्वतों का जलवायु पर प्रभाव– किसी स्थान की जलवायु पर्वतों से पूरी तरह प्रभावित रहती है। पर्वतों से टकराकर ही जल भरी पवनें वृष्टि करती हैं, जबकि विपरीत भाग वृष्टिछाया में आ जाने से सूखा रह जाता है। हिमालय उत्तरी भारत की वर्षा का प्रमुख कारण है। यह मध्य एशिया की कठोर जलवायु से भारत की रक्षा करते हैं। पहाड़ी धरातल एवं ऊँचाई के कारण ही बेल्जियम वासियों ने पूर्वी द्वीप समूह में सबसे पहले जावा को विकसित किया एवं वह सघन बसाव का क्षेत्र बन गया।
- पर्वत और कृषि– पर्वतों पर धरातल की विषमता से भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। पर्वतों से मिट्टी कटकर घर्षण एवं जल प्रवाह के कारण बह जाती है एवं वहाँ का धरातल भी पथरीला बना देती है। कभी वर्षा का आधिक्य और कभी उसका अभाव दोनों ही कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वनों से आच्छादित पर्वत प्रदेश में वन काटकर झूमिंग प्रणाली से खेती की जाती है। कभी-कभी पर्वतों के ढाल और तलहटी पर सीढ़ियाँ (Terraces) बनाकर खेती की जाती है, किन्तु यह बड़ी खर्चीली एवं थका देने वाली प्रणाली है। पर्वतों से ही नदियाँ निकलती हैं जिनसे मैदानी भागों की सिंचाई करके वहाँ पर उपजाऊ मैदानों में सघन कृषि करना सम्भव हो पाया है।
- पर्वत और खनिजसम्पति एवं उद्योग– विश्व के प्रसिद्ध पर्वतसमूह खनिज के अक्षय भण्डार हैं। जर्मनी की रूर घाटी में लोहा, कोयला दक्षिणी अमरीका के एण्डीज पर्वत प्रदेश में ताँबा, सोना, चाँदी, सीसा और पेट्रोलियम प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। रूस के धातु खनिज अधिकांशत: यूराल पर्वतमाला में पाए जाते हैं। ब्रिटेन की पिनाइन पर्वतमाला में कोयला और संयुक्त राज्य अमरीका के अप्लेशियन क्षेत्र में कोयला और खनिज तेल बहुतायत से पाया जाता है। खनिज पदार्थों के इसी प्रलोभन ने मनुष्यों को पर्वत की ओर आकृष्ट किया है, जिसके फलस्वरूप बड़े-बड़े खनिज केन्द्र आबाद हो गए हैं। पर्वतों के ढालों पर एवं गहरी नदीघाटियों के दोनों ओर से खनिजों का विदोहन अधिक सरलता से किया जा सकता है, किन्तु पहुँच की कठिनाई एवं विरल बसाव से वहाँ उद्योगों का विकास विशेष कठिन रहा है। प्रतिकूल मानव स्वभाव भी ऐसे विकास में बाधक रहा है।
- पर्वत और प्राकृतिक वनस्पति– पर्वतों का प्राकृतिक वनस्पति से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यूरोप के निवासी तो वन और पर्वतों में कोई स्पष्ट अन्तर ही नहीं मानते, क्योंकि जर्मनी के काले पहाड़ को काला जंगल के नाम से पुकारते हैं। वनों का पर्वतों से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है जिसके तीन कारण मुख्य हैं- 1) पर्वतीय प्रदेश में खेती के विकास की सम्भावना कम रहती है। 2) पर्वतों पर जल मैदानों की अपेक्षा अधिक बरसता है जिससे वनों के विकास में बहुत सहायता मिलती है। 3) वनों की उत्पत्ति के लिए खेती की भाँति किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती।

पर्वतों की वन सम्पति से अनेक उद्योगों को कच्चा माल मिलता रहता है। यहाँ से कागज की लुग्दी, फर्नीचर, मकान बनाने की लकड़ी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक उपजें, जड़ीबूटियाँ, माचिस, प्लाई, कृत्रिम रेशा व जलाने का ईधन मिलता है। निचले ढालों पर फल भी पैदा किए जाते हैं। ढालू मैदानों पर पशु चराए जाते हैं।
- पर्वत और परिवहन– उबड़-खाबड़ एवं विषम धरातल होने से पर्वतीय प्रदेशों में परिवहन के मार्ग बनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रेलें अथवा पक्की सड़कें बनाना श्रमसाध्य एवं महंगा पड़ता है। वहाँ केवल खच्चर, याक तथा पहाड़ी कुली ही अधिकतर बोझा ढोते हैं। कहीं कहीं पर्वतों को काटकर एक विशेष खर्चा उठाकर रेल लाइन बिछाई गयी हैं, जैसे बनिहाल सुरंग से होकर जम्मू-श्रीनगर सड़क तथा ऐल्प्स पर्वत के आर-पार सिम्पसन सुरंग खोदकर स्विट्ज़रलैंड से इटली तक बनाया गया है। पर्वत परिवहन में बाधा पहुँचाते हैं।
- पर्वत और सुरक्षा- पर्वतमालाएँ जिन देशों के चारों ओर होती हैं वहाँ से सन्तरी का सा कार्य करती हैं। भारत की उत्तर-पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा पर हिमालय के कारण बाहरी आक्रमण बहुत कम अथवा कुछ विशेष दरों से होकर ही हो सके हैं। नेपाल पर्वतमालाओं की गोद में निश्चिन्त है जिससे उसने विदेशी प्रभाव से अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने में सफलता पायी है। अपनी पर्वतीय स्थिति के कारण ही स्विट्जरलैण्ड विश्व के महायुद्धों में तटस्थ बना रहा।
- पर्वत और जल विद्युत शक्ति- पर्वतीय प्रदेश का धरातल ऊबड़-खाबड़ होने से वहाँ नदियाँ तेज गति से बहती हैं। अतः जलविद्युत के लिए बाँध बनाने में आसानी रही है। ऐसी अनुकूलता के कारण ही जापान, स्वीडन, नार्वे, इटली संयुक्त राज्य, ब्राजील, दक्षिण-पूर्वी कनाडा, आदि देशों में बड़ी मात्रा में जल विद्युत पैदा की जाती है। पर्वतीय प्रदेशों में बाँध व झीलों के आधिक्य के कारण नदियों में जल की कमी पड़ने की कम सम्भावना रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत के लिए कम खर्चे पर ही सारी सुविधाएँ नैसर्गिक रूप से सुलभ हैं यह अन्य क्षेत्रों में नहीं हैं।
- पर्वत मनुष्य जाति के आकर्षण केन्द्र- मानव प्रारम्भ से ही सौन्दर्य प्रेमी रहा है। मैदानों की ग्रीष्म की प्रचण्ड वायु जब शरीर को झुलसाने लगती है तो उस समय इन पर्वतमालाओं का महत्व और भी बढ़ स्थल पर्वत एवं पर्वतीय घाटियों में ही स्थित हैं। पर्वतों पर घूमना और बर्फ पर स्केटिंग करना एवं झीलों में नौकाविहार बड़ा मनोहारी होता है।
- पर्वत और जनसंख्या- ऊँचे पर्वतीय भाग जीवनयापन के लिए उपयुक्त स्थल नहीं हैं। पर्वतीय ढालों पर जहाँ ऊँचाई कम होती है तथा मिट्टी का कुछ भ्रंश पाया जाता है वहाँ जनसंख्या पायी जाती है, क्योंकि वहाँ खेती की जा सकती है, किन्तु ऐसे स्थल दूरदूर होते हैं, अतः जनसंख्या बिखरी हुई पायी जाती है। सिर्फ घाटियों या वादियों में ही अधिक आबादी पायी जाती है।
- पर्वत और मानव स्वभाव- पर्वतीय भागों में निवास करने वाले मनुष्यों का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, क्योंकि पर्वतीय भागों में जीविकोपार्जन के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यही कारण है कि पहाड़ी लोग हृष्टपुट, परिश्रमी, साहसी तथा वीर होते हैं, किन्तु बाह्य संसार के प्रभाव से अलग होने के कारण यहाँ के निवासी अपनी रूढ़िवादी परम्पराओं के भक्त होते हैं। ये स्वभाव से कट्टर, सच्चे और ईमानदार होते हैं, किन्तु इनमें असहयोग की प्रवृत्ति होती है। मैदानी क्षेत्रों से इनका सम्बन्ध होने से ये विकसित होने लगे। हैं। स्विट्जरलैण्ड के निवासी शक्तिशाली किन्तु शान्तिप्रिय हैं, अफगानिस्तान के लोगों का समाज शक्तिशाली पर युद्धप्रिय है, जबकि तिब्बत के लोगों का समाज दुर्बल व शान्तिप्रिय लामापन्थी आधार पर बना है।
पठार Plateaus
पठार धरातल के मुख्य भू-आकार हैं। इनके द्वारा पृथ्वी का एक विशाल भाग आवृत्त है। यह धरातल का वह ऊँचा भाग होता है जो समुद्र तल से काफी उठा हुआ, ऊँचा-नीचा तथा आधार की अपेक्षा ऊपर की ओर कम चौड़ा होता है। इनी मुख्य विशेषता निकटवर्ती क्षेत्रों से अधिक ऊँचाई, विशाल विस्तार तथा शिखर का प्रायः समतल होना हैt अपरदन के प्रभाव से पठार जटिल धरातल वाला हो जाता है जैसे दक्कन का पठार।
पठारों का मानव जीवन पर प्रभाव Effectof Plateaus on Human Life
- पठार और जलवायु- यद्यपि पठारों की औसत ऊँचाई 600 मीटर मानी गयी है, किन्तु कुछ पठार इससे भी अधिक ऊँचे होते हैं जैसे, तिब्बत, पामीर, बोलीविया के पठार। इन पठारों पर शीत की अधिकता के कारण हिम जम जाती है जिससे वहाँ की जलवायु अत्यन्त ठण्डी हो जाती है। कठोर जलवायु व शुष्कता के कारण यह पठार प्रायः जन शून्य हैं। कुछ पठारों पर जल तो अधिक बरस जाता है, किन्तु उसके निकास का समुचित साधन न होने के कारण यह जल वहाँ एकत्र हो जाता है, जिससे मलेरिया आदि के फैलने का डर रहता है।
- पठार और कृषि- कुछ पठार जैसे पामीर, तिब्बत, आदि अत्यधिक ऊँचाई के कारण हिमाच्छादित रहते हैं, जहाँ कृषिकार्य के अनुकूल जलवायु नहीं मिलती। यदि कहीं ऊँचाई कम और धरातल चौरस पाया जाता है तो भी पथरीला या रेतीला धरातल एवं शुष्कता के कारण वहाँ फसलों के विकास में बाधा पहुंचती है जैसे कि अरेबिया का पठार। जहाँ कहीं उपजाऊ एवं महीन व चिकनी लावा की शैलें काली मिट्टी का रूप लेकर जम जाती हैं वहाँ कपास, गन्ना, तिलहन, आदि पैदा की जाती है। दक्षिणी भारत के पठार को काली मिट्टी में कपास की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है।
- पठार और वनस्पति- प्राकृतिक वनस्पति के लिए इनका स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निचले ढालों पर अनेक प्रकार की घासें उगती हैं, जिससे वहाँ पशुपालन आसानी से किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और आस्ट्रेलिया के पूर्वी पठार पशुपालन के लिए इसी कारण प्रसिद्ध हैं। अर्द्धशुष्क पैटागोनिया पर भेड़ पालने से ऊन व माँस व्यवसाय अधिक उन्नतावस्था में है। कई पठारों पर वर्षा की अधिकता के कारण सघन वन अधिक पाए जाते हैं जिनमें बहुमूल्य लकड़ियाँ पायी जाती हैं। जैसे दक्कन के पठार (भारत) पर वहुमूल्य सागवान के वनों सघन का विस्तार ब्राजील के दक्षिण पूर्वी पठार के आद्र भागों में भी घने वन पाये जाते हैं।
- पठार और परिवहन- पठारी प्रदेश अधिकांशत: कम ऊँचे होते हैं और उनका ढाल घीमा होता है। पत्थर तथा कंकड़ आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। चट्टानी नीव के कारण धरातल ठोस और दृढ़ होता है। अतः इन प्रदेशों में पक्की एवं मजबूत सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है।
- पठार और खनिज सम्पति- खनिज सम्पति के तो ये भण्डार ही होते हैं। प्राचीन पठारी प्रदेश जिनमें रवेदार शैलें पायी जाती हैं) खनिज की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के हैं। साइबेरिया पठार के लीना नदी के पास का प्रदेश सोने की खानों अन्य धातुओं एवं प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया में सोना, बक्साइट, लौह-अयस्क, दक्षिण अफ्रीका में सोना, तांबा और हीरे, बाजील के पठारों पर मैंगनीज़, सोना और हीरे भारत के पठारी भाग पर मैंगनीज, लोहा, बॉक्साइट, कोयल, अभ्रक और यूरोप के पठारों पर लोहा तथा कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- पठार और उद्योग- पठारी प्रदेशों में स्थानीय वन, कृषि एवं खनिज, संसाधनों के अनुसार उद्योगों का विकास हुआ है। अत: इन प्रदेशों में धातु सम्बन्धित निर्माणी उद्योगों का कुछ विशेष केन्द्रों पर विकास हो जाता है। कम ऊँचे पठारों जैसे-भारत, ब्राजील, दक्षिण मध्य रूस, उत्तर-पूर्वी संयुक्त राज्य के नीचे पठारों पर अधिक खनिज सम्पदा मिलने पर वहाँ का औद्योगिक विकास विशेष व्यापक स्तर पर हुआ है। सामान्यत: ऊँचे पठारी प्रदेशों में आर्थिक कार्यकलापों की गतिविधियाँ मैदानी प्रदेशों की अपेक्षा घीमी होती हैं। लोगों का प्रमुख व्यवसाय खनिज निकालना, पशुपालन या लकड़ी काटना, आदि ही होता है।
- पठार और जनसंख्या- पठारों पर जनसंख्या उन स्थानों पर ही पायी जाती है जहाँ या तो खानों की प्रचुरता हो अथवा खेती करने की सुविधा हो या अन्य किसी प्रकार के जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हो। पठारों पर अधिक जनसंख्या के केन्द्र कुछ अनुकूल स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जिनमें खनन व औद्योगिक केन्द्र मुख्य हैं। पूर्वी अफ्रीका दक्षिण-पूर्वी ब्राजील का पठार विकसित कृषि, पशुपालन, खनन एवं सीमित औद्योगिक विकास के कारण सघन बसाव के क्षेत्र हैं ।
मैदान Plains
सामान्य रूप से मैदान धरातल के वे विस्तृत भाग होते हैं जो प्रायः समतल एवं समुद्रतल से 200 मीटर से अधिक ऊँचे नहीं हैं। इनका ढाल मन्द होता है। कुछ मैदान पूर्णतः समतल होते हैं जबकि कुछ ऊँचे-नीचे होते हैं। कुछ समुद्रों के किनारे स्थित होते हैं तो कुछ महाद्वीपीय भागों में भीतर की ओर। कुछ उपजाऊ अवसादी मिट्टी के बने होते हैं तो कुछ चूने और शैल के।
मैदानों का मानव जीवन पर प्रभाव Effects of Plains on Human Life
मैदान मानव जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। मानव सभ्यता यहीं फलती-फूलती है और यहीं से अन्यत्र फैलती है। सिन्धु, , गंगा व यमुना के मैदानों में ही वैदिक सभ्यता पनपी है। मैदान आर्थिक जीवन का केन्द्रीय प्रदेश होने के साथसाथ राजनीतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के भी केन्द्र बने रहते हैं। महान् विद्वान कुमारी सेम्पल के अनुसार, “मैदान ही ऐसे भाग हैं जहाँ मनुष्य, व्यापार व वाणिज्य और राजनीतिक व्यवस्था तीनों का ही उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। आधुनिक जीवन की धुरी अर्थतन्त्र है और अर्थतन्त्र का सबसे प्रबल माध्यम है व्यापार”।
मैदानों में ही यातायात व विकसित संचार तन्त्र की सर्वाधिक सुविधाएँ सुलभ हैं और इसी से यहाँ परिवहन मार्गों का जाल बिछा है। यहाँ की परिस्थितियाँ मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए अनुकूल पर्यावरण उपस्थित करती हैं। यहीं पर ऐतिहासिक नगरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं और यहीं आधुनिक काल के विशाल नगरों का प्रसार होता जा रहा है।
मैदान और वनस्पति- विश्व के अर्द्धोष्ण, उष्ण एवं शीतल शीतोष्ण प्रदेशों के उपजाऊ मैदानी भागों से निरन्तर मानव बसाव के विस्तार से प्राकृतिक वनस्पति नष्ट कर दी गई है। अब यहाँ कृषि, पशुपालन उद्योग, बस्तियाँ, आदि का विकास हो गया है। अत: केवल उष्ण व आर्द्र प्रदेशों के विरल बसाव के भागों एवं टैगा प्रदेशों में ही वास्तविक या प्राकृतिक वन पाए जाते हैं।
मैदान और कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन- मैदान कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। मैदानों पर समतल एवं उपजाऊ भूमि का विस्तार होने के कारण खेती करना सुगम और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। यहाँ सिंचाई के लिए नदियों से नहरें बनाना तथा ट्यूबवेल व कुएँ खोदना सुगम होता है। ढाल कम होने से भूमि का जल व वायु से कटाव कम होता है। अतः यहाँ की समतल, विस्तृत, गहरी, उपजाऊ भूमि विभिन्न प्रकार की विकसित फसलें उत्पन्न करने तथा पशुपालने की सुविधा मनुष्य को प्रदान करती हैं। सिन्धु-गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन का यॉगटिसीक्यांग और सीक्याँग का मैदान, मिसीसिपी तथा अटलाण्टिक का तटीय मैदान, नील नदी की घाटी, दजलाफरात का मैदान विश्व के अनेक कृषि पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सन, जूट, आदि के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। ये मैदान मानव को खाद्यान्न तथा अधिकांश व्यापारिक फसलें प्रदान करते हैं। उष्णकटिबन्ध के तटीय मैदान चावल और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व के प्रायः सभी मैदानों में ही महत्वपूर्ण घास के मैदान भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे स्टेपी, प्रेयरी, आदि। शीतोष्ण कटिबन्ध वाले देशों के मैदानों में चरागाहों की अधिकता के कारण पशुपालन व्यवसाय बड़े वैज्ञानिक और व्यापारिक ढंग पर किया जाता है।
मैदान् ओर खनिज सम्पति- पर्वतीय एवं पट्टारी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र खनिज सम्पदा की दृष्टि से निर्धन होते हैं। नवनिर्मित मैदानी क्षेत्रों में कोयला और पेट्रोलियम के भण्डार भी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश पेट्रोलियम के भण्डार उष्ण मरुस्थलीय मैदानों में मिलते हैं। मैदानी प्रदेशों में चूना पत्थर अथवा कहीं-कहीं विशेष उपयोगी मिट्टियों के भण्डार भी पाए जाते हैं।
मैदान और परिवहन व संचार- मैदानों की भूमि समतल होने के कारण यातायात के साधनों के विस्तार के लिए बहुत अनुकूल होती है। यही कारण है कि विश्व के सभी मैदानों में यातायात का जाल सा बिछा है। मैदानी भागों में समतल धरातल एवं मन्द ढाल के कारण नदियाँ मन्द गति से बहती हैं जो नौकारोहण की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। मैदानी प्रदेशों की गंगा, सिन्धु और यॉगटिसीक्यांग (एशिया में) डेन्यूब, रोन और राइन (यूरोप में) मिसीसिपी उत्तरी अमरीका विकसित परिवहन व संचार प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त भारत के गंगा के मैदान में तथा यूरोप के नीदरलैण्ड, बेल्जियम, आदि देशों में अनेक बड़ी नहरें हैं जो सिंचाई तथा यातायात की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। समतल धरातल के कारण रेलमार्ग, वायुमार्ग तथा सड़कें बहुतायत से मैदानों में मिलती हैं। आज तृतीयक व्यवसाय के विकास का आधार भी विकसित परिवहन एवं संचार प्रणाली ही है।
मैदान और उद्योग-धंधे- मैदानी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों में कृषि और पशुपालन प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं प्रदेशों से विश्व की खाद्यान्न और अधिकांश कृषि जन्य व्यापारिक फसलों की प्राप्ति होती है। मैदानी प्रदेशों में निर्माण उद्योगों को विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कृषिजन्य कच्चा माल उपलब्ध होता है और उस पर आधारित उपभोक्ता से सम्बन्धित निर्माणी उद्योग स्थापित होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में घनी आबादी होने के कारण निर्माणी उद्योगों को निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती और यातायात की सुलभता के कारण दूर के बाजारों में भी पहुंचाया जाता है।
मैदान और मानव सभ्यता- मैदानों में जीविकोपार्जन की सुविधा, कृषि, यातायात, जलपूर्ति के कारण आदिकाल से जनसंख्या का जमघट रहा है जिससे इनमें अनेक सभ्यताएँ विकसित हुई। जैसे चीन की वीहो घाटी, सिन्धु घाटी, नील घाटी, बेबीलोन, आदि की सभ्यताएँ मैदानों में ही विकसित हुई।
मैदान और जनसंख्या- मैदानी प्रदेशों में जीविकोपार्जन के सभी प्रकार के साधन परम्परागत से लेकर अभिनव तकनीक के विकसित स्वरूप सभी सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि विश्व की 90 प्रतिशत जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। मैदानी प्रदेशों में कृषि, पशुपालन, उद्योगों एवं परिवहन के विकास के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। यहाँ निवासस्थानों एवं निर्माण के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भूमि, शुद्ध व स्वच्छ जल, निर्माण सामग्री, आदि सभी मिल जाते हैं। इन सब सुविधाओं के कारण मानव मैदानों की ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि गंगा-यमुना दोआब, ह्वांगहो, मिसीसिपी-मिसौरी, आदि नदियों के मैदानों में अधिक जनसंख्या मिलती है। विश्व के 90 प्रतिशत नगर व महानगर मैदानों में ही स्थित हैं।
जलाशाय या जल संसाधन
जल मानवजीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्थल खण्डपृथ्वी के प्रमुख जल स्रोत, सागर, नदियाँ और झीलें हैं। इन्हीं के कारण स्थल पर वृष्टि होती है। सागरीय भागों में तापान्तर कम रहते हैं और सागर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं।
सागरों का मानव-जीवन पर प्रभाव- सागर मानव के आर्थिक जीवन को इस प्रकार प्रभावित करते हैं-
- सागरों से उठने वाली वाष्पयुक्त पवनों से ही पृथ्वी पर वर्षा होती है।
- ये अपने निकटवर्ती धरातल के तापमान को समान बनाए रखते हैं। उसे न अधिक गर्म होने देते हैं और न ही अधिक शीतल।
- ये मछलियों के भण्डार के रूप से मानव को भोजन प्रदान करते हैं।
- इनमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे, नमक, ताँबा, पेट्रोलियम, मैंगनीज, जस्ता, सोना, चाँदी, लोहा, कोबाल्ट, आदि लेकिन अभी इनका शोषण नहीं हो रहा है।
- ये व्यापार के लिए सस्ते और सर्वोत्तम जलमार्ग प्रस्तुत करते हैं। सामुद्रिक धाराएँ तथा ज्वारभाटे भी मनुष्य की आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाओं को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं।
- उष्ण कटिबन्धीय तट पर ठण्डी धाराएँ एवं शीतोष्ण कटिबन्धीय तट पर गर्म धाराएँ जलवायु को उत्साहवर्धक एवं कार्यक्षमता बढ़ाने वाली होती हैं। पूर्वी संयुक्त राज्य, पश्चिमी यूरोप, जापान अलास्का का दक्षिणी तट गर्म धाराओं के प्रभाव से खुला रहता है एवं वहाँ की जलवायु विकास के अनुकूल बनी रहती है।
- पोताश्रयों एवं नदी के मुहानों में ज्वारीय लहर के प्रभाव से जल की गहराई बढ़ जाती है इससे सरलता से जहाज आ जा सकते हैं। अब तो ज्वार भाटा से विद्युत भी पैदा की जाती है। केवल ऊँची एवं वेगवती ज्वारीय लहरों से कभी-कभी जन-धन की हानि होती है, किन्तु ज्वार के लौटते समय कूड़ा करकट भी तट से दूर हटा दिया जाता है।
नदियों, झीलों जलाशयों का मानवजीवन पर प्रभाव- नदियाँ उपजाऊ मैदानों को जन्म देती हैं। गंगा, सिन्धु, नील, ह्वांगहो, आदि के मैदानी भाग अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। कछारी भाग प्रति वर्ष उपजाऊ मिट्टी प्राप्त कर लेते हैं, अतः वे खाद्यान्न तथा अन्य व्यापारिक फसलों के मुख्य उत्पादन क्षेत्र बन गए हैं। नदी घाटियों में इसी कारण जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। इन घाटियों की जलवायु उपयुक्त हुई तो इन भागों में गहरी कृषि की जाने लगती है। इसके अतिरिक्त नदियाँ मछलियाँ प्रदान करती हैं। इसी भाँति बड़ी झीलों के आसपास की उपजाऊ भूमि एवं जल की सुविधा का मानव वसाव पर स्थानीय रूप से प्रभाव पड़ता है। कई झीलें नदियों के माध्यम से नाव्य सागर से जुड़ी हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की बड़ी झीलें व केस्पियन सागर अतः यहाँ कई औद्योगिक केन्द्र भी विकसित हो गए हैं। मछलियाँ भी यहाँ खूब पकड़ी जाती हैं।
औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से नदियों के जल को रोककर जल- विद्युत उत्पन्न की जाती है जो विश्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण, स्वच्छ एवं सस्ता औद्योगिक ईंधन व ऊर्जा है। पर्वतों पर यह शक्ति जलप्रपातों तथा मैदानी भागों में कृत्रिम बाँध बनाकर उत्पन्न की जाती है। नदियाँ उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में जल प्रदान करती हैं। लगभग सभी बड़े औद्योगिक केन्द्र नदियों के समीप ही स्थित हैं। कुछ उद्योगों को बहुत अधिक मात्रा में स्वच्छ तथा मीठे जल की आवश्यकता होती है, अतः वे नदियों के समीप ही स्थित होते हैं जूट जैसे उद्योग, कागज उद्योग, धातु उद्योग, आदि। नदियाँ भारी व्यापारिक एवं औद्योगिक वस्तुएँ ढोने के लिए सस्ते आन्तरिक जल मार्ग प्रदान करती हैं।
जलवायु Climate
प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व समान रूप से मानव-जीवन को प्रभावित नहीं करते। कुछ तत्व स्थान एवं प्रदेश विशेष के लिए सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान होते हैं। इनमें जलवायु विशेष महत्वपूर्ण है इसका प्रभाव मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में होता ही है।
मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु का सर्वोच्च स्थान होता है। यह इसलिए नहीं कि जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वरन् यह सबसे अधिक प्राकृतिक मौलिकता रखती है। जलवायु के विभिन्न तत्वों का बहुमुखी प्रभाव व नियन्त्रण उत्पादन, वितरण और वस्तुओं के व्यापार में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। मानव सभ्यता तथा विकास जलवायु पर निर्भर रहा है।
सभ्यता के प्रारम्भ तथा विकास में जहाँ तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध रहता है वहाँ जलवायु एक बड़ा शक्तिशाली अवयव है।
मानव-जीवन पर जलवायु का प्रभाव Effect of Climate on Human Life
मानव-जीवन पर जलवायु का प्रभाव निम्न प्रकार दृष्टिगोचर होता है-
जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति- किसी देश की प्राकृतिक वनस्पति न केवल धरातल और मिट्टी के गुणों पर निर्भर करती है, वरन् वहाँ के तापमान और वर्षा का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पौधे के विकास के लिए वर्षा, तापमान, प्रकाश और वायु की आवश्यकता पड़ती है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में निरन्तर तेज धूप, कड़ी गर्मी और अधिक वर्षा के कारण ऐसे वृक्ष उगते हैं, जिनकी पतियाँ घनी, ऊँचाई बहुत और लकड़ी अत्यन्त कठोर होती है। इसके अतिरिक्त इन वृक्षों में सहारे कई प्रकार की बेलें, झाड़ियाँ एवं जंगली फूल, आदि उग आते हैं जो इनकी सघनता में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत, मरुस्थलों में काँटेदार झाड़ियाँ भी बड़ी कठिनाई से उग पाती हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा का अभाव होता है। सूडानी तथा प्रेयरी प्रदेशों में केवल घास ही उगती है क्योंकि वहाँ वर्षा केवल इतनी ही होती है कि घास पैदा हो सके। ध्रुवीय प्रदेशों में सदैव हिम जमे रहने के कारण काई के सिवाय कोई पौधा नहीं मिलता। लगभग ही स्थिति शीतोष्ण प्रदेशों के वनस्पति क्षेत्रों की है। संक्षेप में, जलवायु वनस्पति का प्राणाधार है।
जलवायु और जीवजन्तु- जलवायु की विविधता ने प्राणियों में भी विविधता स्थापित की है। जिस प्रकार विभिन्न जलवायु में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पायी जाती है वैसे ही विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अनेक प्रकार के जीवजन्तु पाए जाते हैं जैसे भूमध्यरेखीय जलवायु में मुख्यतः चार प्रकार के जीवजन्तु पाए जाते हैं। पहले, वे जो वृक्षों की शाखाओं पर रहकर सूर्य की गर्मी और प्रकाश प्राप्त करते हैं जैसे नाना प्रकार के बन्दर, चमगादड़ , आदि। दूसरे, वे जो बहुत भारी और मोटे शरीर के होते हैं जो सघन वनों में अपना रास्ता बना सकते हैं, जैसे-हाथी, गैंडा, आदि। तीसरे, वे जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आजा सकते हैं, जैसे- कीड़े-मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, आदि जिनकी भनभनाहट से यहाँ के वन गूंजते रहते हैं। चौथे, वे जो जल में निवास करते हैं, जैसे-मगर, दरियाई घोड़े, आदि। ठीक इससे भिन्न प्रकार के प्राणी टुण्ड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं जिनके शरीर पर लम्बे और मुलायम बाल होते हैं, जिनके कारण वे कठोर शीत से अपनी रक्षा करते हैं। इस प्रदेश के प्रमुख पशु सफेद , सफेद लोमड़ी, भेड़िया, लोमिंग, रेण्डियर, आदि हैं। यहाँ जलचर के रूप में मानव का मुख्य भोज्य पदार्थ सील, वालरस, आदि मछलियाँ पायी जाती हैं। ये जीव-जन्तु इस प्रदेश के निवासियों के लिए वरदानस्वरूप हैं।
जलवायु और कृषि- किसी प्रदेश विशेष में कौन-सी फसलें उत्पन्न की जाती हैं, साल में कितनी फसलें ली जा सकती हैं और कृषि कार्य का क्या स्वरूप होता है, यह सब जलवायु पर ही निर्भर करता है। जिन प्रदेशों की जलवायु गर्म तथा नम होती है, वहाँ कृषि के लिए अनुकूल वातावरण होता है। जहाँ वर्षा साधारण होती है, वहाँ सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है या शुष्क फसलें उगायी जाती हैं। उष्ण प्रदेश में चावल, गन्ना, रबड़, काफी, केला, आदि केवल इसलिए अधिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनको ऊँचे तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शीतोष्ण प्रदेशों में गेहूं, चुकन्दर, आदि की खेती वहाँ की जलवायु के कारण ही है। जैतून केवल भूमध्यसागरीय जलवायु की, रबड़ भूमध्यरेखीय जलवायु की, जूट और चावल दक्षिण-पूर्वी एशिया के मानसूनी जलवायु प्रदेशों की उपज हैं। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न फसलों का उत्पादन वहाँ की जलवायु की ही देन है। ) जलवायु और उद्योगजलवायु का प्रभाव मानव के उद्योगों पर भी पड़ता है। शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में मछलियाँ और वालदार पशुओं का शिकार करना तथा लकड़ी काटना ही मुख्य उद्यम होता है, कुछ विशेष उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आद्र जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुष्क जलवायु में कातने में सूत बारबार टूट जाता है और वह अधिक लम्बा भी नहीं काता जा सकता। आर्द्र जलवायु के कारण ही भारत में मुम्बई और अहमदावाद में, जापान में ओसाका में और ब्रिटेन में मैनचेस्टर में सूती वस्त्रों के कारखाने केन्द्रित हैं।
जलवायु उद्योगों पर परोक्ष रूप से काफी प्रभाव डालती रही है। अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों में उद्योगों का पर्याप्त विकास होता है। समशीतोष्ण प्रदेशों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, जबकि उष्ण कटिबन्धीय भूमध्यरेखीय सवाना और मरुस्थलीय प्रदेशों में प्रतिकूल जलवायु के कारण ही औद्योगिक विकास बहुत ही कम हुआ है।
जलवायु और परिवहन- परिवहन के विकास पर जलवायु के तत्वों का प्रभाव लगभग धरातल जैसा पड़ता है। मौसम के प्रतिकूल होने पर परिवहन के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भारी हिमपात, अधिक वर्षा, तूफान एवं बाढ़ से रेल की पटरियाँ और पुल नष्ट हो जाते हैं। मरुस्थलों में बालू के टीलों के कारण न तो सड़कें ही बनायी जा सकती हैं और रेलमार्ग ही ठण्डे प्रदेशों में समुद्र और नदियाँ शीतमें जम जाती हैं, फलतः इनके द्वारा होने वाला व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। घने कोहरे के कारण अनेक दुर्घटनाएँ होती हैं। वायु तथा जल परिवहन के लिए भी स्वच्छ तथा अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है।
जलवायु और व्यापार- जलवायु की विभिन्नता के अनुसार ही विभिन्न प्रदेशों में मानव की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं और उनको पूरा करने के लिए वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव पड़ती है। जलवायु पर ही कृषि पदार्थ, वन पदार्थ तथा पशुपदार्थों का उत्पादन एवं उपलब्धता निर्भर रहती है। अतः अनुकूल जलवायु में ये वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में पैदा होती हैं और अन्य क्षेत्रों में इनकी कमी रहती है। इस प्रकार प्रचुरता वाले क्षेत्रों में अभाव वाले क्षेत्रों में उन वस्तुओं का निर्यात कर दिया जाता है। गंगा की निचली घाटी में जूट के व्यापार का विश्व में एकाधिकार का श्रेय जलवायु को ही है। यूरोप और अमरीका के देश अपनी चाय और कॉफी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उष्ण कटिबन्ध आर्द्र प्रदेशों पर ही आश्रित हैं। इसी प्रकार जलवायु का पशुजन्य पदार्थों पर भी प्रभाव पड़ता है।
जलवायु और मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास- मानव शरीर और मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस कुछ प्रदेशों के निवासी शारीरिक और मानसिक शक्ति में अधिक बढ़े-चढ़े हैं और अनेक देशों पर अधिकार जमाए हुए हैं, जबकि कुछ देशों के निवासी शारीरिक और मानसिक शक्ति की दृष्टि से क्षीण और दुर्बल हैं। साधारण गर्म तथा शीतोष्ण जलवायु मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की दृष्टि से सशक्त बनाती है। इसके विपरीत, उष्ण और आर्द्र जलवायु न केवल मनुष्य के स्नायुओं को शिथिल बना देती है, किन्तु उनको कई रोगों का विशेषकर मलेरिया, पेचिश तथा अन्य प्रकार के रोगों का शिकार बना देती है। शारीरिक कार्य के लिए आदर्श तापमान दिनरात औसत तापमान) 18° सेण्टीग्रेड माना गया है। मानसिक कार्य के लिए 5° सेण्टीग्रेड तापमान उपयुक्त माना गया है। नम जलवायु के साथ 32° सेण्टीग्रेड की गर्मी अथवा शुष्क जलवायु मनुष्य को दुर्बल बना देती है।
जलवायु और मनुष्य का जीवन स्तर एवं आवास- जलवायु का प्रभाव मनुष्य के रहनसहन एवं आवास पर भी पड़ता है। मनुष्य का भोजन और वस्त्र जलवायु पर निर्भर होते हैं। उष्ण प्रदेशों में हल्के और कम मात्रा में भोजन, वस्त्र एवं खुले आवास की आवश्यकता होती है, किन्तु ठण्डे प्रदेशों में शरीर में गर्मी और शक्ति बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में भोजन एवं ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भवन भी ठण्ड से सुरक्षा हेतु प्रायः बन्द होते हैं अथवा यन्त्रों से ताप ऊँचा बनाए रखा जाता है। इसी भाँति अधिक उष्णता प्राप्ति के लिए शीतोष्ण कटिबन्धीय देशों में माँस, मदिरा, चाय, कॉफी, मक्खन, मछली, आदि अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि भारत जैसे उष्ण देश में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है।
जलवायु और जनसंख्या- जनसंख्या के वितरण में जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्म और आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश के निवासियों की प्रजनन शक्ति, शीत एवं शीतोष्ण प्रदेशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक होती है, इसी कारण उष्ण प्रदेशों में सन्तुलित आर्थिक विकास हेतु परिवार नियोजन पर जोर दिया जाता है। मानव उन्हीं भागों में रहना पसन्द करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए तथा उद्योग-धन्घों के लिए अनुकूल होती है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिण-पूर्वी एशिया, मध्य और उत्तरपश्चिमी यूरोप और उत्तर-पूर्वी संयुक्त राज्य अमरीका में निवास करती है। दक्षिण-पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु के कारण प्राचीन काल से ही जनसंख्या अन्य सब भागों की अपेक्षा अधिक रही है।
प्राकृतिक वनस्पति
प्राकृतिक वनस्पति प्रधानतः जलवायु पर निर्भर करती है। अतः इसका मनुष्य के आर्थिक विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वह परोक्ष रूप में जलवायु का ही प्रभाव है। प्राकृतिक वनस्पति के अन्तर्गत वे पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, समुद्री पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो स्वतः ही उग आते हैं। जैसी जलवायु होगी उसी के अनुरूप विविध प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, आदि पाए जाते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति और पशुपालन- वन प्रदेशों तथा घास के मैदानों में चारे की प्रचुरता होती है, फलतः वहाँ पशुपालन व्यवसाय खूब उन्नति करता है। भेड़, बकरियाँ, गाय, आदि पालकर दूध, मक्खन, माँस, , आदि प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे मनुष्य को भोजन तथा वस्त्र की प्राप्ति होती है। अधिकांश पूर्व के घास के मैदानों में अब कृषि होती है, अतः वहाँ कृषि एवं पशुपालन दोनों का ही आधुनिक तकनीक से पर्याप्त विकास हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति और कृषि- वन प्रदेश कृषि कार्य के लिए आर्थिक दृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे अपनी उपस्थिति से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक हैं। वनों की अधिकता से वर्षा अधिक होती है, वन वर्षामें बाढ़ों की भयंकरता को कम करके कृषि को नष्ट होने से बचा लेते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वनों में वृक्षों की पत्तियों के सड़नेगलने से वहाँ की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है जो पानी के साथ बहकर खेतों में पहुंच जाती है।
प्राकृतिक वनस्पति और उद्योग- वनों तथा घास के मैदानों से अनेक प्रकार के कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जिन पर अनेक कुटीर तथा निर्माणी उद्योग निर्भर करते हैं। वनों से कागज की लुग्दी, नकली रेशम की लुग्दी, तारपीन का तेल, गोंदलाख, रबड़, इत्यादि अनेक कच्चे पदार्थ मिलते हैं। कागज उद्योग, दियासलाई अनेक उद्योगों का विकास प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर करता है। इसी भाँति अनेक खाद्य पदार्थ, फल व मेवे के वृक्ष वनों में पाए जाते हैं। जैसे- वृक्षों से भाँतिभाँति के फल (केले, अंजीर, आम, अनन्नास) प्राप्त होते हैं। अखरोट, काजू, बादाम, आदि भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। वनों से विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भी मिलती हैं।
जीव-जंतु
जीव-जन्तु भी मनुष्य की आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाओं को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं-
जीव-जन्तु और कृषि- कुछ पालतू पशु जैसे-गाय, बैल, भैस, ऊँट, घोड़े, आदि कृषि कार्य में प्रयुक्त होते हैं। भारत में तो कृषि प्रायः बैलों पर ही निर्भर रही है, अन्य देशों में घोड़े, ऊँट, भैसे, आदि भी खेती के काम में प्रयोग किए जाते हैं, कृषि कार्य के लिए पशुओं से अनेक प्रकार की खादें भी प्राप्त होती हैं। छोटे-छोटे जीवजन्तु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं यहाँ तक कि भूमि को पोला करने तथा फसल के वृद्धि हेतु सेचन क्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं। डेयरी व्यवसाय पूरी तरह गाय व भैस पर ही निर्भर है।
जीव-जन्तु और परिवहन- अल्प विकसित एवं विकासशील प्रदेशों में परिवहन के क्षेत्र में आज भी पशुओं का महत्व अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में वैल, भैसे, घोड़े, खच्चर, ऊँट, याक, रेण्डियर गाड़ियाँ तथा बोझा ढोते हैं। हाथी बहुत शान की सवारी समझा जाता है। मरुभूमि की प्रमुख सवारी ऊँट है जिसे मरुस्थल का जहाज (Ship of Desert) कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात एवं परिवहन का सारा भार याक, लामा, आदि पशुओं पर है। अब विशेष प्रकार के शक्तिशाली वाहनों एवं घुमावदार मार्गों से पर्वतों की परिवहन व्यवस्था में सुधार आया है।
जीवजन्तु और उद्योग- गाय व भैस के दूध से डेयरी उद्योग पनपता है। मछली पकड़ना काफी पुराना उद्यम है, किन्तु आज भी इसका स्थान महत्वपूर्ण है। इस पर कॉड, सामन और शार्क लिवर से तेल बनाने तथा मछलियाँ सुखाने का उद्योग विकसित किया गया है। मछली से खाद भी बनती है। पशुओं से , बाल व फर प्राप्त करके ऊनी वस्त्र के कारखाने चलाए जाते हैं। रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करके रेशमी वस्त्र उद्योग चलता है। पशुओं की खालों से जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएँ बनायी जाती हैं। पक्षियों से माँस तो मिलता ही है, इनके पंखों से सजावट की वस्तुएँ भी तैयार की जाती हैं।
जीव-जन्तु और मनुष्य का रहनसहन- जीव जन्तुओं से मनुष्य के भोजन और वस्त्र की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। गाय, भैस, बकरी, भेड़, रेण्डियर से मानव को पौष्टिक दूध प्राप्त होता है। इनका माँस खाया जाता है। मछली से भी पौष्टिक भोजन मिलता है। अनेक जंगली पशुओं का शिकार करके उनका माँस खाया जाता है। खाल तथा समूर से वस्त्र बनाए जाते हैं। भेड़, बकरी, याक, लामा, इत्यादि जीवों के बाल(ऊन) से भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
खनिज संसाधन
यदि कहा जाए कि “मानव के विकास और प्रगति के इतिहास में खनिज पदार्थों का अटूट सम्बन्ध रहा है” तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाषाण ” (Stone Age), ताम्र युग (Bronze Age), लौह युग (Iron Age), इस्पात युग (Steel Age), अणु युग (Atomic Age) आदि शब्द मानव उत्थान की विभिन्न सीढ़ियों में खनिज पदार्थों का महत्व हैं। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, त्यों-त्यों उसने अपने व्यवहार में आने वाले खनिज पदार्थों में भी परिवर्तन किया। वर्तमान युग में लोहे और इस्पात के उपयोग के साथ खनिज पदार्थों निकिल, वैनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, आदि का उपयोग होता है। इस सम्वन्ध में व्हाइट और रैनर के शब्द उल्लेखनीय हैं। वे कहते हैं, “आधुनिक मनुष्य जिन औजारों और यन्त्रों का उपयोग करता है, वे सब उन खनिज पदार्थों द्वारा बने हैं जो केवल पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाते हैं।” धातु खनिजों और जैविक ईधनों के अभाव में आधुनिक मानव की दिशा प्रस्तुर (पाषाण) युग के अपने पुरखों से अधिक अच्छी नहीं हो सकती वर्तमान सभ्यता खनिज संसाधनों के बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग पर टिकी हुई है। सीमित खनिजों की आयु लम्वी करने हेतु अनेक प्रकार के प्लास्टिक, सेल्यूलोज, नाइलोन, फाइबर एवं फाइवर ग्लास जैसे टिकाऊ स्थानापन्न ढूंढे जा रहे हैं, फिर भी खनिजों का उपयोग अनिवार्य एवं विशेष महत्वपूर्ण बना हुआ है। खनन क्षेत्रों का आवासीय जीवन खनिज का आर्थिक उपलब्धता पर निर्भर करता है, अतः इनका विकास भी शीघ्रता से होता है। जिन देशों में विकास में महत्वपूर्ण खनिज कोयला, लोहा, बाक्साइट, मैंगनीज, ताँबा, सीसा, जस्ता आदि का अभाव है वहाँ ऐसे खनिजों का आयात अनिवार्य हो जाता है, तभी औद्योगिक विकास सम्भव है। जापान, संयुक्त राज्य, ब्रिटेन जैसे देशों को भी ऐसे आयात करने पड़ते हैं। अतः खनिजों में अन्तनिर्भरता अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं, वहाँ मानव का प्रभाव बड़ी शीघ्रता से बढ़ता है, जिससे उसकी समाप्ति पर वह उजड़ जाते हैं। मानव अन्यत्र चला जाता है और वह क्षेत्र दरिद्र होता जाता है।
मानव और पर्यावरण का सम्बन्ध और सामंजस्य
अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव का सम्बन्ध व सामंजस्य अत्यन्त प्राचीनकाल से चला रहा है जबकि वह पत्थर युग में था। इस युग में मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाने, प्रकृतिदत्त वस्तुओं का भोजन के रूप में उपयोग करने, पत्थर को कांट-छाँटकर, घिसकर औजार बनाने, जंगली पशुओं को पालतू बनाने, जादू, आदि पर विश्वास करने और सामूहिक रूप से सुरक्षा आदि करने के रूप में मनुष्य ने अपने सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देने में योग दिया है। तभी से मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाता रहा है, किन्तु यह परिवर्तन अत्यन्त थोड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति की आधारभूत क्रियाएँ बिल्कुल नहीं बदली हैं। मनुष्य ने विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और आर्थिक क्रियाओं में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए हैं। फलत: अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ सहसम्बन्धित रहकर सामंजस्य करने की रीतियों का बड़ा प्रसार हुआ है। इस प्रकार के सम्बन्धों सामंजस्यों को प्रधानतः तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक।
आर्थिक सामंजस्य व सम्बन्ध
इस प्रकार का मुकाबला समाज द्वारा कार्यप्रतिमानों के रूप में किया जाता है। मनुष्य कौन-सा कार्य करता है यह उसकी इच्छाओं, विचारों और कुशलता पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर यह बात प्राकृतिक पर्यावरण से मिलने वाली सम्पदा द्वारा प्रभावित होती है। आर्थिक सम्बन्ध मुख्यतः चार श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं-
- प्राथमिक उद्यम- जिनमें मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ना तथा खानें खोदना सम्मिलित किया जाता है। इन कार्यों में प्रकृति से सीधे ही वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य वस्तु उपयोगिता उत्पन्न करता है।
- उत्पादक उद्योग- जिनके अन्तर्गत मनुष्य भूमि से उन वस्तुओं को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कृषि, पशुपालन तथा रेशम के कीड़े पालकर उनका आपसी सम्बन्ध स्थापित कर अधिक उत्पादन प्राप्त करना।
- निर्माण उद्योग- जिनके अन्तर्गत खदानों अथवा कृषि से प्राप्त वस्तुओं को पिघलाकर, साफसुथरा कर उनसे वस्तुएँ निर्मित की जाती हैं। इस प्रकार के उद्योग से स्वरूप उपयोगिता प्राप्त की जाती है।
- व्यापारिक व सहायक उद्यम– जिनमें यातायात, एकत्रीकरण, विनिमय संचार तन्त्र एवं अर्थप्रवन्धन की क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं। इनके द्वारा स्थान और समय की उपयोगिता प्राप्त की जाती हैं। इनके साथसाथ मनुष्य की अन्य व्यावसायिक सेवाएँ शिक्षा, कानून, डाक्टरी, आदि एवं व्यक्तिगत सेवाएँ (घरेलू कार्य, सफाई का कार्य, आदि) भी सम्मिलित की जाती हैं।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध
मानव समाज अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ विशेष प्रकार से सम्वन्ध एवं सामंजस्य भी स्थापित करता है। इसके अन्तर्गत जनसंख्या का घनत्व, भूमि पर स्वामित्व, सामाजिक वर्ग, परिवार, समाज सम्बन्ध, आदि बातें सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार के सम्वन्धों से ही मनुष्य के व्यवहार एवं उसकी आदतें भी निर्धारित होती जाती हैं। उसका स्थायी जीवन या घुमक्कड़ जीवन, उसके वस्त्र, भोजन, घर, आचार-विचार, धार्मिक विश्वास एवं आस्थाएँ, कला, आदि बातों पर भी प्राकृतिक पर्यावरण के विविध तत्वों का सुस्पष्ट प्रभाव पड़ता है।
राजनितिक सम्बन्ध व् उनका सामंजस्य
मानव समाज की सुव्यवस्था हेतु प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों के प्रभावी स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के लिए सम्बन्ध व सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। इस क्रिया के अन्तर्गत, स्थानीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, विदेश नीति, क्षेत्रीय सन्तुलन व सम्वन्ध स्वरूप, सैन्य नीतियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानने, आदि का निर्धारण सम्मिलित होते हैं।