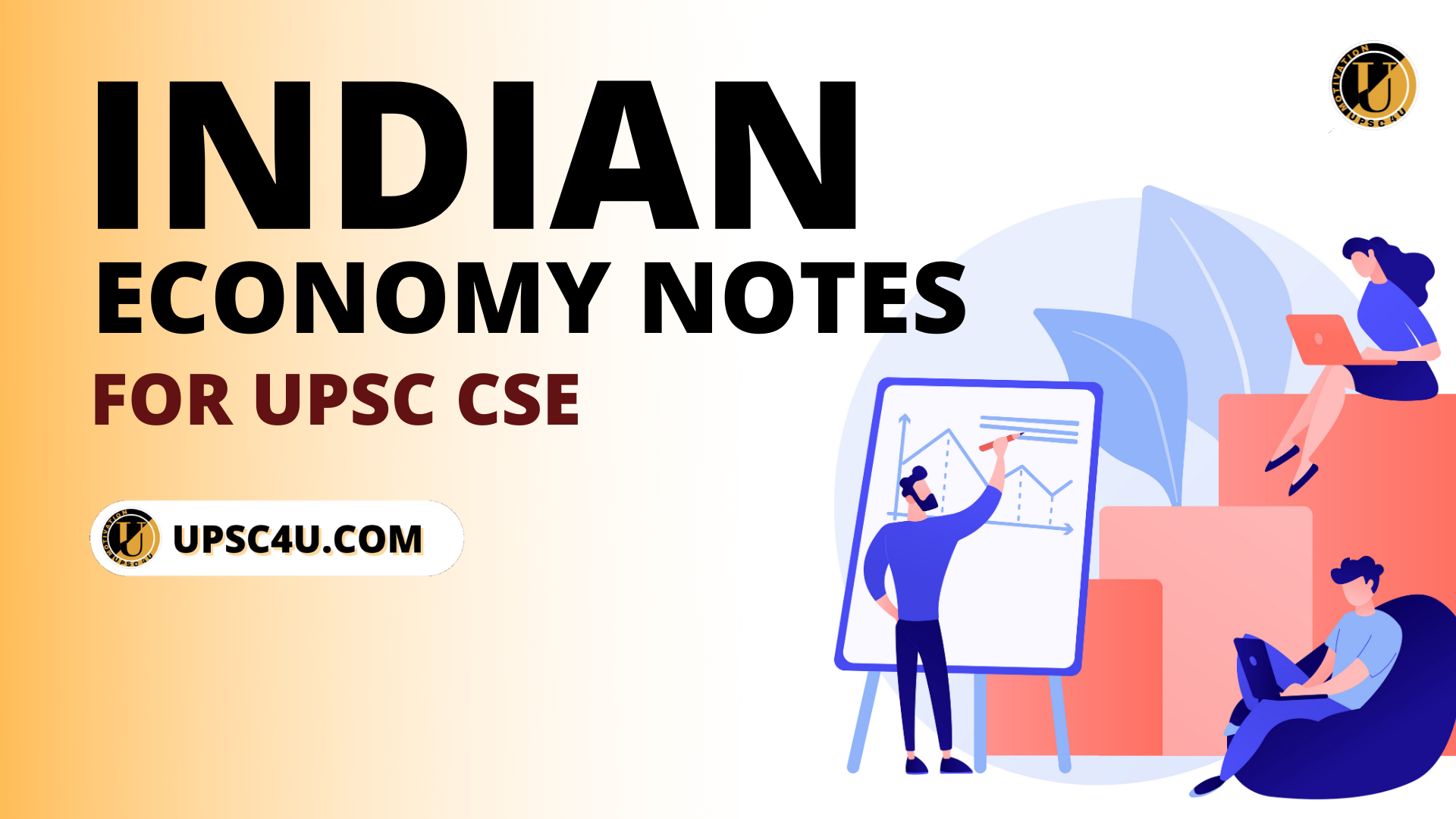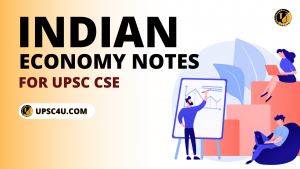बाजार का अर्थ एवं वर्गीकरण
बाजार का अर्थ:-
बोलचाल की आम भाषा में हम यह कह सकते हैं कि बाजार का आशय किसी ऐसे स्थान विशेष से हैं जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता इकठ्ठा होते हैं। तथा वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं।
परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ इससे अलग है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द का आशय उस सम्पूर्ण क्षेत्र से है। जहां तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं तथा उनमे वस्तुओं के खरीदने और बेचने की स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है जिसके कारण वस्तु के मूल्य में एकरूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसे बाजार कहते है। अर्थशास्त्र में बाजार का वर्गीकरण:-
निम्नलिखित दृष्टिकोण से किया जाता है।
1. क्षेत्र की दृष्टि से
2. समय की दृष्टि से
3. कार्यों की दृष्टि से
4. प्रतियोगिता की दृष्टि से
वैधानिकता की दृष्टि से
दोस्तों यहाँ पर हम केवल क्षेत्र की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे।
1. क्षेत्र की दृष्टि से:- क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण का आधार है कि वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं यह चार प्रकार का होता है।
1.स्थानीय बाजार:- जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं तब उस वस्तु का बाजार स्थानीय होता है।
स्थानीय बाजार में भारी एवं कम मूल्य वाली वस्तुएं तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे ईट दूध और सब्जी आदि आते है।
2. प्रादेशिक बाजार:- जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता केवल एक ही प्रदेश तक पाये जाते है। तो ऐसा बाजार प्रदेशिक बाजार होता है।
जैसे:- राजस्थान की पगड़ी, और लाख की चूड़ियां केवल राजस्थान में ही इनका प्रयोग किया जाता है। यह अन्य राज्यों में नहीं पाई जाती।
3. राष्ट्रीय बाजार:- किसी वस्तु का क्रय विक्रय केवल उस राष्ट्र तक ही सीमित हो जिस राष्ट्र में वह वस्तु बनाई जाती हैं। तब वस्तु का बाजार राष्ट्रीय होता है।
जैसे:- जवाहर कट धोतियां
4. अंतरराष्ट्रीय बाजार:- जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के अलग अलग राष्ट्र से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। या किसी वस्तु की मांग देश या विदेश में हो तो उस वस्तु का बाजार अंतराष्ट्रीय होता है।
जैसे:- सोना, चांदी, चाय, गेहूं
2. समय की दृष्टि से:- प्रोफेसर मार्शल ने समय के अनुसार बाजार को 4 वर्गों में बांटा है
1. अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार:- जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता तब ऐसे बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं।
जैसे:- शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुएँ दूध, सब्जी मछली आदि। इनका भंडारण ज्यादा समय तक नही किया जा सकता। ये दैनिक बाजार के अंतर्गत आते है।
2. अल्पकालीन बाजार:- अल्पकालीन बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन के लिए कुछ समय मिलता है। किंतु यहां पर्याप्त नहीं होता। पूर्ति में मांग के अनुसार कुछ सीमा तक घटाया या बढ़ाया जाता है। किंतु यह पर्याप्त नहीं है।
3. दीर्घकालीन बाजार:- जब किसी वस्तु का बाजार कई वर्षों के लंबे समय के लिए होता है तो उसे दीर्घ कालीन बाजार कहते हैं।
अति दीर्घकालीन बाजार:- इस बाजार में उत्पादकों को पूर्ति बढ़ाने के लिए इतना लंबा समय मिल जाता है कि उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव रुचि फैशन आदि के अनुरूप उत्पादन कर सकता है।
3. बिक्री की दृष्टि से
1. सामान्य अथवा मिश्रित बाजार:- मिश्रित बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें अनेक एवं विविध प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यहां क्रेताओं की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है।
2. विशिष्ट बाजार:- यह वह बाजार होते हैं जहाँ किसी वस्तु विशेष का क्रय-विक्रय होता है।
जैसा:- सराफा बाजार, बजाज बाजार, दाल मंडी, गुड मंडी आदि
3. नमूने द्वारा बिक्री का बाजार:- ऐसे बाजार में विक्रेता को अपना संपूर्ण माल कहीं ले जाना नहीं पड़ता है वह माल को देखकर सौदा तय करते हैं सौदा तय होने पर माल गोदाम से भिजवा देते हैं। लोग अपने घर बैठे ही नमूना देखकर उस में चुनाव करके बहुत सा सामान मंगा लेता है।
4. ग्रेड द्वारा विक्री का बाजार:- इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं की बिक्री उनके विशेष नाम अथवा ग्रेड द्वारा होती है खरीददार को ना तो वस्तुओं के नमूने दिखाने पढ़ते हैं और ना ही क्रेता को कुछ बताना पड़ता है।
जैसे:- फिलिप्स रेडियो
5. निरीक्षण बाजार:- इस बाजार में निरीक्षण करके उसकी कीमत लगाई जाती है।
जैसे:- गाय, बैल, बकरी, घोड़े आदि
6. ट्रेड मार्का बिक्री बाजार:- बहुत से व्यापारी के माल व्यापार चिन्ह के आधार पर बिकते हैं। उसे ट्रेड मार्का बिक्री बाजार कहते है।
जैसे:- ऊषा मशीन, बिरला सीमेण्ट आदि।
भारत में पत्र-मुद्रा का चलन तथा उसके लाभ, हानि
मुद्रा का अर्थ – कागज पर छपी मुद्रा को पत्र मुद्रा कहते हैं। यह कागज पर छपी निश्चित राशि के भुगतान का प्रतिज्ञा पत्र है जो किसी सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी मुहर लगाकर जारी किया जाता है।
भारत में पत्र मुद्रा का चलन
- 1861 के पूर्व भारत में पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि ने विभिन्न देवनागरी लिपि में कागजी मुद्रा निर्गत की। सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ।
- 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया था। और जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट 1938 में जारी किए गए। इसके बाद 1947 में जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंह के चित्र वाले पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। महात्मा गांधी के चित्र वाले ₹500 के नोट 1987 में आये।
- 1996 से सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंघो के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए। जो अब तक चल रहे है।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वाई. वी. रेड्डी ने अपने कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्मित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छापना शुरू कर दिया।
- पहला निर्मित नोट ₹1 का था जो सन् 1949 में चलन में आया जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा था।
- ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित होता है। जिस पर वित्त सचिव के होते हैं। जबकि ₹1 से अधिक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा होता है।
- इन नोटों पर हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है।
- रुपए के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की है।
- देवनगरी के रोमन अक्षर R से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह (₹) को रुपए के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारत अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला विश्व का पांचवा देश बन गया।
पत्र मुद्रा के लाभ
पत्र मुद्रा के लाभ निम्न है-
- पत्र मुद्रा बहुत हल्की होती है। सुविधा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में ले जाया जा सकता है। इस कारण पत्र मुद्रा में वहनीयता का गुण पाया जाता है।
- पत्र मुद्रा के चलन से बहुमूल्य धातु की बचत होती है। इस धातु का प्रयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता है।
- पत्र मुद्रा में लोचता पाई जाती है पत्र मुद्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- पत्र मुद्रा के चलन से धातु के सिक्के चलन में नहीं होते हैं। या कम होते हैं। इससे सिक्कों की घिसावट बचती है।
- पत्र मुद्रा को गिनने तथा परखने में सुविधा होती है। इस प्रकार पत्र मुद्रा उपयोग में सुविधाजनक है।
- पत्र मुद्रा अधिक सुरक्षित होती है। चोरी की स्थिति में चोरी किए गए नोटों को नंबरों की सहायता से पहचाना जा सकता है। पत्र मुद्रा को छुपा कर रखने में भी सुविधा रहती है।
- पत्र मुद्रा को संकट कालीन मित्र माना जाता है। सरकार युद्ध अथवा विकास कार्यों के लिए पत्र मुद्रा छापकर संकट को दूर कर सकती है।
पत्र मुद्रा के दोष
- पत्र मुद्रा के प्रयोग का क्षेत्र देश की सीमाओं तक सीमित होता है। देश की सीमाओं से बाहर उसका कुछ भी मूल्य नहीं होता है।
- पत्र मुद्रा का जीवनकाल कम होता है। कागजी नोट हस्तांतरण होने से शीघ्र ही गन्दे व् खराब हो जाते हैं।
- पत्र मुद्रा में मुद्रा स्फीति का भय रहता है। मुद्रा या प्रसार स्फीति से देश में महंगाई व बेरोजगारी बढ़ जाती है। सट्टा चोर बाजारी व भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है।
- पत्र मुद्रा का स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता है। पत्र मुद्रा सरकार की साख पर चलती है। पत्र मुद्रा का मूल्य सरकार की मान्यता पर निर्भर करता है। अन्यथा वह कागज के टुकड़े मात्र होते हैं।