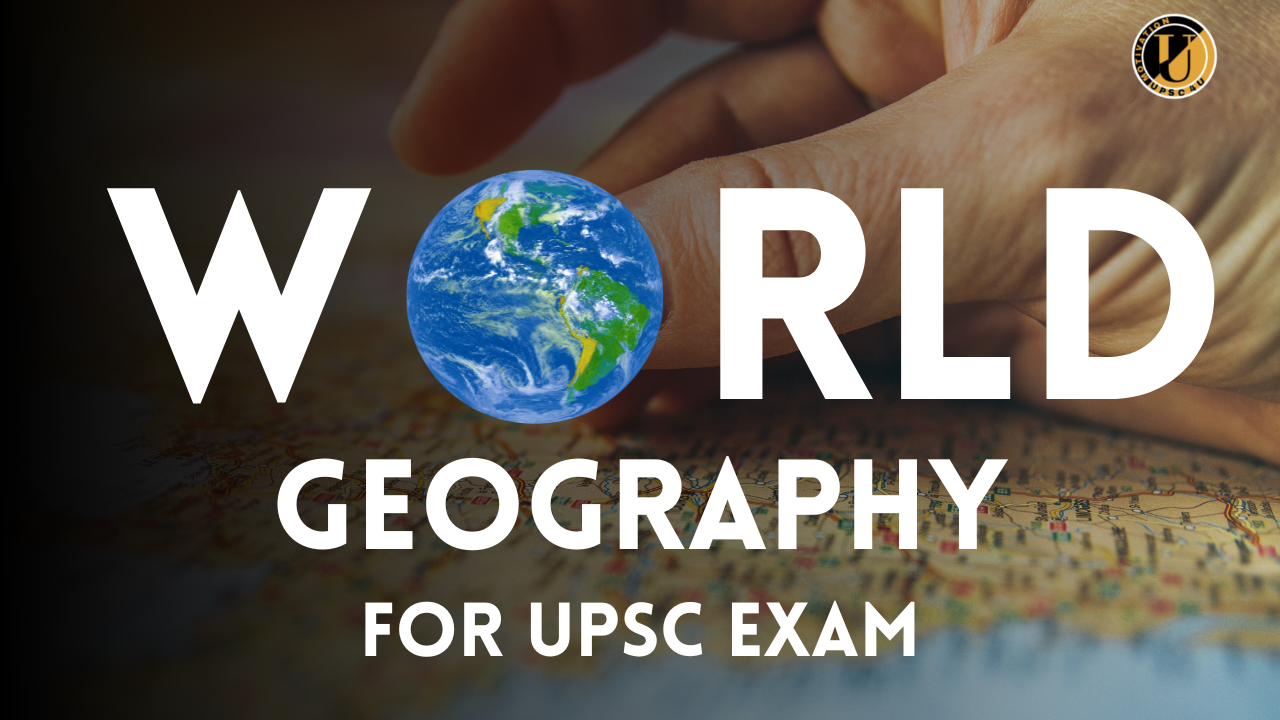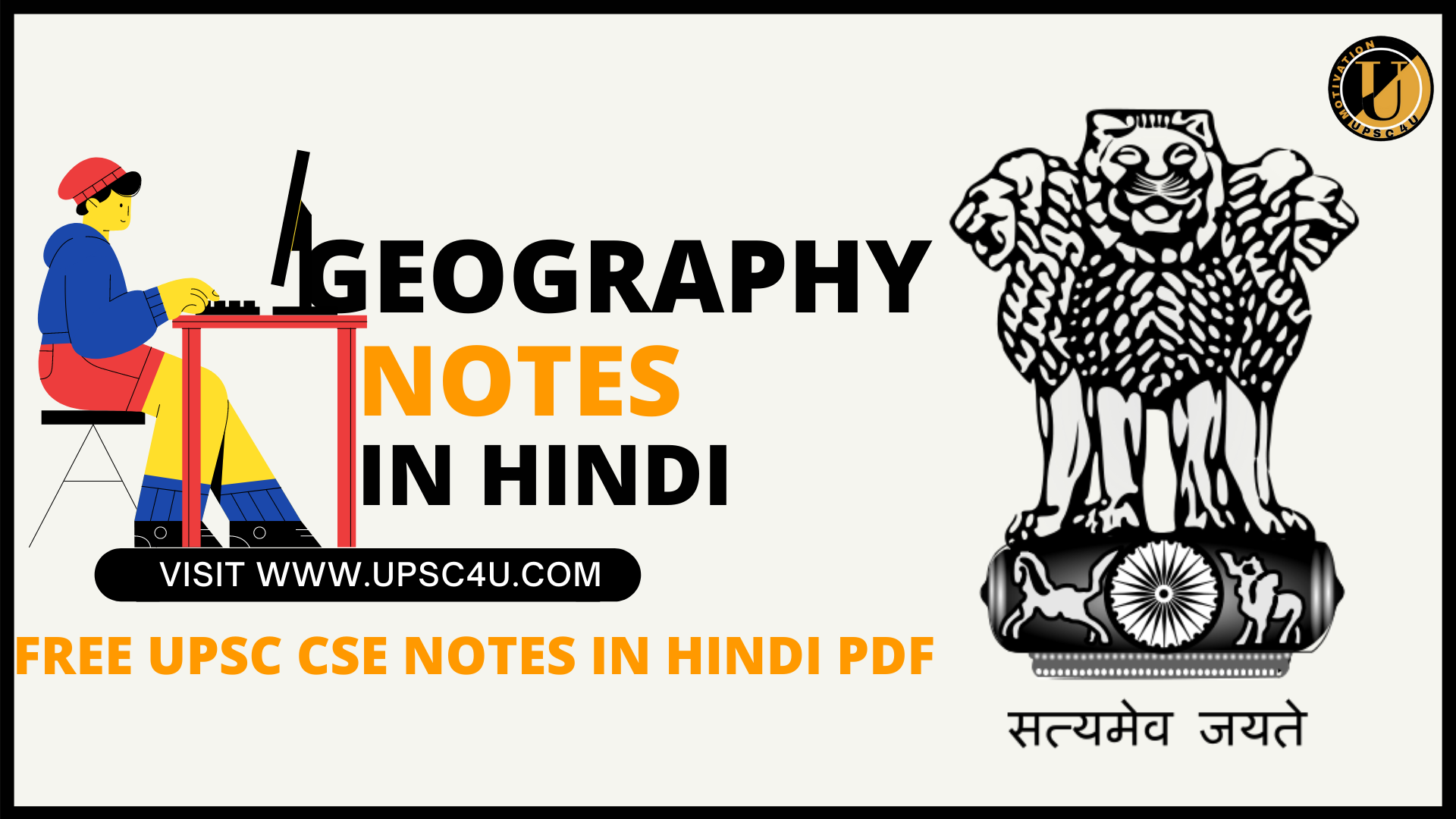विदेश व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं और वितीय संसाधनों का अंतर्देशीय प्रवाह शामिल हैं। विदेश व्यापार द्वारा विदेशी पूंजी और विशेषज्ञों की मदद से देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। यह एक देश को विदेशी विनिमय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। आयात और निर्यात अक्सर दुर्लभ या बहुतायत में प्राप्त वस्तु की कीमतों में भारी परिवर्तन (उतार-चढ़ाव) को कम करता है। व्यापार एक देश की उपभोग क्षमताओं का विस्तार करता है, और दुर्लभ संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है और उत्पाद के लिए विश्वभर के बाजार तक विस्तार देता है जो संवृद्धि के लिए आवश्यक है। अंततः विदेश व्यापार नीति संवृद्धि एवं विकास को बढ़ाने में सहायक होती है।
विदेशी व्यापार की रूपरेखा
भारत के विश्व के भौगोलिक प्रदेशों और बड़े व्यापारिक समूहों के साथ व्यापारिक संबंध हैं जिसमें पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्ववर्ती सोवियत संघ (रूस) और बाल्टिक राज्य, एशिया, ओसीनिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका आते हैं। 1950-51 में भारत का कुल विदेश व्यापार (आयात एवं निर्यात) ₹ 1214 करोड़ था। तब से, यह समय-समय पर मंदी के साथ लगातार वृद्धि करने का साक्षी है।
जबकि भारत की व्यापार संवृद्धि का विश्व व्यापार बढ़ोतरी के साथ एक मजबूत सह-संबंध है, यह विश्व व्यापार संवृद्धि की तुलना में ऊंचा रहा है, विशेष रूप से, 1990 के सुधार का अनुसरण करने पर और वर्ष 2003 के बाद की दो समयावधियों में।
संगठन
व्यापार संगठन का दो श्रेणियों के तहत् अध्ययन किया जा सकता है: आयात और निर्यात। (हालांकि तकनीकी रूप से, व्यापार में सेवाओं और वित्तीय संसाधनों को शामिल किया जाता है, भारत में व्यापार से संबंधित आंकड़ों में सामान्यतः केवल वस्तुओं पर सूचना शामिल होती है)।
आयात
आयात को अम्बारी आयात (Bulk Imports) और गैर-अम्बारी आयात (Non bulk Imports) में वर्गीकृत किया जा सकता है: अम्बारी आयात मदों में शामिल हैं-
- पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट (पीओएल)
- नॉन-पीओएल जैसी उपभोग वस्तुएं (खाद्य तेल, चीनी इत्यादि), उर्वरक और लौह एवं इस्पात।
गैर-अम्बारी आयात मदों में शामिल हैं-
- पूंजी वस्तुएं जिनमें धातुएं, मशीनी औजार, इलेक्ट्रिक एवं गैर-इलेक्ट्रिक मशीनरी
- मोती, बहुमूल्य और अल्प मूल्य पत्थर
- अन्य
अभी हाल तक, भारत के आयात की संरचना देश द्वारा द्वितीय नियोजन के दौरान 1956 की शुरुआत में अपनाई गई औद्योगीकरण की रणनीति को प्रतिबिम्बित करती है। इस समय बड़ी मात्रा में मशीनरी, परिवहन उपकरण, यंत्र एवं उपकरण इत्यादि पूंजीगत सामान का आयात हुआ। लौह एवं इस्पात, पेट्रोलियम, रसायनों इत्यादि के औद्योगिक विकास हेतु आगतों का भी आयात किया गया। इन वस्तुओं के आयात ने औद्योगिक विकास को प्रारंभ करने में मदद की और कई वर्षों के लिए इसके विस्तार में भी मदद की। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि के कारण घरेलू उत्पादन में आयी कमी को पूरा करने के लिए भी उपभोक्ता वस्तुओं जिसमें बड़ी मात्रा में अनाज एवं इनके बने उत्पाद भी आयात किए गए।
निर्यात
भारत के निर्यात मोटे तौर पर चार वगों में विभक्त किये जाते हैं-
- कृषि और सम्बंधित उत्पाद जिसमें कॉफी, चाय, खल (oil Cakes), तम्बाकू, काजू, गरम मसाले, चीनी, कच्ची रुई, चावल, मछली और मछती से बनी वस्तुएं, गोश्त और गोश्त से बनी वस्तुएं, वनस्पति तेल, फल, सब्जियां और दालें।
- अयस्कों और खनिजों में मैंगनीज अयस्क, अभ्रक और कच्चा लोहा शामिल किए जाते हैं।
- निर्मित वस्तुओं में सूती वस्त्र और सिले-सिलाए कपड़े, पटसन की बनी वस्तुएं, चमड़ा और जुटे., हैंडीक्राफ्ट्स, हैण्डलूम, कुटीर एवं क्राफ्ट वस्तुएं, मोटी और बहुमूल्य पत्थर, रसायन, इंजीनियरिंग वस्तुएं तथा लौह एवं इस्पात शामिल किए जाते हैं।
- खनिज, ईधन और लुब्रिकेन्ट्स।
भारत ने धीरे-धीरे स्वतंत्रता पूर्व मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पाद निर्यात करने वाले देश से वर्तमान में निर्मित उत्पादों के निर्यातक के रूप में स्वयं को परिवर्तित किया है। अर्थव्यवस्था में हुए विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए, निर्यात की जाने वाली मदों में परम्परागत से गैर-परम्परागत मदों की ओर परिवर्तन हुआ।
[table id=21 /]
रुपये में निर्यात ने वृद्धि के चलन का प्रदर्शन किया और सालों में इसके आधार का विविधिकरण किया। जबकि साल-दर-साल परिवर्तन होता रहा, वस्तुएं जिनकी विगत् कुछ वर्षों में निर्यात में वृद्धि परिलक्षित हुई, उनमें कृषि और सम्बद्ध उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, हीरे-जवाहरात, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग समान, इलेक्ट्रॉनिक समान, कपडा, पेट्रोलियम उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
वर्तमान में हमारे निर्यात की मदों में टेक्सटाइल (कारऐट, हस्तकला, कपास), हीरे-जवाहरात, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, (विशेष रूप से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद) कृषि एवं सम्बद्ध उत्पाद,चमड़ा एवं चमड़ा निर्मित वस्तुएं (विशेष रूप से जूते-चप्पल), वनीकरण, इंजीनियरिंग सामान, निर्मित कपड़े, फूलों के उत्पाद तथा समुद्री उत्पाद शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में नए कदम बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेहद व्यापक निर्यात क्षमता के साथ एक संभावित क्षेत्र के तौर पर उभर रहा है।
आयात-निर्यात नीति 1997-2002: वर्ष 1997-2002 के लिए पंचवर्षीय आयात-निर्यात नीति की घोषणा 31 मार्च, 1997 को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने की। आयात-निर्यात नीति के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा की गई है-
- विश्व बाजार के विस्तार का लाभ उठाना एवं इसके लिए अर्थव्यवस्था में समुचित परिवर्तन लाना व उसे गत्यात्मकता प्रदान करना।
- उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, कलपुजों, उपभोग व पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सके।
- भारतीय कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पद्धी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी में उन्नयन करना, रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना एवं विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना।
- उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं समुचित कीमतों पर उपलब्ध करवाना।
नवीन आयात-निर्यात नीति के अनुकूल अधिक पारदर्शी व अल्प विवेकाधीन नीतियों को अपनाने व अनुकूल कार्यप्रणाली विकसित करने के प्रयास करने की भी घोषणा नवीन नीति में की गई है।
आयात-निर्यात (एक्जिम) नीति, 2002-07: विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजना को अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के गठन, वस्तु मूल्य जोखिमों के बचाव तथा लघु अवधि विदेशी वाणिज्यिक उधारों को जुटाने की अनुमति देकर मजबूत किया गया है। इस नीति ने एसईजेड इकाइयों द्वारा की गई उपसंविदा की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक सरलीकरण भी सुनिश्चित किया है। एसईजेड में तथा इसके आस-पास विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए,वियुत की उत्पादन तथा वितरण की इकाइयों की एसईजेड में स्थापना की अनुमति दे दी गई है।
विदेशी व्यापार निदेशालय, सीमाशुल्क तथा बैंकों की लेनदेन लागत को और कम करने के लिए एक्जिम नीति में प्रक्रियात्मक सरलीकरण किए गए हैं। एक्जिम नीति 2002-07 के अन्य मुख्य लक्षणों में निर्यातों के बाजार संवर्धन पर ध्यान देने के लिए आवश्यक समझी गई गतिविधियों को शामिल करने के लिए बाजार पहुंच पहल योजना के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना, निर्यातकों को एक सुविधाकारी माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्यातकों/व्यावसायियों से विदेश में इंडिया मिशनों में व्यापार केंद्र की स्थापना, पूर्वोत्तर, सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित इकाइयों को निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी तया बाजारों को विविध रूप देने के लिए अनुसरण हेतु फोकस सीआईएस सहित फोकस अफ्रीका का सूत्रपात करना शामिल है।
विदेशी व्यापार की दिशा
आजादी के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तुलनात्मक लागत लाभ स्थितियों के द्वारा निर्धारित न होकर ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों द्वारा निर्धारित थी। दूसरे शब्दों में, भारत किन देशों से आयात करेगा और कहां पर अपना माल बेचेगा, यह ब्रिटिश शासक अपने देश के हित में तय करते थे। यही कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और मित्र राष्ट्रों के साथ था। यही प्रवृत्ति आजादी के बाद कुछ वर्षों में भी देखने को मिलती है क्योंकि तब तक भारत की अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। उदाहरणार्थ, 1950-51 में भारत की निर्यात आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42 प्रतिशत था। उसी वर्ष भारत के आयात व्यय में उनका हिस्सा 39.1 प्रतिशत था। अन्य पूंजीवादी देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि और समाजवादी देशों जैसे सोवियत संघ, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि के साथ बेहद थोड़ा व्यापार था। जैसे-जैसे इन देशों के साथ राजनैतिक संबंधों का विकास हुआ वैसे-वैसे आर्थिक संबंध भी मजबूत होने लगे। इस प्रकार बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विकास करने के अवसर खुलने लगे। अब स्थिति काफी बदलचुकी है और 6 दशक के आयोजन के बाद व्यापारिक संबंध काफी बदल चुके हैं।

भारत के व्यापार भागीदार देशों को प्रमुख तौर पर पांच भागों में बांटा जा सकता है-
- आर्थिक विकास सहयोग संगठन: जिसमें यूरोपीय समुदाय, अमेरिका, कनाडा, जापान, इत्यादि शामिल हैं।
- तेल निर्यातक देशों का संगठन: जिसमें इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, इत्यादि शामिल हैं।
- पूर्वी यूरोप: जिसमें रूस प्रमुख राष्ट्र है।
- विकासशील राष्ट्र: जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबिया के विकासशील राष्ट्र शामिल हैं।
- पांचवां समूह अन्य राष्ट्रों का है।
भारतीय निर्यातों की चुनौतियां
भारत में कई निर्यात मदें उच्च आयात प्रवृति रखती हैं जो उनके प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में कमी करते हैं, विशेष रूप से तब जब रुपये की कीमत कमजोर होती है। उदाहरण के लिए, भारत का हीरा उद्योग कीमती एवं कम कीमती पत्थरों के आयात पर भारी धन खर्च करता है। मुद्रास्फीति भारतीय मुद्रा को कमजोर करने में योगदान करके स्थिति को और अधिक बदतर बना देती है।
हस्तांतरण की उच्च लागत एक अन्य बड़ी समस्या है। यह निर्यात उद्योग के लाभ को खा जाती है।
एक और सम्बद्ध कारक है जो भारतीय निर्यात में रुकावट डालता है और वह है निर्यात अवसंरचना की खराब स्थिति। उदाहरण के लिए, हमारे पत्तनों में निर्यात मदों के सुचारू परिवहन के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं मानकों का अभाव है।
भारत और अन्य विकासशील देशों से निर्यात को हस्तोत्साहित करने के लिए इन पर गैर-टेरिफ बाधाओं (श्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य मानक, एंटी डम्पिंग) का आरोपण आज भारतीय निर्यात क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली बेहद गंभीर चुनौती है।
प्रविधि पर केंद्रीकरण के परिणामस्वरूप निर्यात दिशाओं का अधिक प्रादेशिक विस्तार होगा और प्रादेशिक संवृद्धि उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न निर्यात चक्र का न्यूनीकरण करेगी।
भारत को नवोदित अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच द्वारा अपने निर्यात बाज़ार का विविधीकरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएं परिवर्तन के दौर में हैं। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए और इन बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए, विशेष तौर पर, क्योंकि, कम से कम कुछ समय के लिए, ये बाजार विकसित देशों के बाजारों की तरह प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं होंगे।
विदेश व्यापार नीति
जब भारत ने 1950 के दौरान नियोजन काल पर पोतारोहण किया, तो आयात प्रतिस्थापन भारत के व्यापार और औद्योगिक नीति के लिए मुख्य चुनौती थी। भारतीय नीति-निर्माताओं ने भारत की आर्थिक संवृद्धि के उत्प्रेरक के तौर पर विदेश व्यापार के विकल्प पर गंभीर रूप से विचार नहीं किया। इसका मुख्य कारण निर्यात आय अर्जन क्षमता के प्रति बेहद निराशाजनक दृष्टिकोण था। विशाल घरेलू बाजार के अस्तित्व ने आंतरिक उन्मुखता की ओर आवेशित होने का काम किया। नीति-निर्माताओं ने न केवल निर्यात क्षमताओं एवं संभावनाओं का अवमूल्यांकन किया अपितु स्वयं आयात प्रवृति के आयात प्रतिस्थापन प्रक्रिया को भी नकारा। हालांकि औद्योगिकीकरण की आंतरिक उन्मुखता प्रक्रिया ने 1956 और 1966 के बीच घरेलू औद्योगिक संवृद्धि की उच्च दर हासिल की, लेकिन इस प्रकार के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया की कई कमियां जल्द ही उजागर हो गई। पूरे तंत्र में अक्षमता फैल गई और अर्थव्यवस्था उच्च लागत की बढ़ती दर में तब्दील हो गई। एक समय पश्चात्, इसने प्रौद्योगिकीय विलम्ब को प्रवृत किया जिससे निर्यात निष्पादन में गिरावट आने लगी।
जबकि, समय के साथ, निर्यात के प्रति दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ, 1970 के दशक के अंत तक बड़ी संख्या में मदों का आयात प्रतिस्थापन भारत की विकास रणनीति का आधारभूत सिद्धांत रहा।
1980 के शुरुआत में, 1970 के अंत में आश्चर्यजनक निर्यात निष्पादन और 1980-82 की मंदी के सफलतापूर्वक अपक्षय ने, भारत की निर्यात क्षमताओं की स्थापना के संबंध में आशाजनक माहौल पैदा किया।
विदेश व्यापार को संसाधनों के दक्षतापूर्ण आवंटन के संचालक के तौर पर और तकनीक में वैश्विक उन्नयन का साधन माना गया।
1991 के बाद व्यापार नीति में आए बदलावों ने मात्रात्मक प्रतिबंधों की भूमिका को न्यून किया और तात्विक रूप से टैरिफ दरों में कमी की। भारत के व्यापार नीति के उदारीकरण ने भी विश्व व्यापार संगठन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित किया।
विदेश व्यापार नीति (2009-14)
भारत सरकार ने 2009-14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति की घोषणा 27 अगस्त, 2009 को की। 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 2014 तक वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों को दोगुना करने का लक्ष्य है। नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर दोगुना करना है।
व्यापार नीति की विशेषताएं–
- फोकस बाजार योजना का विस्तार: वैश्विक वित्तीय संकट के कारण मांग में गिरावट की समस्या के निदान के लिए इस नीति में फोकस बाजार योजना के अंतर्गत 26 नए बाजार शामिल किए गए हैं।
- फोकस बाजार योजना एवं फोकस उत्पाद योजना में प्रेरणाएं: फोकस बाजार योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रेरणाओं (या रियायतों) को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.0 प्रतिशत तथा फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रेरणाओं को 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।
- निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु योजना: एफटीपी (2009-14) में इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मूल रसायनों व औषधियों, वस्त्रों, प्लास्टिक, हस्तशिल्प तथा चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं को बिना सीमा शुल्क दिए, आयात करने की सुविधा दी गई है।
- डीईपीबी की समयावधि बढ़ाना: इयूटी इन्टाइटलमेंट पासबुक योजना (डीईपीबी) को जो निर्यात उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त आयातों पर प्रशुल्क दरों को निष्प्रभावी करती है।
- निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू): पहले निर्यात उन्मुख इकाइयों को यह छूट थी कि अपने उत्पादन का अधिकतम 75 प्रतिशत घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेच सकती है। एफटीपी में इस अधिकतम सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया।
- ईपीसीजी योजना के अधीन आवेदन पत्रों व ऋणमोचन पत्रों को सरल बना दिया गया है।
- कार्य संपादन लागतों को कम करने के लिए आयातित वस्तुओं को बंदरगाहों से सीधे उत्पादन स्थल ले जाने की सुविधा दी गई है।
- सरकार द्वारा उत्पादकों को यह छूट दी गई है कि वे उत्पाद शुल्क की अदायगी के बाद विनिर्माण अपशिष्ट का निपटान कर सकते हैं।
- शीघ्र कार्यवाही व निर्णय के लिए अधिकाधिक कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की जाएगी तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।
- परियोजना के निर्यातों एवं कई विनिर्मित उत्पादों को फोकस उत्पाद योजना के अधीन शामिल किया गया है।
- टेक्सटाइल्स (हथकरघा समेत) हैंडीफ्राफ्ट, कारपेट, चमड़ा, रत्न एवं जवाहरात, समुद्री उत्पाद एवं एसएमई जैसे निर्यात के श्रम गहन क्षेत्रों को 1 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर, 2009 तक 2 प्रतिशत की व्याज सहायता। बाद में इसे बढ़ाकर मार्च 2010 तक किया गया।
- विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना में दस्तकारी मदों का समावेशन।
- ऐसी सभी मदों के लिए डीईपीबी दरों की बहाली, जहां इन्हें नवंबर 2008 में घटाया गया तथा सितंबर 2008 से कतिपय मदों पर इयूटी ड्रा बैक की दरों में वृद्धि की गई।
- पेट्रोलियम उत्पादों तथा ऐसे उत्पादों को छोड़कर जहां वर्तमान दर 4 प्रतिशत से कम थी, सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क को घटाकर 4 प्रतिशत करना।
- प्रौद्योगिकी स्तरोन्यून निधि (टीयूएफ) के पिछले दावों को निपटाने हेतु टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए ₹ 1400 करोड़ की अतिरिक्त निधि का प्रावधान।
- मार्च 2010 तक बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को 95 प्रतिशत का परिवर्द्धित निर्यात क्रेडिट गारंटी (ईसीजीसी) कवर प्रदान करने हेतु समायोजन सहायता योजना का विस्तार।
- एसटीपीआई एवं ईओयू योजनाओं हेतु समापन खण्ड से संबंधित क्रमशः धारा 10क एवं 10ख का वित वर्ष 2010-11 के लिए विस्तार किया गया।
- फोकस बाजार योजना तथा बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओसियाना एवं सीआईएस देशों के उभरते बाजारों के निर्यात का विविधीकरण।
- सेवा कर से संबंधित उपाय जिनमें अन्य बातों के साथ शमिल हैं- निर्यात संबद्ध सेवाओं पर सेवाकर से छूट, जैसे-सड़क मार्ग से माल की दुलाई विदेशी एजेंटों को संदत कमीशन।
- मार्च 2011 के अंत तक इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, बुनियादी रसायनों, फार्मास्युटिकल्स, अपैरल्स एवं टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, दस्तकारी तथा चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए शून्य उत्पाद शुल्क पर ईसीजीसी शुरू करना।