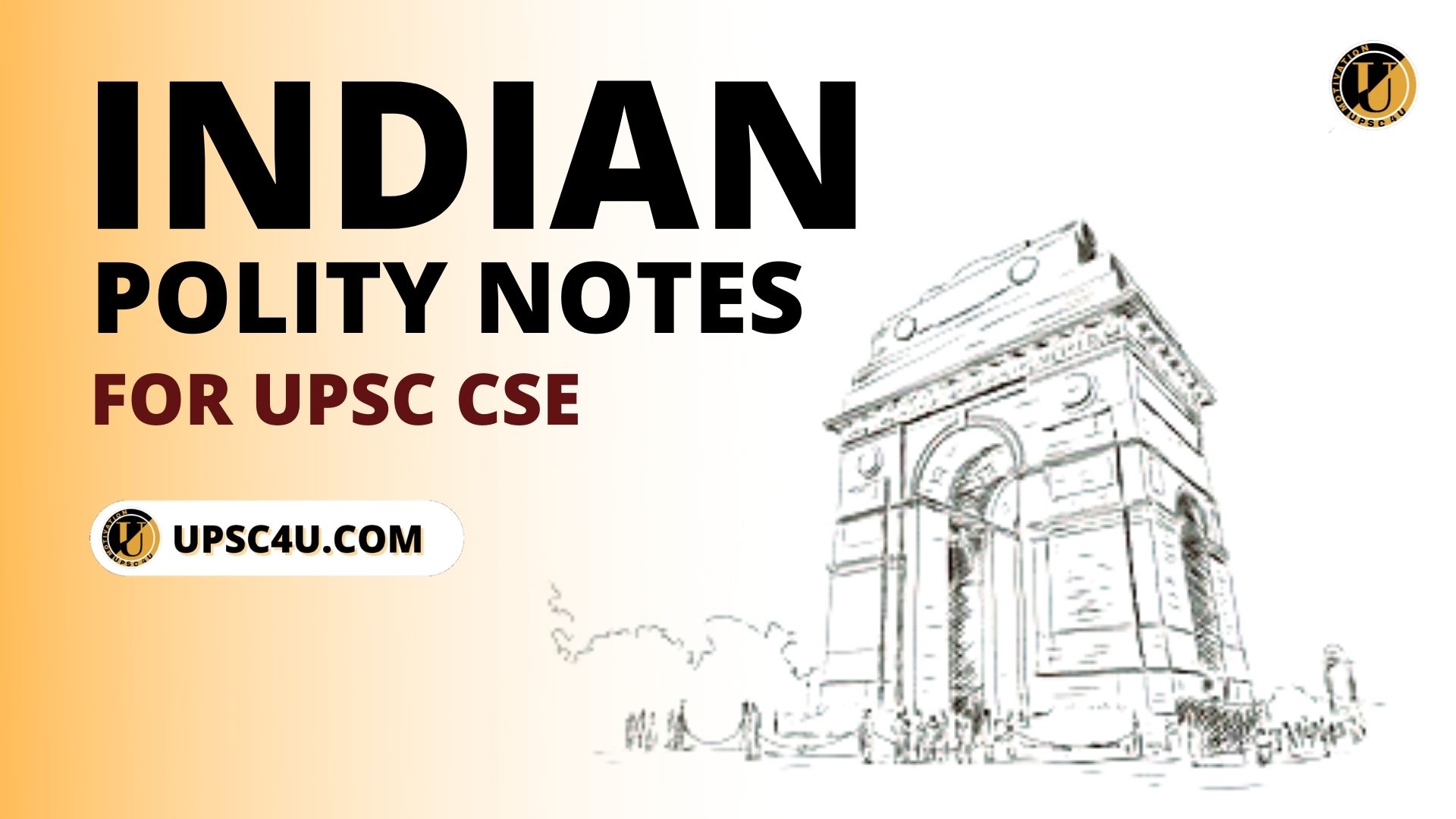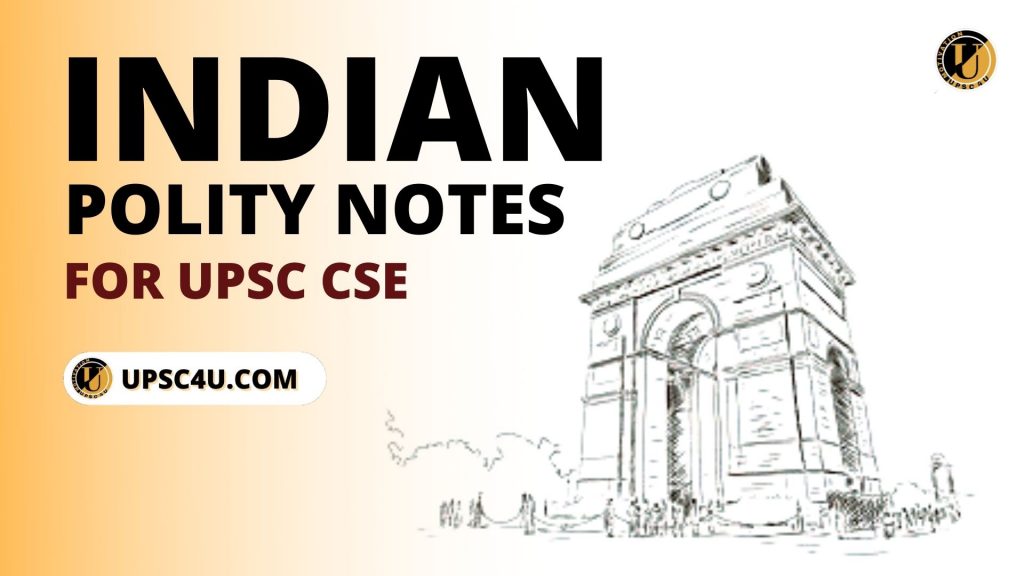भारत के संविधान के ऐतिहासिक आधार को समझने के लिए हम पहले यह समझते हैं कि हमारे ऐतिहासिक आधार का तात्पर्य क्या है?
ऐतिहासिक आधार का मतलब हमारे संविधान के
- सांस्कृतिक आधार
- सामाजिक अधिकार
- आर्थिक आधार और
- राजनीतिक अधिकार से है।
सांस्कृतिक आधार-
- बहुलवाद- सदमेकम विप्रा बहुधा वदंति
- सहनशीलता
- बंधुता- वसुधैव कुटुम्बकम
- पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता- वृक्ष पूजा, नदी पूजा, जल पूजा आदि।
अब यदि संविधान का अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कही गई बातें इन आदर्शों से प्रेरित लगतीं हैं।
सामाजिक आधार-
- वर्ण व्यवस्था
- जाति भेद
- अस्पृश्यता
- महिलाओं की हीन दशा
इस सामाजिक अधिकार को अगर हम संविधान में ढूंढने की कोशिश करें तो यह सभी बातें हमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 15, 16, 17, 23 में दिखाई देते हैं। इन अनुच्छेदों का लक्ष्य हमारे समाज की इन बुराइयों को दूर कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
आर्थिक आधार-
- अल्पविकसित अर्थव्यवस्था
- गरीबी
- असमानता
- सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण
- बंधुआ मजदूरी
- बेगार
- Sc/ST की खराब स्थिति
- अशिक्षा
यह सभी बातें राज्य के नीति निदेशक दिखाई देती हैं। इनके अलावा मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 23, 24 जो मजदूरी और बेगार से संबंधित है, को रेखांकित करता है।
राजनीतिक आधार-
- स्वतंत्रता
- समानता
- बन्धुत्व
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विकसित आदर्श यानी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, जो हमें संविधान की प्रस्तावना और इसके अलावा संविधान में कई जगह कई अनेक शब्दों में यह सब बातें दिख जाती हैं।
अतएव ऐसा कहना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, प्रासंगिक नहीं लगता है। इसका मूल स्वर भारतीय है। हमने विदेशी संस्थाओं से, विदेशी संविधान से प्रेरणा अवश्य ली किंतु उन्हें भारत के संदर्भ में संशोधित किया और केंद्र में उपर्युक्त ऐतिहासिक आधार को रखा।
भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1947 से पहले, भारत को दो मुख्य संस्थाओं में विभाजित किया गया – ब्रिटिश भारत जिसमें सहायक प्रांत गठबंधन नीति के तहत भारतीय राजकुमारों द्वारा शासित 11 प्रांत और रियासत राज्य शामिल थे। दोनों इकाइयां भारतीय संघ बनाने के लिए मिलकर मिल गईं, लेकिन ब्रिटिश भारत में कई विरासत प्रणालियों का भी पालन किया जाता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास को भारतीय स्वतंत्रता से पहले पारित कई नियमों और कृत्यों के लिए खोजा जा सकता है।
भारतीय प्रशासन प्रणाली
भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र का एक संसदीय रूप है जहां कार्यकारी संसद के लिए जिम्मेदार है। संसद में दो घर हैं – लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही, शासन का प्रकार संघीय है, यानी केंद्र और राज्यों में अलग-अलग कार्यकारी और विधायिका है। स्थानीय सरकार के स्तर पर भी आत्म-शासन है। इन सभी प्रणालियों को ब्रिटिश प्रशासन के लिए उनकी विरासत का श्रेय देना है।
भारत के संवैधानिक विकास में कोई अचानक से बदलाव नहीं आए थे. बल्कि यह एक चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए विभिन्न एक्टों और बिलों का का परिणाम था. अंग्रेजों ने समय-समय पर नए नए प्रावधान किए और नए-नए एक्ट पारित किए।
ईस्ट इंडिया कंपनी शासन- आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को व्यापारिक कार्य तक ही सीमित रखा लेकिन विभिन्न घटनाओं के परिणाम स्वरूप उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ और सन 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह से बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर दिया इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संगठन से राजनीतिक संगठन में परिवर्तित हो गई 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारत दोनों के लिए अनुभवहीन रहा कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार से दस लाख पाउंड का कर्ज लिया और ब्रिटिश सरकार ने इस कर्ज के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया. इस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया यह भारत के संवैधानिक विकास का पहला चरण था.
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन मे 31 दिसम्बर 1600 ई को हुई थी 1608 ई मे इसका पहला व्यापारिक जहाज सूरत बन्दरगाह पहुचा उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का भारत में शासन था l
1773 का विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट क्या है?
रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में पारित किया गया इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संविधान कंपनी तथा सरकार के मध्य संबंध तथा भारत में शासन की व्यवस्था तीनों को प्रभावित किया गया जो निम्नलिखित हैं
- बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया गया
- कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए अब कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे
- कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदों पर हो वह किसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपहार, दान आदि ग्रहण नहीं कर सकता था.
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला कदम उठाया गया था।
➫इसने बंगाल के राज्यपाल (फोर्ट विलियम) को गवर्नर जनरल (बंगाल) के रूप में नामित किया।
➫वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने।
➫ गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई (चार सदस्य)। कोई अलग विधायी परिषद नहीं थी।
➫इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों का अधीन रखा।
➫सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हुई थी।
➫इसने कंपनी के किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासी से रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया।
➫निदेशक मंडल (कंपनी के शासी निकाय) को अपने राजस्व की रिपोर्ट करनी चाहिए।
1781 ईस्वी का संशोधन विधेयक
1781 के संशोधन विधेयक के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों के द्वारा अपने कार्यकाल के रूप में किए गए विभिन्न कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से स्वयं को बाहर रखना था इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार का क्षेत्र स्पष्ट किया गया जिसमें कोलकाता के सभी निवासियों को इस कानून के अंतर्गत लाया गया तथा प्रतिवादी का निजी कानून लागू करने की बात की गई
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट के नाम पर बना. मराठा और अंग्रेजो के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति गर्त में चली गई इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस लाख पाउंड का ब्रिटेन सरकार से कर्ज मांगा तो कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए पहले से ही प्रवर समिति एवं गुप्त संगति नियुक्त की गई थी जिनकी रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के शासन की अच्छी छाप नहीं थी लॉर्ड फॉक्स एवं नॉर्थ नॉर्थ की सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया लेकिन वह विधेयक हाउसोप्लांट में पास नहीं हो सका और फॉक्स एवं लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा
भारतीय इतिहास में यह पहला और अंतिम अवसर था. जब भारतीय मामलों के लिए अंग्रेजी सरकार भंग हो गई. यदि यह बिल पारित हो जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती.
➫ कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच प्रतिष्ठित।
➫राजनीतिक मामलों के लिए वाणिज्यिक कार्यों और नियंत्रण बोर्ड के लिए निदेशक मंडल।
➫ गवर्नर जनरल की परिषद की ताकत को तीन सदस्यों तक कम कर दिया।
➫ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारतीय मामलों को रखा।
➫भारत में कंपनियों के क्षेत्र को “भारत में ब्रिटिश कब्जा” कहा जाता था।
➫मद्रास और बॉम्बे में राज्यपाल परिषदों की स्थापना की गई।
1786 का एक्ट
1786 के एक्ट ने गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति के सभी अधिकार प्रदान किए तथा उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया तथा अपने निर्णय लागू करने का भी अधिकार दिया गया सबसे पहले इस एक्ट ने यह अधिकार ‘लॉर्ड कार्नवालिस’ को प्रदान किया
1793 का चार्टर अधिनियम
1793 का चार्टर अधिनियम दे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय को से देने का निर्णय दिया
1813 का चार्टर एक्ट
1813 का चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक और व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया कि वह अपने व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को नहीं संभाल सकती थी तो लेसेज फायर की नीति तथा नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इसी परिदृश्य में सन 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ तथा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और चीन का कंपनी के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों पर तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया इसमें शिक्षा के लिए ₹100000 अलग से दिए गए.
1833 का चार्टर अधिनियम
सन 1813 तथा 1833 ईसवी के चार्टर के मध्य इंग्लैंड में बहुत परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित हैं
- औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन में वृद्धि करना
- 1830 में वही गदल इंग्लैंड की सत्ता में आया और उसके द्वारा उदारवादी नीति का अनुपालन ऐसे वातावरण में यह मांग उठने लगी कि कंपनी को समाप्त किया जाए और क्राउन द्वारा भारत का प्रशासन अपने हाथों में सीधे ले लिया जाए इसी पृष्ठभूमि में 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हो गया
1853 का चार्टर अधिनियम की जानकारी
1833 का चार्टर अधिनियम पहले के चार्टरो बिल्कुल भिन्न था यह अधिनियम निर्धारित अवधि के लिए ना होकर अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया 1853 के एक्ट की 53 की धारा में एक विधि आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान था पहला विधि आयोग 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित हुआ जो लगभग 1843 तक बना रहा इसके बाद 1853 में दूसरा विधि आयोग स्थापित किया और 1861 में तीसरा अधिनियम बनाया गया जिसने 1872 ईसवी तक कार्य किया कानून निर्माण के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति भारत में एक स्वतंत्र विधायक का कारण मानी जाती है
गवर्नर जनरल के विधाई कार्य में सहयोग के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश एक अन्य न्यायाधीश तथा 4 प्रेसिडेंटियो मद्रास बंगाल मुंबई और उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रतिनिधि शामिल थे जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला
➫गवर्नर जनरल काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया।
➫केंद्रीय विधायी परिषद में 6 सदस्य। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की अस्थायी सरकारों में से छह सदस्यों में से चार नियुक्त किए गए थे।
➫इसने कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू की (भारतीय नागरिक सेवा सभी के लिए खोली गई)।
1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारें जानकारी
1858 के सुधार कानून से गृह सरकार के ढांचे को पूरी तरह से दिया गया परन्तु भारतीय सरकार के क्षेत्र में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया गया इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया 1861 ईसवी के सुधार कानून से हुई जिसके पीछे निम्नलिखित कारण थे
भारत परिषद अधिनियम
सर सैयद अहमद, सर वार्टल फ्रेरे जैसे विद्वानों का मानना था कि 1857 की घटना का मुख्य कारण भारतीयों का शासन के प्रति असंतोष होना था
गवर्नर जनरल की परिषद संसद की भांति कार्य करने लगी थी जिससे भारतीय क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हुई वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई ➫इसने पहली बार वाइसराय के कार्यकारी + विधायी परिषद (गैर-आधिकारिक) जैसे संस्थानों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया। 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया।
➫केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई।
➫यह मुहैया कराया गया कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद के पास कुछ भारतीयों को विधायी व्यवसायों के दौरान गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में होना चाहिए।
➫इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को वैधानिक मान्यता दी।
➫बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
सन 1861 में स्थापित व्यवस्था ने दो घटनाओं ने गुणात्मक परिवर्तन ला दिए जो निम्नलिखित है।
- लॉर्ड रिपोन द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव तथा इससे संबंधित विधान परिषद में भी मांगे उठी.
- 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस की प्रमुख मांग थी विधान परिषदों को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाना था.
भारत में विधान परिषदस्थापना कब और कहाँ हुई
- मुंबई में 1861 ईसवी में
- बंगाल में 1862 ईसवी में
- उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1886 ईसवी में
- पंजाब में 1897 ईसवी में
भारतीय परिषद एक्ट 1909 (मिंटो मार्ले सुधार)
गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो तथा भारत मंत्री लॉर्ड जान मार्ले
बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में ही भारत में संवैधानिक परिवर्तन की मांग उठने लगी जो निम्नलिखित थी।
- मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया।
- मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग से मताधिकार तथा प्रथम निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थि.
- परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया।
1919 का अधिनियम
20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमंस में संसद के सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट्स के एक प्रश्न का जवाब देते हुए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने भारत में ब्रिटिश शासन के मकसद को लेकर घोषणा की “ब्रिटिश शासन का मकसद प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना और क्रमश उत्तरदाई सरकार की स्थापना के मकसद से ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना है“
घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वशासन के विकास की प्रत्येक चरण की सीमा और समय का निर्धारण ब्रिटेन सरकार करेगी और इसी घोषणा को आधार मानकर के 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया।
प्रमुख प्रावधान
1-प्रांतीय संविधान
भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को क्रमशः विधायी, प्रशासनिक और द्वितीय क्षेत्रों में बांटा गया प्रांतों के विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया
आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था तथा हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई थे उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता था गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई नहीं थे प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य का प्रशासन एवं हस्तांतरित विषय का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषय के विभाजन के पीछे सामान्य सिद्धांत यह था कि यदि कोई इसे एक से अधिक प्रांतों से संबंधित हो तो हुए केंद्र संख्या की परिधि में आता था 1919 के अधिनियम में कोई समवर्ती सूची नहीं थी विषयों के विवाद पर गवर्नर जनरल का अंतिम निर्णय होता था द्वैध शासन प्रणाली इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी इस प्रणाली के जन्मदाता लियोनेल काटिश थे जिन्होंने सर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक सत्र में यह व्यवस्था का स्पष्टीकरण दिया था।
2-प्रांतीय विधायिका
प्रांतीय विधायिका 1909 की तरह ही अतिरिक्त सदस्यों से निर्मित ना होके वार्षिक रूप से चयनित की हुई कार्यकारिणी के स्वतंत्र संवैधानिक इकाई के रूप में थी और प्रांतीय विधायिका का एक सदनात्मक थी।
प्रांतीय विधायकों की अध्यक्षता गवर्नर के हाथों में ना होकर के स्वतंत्र पीठासीन अधिकारी के पास थी इसकी सदस्य संख्या बाद में बढ़ाई गई जिसमें 70 फीसदी सदस्य निर्वाचित होती थी इसके सदस्यों को चुनने की प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन थी फिर भी भारत की जनसंख्या की दृष्टि से मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी कुल जनसंख्या का लगभग 2 फीसदी मत ही डाला जा सकता था।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पूर्णता में स्थापित कर दिया गया और प्रांतीय व्यवस्था सभाएं किसी भी प्रस्ताव को पेश कर सकती थी किंतु से पारित होने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी गवर्नर को इसे रद्द करने का भी अधिकार था प्रांतीय परिषदों को और विधान परिषद का नाम दिया गया और चुनाव नियमों के अनुसार महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था लेकिन प्रांतीय विधायक आए लिंगभेद को अपनी सदन में समुचित प्रस्ताव पारित करके दूर कर सकती थी।
3-केंद्र सरकार
केंद्र की कार्यकारिणी गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी को मिलाकर के सपरिषद गवर्नर जनरल बनी। इस व्यवस्था में उत्तरदायित्व का सिद्धांत गौण था। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद अभी भी भारत सचिव के प्रति और उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदाई थी।
4-केंद्रीय विधायिका
भारत में 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया था। इसके तीन अंग थे। गवर्नर जनरल लेजिसलेटिव असेंबली एवं काउंसिल ऑफ स्टेट।
लेजिसलेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा की निम्न सदन थी। इसमें 145 सदस्य थी और इनमें 104 सदस्य निर्वाचित और 41 सदस्य मनोनीत होते थे।
राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। तथा केवल पुरुषों को ही इसका सदस्य बनाया जा सकता था. केंद्रीय विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित था. तथा सदस्य सदन में प्रश्न पूछ सकते थे. अनुपूरक मांग कर सकते थे। और स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे।
5-कार्यपालिका
- प्रांतों के आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल का अधिकार था
- कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में 3 सदस्य भारतीय नियुक्त किए जाते थे
- कार्यपालिका की सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया प्रांतीय और केंद्रीय।
1935 का भारत सरकार अधिनियम
➫ इस अधिनियम को अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रदान किया गया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि पर विचार किया गया संघ कभी नहीं हुआ।
➫तीन सूचियां: अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों, अर्थात् संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया।
➫केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 आइटम शामिल थे, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची जिसमें 54 आइटम शामिल थे और 36 वस्तुओं सहित दोनों के लिए समवर्ती सूची शामिल थी
➫अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल के साथ निहित किया गया था।
➫ अधिनियम ने प्रांतों में डायरची को समाप्त कर दिया और ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ पेश की।
➫यह केंद्र में डायरैची को अपनाने के लिए प्रदान किया गया।
➫11 प्रांतों में से 6 में द्विपक्षीयता का परिचय दिया।
➫ये छह प्रांत असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत थे।
➫संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया।
➫भारत की परिषद को खत्म कर दिया।
1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
➫ इसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया।
➫केंद्र और प्रांत दोनों में जिम्मेदार सरकारों की स्थापना की।
➫वाइसराय इंडिया और प्रांतीय गवर्नर्स को संवैधानिक (सामान्य प्रमुख) के रूप में नामित किया गया।
➫ इसने संविधान सभा में दोहरी कार्य (संविधान और विधान) को सौंपा और इस प्रभुत्व विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित कर दिया।
भारत का संविधान
➫1833 के चार्टर अधिनियम से पहले किए गए कानूनों को विनियमन कहा जाता था और जिन्हें बाद में अधिनियम कहा जाता था।
➫ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया, लेकिन बाद में कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक शक्तियों को जिला कलेक्टर से अलग कर दिया गया।
➫ अनियंत्रित अधिकारियों के शक्तिशाली अधिकारियों से, भारतीय प्रशासन विधायिका और लोगों के उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार में विकसित हुआ।
➫बिजली के विभाजन के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली और बजट बिंदुओं का विकास।
➫वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों (1870) के विकास की कल्पना की।
➫1882: लॉर्ड रिपोन के संकल्प को स्थानीय स्व-सरकार के ‘मगना कार्टा’ के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्हें ‘भारत में स्थानीय स्व-सरकार के पिता’ के रूप में जाना जाता है।
➫1921: रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था।
➫1773 से 1858 तक, अंग्रेजों ने सत्ता के केंद्रीकरण की कोशिश की। यह 1861 परिषदों के कार्य से था, उन्होंने प्रांतों के साथ सत्ता के विभाजन की ओर स्थानांतरित किया।
➫1833- 1909 के कार्य से पहले चार्टर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।
➫1947 तक, भारत सरकार ने 1919 अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम किया। फेडरेशन और डायरैची से संबंधित 1935 अधिनियम के प्रावधान कभी लागू नहीं किए गए थे।
➫1919 अधिनियम द्वारा प्रदान की गई कार्यकारी परिषद ने 1 9 47 तक वाइसराय को सलाह देना जारी रखा। आधुनिक कार्यकारी (मंत्रिपरिषद) ने कार्यकारी परिषद को अपनी विरासत दी है।
➫आजादी के बाद विधानसभा और लोकसभा में विधान परिषद और विधानसभा विकसित हुई।