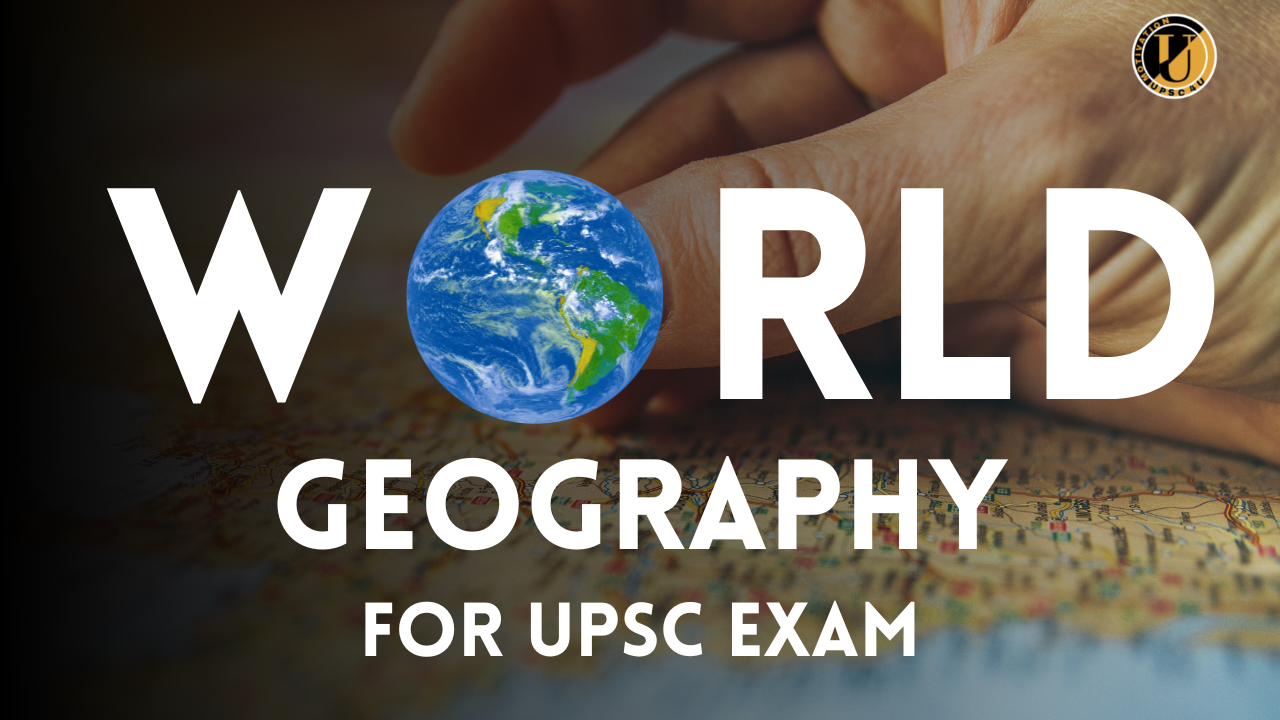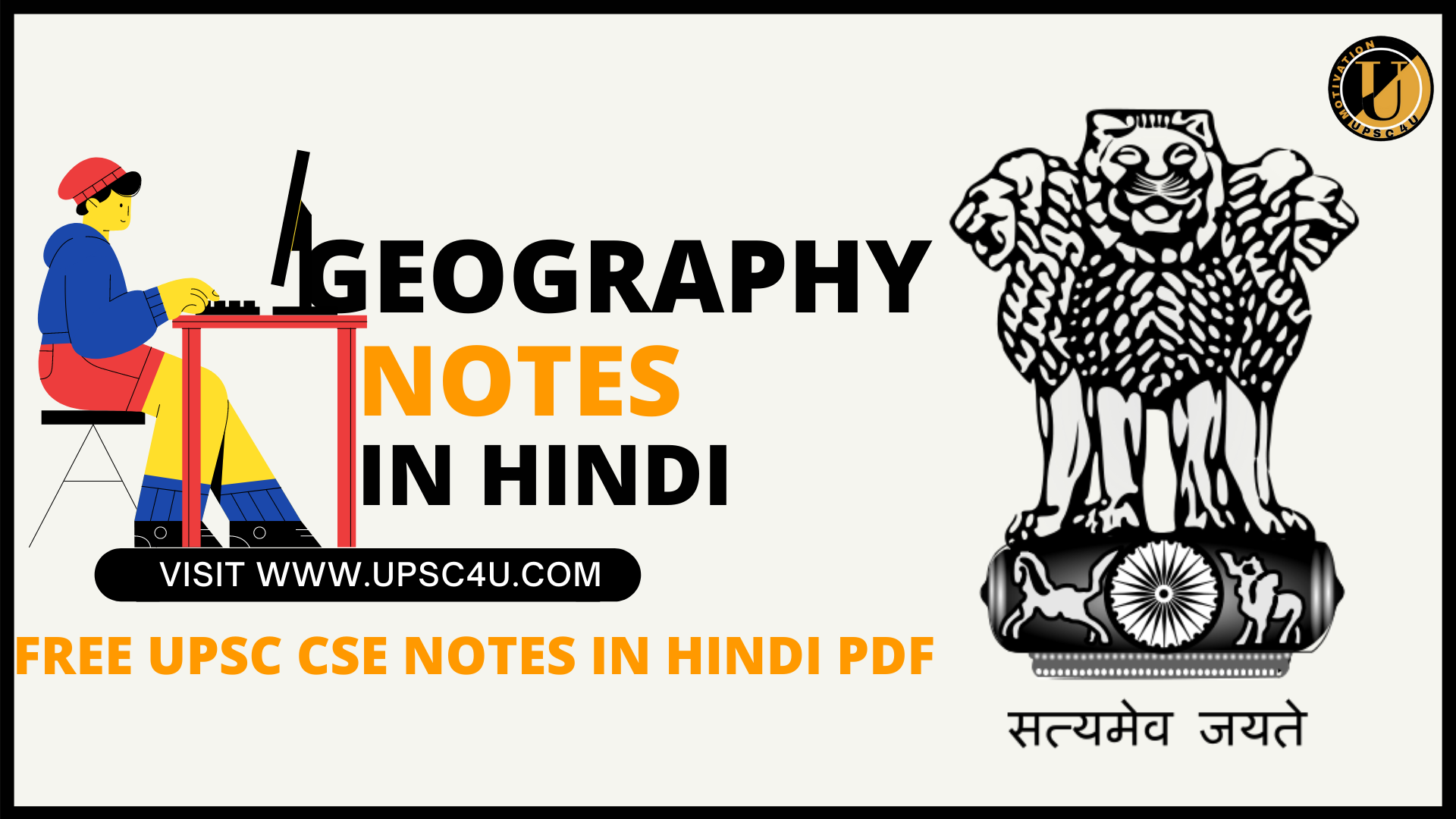नागा: नागा जनजाति के लोग इण्डो-मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। इनकी त्वचा हल्की, बाल सीधे व नाक चपटी होती है।
अरुणाचली व असमी नागाओं के पांच बड़े वर्ग हैं:
- उत्तर में रंगपण और कोन्यक
- पश्चिम में रेंगमा, सेमा और अंगामी
- मध्य में आओ लोहता, फोम, चग, सन्यम और थिम्स्तमुंगर
- दक्षिण में कचा और काबई, तथा
- पूर्वी क्षेत्रों में तेलुल और काल्पो-केंगु।
निवास: नागा जनजाति का प्रमुख निवास प्रदेश नागालैण्ड है किंतु मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और असम में भी नागा जनजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड के पर्वतीयप्रदेश के उत्तर-पूर्व में पटकोई पहाड़ियां तथा दक्षिण में मणिपुर और अराकान योमा पर्वत श्रेणियां हैं। समस्त भाग ऊबड़-खाबड़ है तथा जंगलों से आच्छादित है। यहां पर उष्ण, आर्द्र व शुष्क जलवायु रहती है। दो हजार छः सौ पचास मीटर से अधिक ऊंचे भागों में ठण्डी शुष्क जलवायु रहती है, जबकि निचले ढालों पर वर्षा-ऋतु में मलेरिया का प्रकोप रहता है। नागाओं की बस्ती इसीलिए 1650 से 2550 मी. की ऊंचाई पर रहती है।
अर्थव्यवस्था: नागाओं के मुख्य व्यवसाय- आखेट, मछली पकड़ना कृषि व कुटीर उद्योग हैं।
सामाजिक व्यवस्था: नागाओं में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है। आखेट केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कृषि स्त्री-पुरुष दोनों द्वारा की जाती है, गांव के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह में लड़के के परिवार की ओर से लड़की के परिवार को दहेज या धन दिया जाता है व विवाह के समय पशुबलि भी दी जाती है।
जादू टोना भी नागाओं में प्रचलित है किंतु अब ईसाई धर्म के प्रभाव से इसका प्रयोग कम हो गया है।
भोजन: चावल, बकरी, गाय, बैल, सांप, मेंढक आदि का मांस खाया जाता है व चावल की शराब जू का भी सेवन किया जाता है।
वेशभूषा: विभिन्न नागा वर्गों में भिन्न-भिन्न वेशभूषाएं प्रचलित हैं, चित्र गुदवाने व सिर पर पंख बांधना प्रचलित है।
खासी: 98 प्रतिशत खासी जनजाति मुख्यतः मेघालय, असम व त्रिपुरा में पाई जाती है। मुख्यतः मेघालय की खासी और जयतियां पहाड़ियों में रहने वाली आदिम जाति के लोग खासी कहलाते हैं। इनमें समाज में कई वर्ग होते हैं, जिनमें निम्न चार प्रमुख सामाजिक श्रेणियां (social Classes) होती हैं|-
- की-साऐम (Kie-Siem), ये राजवंशी होते हैं।
- की-लिंगोह (Kie-Lingoh), पुजारियों के वंशज।
- मंत्री वंशज।
- प्रजा वंशज।
यद्यपि इन सामाजिक वर्गों में ऊचे-नीचे स्तर होते हैं, फिर भी इनमें परस्पर संबंध हो सकते हैं।
अर्थव्यवस्था: खासी जाति का पेशा सीढ़ीदार खेतों में कृषि करना है। इसके अतिरिक्त खासी लोग झूम कृषि करते हैं। शताब्दियों से पहाड़ी मोटे अनाज, जैसे-कोदों, चौलाई,फाफड़ा, कोटू इत्यादि झूम कृषि द्वारा ही उत्पन्न किये जाते रहे हैं।
सामाजिक व्यवस्था: खासी जाति में मातृसत्ताप्रधान सामाजिक संगठन होता है। इसमें सबसे छोटी पुत्री का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार की सम्पति की वही उत्तराधिकारी होती है और वही धार्मिक पूजाएं करती है। इनमें एक पति व पत्नी की ही प्रथा है। विवाह के बाद तलाक या पुनर्विवाह भी होते हैं। मृतक का दाह संस्कार होता है, परंतु चेचक, हैजा, आदि रोगों से मृत्यु होने पर शव को भूमि में गाड़ दिया जाता है। भारत में अंग्रेजी राज्य के समय से ईसाई मत के प्रचारकों ने बहुत-से खासी आदिवासियों को ईसाई बना दिया है। खासी जनजाति आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की मोन-खमेर भाषा बोलती है।
राजव्यवस्था राजनीतिक संगठन, इसके मुखिया और उसकी मत्रिपरिषद् द्वारा बनता है। पूरे राज्य की जनजाति के अध्यक्ष को सियम कहा जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां बेहद सीमित हैं। वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता और उसे अपनी कार्यकारी परिषद् पर निर्भर रहना पड़ता है।
संथाल: संथाल भारत की सबसे बड़ी आदिम जाति है। ये मुख्यतः राजमहल पहाड़ी व छोटानागपुर पठार क्षेत्रों में पायी जाती है। इनके दो मुख्य क्षेत्र हैं- एक संथाल परगना (बिहार) व दूसरा मयूरभंज (ओडीशा)। संथाल बांग्लादेश में (लगभग 70,000) और नेपाल में (लगभग 10,000 हजार) रहते हैं।
ये ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा व काला, बाल घने व सीधे, नाक लम्बी तथा उठी हुयी व मुंह फैला या चौड़ा, होंठ पतले परंतु उभरे हुए व कद छोटा होता है।
समाज एव संस्कृति: संथाल के 12 कुल हैं जिसे परीज कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक को कई उप-प्रभागों में बांटा जाता है जिसका आघार भी वंश होता है और जो पितृसत्तात्मक होता है। प्रत्येक परी या कुल उप-कुलों या उप-समूहों में विभाजित होता है जिसे खुट कहा जाता है। विभिन्न परीज में खुटों की संख्या 13 से 28 के बीच होती है। इसमें एकल विवाह प्रचलित है। हालांकि बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन व्यवहार में दुर्लभ है। उनकी भाषा संथाली है, बोली खेरवारी है। यह मुंडा आस्ट्रिक परिवार की भाषा के साथ संबंध रखती है।
राजव्यवस्था– भजही संथाल ग्राम का मुखिया होता है। सभी लोगों को उसके निर्देशों का पालन करना होता है। परम्परागत रूप से, उसे पूरे गांव द्वारा चुना जाता है। वह गांव के बाहरी एवं आंतरिक दोनों मामलों का प्रतिनिधि होता है। न्यायिक मामलों के लिए संथाल के पास ऑतिम अपीलीय न्यायालय भी है।
अर्थव्यवस्था: पहले, संथाल मुख्य रूप से आखेट पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब उन्होंने चाय बागानों और खदानों में भी काम करना शुरू कर दिया है। पुरुष एवं महिला दोनों ही कृषि कार्य करते हैं। वनों की सफाई या जुताई या मिट्टी के बांध बनाने जैसे भारी काम पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। सुअर, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, कबूतर, मुर्गी इत्यादि जैसे घरेलू जानवरों की देख-रेख एवं कार्य परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी समझी जाती है।
गौंड: यह प्राक् द्रविड़ जनजाति है। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले व आंखे, नाक फैली, होंठ मोटे, शारीरिक गठन संतुलित पर सुंदर नहीं होते।
इनकी भाषा गोंडी है। यह जनजाति मुख्यतः बस्तर पठार, नर्मदा, गोदावरी व महानदी की ऊपरी पहाड़ियों में निवास करती है। ये मध्य भारत के आठ राज्यों के 181 जिलों में फैले हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार यह जनजाति मध्यप्रदेश, ओडीशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सभी जिलों में, आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में, बिहार के 29 जिलों में, गुजरात के 13 जिलों, पश्चिम बंगाल के 15 जिलों में पाई जाती है।
मध्य प्रदेश के बस्तर पठार में इनके मुख्य वर्ग- मरिया, मुरिया, परजा, भटरा, गडाबा, हालबा तया ढाकर हैं।
आंध्र प्रदेश के गंजाम और विशाखापट्टनम जिलों में साओरा वर्ग, कुरुश (Kurush) और केवट वर्ग के गॉड रहते हैं।
अर्थव्यवस्था: गौंड जनजाति नगले अर्थात् पल्ली और छोटे-छोटे गांवों में निवास करती है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और निम्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं।
- दिप्पा कृषि: यह स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है, जिसमें एक भूमि पर दो-चार वर्ष कृषि करने के बाद उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि पर कृषि करते हैं।
- पैण्डा कृषि: बस्तर के पहाड़ी भागों में, जहां ढालों पर वन खड़े हैं- पैण्डा कृषि की जाती है, जिसमें सीढ़ीदार खेतों पर कृषि होती है।
- मत्स्य कर्म: केवट, कुरुख (Kurukh) और धीमर लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और अनाज के बदले ये मारिया लोगों की मछलियां देते हैं।
- पशुचारण: रावत वर्ग गौंड जाति का एक उपवर्ग है। इसका प्रमुख पेशा पशुपालन है।
- लघु एवं कुटीर उद्योग: अध्रिप्रदेश में गंजम और विशाखापट्टनम् जिलों में सावरा (sawra) वर्ग के बहुत-से गौंड परिवार छोटे कुटीर उद्योग में लगे रहते हैं, जैसे-अरीसी (Arisi) वर्ग के लोग हथकरघों से कपड़ा बुनते हैं। कुन्डाल वर्ग के लोग टोकरियां बनाते हैं और बहुत-से परिवार लोहार हैं।
औजार: इनके औजार साधारण किस्म के होते हैं। स्थानीय लोहार ही हलों के फल, खुरपे, फावड़े, दरांती, हसिए, कुल्हाड़ी, तीर, हल की लकड़ी आदि बनाते हैं।
वेशभूषा: ये सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, स्त्रियां मूंगे, नकली मोतियों के आभूषण, कौड़ियों की माला, बालों को संवारने के लिए सफेद बांस या पशुओं के सीगों के कघों का प्रयोग करती हैं।
बलि प्रथा: ये लोग देवी-देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पशु बलि देते हैं। इनका विश्वास है कि बलि देने से खेती की उपज कई गुना बढ़ेगी अन्यथा देवताओं के नाराज होने पर फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी।
श्रम-मजदूरी: ये लोग मजदूरी कार्य में भी लगे हैं। साधारणतः मजदूरी के बदले रुपए व अनाज दिया जाता है। कभी-कभी खेतिहर मजदूर दास भी बनाये जाते हैं

भील: जनजाति का निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्यप्रदेश, खानदेश और गुजरात है। भीलवाड़ा क्षेत्र भील निवास का संकेतक है। अनुमान है कि, भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा के विल्लवर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ धनुर्धारी (Bowman) होता है। कुछ मानव शास्त्रियों का मत है कि मील जाति भारत की प्राक् द्रविड़ जातियों में से है। शारीरिक बनावट की दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं। इनका कद छोटा व मध्यम, बाल रूखे, आंखें लाल व जबड़ा बाहर निकला होता है।
ये इण्डो-आर्यन परिवार की भाषा बोलते हैं। भाषा की दृष्टि से इनके तीन मुख्य समूह हैं- भिलाली, भिलोदी और कोहना/कोकनी या कूकना।
उप-जातियां: भील जनजाति में राजपूत रक्त का मिश्रण है- दूवल, बूंदी, परमार व चौहान इसकी उप-जातियां हैं।
सामाजिक व्यवस्था: इनके एक गांव में 20 से 30 परिवार होते हैं। छोटे गांव को फला और बड़े ग्राम को पाल कहते हैं। पाल का नेता ग्रामपति या मुखिया होता है। इनमें सामुदायिक भावना पायी जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। स्त्रियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। बहिर्विवाह की प्रथा पायी जाती है।
अर्थव्यवस्था: ये सामान्यतया निर्धन हैं। कई भील अपराधी हैं। कई लघु स्तरीय कृषक हैं व जहां भूमि का अभाव है वहां ये पशुपालन करते हैं।
भोजन: इनका मुख्य भोजन मक्का, चावल, सांवा-रोटी, दूध, मांस, मछली व शराब है।
वेशभूषा: भील स्त्रियां लंहगा-चोली, कांचली व ओढ़नी पहनती हैं। पोतियावाल भील धोती पहनते हैं जबकि लंगोटिया भील लंगोटी धारण करते हैं।
थारू: थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड सहित) में तराई और भावर की संकीर्ण पट्टी का प्रदेश है, जो कुछ पूर्व के बिहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है।
थारू शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। एक मत के अनुसार ये अथर्ववेद से संबंधित हैं, पहले इनका नाम अथरू था, बाद में थारू हो गया। थारू शब्द का अर्थ है- ठहरे हुए। मलेरिया और मच्छरों की भावर-तराई पेटी में भी ये लोग अपने जीविका निर्वाह और निवास के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए ठहरे रहे हैं, इसलिए इनका नाम थारू हो गया।
अर्थव्यवस्था: थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। थारू लोग चावल उत्पादन में बड़े निपुण हैं। यद्यपि अपरदन (erosian) द्वारा मिट्टी कटकर बहती है, फिर भी ये लोग खेतों की मेढ़ें बनाकर अपरदन रोकते हैं और गोबर की खाद से भूमि की उर्वरता को बनाये रखते हैं। खेतों को जीतने का काम पुरुष करते हैं, नराई (weeding), कटाई (harvesting) आदि कार्य स्त्रियां करती हैं। धान की रोपाई के लिए स्त्रियों को जल से भरे या कीचड़युक्त खेतों में प्रायः दिनभर रहना पड़ता है, जिसके कारण उनके पैरों की उंगलियां गल सी जाती हैं, हाथों की उंगलियों के नाखून भी गले हुये से हो जाते हैं।
सामाजिक व्यवस्था: थारू जनजाति की प्राथमिक सामाजिक इकाई या संगठन परिवार है। परिवारों से मिलकर कुरी (कुल) बनता है और कुल उच्च अंश और निम्न अंश बनाने के लिए दो समूहों में इकट्ठा होते हैं जिससे अंतिम रूप से जनजाति का निर्माण होता है। उच्च अंश में बाथा, बरीटिया, बदवैत, दाहेत, और महातुम आते हैं जबकि निम्न अंश में रावत, बुक्सा, खुका, रजिया, सांसा, जुगिया और डांगरा आते हैं।
थारू जनजाति जड़ात्मवाद, जादू-टोना और पूर्वजों की पूजा करते हैं। ये अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत करते हैं जिसे बुद्धि बाबू या निराधार के रूप में जाना जाता है। ये ऐसी आत्माओं को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि ये आत्माएं घर के लोगों की रक्षा करेंगी। थारू लोगों का मानना है कि बेमिया देवी नवजात शिशु को बुरी आत्मा के प्रभाव से बचाती है।
खरिया: खरिया लोग ओडीशा में मयूरभंज की पहाड़ियों के और बिहार में ढाल भूमि (सिंहभूम) तथा बड़ाभस (मानभूमि) की पहाड़ियों के निवासी हैं। ये पहाड़ियां छोटी-छोटी नदियों, संजाई, करकाह और बूरावलडीग नदियों के बेसिन में स्थित हैं।
समाज: खरिया समाज पितृसत्तात्मक होता है। यहां एकल परिवार व्यवस्था के साथ एकल विवाह व्यवस्था है। खरिया लोगों का मुख्य खान-पान चावल, सब्जी, मांस, मछली और वनोत्पाद हैं। खरिया जनजाति की चार से बारह झोंपड़ियों की बेहद छोटी बस्ती होती है। दुध और देकी खरिया प्रजाति किसी नदी या सहायक नदी के किनारे पर बसती है और इसमें 40-50 परिवार होते हैं।
अर्थव्यवस्था: इन लोगों के मुख्य उद्यम हैं- (i) झूम कृषि, (ii) जंगल की वस्तुएं इकट्ठा करना, (iii) आखेट, तथा; (iv) मछली पकड़ना। वर्तमान समय में लोहे की खानों में तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के कारखानों, जैसे- राउरकेला, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हीराकुंड आदि, में मजदूरी करने से खरिया लोगों का सम्पर्क शिक्षित और कारीगर लोगों से होता रहा है, इसके फलस्वरूप इनमें शिक्षा का प्रचार हुआ है।
राजव्यवस्था: खरिया ग्राम पंचायत में प्रभावी और गांव के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। जैसाकि उनके गांव में कुछ खास संख्या में जनजाति से बाहर के लोग भी होते हैं, सभी समूहों को पंचायत में प्रतिनिधित्व मिलता है। पंचायत के निर्णयों को प्रायः बिना किसी विरोध के मान लिया जाता है। गांव का मुखिया सभी धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक कार्यों का भी मुखिया होता है। वह कई नामों–कालो, देहुरी या पाहन, से जाना जाता है। गांव के पुजारी का प्रतीक सामु (पवित्र टोकरी) है जिसमें कुछ अरुआ (कच्चे चावल) रखे होते हैं जिसे गांव के देवताओं एवं आत्माओं की पूजा में प्रयोग किया जाता है। कालो पुजारी के रूप में सामूहिक पूजन समारोह में कार्य करता है और वह ग्राम देवताओं को पूजा और बलि अर्पित करता है।
टोडा: टोडा जाति के लोग नीलगिरि की पहाड़ियों में निवास करते हैं, नीलगिरि पहाड़ियों पर निवास करने वाली अन्य आदिम जातियों-बडागा, कोटा, इख्ता औद कुरुम्बा हैं। इनमें टोडा लोग सबसे प्राचीन निवसी हैं।
शारीरिक लक्षण: टोडा नर-नारी सुंदर आकृति के, सुगठित शरीर वाले व्यक्ति होते हैं। इनका कद प्रायः लम्बा होता है। नाक पतली और लम्बी (aquiline), जबड़ा बड़ा और नेत्र बड़े होते हैं। ये दक्षिण भारत की अन्य आदिम जातियों में बिल्कुल भिन्न दिखलायी देते हैं।
भोजन: टोडा लोग शाकाहारी होते हैं, जो केवल पूजा, उत्सवों त्योहारों, आदि के समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी गयी पशुबलि के पश्चात् कर्मकाण्ड (ritual) के रूप में मांस भक्षण करते हैं। इनका मुख्य भोजन मैंस का दूध, दही, कन्द-मूल-फल और शाक-सब्जियां हैं।
वेशभूषा: ये लोग धोती बांधते हैं और कंधों से लेकर नीचे तक एक सूती चोगा पहनते हैं, जो गर्दन से पैरों तक शरीर को ढके होता है, इसमें से दोनों हाथ बाहर निकले होते हैं। इस चोगे की शैली रोमन चोगे से मिलती-जुलती होती है। पुरुष और स्त्रियां सभी इस प्रकार के लम्बे चोगे पहनते रहते हैं, सभी के सिर नंगे होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात्, दूसरे प्रदेशों के लोगों के सम्पर्क में आने से स्त्रियां लम्बी धोती बांधने लगी हैं तथा छोटी चोली भी पहनने लगी हैं।
अर्थव्यवस्था: जीविका निर्वाह का मुख्य साधन पशुचारण तथा जंगल से कन्दमूल, शहद, गोंद इत्यादि इकट्ठा करना है। कुछ लोग शाक-सब्जियां उत्पन्न कर लेते हैं, परंतु मुख्य व्यवसाय भैंस पालना है।
सामाजिक व्यवस्था: टोडा लोगों में सम्मिलित बहु-पत्नी प्रथा (Polyandry) है, जिसके अनुसार एक परिवार में दो या अधिक भाइयों की एक पत्नी अथवा एक से अधिक पत्नियां सम्मिलित प्रकार से होती हैं। जनसंख्या में पुरुष-स्त्री संख्या के अनुपात में पुरुष अधिक हैं। प्रत्येक गांव का एक ग्राम देवता होता है।
भाषा: दूसरे लोगों से बातचीत करते समय टोडा लोग तमिल और कन्नड़ मिश्रित भाषा बोलते हैं, परंतु वे आपस में अपनी आदिम भाषा बोलते हैं।
मुण्डा: इस जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः छोटानागपुर का पठार है। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक ये लोग वन में प्रायः झोंपड़ियों के समूहों में रहते थे, परंतु बाद में ये उरांव, आदि अन्य जनजातियों की तरह छोटे-छोटे गांवों की बस्तियों में रहने लगे और खाद्य-संग्रह तथा स्थानांतरण कृषि के साथ-साथ स्थायी कृषि भी करने लगे हैं।
भाषा: मुण्डा भाषा प्रोटो-इण्डिका वर्ग की है, जो गोंडवाना की जनजातियों की भाषा का तथा दक्षिणी बिहारी भाषा का मिश्रण है।
अर्थव्यवस्था: मुण्डा जनजाति की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या तो अब अपने वन प्रदेशीय गांवों में स्थायी कृषि करती है, यद्यपि प्राचीन परम्परा के अनुसार वनों से खाद्य-संग्रह और कन्द-मूल-फल भी एकत्रित करते हैं। अब मत्स्यपालन और कुक्कुटपालन पर भी बल दिया जा रहा है। लगभग एक-तिहाई मुण्डा जनसंख्या, झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडीह की कोयला खानों में, सिंहभूम की पसिराबुरू, बड़ाबुर और गुआ की लौह-खानों में, मानभूमि और नोआमुण्डी की लौह खानों में तथा मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक की खानों में खनिजों और अन्य श्रमिकों का कार्य करते हैं।
सामाजिक व्यवस्था: मुण्डा जनजाति हिन्दू समाज की मुख्य प्रथाओं में से लगभग सभी को अपना चुकी है। ये लोग अपने गोत्र और कुल के नाम को धारण करते हैं। परिवार एक प्रमुख संस्था होती है, जो व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रबंध करती है। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। गोत्र पितृवंशीय होते हैं। विवाह के पश्चात् लड़की का गोत्र बदल कर वही हो जाता है, जो पति का होता है। गोत्रों के नाम प्रायः ऋषियों, नदियों, पक्षियों, जंतओं, वृक्षों या फलों के नाम से मितते हैं।
गांव में पंचायत का बड़ा महत्व होता है। सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है।
मुण्डा लोग एक ईश्वर को मानने के साथ-साथ देवी-देवताओं को भी मानते हैं। देवी-देवताओं के पूजन के लिए प्रत्येक दो-तीन महीनों में सामूहिक मेले लगते हैं। इन सामूहिक मेलों में सामूहिक गान-वाद्य-नृत्य होते हैं। नृत्य कई प्रकार के होते हैं। शिकार की नकल प्रदर्शित करने के नृत्य को जापी कहते हैं; परन्तु सर्वप्रमुख कृषि नृत्य होता है, जिसमे भूमि जोतने, बोने निराई करने, फसल काटने आदि क्रियाओं की नकल प्रदर्शित की जाती है।
इनमें मौखिक साहित्य को परम्परा द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चालू रखा जाता है।
ओरांव या उरांव: उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र छोटानागपुर का पठार व रांची का पठार है। कुछ उरांव लोग उत्तरी बिहार में और बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी रहते हैं।
शारीरिक लक्षण: उरांव लोगों की शारीरिक रचना प्राचीन भारतीय वन्य जातियों की है। ये लोग गोंडिड उपजाति के होते हैं। इनका कद मध्यम, त्वचा का वर्ण कत्थई या ताम्रवर्णी काला,सिर लम्बा, बाल धुंधराले, नाक चौड़ी और चपटी होती है। आंखें खुली व होंठ मोटे होते हैं।
भाषा: उरांव लोगों की भाषा मुण्डा भाषा से मिलती हुयी बंगाली और हिंदी मिश्रित बिहारी भाषा है।
अर्थव्यवस्था: इनका मुख्य व्यवसाय स्थायी खेती करना है, यद्यपि वनों में बसे हुए कुछ परिवार स्थानांतरण कृषि भी करते हैं। स्थायी कृषि की मुख्य फसल चावल है, जिसकी वर्षभर में दो या तीन फसलें होती हैं। अन्य फसलें- मक्का, गन्ना तथा तम्बाकू हैं। उरांव जनजाति की लगभग चौथाई जनसंख्या श्रमिक व्यवसाय में कार्य करती है। ये लोग अन्य भारतीय जनजातियों के साथ, खानों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं।
सामाजिक व्यवस्था: उरांव जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। ऐसे परिवार में पति या पिता के हाथ में अधिकार रहता है। बच्चे पिता के कुल और वंश के नाम को धारण करते हैं।
एकल विवाह प्रथा ही सर्वाधिक प्रचलित है। लड़के या लड़की का विवाह गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में ही होता है।
पहले उरांव जनजाति में अविवाहित लड़के-लड़कियों के युवागृह घुमकुड़िया होते थे, जिनका प्रचार अब बंद हो गया है।