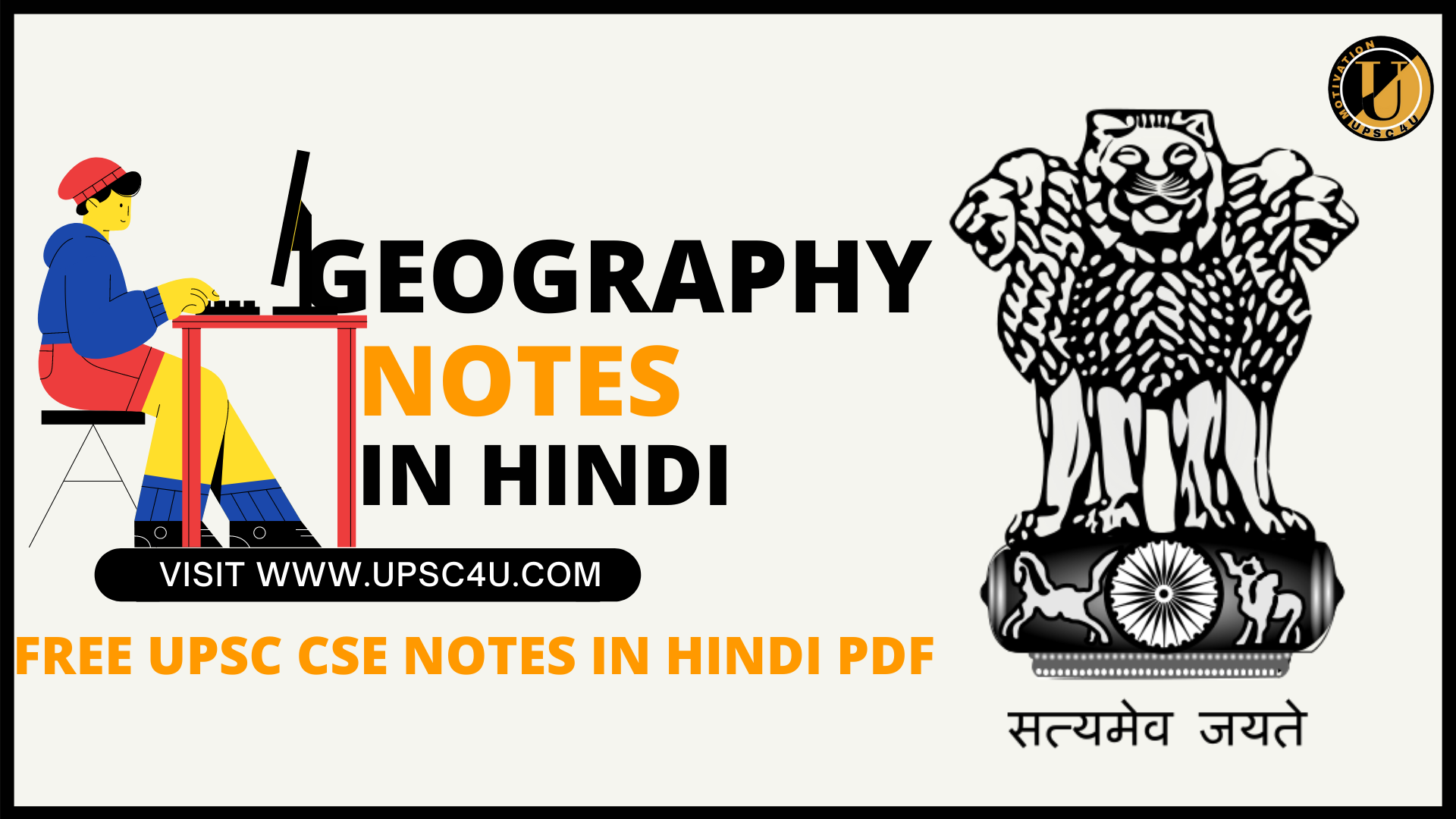भारत के प्रमुख उद्योग
उद्योग
औद्योगिक क्षेत्र
भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निम्नवत् हैं –
1. हुगली परिक्षेत्र (Hoogly Belt)
2. बाम्ब-पूना परिक्षेत्र (Bombay-Poona Belt)
3. अहमदाबाद-बड़ौदा परिक्षेत्र (Ahmedabad-Baroda Belt)
4. मद्रास-कोयम्बटूर-बंगलौर परिक्षेत्र (Madras-Combatour Region)
5. छोटानागपुर परिक्षेत्र (Chhota Nagpur Region)
6. मथुरा-दिल्ली-सहारनपुर-अम्बाला परिक्षेत्र .-(Mathura-Delhi-Saharanpur-Ambala Region)
लौह- इस्पात
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956-61 में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रमुख लौह-इस्पात कारखाने स्थापित किये गये है-
- हिन्दुस्तान स्टील लि. भिलाई (दुर्ग जिला, छत्तीसगढ)
- हिन्दुस्तान स्टील लि. राउरकेला (सुन्दरगढ़, उडीसा)
3. हिन्दुस्तान स्टील लि. दुर्गापुर (वर्धमान, प. बंगाल)
- तृतीय पंचवर्षीय योजना काल (1961-66) में झारखण्ड के बोकारो नामक स्थान पर एक नये कारखाने की आधारशिला रखी जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्पादन प्रारम्भ हुआ।
- आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम इस्पात संयंत्र देश का पहला ऐसा समन्वित इस्पात कारखाना है, जिसने ISO प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।
- कर्नाटक के बेलारी- विजयनगर इस्पात परियोजना
- तमिलनाडु के सलेम – सलेम
- देश में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
वायुयान उद्योगः-
- देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलुरू में ‘हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे ‘हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (HAL) के नाम से जाना जाता है।
- HAL की प्रमुख इकाइयांः
- नासिक शाखा जहां विमान बनते है।
- कोरापुट शाखा, जहां मिग का इंजन बनता है।
- हैदराबाद में मिग के इलेक्ट्रोनिक उपकरण बनते है।
- कानपुर जहां एचएस- 748 हवाईयान बनता है।
- लखनउ, वायुयान के उपकरण एवं औजार बनते है।
रेलवे उपकरणः-
- पहली कम्पनी झारखण्ड के सिंहभूम जिले में पेनिन्सुलर लोकोमोटिव कम्पनी के नाम से 1921 में स्थापित की गयी थी। इसको 1945 में टाटा समूह ने खरीद कर ‘‘टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी’ (टेल्को) नाम दिया।
- 1950 में प. बंगाल के मिहीजाम नामक स्थान पर चितरंजन लोको. वर्क्स की स्थापना की गयी। यहां 1961 से बिजली के इंजन बनाये जाने लगे।
- 1961 में डीजल लो. वर्क्स, मडुआडीह (वाराणसी) की स्थापना हुई। यहां रेल के डीजल इंजन बनाये जाते है।
- वर्तमान में रेल की पटरियों का निर्माण स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया IAS कंपनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
- रेल के वैगनों का निर्माण बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. भारत वैगन एण्ड इंजी. कंपनी लि., जेस्सप एण्ड कंपनी तथा ब्राथवैट एण्ड कं. भरतपुर में सिमकों।
- रेलवे की सवारी डिब्बों का निर्माणः
- इण्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर ‘चेन्नई’1955
- भारत अर्थ मूवर्स लि. बंगलुरू, जेस्सप एण्ड कंपनी लि. कोलकाता तथा रेलवे कोच फैक्टरी, कपूरथला, पंजाब
जलयान निर्माणः
- पहला कारखाना 1941 में मै. सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कं. द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके ‘हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम’ नाम दिया गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र में 3 इकाइयांः
- गार्डेनरिच वर्कशॉप, कोलकाता
- गोवा शिपयार्ड लि. कोचीन,गोवा ‘जापान के सहयोग से’
- मझगांव डाक मुम्बई, युद्धपेात निर्माण
प्रमुख उद्योग
जूट उद्योग
भारतीय जूट उद्योग विष्व विख्यात है । भारत में जूट उद्योग का आरम्भ 1855 में स्कॉटलैंड निवासी जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा हुगली के किनारे किया गया । जूट से टाट, बोरे, परदे, कालीन, दरियाँ गद्दे, वाटर प्रूफ कपड़े इत्यादि अनेक वस्तुएँ बनायी जाती हैं। जूट का प्रयोग प्लास्टिक, फर्नीचर, कम्बल, विद्युत निरोधक सामग्री तथा ऊन या कपास के साथ मिलाकर मिश्रित वस्त्र तैयार करने में होने लगा है ।
प. बंगाल में यह उद्योग सबसे अधिक विकसित है । अधिकांष कारखाने हुगली के दोनों किनारों पर लगभग 100 कि.मी. लम्बी तथा 3 कि.मी. चैड़ी पेटी में स्थित है । इस क्षेत्र में जूट उद्योग के विकसित होने के निम्न कारण हैं –
(i) गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने से परिवहन पर व्यय कम होता है, और जूट का रेषा आसानी से पहुँच जाता है ।
(ii) कारखानों को चलाने के लिए समीप ही रानीगंज तथा झरिया से कोयला मिल जाता है।
(iii) जूट को धोने और रंगने के लिए हुगली का जल मिल जाता है ।
(iv) इस क्षेत्र की नम जलवायु जूट की कताई तथा बुनाई के लिए सुविधाजनक है ।
(v) यह क्षेत्र पर्याप्त घना बसा है । इसलिए श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं ।
यह उद्योग अन्य राज्यों मे भी स्थापित किया गया है । उत्तर प्रदेष में जूट के कारखाने कानपुर में और गोरखपुर में हैं । आन्ध्र प्रदेष, मध्य प्रदेष, उड़ीसा, बिहार, असम और त्रिपुरा में भी कारखाने स्थापित हैं।
विदेषी बाजारों में बंगला देष व चीन के सस्ते माल तथा सिन्थेटिक रेषों की स्पर्धा के कारण भारतीय जूट उद्योग में निरन्तर गिरावट आ रही है ।
कई कारखाने बीमार व बन्द हो गये हैं । विदेषों में भारतीय जूट पदार्थों की मांग बहुत घट गयी है। जूट उद्योग को जीवित रखने के लिए विकल्पों पर ध्यान देना आवष्यक है ।
सूती वस्त्र उद्योग
कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा, संगठित एवं व्यापक उद्योग है, जो देष के औद्योगिक उत्पादन का 14 प्रतिषत, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिषत, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20 प्रतिषत व कुल निर्यातों क 30 प्रतिषत की आपूर्ति करता है, जबकि देष के कुल आयात खर्च में इसका हिस्सा केवल 7 है । यह उद्योग देष के लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है । कृषि क्षेत्र के साथ यह उद्योग करीब 9 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है । भारत इस क्षेत्र में चीन, बांग्लादेष और पाकिस्तान जैसे देषों के साथ प्रतियोगिता रखता है ।
भारत के आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन् 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, किन्तु यह मिल लक्ष्य प्राप्ति में सफल न हुई । द्वितीय मिल ‘बम्बई स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी’ सन् 1854 में बम्बई में ‘कवास जी. एन. डाबर’ द्वारा स्थापित की गई । सच्चे अर्थों में इस कारखाने ने भारत के आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी सन् 1854 के पश्चात् सूती कपड़ा मिलों की संख्या लगातार बढ़ती गई ।
प्रमुख सूत्री वस्त्र उद्योग केन्द्र – विष्व में सूती वस्त्र उद्योग में भारत का तृतीय स्थान है । परन्तु हमारे देष का यह सबसे बड़ा उद्योग है । हमारे देष में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं –
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पष्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेष, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेष, बिहार तथा कर्नाटक । इसके अतिरिक्त राजस्थान, देहली, पांडिचेरी, केरल इत्यादि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग स्थापित हैं । विदेषों में भारतीय रेड़ीमेड वस्त्रों की मांग काफी बढ़ रही है । कपड़े के कुल निर्यात में इसका योगदान लगभग 41 प्रतिषत है ।
सीमेन्ट उद्योग
भारत में सीमेन्ट उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना मद्रास में हुई । परन्तु आधुनिक विकास मध्य प्रदेष के सतना, कटनी एवं गुजरात के पोरबन्दर नामक स्थानों में सीमेन्ट कारखानों की स्थापना से प्रारम्भ होता है ।
सीमेन्ट उद्योग में 60 से 65 प्रतिषत चूना, 20 से 25 प्रतिषत सिलिका एवं 5 से 12 प्रतिषत एल्युमिना का उपयोग होता है । सामान्यतया एक टन सीमेन्ट तैयार करने के लिए 2 टन कच्चे माल की आवष्यकता होती है ।
सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग 60 प्रतिषत मात्र चार राज्यों में – क्रमषः मध्य प्रदेष, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेष एवं राजस्थान में होता है ।
लौह-इस्पात उद्योग (Iron and Steel)
वर्तमान युग का आधार लौह-इस्पात उद्योग है । लौह अयस्क अपनी प्राकृतिक दषा में आक्साइड के रूप में मिलता है जिसमें मिट्टी, गन्धक, फास्फोरस तथा अन्य खजिनों का मिश्रण होता है । मिट्टी गलाकर इन मिश्रणों को अलग-अलग करके उसमें कार्बन, मैगनीज आदि मिलकार इस्पात बनाया जाता है ।आधुनिक प्रकार का पहला सफल कारखाना सन् 1875 में कुल्टी बर्नपुर में लगाया गया था । परन्तु देष में इस उद्योग का आरंभ 1907 में तब हो पाया, जब जमषेद जी टाटा द्वारा सांकची नामक स्थान (वर्तमान जमषेदपुर) पर लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गयी ।
द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विदेषी तकनीकी की सहायता से तीन नए एकीकृत इस्पातल कारखाने भिलाई (रूस की मदद से), राउरकेला (जर्मनी की सहायता से) और दुर्गापुर (ब्रिटेन की मदद से) स्थापित किए गए । तीसरे योजनाकाल में बोकारो में एक अन्य इकाई स्थापित की गई । वर्तमान समय में देष में लौह-इस्पात के 9 बड़े कारखाने हैं, जिनमें से 8 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं । केवल टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी जमषेदपुर निजी क्षेत्र में है । सन् 1974 में सरकार ने स्टील एथारिटी आॅफ इंडिया की स्थापना करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जिम्मेदारी उसे दी थी । बड़े लौह-इस्पात के एकीकृत कारखानों के अलावा देष में 167 मिनी स्टील प्लांट भी कार्यरत हैं ।
भारत में भी इस उद्योग के स्थानीकरण पर कच्चे माल और कोयले की उपलब्धता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है । कुछ कारखाने कोयला पेटी में स्थित हैं; जैसे – कुल्टी बर्नपुर, बोकारो और दुर्गापुर के कारखाने । दूसरी ओर लौह अयस्क की सुविधा को ध्यान में रखकर भिलाई, राउरकेला, भद्रावती तथा संदुर जैसे कारखाने लौह-अयस्क क्षेत्रों के समीप लगाये गये हैं । टाटा का जमषेदपुर का कारखाना इन दोनों के मध्य स्थित है । इसी तरह विषाखापटट्टनम स्टील प्लांट भी लौह अयस्क और आयातित कोयले के परिवहन को ध्यान में रखकर बंदरगाह पर स्थापित किया गया है । इस उद्योग में लगभग 90 हजार करोड़ रूपये की पूंजी लगी हुई है । इसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है ।
चीनी उद्योग
इस उद्योग में का भारत में प्रथम स्थान है। यहीं सम्पूर्ण राष्ट्र की लगभग एक तिहाई चीनी उत्पन्न होती है । यहाँ चीनी मिलों का स्थानीयकरण उत्तर में मनमाड़ से कोल्हापुर तक पतली पट्टी में हुआ है।
सम्पूर्ण राष्ट्रीय चीनी उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेष का सापेक्षिक महत्त्व गिरा है । वस्तुतः यहाँ चीनी मिलें अत्यधिक पुरानी एवं अनार्थिक हो गयी हैं । उत्तर प्रदेष की चीनी मिलें दो क्षेत्रों में क्रमषः तराई क्षेत्र एवं गंगा-यमुना दोआब में केन्द्रित है।
तमिलनाडु भी भारत का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है । इसका महत्त्व विगत वर्षों में अधिक बढ़ा है । अधिकांष मिलें तिरुचिरापल्ली, मदुराई एवं कोयम्बटूर जिलों में केन्द्रित हैं ।
चीनी उद्योग की समस्याएँ
1. चीनी मिलों द्वारा कुल गन्ना उत्पादन का एक छोटा-सा भाग ही प्रयुक्त कर पाना ।
2. प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता ।
3. उत्तम किस्म के गन्ने की कमी ।
4. उत्पादन लागतों में वृद्धि ।
5. मिलों के आधुनिकीकरण की समस्या ।
6. मौसमी उद्योग ।
7. अनुसंधान की कमी ।
8. चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने के मूल्य का पूरा-पूरा भुगतान न कर पाना ।
रासायनिक उर्वरक उद्योग
रासायनिक उर्वरक कारखाने के लिए प्रमुख कच्चा माल नेप्था है, जो तेल शोधन कारखाने से प्राप्त होता है । अतः इस कारखाने की स्थापना वहीं होती है, जहाँ नेप्था या तो उपलब्ध हो या नेप्था आयात करने की सुविधा हो । वस्तुतः नेप्था एक शुद्ध पदार्थ है जिसकी उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता । अतः परिवहन की सुविधा रहने पर कहीं भी इस उद्योग की स्थापना हो सकती है । नेप्था के अतिरिक्त लौह इस्पात कारखानों का अपषिष्ट पदार्थ भी कच्चा माल है, जिससे अमोनियम सल्फेट उर्वरक प्राप्त होता है । फास्फेट युक्त खाद बनाने के लिए फास्फेट खनिज का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका उत्पादन मात्र मध्य प्रदेष, राजस्थान (66.4 प्रतिषत) एवं उत्तर प्रदेष (14.9 प्रतिषत) में होता है ।
भारत में उर्वरक उद्योग अत्यन्त नवीन है । इसका आधुनिक तकनीकी पर आधारित सर्वप्रथम कारखाना सिन्द्री (झारखण्ड) में 1951 में लगा था । भारतीय उर्वरक निगम देष की महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसने सिन्द्री, ट्राम्बे, नांगल, गोरखपुर, नामरूप एवं दुर्गापुर, बरौनी, तालचर एवं कारेबा में रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना का कार्य किया है ।गुजरात एवं तमिलनाडु इस उद्योग में अग्रणी हैं । ये दोनों संयुक्त रूप से 68 प्रतिषत फास्फेट उर्वरक एवं 28 प्रतिषत नाइट्रोजन उर्वरक तैयार करते हैं ।
गुजरात देष का वृहत्तम नाइट्रोजन (25.2 प्रतिषत) उर्वरक उत्पादक एवं फास्फेट उर्वरक 25.6 प्रतिषत) उत्पादक राज्य है । बड़ोदरा उर्वरक कारखाने से नाइट्रोजन एवं फास्फेट दोनों का उत्पादन होता है।
पंजाब में उर्वरक के दो कारखाने (नाइट्रोजन उर्वरक) नांगल एवं भटिण्डा में हैं। महाराष्ट्र का एक मात्र कारखाना ट्राम्बे में है । बिहार में उर्वरक के कारखाने बरौनी एवं सिन्द्री में हैं । भारत का उत्पादन घरेलु उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है एवं आयात की मात्रा विभिन्न वर्षों में क्रमषः बढ़ती गयी है । उर्वरक का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, कनाड़ा, पोलैण्ड एवं नीदरलैण्ड तथा पूर्वी यूरोपीय देषों से होता है । उत्पादन एवं उपभोग के अनुपात से स्पष्ट है कि भारत आगामी वर्षों में भी आयातक बना रहेगा ।
पेट्रो-रसायन
पेट्रो-रसायन प्राकृतिक गैस तथा नेप्था जैसे पेट्रोलियम पदार्थों से तैयार किये जाते हैं । ऐलकहॉल एवं कैल्सियम कार्बाइड से भी इन्हें निकाला जाता है । सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ोदरा में भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि. (IPCL) द्वारा एक विषाल पेट्रो रसायन काम्पलेक्स की स्थापना की गयी है । बोंगाई गाँव (असम) में एक अन्य काम्पलेक्स स्थापित कया गया है ।
पेट्रो रसायन उद्योगों के अन्तर्गत विविध प्रकार के महत्त्वपूर्ण पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है । इलेक्ट्रनिक्स, आटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, हाउसिंग तथा पैकिंग आदि में भी पेट्रोरसायन उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है ।
मोटर निर्माण उद्योग
भारत में मोटर उद्योग का आरम्भ 1928 में बम्बई में ‘जनरल मोटर्स कम्पनी’ के रूप में हुआ, जहाँ विदेषी पुर्जों को जोड़कर मोटरें बनाई जाती थीं । 1944 में हिन्दुस्तान मोटर्स लि. कलकत्ता एवं प्रीमियर मोटर्स लि. बम्बई द्वारा कुछ विदेषी पुर्जे बनाकर मोटर बनाने का कार्य आरम्भ किया गया । 1949 में विदेषी पुर्जों के आयात पर भारी कर लगाने पर भारत में ही अधिकांष पुर्जे भी बनाये जाने लगे ।
टाठवें दषक में हरियाण के गुड़गाँव में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना से कार निर्माण उद्योग में एक क्रान्ति आई । वर्तमान में जापान एवं कोरिया की अनेक कम्पनियाँ कार निर्माण में प्रवेष कर गईं हैं, और अब यह भारत के मध्यम वर्ग की एक आवष्यकता बन गई है । यहाँ तक कि अब भारत में निर्मित कारें केवल विकासषील देषों का ही नहीं, बल्कि इंग्लैण्ड जैसे विकसित देषों को (इंडिका कार) निर्यात की जा रही हैं ।
रेशम उद्योग
आदिकाल से ही रेषम भारत का प्रमुख उद्योग रहा है । वर्ष 1999-2000 में देष में कुल रेषम उत्पादन में से मलबरी किस्म के रेष का उत्पादन 91.7:, इरी रेषम का 6.4:, टसर रेषम का 1.4: तथा मूंगा किस्म की रेषम का उत्पादन 0.5: था । रेषम व्यवसाय कृषि पर आधारित गृह उद्योग है । वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 64 लाख लोग इस उद्योग के जरिए अपनी आजीविका चला रहे थे । चीन के बाद भारत विष्व में प्राकृतिक रेषम उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देष है । भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेषमी वस्त्रों का हिस्सा लगभग 3: है । 2001-2002 के दौरान 433.39 मिलियन डॉलर मूल्य के रेषमी वस्त्रों का निर्यात किया गया ।
विष्व में रेषम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारम्भ हुआ । भारत में भी रेषम का उत्पादन प्राचीन युग से होता आ रहा है ।विष्व के कुल रेषम उत्पादन का लगभग 16: रेषम भारत में उत्पन्न होता है । भारत के मुख्यतः 5 राज्यों – कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेष, तमिलनाडु, पं. बंगाल तथा जम्म-कष्मीर में अधिकांष रेषम का उत्पादन होता है । देष के कुल रेषम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है । नए किस्म के रेषमों का सर्वाधिक उतपादन मणिपुर एवं जम्मू-कष्मीर के पठारी क्षेत्रों में किया जा रहा है ।
रेषम उद्योग के विकास हेतु सरकारी प्रयत्न – भारत में रेषम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 1949 में केन्द्रीय रेषम बोर्ड की स्थापना की गई । केन्द्रीय रेषम अनुसंधान प्रषिक्षण संस्थान की स्थापना मैसूर (कर्नाटक) एवं बरहमपुर में की गई है । केन्द्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान मेन्द्रीपाथर (मेघालय) में एवं केन्द्रीय टसर अनुसंधान प्रषिक्षण संस्थान रांची (झारखण्ड) में स्थापित किए गए हैं । इसको और व्यापक बनाने के लिए 13 स्थानों पर क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेषन स्थापित किए गए हैं ।
रत्न एवं आभूषण उद्योग
रत्न एवं आभूषण उद्योग भारत में निर्यातोन्मुखी उद्योग की एक उल्लेखनीय सफलता है । इस क्षेत्र में भारत अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन श्रृंखलाओं से भली प्रकार से जुड़ा है, जहाँ विदेष से कच्चा माल आता है, भारत में मूल्यवर्धन किया जाता है और पुनः निर्यात किया जाता है । देष के कुल निर्यातों में रत्नों और आभूषणों के निर्यातों का हिस्सा 16 से 20 प्रतिषत के बीच है । वित्तीय वर्ष 2002-03 में भारत सरकार ने रत्नों और आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं ।
केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेष में हीरों एवं अन्य बहुमूल्य खनिजों के अन्वेषण के लिए अनेक कम्पनियों को अनुमति दी । केन्द्र ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेष और उड़ीसा में बहुमूल्य रत्न खनन के क्रियाकलापों को तेज करने के लिए अपनी योजनाओं की भी घोषणा की है ।
सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से अपरिष्कृत हीरों के आयात को लाइसेंस मुक्त कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप भारत में अपरिष्कृत हीरों का आयात सम्पूर्ति/हीरा अग्रदाय लाइसेंसों की आवष्यकता या उपयोग के बिना भी सम्भव हो सकता है । नई निर्यात-आयात नीति में बहुमूल्य धातु आभूषणों के निर्यात के संदभ्र में मूल्य आधारित सम्पूर्ति नीति की समाप्ति हुई ।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी उद्योग भारत ने इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में जबर्दस्त प्रगति की है । वर्ष 1996-97 से 2001-02 तक इस उद्योग का तिगुने से भी अधिक विकास हुआ है । सॉफ्टवेयर निर्यात भारत के निर्यात और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं । सॉफ्टवेयर में भारत की सफलता मानव पूँजी में सरकारी निवेष, नीतियों को बहिर्मुखी बनाने और एक उच्च प्रतियोगी निजी क्षेत्रक उद्योग की आधारषिलाओं पर निर्मित की गई है ।
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख उद्योग – सोना, तांबा, पायराइट्स, रॉक साल्ट, माइका, जिप्सम आदि
मणिपुर के प्रमुख उद्योग – हथकरघा, रेशम उत्पादन, बांस, आदि
मिजोरम के प्रमुख उद्योग – बांस तथा इमारती लकडी के उत्पाद, वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि
सिक्किम के प्रमुख उद्योग – कलाई घडी, फलों के जैम, बियर, माचिस, चाय उद्योग आदि
हरियाणा के प्रमुख उद्योग – सीमेंण्ट, चीनी, कागज, सूती कपडा, टेलीविजन, कॉच, पीतल अादि
मेघालय के प्रमुख उद्योग – कोयला, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, चूनापत्थर आदि
पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योग – इलेक्ट्रॉनिक मोटर, रासायनिक पदार्थ, दवाइयॉ, चमडा आदि
पंजाब के प्रमुख उद्योग – कपड़ा, सिलाई मशीन, खेल के समान, बिजली की मशीनें, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग
नागालैंड के प्रमुख उद्योग – बांस, बागवानी, रेशम उत्पादन, खनिज और खनन आदि
दिल्ली के प्रमुख उद्योग – औषधि, रासायनिक पदार्थ, वस्त्र, टेलीविजन सेट आदि
तमिलनाडु के प्रमुख उद्योग – सूती कपडा, चमडा, सीमेंट, कागज, माचिस, ऑटोमोबाइल आदि
तेलंगाना के प्रमुख उद्योग – ऑटो पुर्जा, औषधियां, मसाले और मुर्गी पालन आदि
बिहार के प्रमुख उद्योग – चीनी, सूतीवस्त्र, रेशम, जूट, तम्बाकू, चमडा आदि
झारखंड के प्रमुख उद्योग – इस्पात, ऐल्युमिनियम, तॉबा, जस्ता, मोटरगाडी, रसायन आदि
जम्मू कश्मीर के प्रमुख उद्योग – कागज की लुगदी से बनी वस्तुएं, लकडी की नक्काशी, कालीन आदि
छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग – इंजीनियरिंग कारखाने, इस्पात फाउंड्री, कृषि व वन आधारित लधु उदयोग आदि
गोवा के प्रमुख उद्योग – कृषि व लघु उद्योग, सी फूड निर्यात, आम की विशेष किस्मों को उत्पादन
गुजरात के प्रमुख उद्योग – रसायन, पेट्रो रसायन, दुग्ध उत्पाद, उर्वरक, सूती वस्त्र उद्घोग, नमक आदि
केरल के प्रमुख उद्योग – शीशम, काजू, चाय, समुद्री उत्पाद, हथकरघा, नारियल जटा तथा हस्तशिल्प आदि
कर्नाटक के प्रमुख उद्योग – सोना, लौह खनिज, तांबा, मैंगनीज, चूना पथ्थर, क्रोमाइट आदि
ओडिशा के प्रमुख उद्योग –स्टील, एलुमिनियम, पावर, आईटी आदि
आंध्र प्रदेश के प्रमुख उद्योग – खान और खनिज, ऑटो कलपुर्जे, रत्न और आभूषण, कपडा, चमडा आदि
असम के प्रमुख उद्योग – चाय, कोयला, तेल, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण आदि
अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उद्योग – चाय, प्लाईवुड, फल, आरा मिलें, साबुन, हथकरघा, दस्तकारी आदि
राजस्थान के प्रमुख उद्योग – वस्त्र, सीमेंट, शीशा, चीनी, कीटनाशक, संगमरमर, कृत्रिम रेशम, उर्वरक आदि
उत्तराखंड के प्रमुख उद्योग – खनन, जडी-बूटी, चूना पथ्थर, पर्यटन, आदि
उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग – वस्त्र उद्योग, चीनी, चूड़ी, चमडा, साईकिल, क़ालीन आदि
इस उद्योग की एक अनूठी विषेषता इसका निर्यातोन्मुखी होना है । पिछले पाँच वर्षों के दौरान से सॉफ्टवेयर निर्यातें में प्रतिवर्ष 50 प्रतिषत से अधिक की मिश्रित वृद्धि दर से विकास हुआ है ।