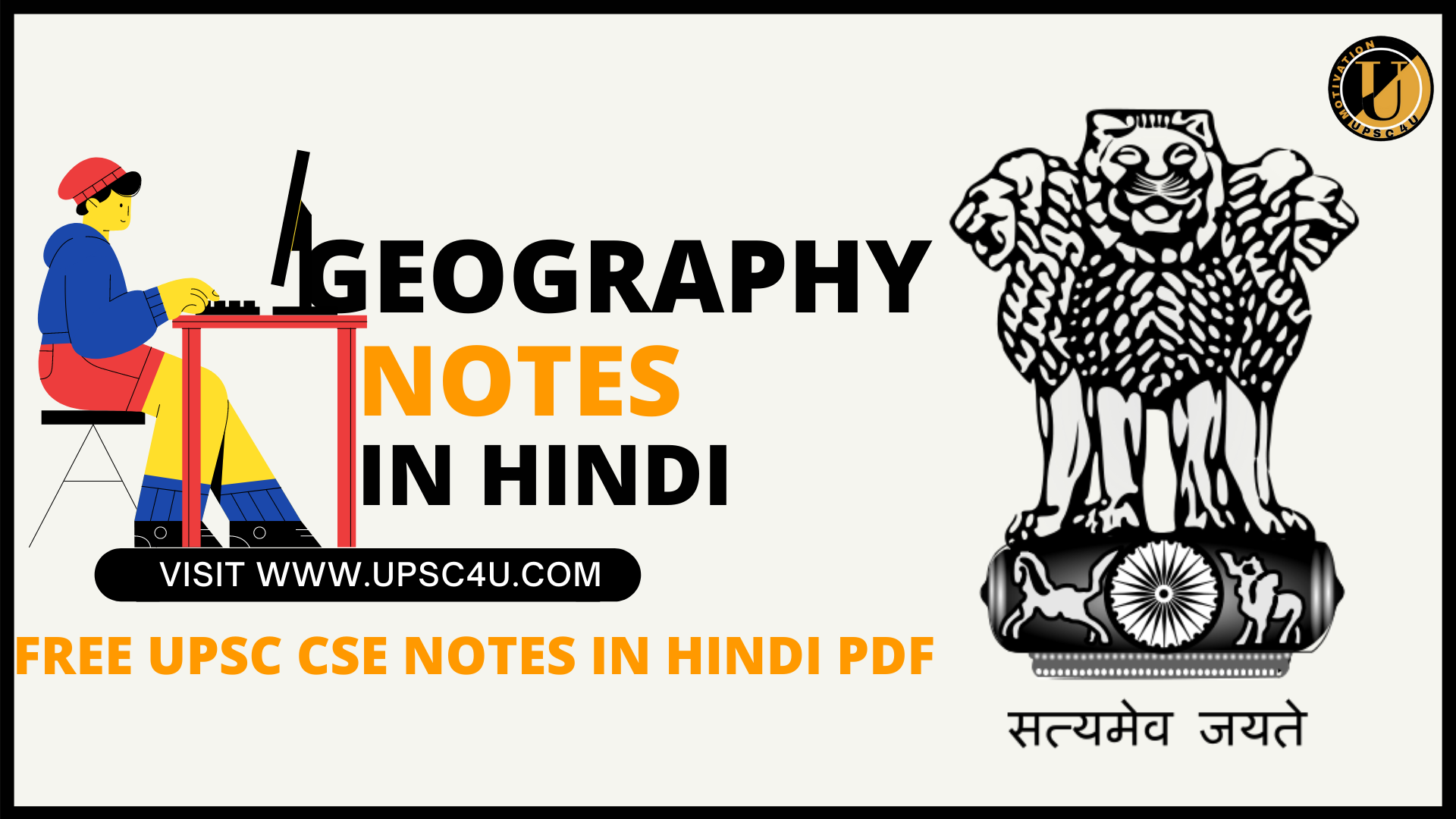विद्यमान सिंचाई क्षमता से जुड़ी समस्याएं
सिंचाई के क्षेत्र में मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं:
सिंचाई क्षमता का व्यापक अनुप्रयोग: बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का अनुप्रयोग निरंतर जारी है। इसके निम्नलिखित कारण विद्यमान हैं:
- क्षेत्रीय चैनलों के निर्माण तथा भू-समतलीकरण में होने वाला विलंब और बाड़बंदी प्रणाली को अंगीकार करना।
- नई फसल प्रणाली को अपनाने में किसानों द्वारा की जाने वाली देरी।
1974-1975 में केंद्र सरकार द्वारा एक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। जिसमें कृषि भूमि के विकास, किसानों के प्रशिक्षण व प्रदर्शन तथा उपयुक्त फसल प्रणाली के चुनाव पर बल दिया गया था।
सिंचाई जल का अपव्यय: इस प्रकार का अपव्यय अतिसिंचाई, अवकर्षण (नहरों के माध्यम से) तथा भूमिगत एवं सतही जल के मध्य उचित संतुलन के अभाव आदि कारणों से होता है। जल के अपव्यय को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है:
- उचित प्रशुल्क संरचना को सुनिश्चित करना तथा अतिसिंचाई को रोकने हेतु अन्य कड़े प्रावधान करना।
- अवकर्षण रोकने के लिए नहरों के उपयुक्त सीमांत बनाना।
- सिंचाई सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु किसानों को प्रशिक्षित करना।
- सिंचाई के सभी स्रोतों (कुंए, नहर व तालाब) के मध्य समन्वय स्थापित करना।
अत:फसल असमानता: एक ओर अनाज फसलों के कुल फसल क्षेत्र का 38 प्रतिशत तथा कपास का 30 प्रतिशत भाग सिंचित भूमि के अंतर्गत आता है, वहीं दूसरी ओर दाल एवं तिलहन फसलों के कुल फसल क्षेत्र का क्रमशः 9.2 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत हिस्सा ही सिंचाई लाभ सुविधाओं को प्राप्त कर पता है। उक्त असमानता को कम करके ही सिंचाई क्षमता का सम्पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है।
राज्य सरकारों की वाणिज्यिक हानियां: सिंचाई शुल्क की दर्रे राज्य सरकारों द्वारा वसूली जाती है। इन दरों में सिंचाई योजनाओं की कार्यपरक लागतों को भी शामिल नहीं किया जाता है। सिंचाई में निवेश करने के लिए भी राज्यों को उचित प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के विद्युत बोडों द्वारा भी सिंचाई हेतु रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाती है, जिससे भारी घाटा उठाना पड़ता है।
शक्ति (पॉवर)
विद्युत या शक्ति की उपलब्धता कृषि विकास के लिए अनिवार्य है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्य अपनी शक्ति क्षमता का क्रमशः 30 और 40 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में खर्च करते हैं और इसी कारण भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि प्रदेशों में गिने जाते हैं।
शक्ति का उपयोग सिंचाई तथा अन्य कृषि संबंधी कार्यो-कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण आदि में किया जाता है। शक्ति, कृषि उत्पादकता के साथ-साथ भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमताओं में भी वृद्धि करती है।
भाखड़ा-नांगल परियोजना से शक्ति प्राप्त करने के बाद ही पंजाब एवं हरियाणा की कृषि क्षमता का विकास संभव हुआ। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के काली मिट्टी क्षेत्र में भी शक्ति के विकास ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने हेतु 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गयी।
उर्वरक
स्वतंत्रता के उपरांत परम्परागत उर्वरक संसाधनों के प्रभावी एवं समग्र उपयोग हेतु अनेक प्रयास किये गये, जैसे-
- गोबर का ईंधन की अपेक्षा खाद के रूप में प्रयोग करना;
- फार्मयार्ड खाद के लिए अधिक प्रभावी व्यवस्था करना;
- खेत बंधों के साफ लगे पेड़ों से हरित खाद प्राप्त करना;
- हड्डियों एवं अन्य पशु उत्पादों का खाद के रूप में उपयोग करना;
- शहरी ठोस कचरे से कॉम्पोस्ट खाद का उत्पादन करना;
- तालाब तलहटी या नहर से प्राप्त गाद;
- शहरी मल निपटान योजनाओं को हाथ में लेना;
- प्रभावी फसल चक्र (जैसे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु फलीदार पौधों का उपयोग) अपनाना, तथा;
- भूमि को कुछ समय के लिए परती छोड़ना, ताकि उसकी उर्वरता पुनः प्राप्त की जा सके।
फिर भी रासायनिक खाद का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य बन चुका है:
- ईंधन लकड़ी का अभाव तथा गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में व्यापक प्रयोग।
- पेड़-पौधों की निरंतर कमी के कारण हरित खाद की त्वरित उपलब्धता का अभाव।
- तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु भूमि पर पड़ रहे भारी दबाव के कारण भूमि को परती छोड़ने के विकल्प का चुनाव असंगत होता है।
- खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ती जरूरत तथा उनकी उच्च उत्पादकता को रासायनिक खादों के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त करना संभव है।
- उर्वरक सिंचित भूमि में ही अच्छे परिणाम देते हैं, अतः सिंचित भूमि के विस्तार के साथ-साथ उर्वरकों का प्रयोग भी बढ़ता जाता है।
- बीजों की उच्च उत्पादक किस्मों, जिनके प्रयोग में 1960 के दशक के उपरांत निरंतर वृद्धि हुई हैं, ने रासायनिक खादों के साथ मिलकर आशानुकूल परिणाम दिये हैं।
उर्वरकों के प्रयोग के प्रभाव: एक अनुमान के अनुसार रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग सम्पूर्ण कृषि वृद्धि के 70 प्रतिशत हेतु उत्तरदायी है। प्रत्येक एक टन खाद के प्रयोग से 8 से 10 टन खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि होती है। उर्वरकों की उच्च खपत वाले राज्यों में कृषि का विकास तीव्र गति से हुआ है।
फसल की पैदावार में वृद्धि के लिए तीन प्राथमिक पोषकों- नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P) और पोटाश (K) का उचित मिश्रण या अनुपात बेहद आवश्यक है। देश के लिए एक आदर्श N:P:K मानक 4:2:1 है, लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में यह मानक अपनाया नहीं गया है। अगस्त 1992 तक फास्फेटिक और पोटाश युक्त उर्वरकों का स्तर पूरे देश में लगभग आदर्श स्तर पर था, लेकिन तत्पश्चात् इनके विनियंत्रण से इसमें तीव्र विचलन दर्ज किया गया।
उर्वरकों के प्रयोग की सीमित करने वाले कारण: उच्च उत्पादक बीज किस्मों का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों एवं फसलों में भी उर्वरकों की निर्धारित मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
- देश के कुल फसल क्षेत्र का आधे से अधिक भाग न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने के कारण उर्वरकों की सीमित मात्रा का अवशोषण ही कर पाते हैं।
- उर्वरकों की आपूर्ति अपर्याप्त होती है और वे उचित समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते।
- संवर्धक उपाय एवं प्रदर्शन पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं।
- छोटे एवं सीमांत किसान कीमती उर्वरकों का व्यय-भार नहीं उठा पाते।
- अपर्याप्त मृदा परीक्षण सुविधाओं के कारण किसानों को मृदा की वास्तविक कमियों की जानकारी नहीं हो पाती।
- अनेक किसान उर्वरकों के प्रयोग को जोखिमपूर्ण मानते हैं।
- पोटॉश उवरंकों को पूरी तरह से आयात किया जाता है। पोटॉश खनिज भंडारों के अभाव के कारण घरेलू उत्पादन नहीं होता है। फॉस्फेट उवर्रकों के सम्बंध में घरेलू उत्पादन विदेशों से आयातित रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल पर आधारित है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट के घरेलू भंडार सीमित एवं निम्न कोटि के हैं। इससे रासायनिक उवरंकों की मंहगी प्रकृति का स्पष्टीकरण होता है।
उर्वरकों के इस्तेमाल में गतिरोध को हटाने के सरकार द्वारा किए गए उपाय: सरकार केंद्र समर्थित एक योजना उर्वरकों का संतुलित एवं समन्वित उपयोग कार्यान्वित कर रही है जिससे परीक्षण के आधार पर जैविक खाद और जैव उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों का न्यायसंगत अनुप्रयोग लोकप्रिय होगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों के अनुप्रयोग पर परामर्श के लिए नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए वित्त मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल पर प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण और शहरी अपशिष्ट से उपयोगी जैविक खाद के उत्पादन पर भी वित्तीय मदद उपलब्ध करा रहा है।
रासायनिक उर्वरकों के महंगे होने का बोध कराकर भी जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खाद सामान्य रूप में पौधों से, पशु मल, शहरी और ग्रामीण कम्पोस्ट, हरी खाद सीवर की कीचड़, बायोगैस तथा अपशिष्ट जल इत्यादि से पोषक तत्व प्राप्त करती है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं जो या तो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं या अन्य पोषकों की पहुंच में वृद्धि करते हैं, विशेष रूप से फॉस्फेट की। ये नाइट्रोजन की आपूर्ति में वृद्धि करते हैं तथा फॉस्फेट की उपलब्धता में थोड़ी मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं। नाइट्रोजन स्थरीकरण वाले बेहद महत्वपूर्ण जैव उर्वरक- राइजीबिया, एजोरपिरिलम, नील-हरित शैवाल (साइनोबैक्टीरिया) और बीजीए-एंजोला संयोजन हैं। राइजीबिया लैगूमस के साथ जैसे तिलहन एवं दलहन में नाइट्रोजन स्थिर करता है। नील हरित शैवाल (बीजीए) और एजोला चावल को नाइट्रोजन आपूर्ति में वृद्धि करते हैं।
बीज
बीजों की उच्च पैदावार किस्मों ने पूरे विश्व में कृषि आर्थिकी में उल्लेखनीय सुधार किया, जिसे जैव-क्रांति कहा गया। उच्च पैदावार के बीजों के प्रयोग ने कृषि रणनीति में मुख्य तत्वों को शामिल किया। उच्च पैदावार किस्मों (एचवाईवी) को बड़े पैमाने पर 1967-68 में प्रस्तुत किया गया जिन्होंने 75 मिलियन हेक्टेयर तक का क्षेत्र शामिल किया। इनका उत्पादन 1950 में शून्य स्तर से 2003-04 में 100 लाख क्विंटल हो गया।
उन्नत बीजों के प्रयोग में वृद्धि हेतु सरकारी प्रोत्साहन: उन्नत बीजों के वितरण एवं उत्पादन हेतु एक त्रि-स्तरीय संगठनात्मक ढांचा निर्मित किया गया है:
- संकर बीज: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में इन बीजों का संकरण सम्पन्न किया जाता है।
- आधारभूत बीज: संकर बीजों से राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य कृषि निगम एवं राज्य बीज निगमों द्वारा आधारभूत बीज तैयार किये जाते हैं।
- प्रमाणित बीज: ये बीज वाणिज्यिक उत्पादन हेतु निकाले जाते हैं। भारतीय बीज कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी शामिल हैं। भारत में बीज क्षेत्र में दो राष्ट्रीय स्तर के निगम शामिल हैं- राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राजकीय कृषि निगम, राजकीय बीज निगम और बीज कंपनियां। गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन के लिए राजकीय बीज प्रमाणन एजेंसियां और राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। निजी क्षेत्र ने बीजों के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की है, हालांकि संगठित बीज क्षेत्र विशेषज्ञ रूप से खाद्य फसलों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व अब भी जारी है।
उन्नत बीजों की कमजोरियां:
- ये बीज उस भौतिक पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, जिसमें इन्हें प्रयोग किया जाता है।
- सामान्य स्रोतों से प्राप्त बीजों के व्यापक प्रयोग से जैव-विविधता को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण अनेक वनस्पति रोग जन्म ले लेते हैं।
- इन बीजों को मंहगें आगतों (उर्वरक एवं सिंचाई आदि) के साथ प्रयोग किये जाने पर ही आशानुकूल परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- उन बीजों के कारण कृषि विकास के सम्बंध में क्षेत्रीय असमानता का उभार हुआ है।
- अंतरफसलीय असमानता का भी जन्म हुआ है, क्योंकि दालों एवं तिलहन फसलों में उन्नत बीजों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया गया है।
- उन्नत बीजों का विकास, बहुगुणन, परीक्षण एवं वितरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा विस्तार सेवाएं भारतीय कृषि की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर पाने में असमर्थ रही हैं।
कृषि उपकरण एवं यंत्रीकरण
कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन के लिए, मानवीय, पशु एवं यांत्रिक/विद्युत ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य के साथ सरकार की रणनीति एवं कार्यक्रम पर्यावरण अनुकूल एवं चुनिंदा कृषि उपकरण के प्रोत्साहन को लेकर निर्देशित की गई। साथ ही इसमें भूमि एवं श्रम की उत्पादकता वृद्धि, आगतों का दक्षतापूर्वक उपयोग (बीज, उर्वरक, कीटनाशक, एवं सिंचाई जल), उपकरण प्रोत्साहन द्वारा खेती करने की गुणवत्ता में सुधार तथा इनके द्वारा उत्पादन की लागत घटाना शामिल किया गया।
कृषि उपकरणों को संशोधित बनाने, किसानों को अपने ट्रैक्टर, पावर पिलर, हारवेस्टर और अन्य मशीने खरीदने में समर्थ बनाने, कस्टम हायर सेवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन विकास की समर्थन सेवाएं, परीक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास के जरिए पारंपरिक एवं अदक्ष उपकरणों को बदलने के लिए रणनीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कृषि मशीनों के निर्माण के लिए व्यापक उद्योग आधार भी विकसित किया गया है। सांस्थानिक क्रेडिट के अलावा विस्तार एवं प्रदर्शन के जरिए तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों को भी प्रस्तुत किया गया है। संसाधन संरक्षण के लिए उपकरण भी किसानों द्वारा अपनाये जा रहे हैं।
कृषि ऋण
सरकार ने कृषि क्षेत्र की संसाधन जरूरतों को समर्थन देने के लिए किफायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते कृषि क्रेडिट डिलीवरी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नीतिगत प्रयास किए हैं। इन नीतियों में किसानों को पर्याप्त क्रेडिट सहायता समय पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है और छोटे तथा सीमांत किसानों और समाज के कमजोर तबकों को आधुनिक तकनीक अपनाने तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती की उन्नत विधियों के इस्तेमाल को समर्थ बनाने पर विशेष थ्यान दिया जा रहा है। इस नीति में अनिवार्य रूप से क्रेडिट नियोजन, क्षेत्र विशेष से संबंधित रणनीति अपनाने और ऋण देने की नीतियों और प्रक्रियाओं को तार्किक बनाने तथा कृषि ऋण पर ब्याज दर को कम करने के जरिये वास्तविक स्तर पर ऋण का प्रवाह बढ़ाने पर बल दिया गया है।
कृषि ऋण मल्टी एजेंसी नेटवर्क के जरिए विरित किया जाता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। सहकारी बैंक देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने और व्यापक कवरेज हासिल करने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। सहकारी ऋण संस्थाएं लघु और दीर्घावधि संरचना के तहत कृषि ऋण प्रदान करने वाली मुख्य संस्थानिक एजेंसी है।
संस्थात्मक कारक
भू-सुधार: जमीदारी भू-धारण प्रणाली का आरंभ कार्नवालिस ने बंगाल में वर्ष 1793 में किया था। जमींदारी भू-धारण प्रणाली मुख्यतः राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी परंतु इसकी लागू करने का उद्देश्य अधिक व्यापक था। इस समय तक ब्रिटिश सत्ता पूर्ण रूप से भारत में स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाई थी और यही कारण था कि अंग्रेज एक ऐसे वर्ग का सृजन करना चाहते थे जिसके हित अंग्रेजों से जुड़े हों। इसके साथ ही अंग्रेजों को इस समय भारतीय व्यापारियों से व्यापार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों द्वारा जमीदारी भू-धारण प्रणाली लागू करना वास्तव में अंग्रेजी आदर्शो को भारत में लागू करने का एक प्रयास था।
जमींदारी प्रथा के अंतर्गत भू-स्वामी न तो राजा को ही माना गया और न ही जोतदार को, बल्कि जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना गया। भारत में जमीदारी भू-धारण न ही प्राचीन काल में और न ही मध्यकाल में प्रचलन में थी।
अंग्रेजों ने जमीदारी भू-धारण प्रणाली को दो रूप में लागू किया था- स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान स्थायी रूप से सुनिश्चित कर दिया गया था और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भविष्य में नहीं होना था। इस प्रणाली को बंगाल, उत्तरी मद्रास और बनारस में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान को अस्थायी रूप से सुनिश्चित किया गया था और इसे 20-40 वर्ष बाद बढ़ाया जा सकता था। अस्थायी बंदोबस्त को अवध में लागू किया गया था। इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत जमीदारों हेतु एकमात्र शर्त थी, समय पर भू-लगान की राशि जमा करना। इसके लिए जमींदारों को 1799 व 1812 में कानून पारित कर विशेष अधिकार प्रदान किये गये।
महलवाड़ी भू-धारण प्रणाली के अंतर्गत भू-राजस्वकी इकाई महल (ग्राम) को माना गया। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी ग्राम समुदाय को संयुक्त रूप से माना गया। भू-लगान को ग्राम समुदाय के सदस्य संयुक्त रूप से या अलग-अलग देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस प्रणाली को आगरा, पंजाब और अवध में लागू किया गया था।
रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भू-लगान का निर्धारण सीधे भूमि के स्वामी से किया गया था। भू-स्वामी व्यक्तिगत रूप से भू-लगान जमा करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी प्रणाली हिंदू परंपरा पर आधारित थी। इस प्रथा को बम्बई, बरार और मध्य भारत में लागू किया गया था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र गंभीर समस्याओं से ग्रस्त था। एक ओर बड़ी रियासतें और बड़े भू-भाग के अधिकारी, अल्पसंख्यक भू-स्वामी वर्ग थे तो दूसरी ओर बहुसंख्यक भूमिहीन खेतिहर और स्वेच्छाचारी काश्तकार थे। सही-सही राजस्व अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण कृषि क्षेत्र से बिचौलियों के उन्मूलन में विशेष कठिनाइयां थीं। उचित राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता ने संपूर्ण जोत गणना की आवश्यक कर दिया था।
भू-सुघार उपाय: स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा भूमिं सुधार हेतु प्रमुखतः निम्नलिखित कदम उठाए गए-
बिचौलियों की समाप्ति: कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की उपस्थिति और उनके हानिकारक प्रभावों की समझ लिया गया था इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात राज्य विधानसभाओं ने इनकी समाप्ति के लिए अधिनियम पारित किये। बिचौलियों की समाप्ति से सम्बंधित प्रथम अधिनियम मद्रास में 1948 में पारित किया गया था। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र व बंबई में कानून बनाये गये। वर्तमान में सभी राज्यों में इस प्रकार के अधिनियम प्रभावी हैं।
काश्तकारी सुधार: काश्तकारों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- प्रथम, वे हैं जिनके काश्तकारी अधिकार स्थायी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्राप्त होते हैं। वास्तव में ये जमींदार को लगान अदा करने वाले छोटे भू-स्वामी ही हैं। दूसरे, इच्छाधीन काश्तकार होते हैं, जो भू-स्वामी की इच्छाधीन दाश्तकारी करते हैं। तीसरे, उप-काश्तकार हैं, जो किसी अन्य काश्तकार से भूमि प्राप्त करते हैं। स्थायी काश्तकारों के सापेक्ष उप-काश्तकार और इच्छाधीन काश्तकारों की स्थिति अत्यधिक कमजोर है।
काश्तकारी सुधारों को इच्छाधीन काश्तकार, उप-काश्तकार और खेतिहर मजदूरों को ध्यान में रख कर प्रभावी बनाया गया था। इसके अंतर्गत लगान का नियमन किया गया, काश्त अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई और काश्तकारों के लिए भू-स्वामित्व अधिकार दिलवाने की व्यवस्था की गई।
भूमि सुधारों को लागू करने के उपायों में जीतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कदम था। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में आय-असमानताओं को कम करने, कृषि में रोजगार को बढ़ावा देने और भूमि-साधन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुसंख्यक लघु किसानों व खेतिहर मजदूरों की भूमि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि भूमिपतियों के लिए अधिकतम जोत सीमा निर्धारित कर उनसे अतिरिक्त भूमि लेकर ऐसे किसानों में वितरित कर दी जाये।
राजस्व लेखों का अनुरक्षण एवं अद्यतन: भूमि सुधारों को लागू किए जाने के काल में राजस्व लेखों के विषय में जानकारी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। 1985-86 में भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा गया। भू-स्वामी और काश्तकार को कानूनी मान्यता प्राप्त पास-बुक जारी की गई। भू-सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अद्यतन भूमि-लेखों का विवरण एक आवश्यक शर्त है।
चकबंदी एव पुनर्वितरण: उप-विभाजन एवं विखण्डन की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई कदम उठाये, जिसमें चकबंदी एक महत्वपूर्ण कदम था। चकबंदी के अंतर्गत किसानों के विभिन्न स्थलों में बिखरे जोतों के स्थान पर उसे एक सुसंहत जोत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य साधनों के अनुकूलतम प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि और आय असमानताओं में कमी करना था। सुसंहत जोत प्रदान करने के दौरान क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि की उत्पादकता एवं सिंचाई साधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखकर ग्राम भू-स्वामियों के मध्य पुनः वितरण किया जाता था।
सहकारी खेती: भूमि के उपविभाजन से जनित समस्याओं का समाधान केवल सहकारी खेती द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अधीन वे छोटे व सीमांत किसान जिनके पास बहुत छोटी कृषि जोते हैं अपनी भूमि मिलाकर मिलजुल कर खेती करते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में 82 प्रतिशत जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है और उनके पास परिचालन क्षेत्र का केवल 39 प्रतिशत है। इन छोटी जोतों पर खेती लाभदायक नहीं हो सकती। परंतु यदि ये किसान अपनी भूमि, संसाधन, उपकरणों इत्यादि को मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं तो उन्हें बड़े पैमाने पर खेती के सभी लाभ मिल सकते हैं।
प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। सरकार ने सहकारी समितियों को कई तरह की रियायतें व सहायता प्रदान की जैसे वित्तीय सहायता, आर्थिक अनुदान, तकनीकी सहायता, उन्नत किस्म के बीजों की सस्ती दरों पर आपूर्ति, उर्वरकों की व अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति इत्यादि। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में सहकारिता का प्रयोग विफल रहा। यह इस बात से स्पष्ट है कि कृषित भूमि के आधे प्रतिशत से भी कम भूमि पर सहकारी खेती को अपनाया गया। जहां तक सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली व वास्तविक कामकाज का प्रश्न है, ऐसा पाया गया है कि बहुत सी समितियों का प्रबंध अत्यंत असंतोषजनक रहा है। बहुत-सी समितियों में व्यापक भ्रष्टाचार है तथा आम सदस्यों की समस्याओं को अनदेखा करके केवल कुछ धनी व प्रभावी जमीदार सदस्यों के हितों का ध्यान रखा जाता है। इस भ्रष्ट व अक्षम प्रबंध व्यवस्था से क्षुब्ध होकर बहुत से सदस्यों ने सहकारी समितियों की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है तथा वापिस वैयक्तिक कृषि की ओर लौट गए।

भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण: वर्ष 1988-89 में भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र से 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित एक योजना विभिन्न राज्यों के आठ जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भू-अभिलेखों के रख-रखाव में सुधार की मैनुअल प्रणाली की मुश्किलों को दूर कर भूमि रिकाडौँ की अद्यतन बनाना और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों की जरूरतों को पूरा करना था।
हरित क्रांति
आजादी के समय खाद्यान्नों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। खाद्यान्नों की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक थी। मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतर को आयात व राशनिंग के माध्यम से पूरा करने के प्रयास किये गये। प्रथम योजना काल में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। मानसून की अनुकूल स्थिति व अधिक महत्व दिये जाने के कारण, कृषि उत्पादन में पहले योजना काल में वृद्धि हुई। दूसरी योजना के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। दूसरी योजना के दौरान 1956 में भारत ने अमेरिका से पी.एल. 480 समझौता किया, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न आयात किये जाने की योजना थी। भारत सरकार की मांग-आपूर्ति के मध्य अंतर को आयात के माध्यम से पूरा करने की नीति चौथी योजना के अंत तक जारी रही। परंतु सरकार को खाद्यान्नों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता के खतरों का अनुभव होने लगा था, इसलिए सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उपाय करने आरंभ कर दिये थे।
खाद्यान्नों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में सरकार का प्रयास पारंपरिक कृषि व्यवहारों के स्थान पर आधुनिक तकनीक व फार्म व्यवहारों को लाने का था। इसके साथ-साथ भूमि सुधारों को लागू करने एवं प्रेरक मूल्य नीति अपना कर खाद्य आपूर्ति में वृद्धि करने की योजना भी थी।
कृषि क्षेत्र में अल्प उत्पादकता को दूर करने का एक उपाय पूंजी की मात्रा में वृद्धि कर उत्पादन तकनीक में परिवर्तन लाना था। इसी बीच मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म सामने आई, जिसने विकासशील देशों के मध्य आशा की किरण जागृत की। नार्मन बोरलाग ने उन्नत बीज प्राप्त करने की दिशा में विशेष कार्य किया। नार्मन बोरलाग को हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं।
भारत में अभी तक भू-सुधारों पर बल दिया जा रहा था, एवं भू-सुधारों के माध्यम से सृजित शक्तियों द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों व सिंचाई पर आधारित नवीन पद्धति को पहले-पहल पायलट योजना के रूप में वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के चयनित सात जिलों में लागू किया गया। उत्पादकता वृद्धि के इस प्रथम प्रयास के उत्साहवर्द्धक परिणामों के फलस्वरूप इस योजना को 1965 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम द्वारा 114 जिलों में लागू किया गया।
रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों व कीटनाशकों पर आधारित नवीन कृषि रणनीति को 1966-67 में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। वर्ष 1967-68 से हरित क्रांति की शुरूआत हुई।
हरित क्रांति का अध्ययन दो चरणों में किया जा सकता है:
प्रथम चरण (1966-67 से 1980-81): हरित क्रांति के प्रथम चरण में इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। उन्नत बीज कार्यक्रम को गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा व ज्वार तक सीमित रखा गया तथा अन्य गैर-खाद्यान्न फसलें इससे दायरे से बाहर थीं। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन को मिला, जिससे उत्पादन व उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। चावल के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई व मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का) का उत्पादन या तो स्थिर रहा या उसमें अनियमित व धीमी वृद्धि हुई। हरित क्रांति का कोई भी लाभ दालों को नहीं प्राप्त हो सका यहां तक कि दालों की उत्पादकता में कमी आई।
द्वितीय चरण (1980-81 से 1996-97): द्वितीय चरण 1980-81 से आरंभ होता है। इस काल में नवीन प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम काल में जहां चावल व तिलहन का निष्पादन अच्छा नहीं रहा था, वहीं दूसरे काल में इनका निष्पादन बेहतर रहा। इस काल में चावल व तिलहन के उत्पादन में वृद्धि दर क्रमशः 3.35 प्रतिशत व 5.81 प्रतिशत थी जो प्रथम काल की (चावल व तिलहन क्रमशः 2. 22 प्रतिशत व 0.98 प्रतिशत) वृद्धि दर से कहीं अधिक थी। इसी प्रकार की प्रवृति उत्पादकता में भी दृष्टिगोचर होती है। चावल की प्रथम व द्वितीय काल में वृद्धि क्रमशः 1.45 प्रतिशत व 2.82 प्रतिशत रही, वहीं तिलहन के लिए यह 0.68 व 2.49 प्रतिशत रही। दूसरी ओर प्रथम काल में हरित क्रांति के वाहक गेहूं के लिए द्वितीय काल में उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि दर क्रमशः 3.62 प्रतिशत व 2.91 प्रतिशत (प्रथम काल में उत्पादन में 5.65 प्रतिशत व उत्पादकता में 2.62 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी) की रहीं।
द्वितीय काल में दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिली। अन्य फसलों के उत्पादन (केवल ज्वार को छोड़कर) व उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस प्रकार द्वितीय काल में उत्पादन व उत्पादकता के संदर्भ में विभिन्न फसलों के मध्य आय अंतर में कमी आई।
हरित क्रांति के प्रभाव
हरित क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव सामने आये:
- हरित क्रांति के माध्यम से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहा।
- हरित क्रांति के प्रभाव से संचित गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को सापेक्षतया अधिक लाभ पहुंचा है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।
- हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक पूंजीनिवेश जरूरी होने के कारण समृद्ध किसान ही इससे लाभावित हुये परंतु समय के साथ लघु व सीमांत किसानों को संस्थानिक वित्त प्रवाह बढ़ने से बढ़ी उत्पादकता का लाभ उन्हें भी प्राप्त हुआ है, परंतु अंतः वैयक्तिक असमानताओं में सुनिश्चित रूप से वृद्धि हुई है।
- हरित क्रांति के माध्यम से कृषि श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1967-68 से 1980-81 के मध्य हरित क्रांति का लाभ गेहूं व एक स्तर तक चावल को मिला। इन दोनों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हुई जबकि अन्य फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। परंतु 1980-81 के बाद के काल में हरित क्रांति के लाभ सभी फसलों को प्राप्त हुये।
- 1980-81 के बाद के काल में उत्पादन वृद्धि में उत्पादकता वृद्धि का बड़ा योगदान रहा है।
- हरित क्रांति के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र में ट्यूबवैल, पम्पसैट, उर्वरक, ट्रिलर व हार्वेस्टर कम्बाइन का प्रयोग बढ़ा है, जो स्पष्टतः भारतीय कृषि की आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की ओर उन्मुखता का परिचायक है। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।
- कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का उपभोग बढ़ा है।
- 1980-81 से पूर्व के हरित क्रांति काल में हरित क्रांति के लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों तक सीमित रहे परंतु 1960-81 के बाद के काल में हरित क्रांति का प्रसार पूर्वी क्षेत्र में हुआ और उड़ीसा, बिहार, बंगाल में तीव्र खाद्यान्न वृद्धि दर दर्ज की गई।
- हरित क्रांति ने जहां एक ओर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की है वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिकी पर भी विपरीत प्रभाव डाला है। सिंचाई सुविधाओं के बिना जल निकास की व्यवस्था करने से मिट्टी में क्षारीयता बढ़ी है। कीटनाशकों के अवैज्ञानिक प्रयोग से मानव व पर्यावरण को अनेक खतरे बढ़ गये हैं। मिट्टी उर्वरता व मिट्टी संरचना के संरक्षण के लिए बिना प्रभावी कदम उठाये सघन कृषि पर बल दिया जा रहा है जिससे खेतों के रेगिस्तान में परिवर्तित होने का खतरा बढ़ा है।
दूसरी हरित क्रांति
कृषि में 4 प्रतिशत की वार्षिक उच्च वृद्धि दर विभिन्न स्तरों पर अनेक राज्यों और एजेंसियों द्वारा किए गये कृषि सुधारों की गुणवत्ता तथा मांग में सुधार करके ही प्राप्त की जा सकती है। इन सुधारों का उद्देश्य सतत आधार पर तथा समग्र ढांचे में संसाधनों के प्रभावी प्रयोग और मृदा, जल तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण पर होना चाहिए। ऐसे समग्र ढांचे में जल, सड़कों और विद्युत जैसी ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्त पोषण शामिल होना चाहिए।
11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इस प्रकार के समग्र ढांचे पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अग्रलिखित नीति का सुझाव दिया है-
- सिंचित क्षेत्र की वृद्धि दर की दुगुना करना
- जल प्रबंधन में सुधार करना, वर्षा जल का संचयन तथा जल संभर विकास
- निम्नस्तरीय भूमिका पुनरुद्धार करना तथा मृदा गुणवत्ता पर ध्यानदेना
- प्रभावी विस्तार के माध्यम से ज्ञान के अंतर को पाटना
- उच्च मूल्य वाली उपज, फल, सब्जियां, फूल, जड़ी-बूटी, मसाले, औषधीय पौधे, बांस, बायोडीजल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना। किन्तु ऐसा करते समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिए
- पशुपालन और मत्स्यपालन को बढ़ावा देना
- वहनीय दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराना
- प्रोत्साहन ढांचा और बाजारों की कार्यप्रणाली को सुधारना
- कृषि सुधार संबंधी मुद्दों पर फिर से ध्यान देना।
राज्यों में कार्यक्रम इस प्रकार बनाए तथा कार्यान्वित किए जाएं कि वे प्रादेशिक परिस्थितियों के अनुकूल ही हों, जिनमें कृषि जलवायु दशाओं और उपयुक्त दशाओं और उपयुक्त अनुसन्धान एवं विकास की उपलब्धता का समावेश हो एवं समय पर और पर्याप्त विस्तार और वित्त की सुविधा हो।
फसल की कई प्रजातियों में विघटन दलहनों के उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने में मुख्य बाधा बन रहा है। ये अनाजों की तुलना में आनुवांशिक रूप से कम उपज और कम निविष्टि वाली फसलें हैं। विदेशों में दलहनों की उपलब्धता सीमित होने के कारण इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर किस्मों का विकास करना इसकी पहली जरूरत बन गई है।
भारत में कृषि पर किया जाने वाला अनुसंधान एवं विकास व्यय इसके उच्च सामाजिक प्रतिलाभ के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है। क्षेत्र विशिष्ट बीजों तथा उनके प्रयोग का विकास विशेष रूप से जल की प्रचुरता वाली पूर्वी पट्टी में होने से इन क्षेत्रों में उपज के स्तरों को बढ़ा सकता है। अनुसंधान एवं विकास में वर्षा-पोषित और सुखा संभावित क्षेत्रों, सुखा रोधी और जैव प्रद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार फसलों तथा जैव-प्रौद्योगिकी, जिसमें वृद्धि और निर्यात की संभावना हो, आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए) उचित क्रियान्वयन किए जाने से, कृषक समूह, पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए जुलाई 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना अग्रणी कृषि विज्ञानों में मूल और नीतिगत अनुसंधान को सुदृढ़ करने में काफी सहायक होगी।

यथार्थ कृषि सतत् हरित क्रांति का मार्ग
हरित क्रांति के संदर्भ में अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि बीज-पानी-उर्वरक तकनीक पर आधारित यह व्यवस्था अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई है एवं उत्पादकता में और अधिक वृद्धि कर पाना अब इस तकनीक से संभव नहीं होगा। इसके साथ ही हरित क्रांति के पर्यावरण पर प्रभावों को देखते हुए भी उत्पादकता वृद्धि के वैकल्पिक मार्गों की खोज की जा रही है। इसी का परिणाम है यथार्थ कृषि।
यथार्थ कृषि में मृदा-प्रबंधन, किस्म संवर्द्धन, जल संवर्द्धन, समेकित किट नियंत्रण, टिशु कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं समेकित बीज प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों के समन्वय के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है। यथार्थ कृषि विधि भूमि व जल के वैज्ञानिक आयोजन पर आधारित होती है जिसके अंतर्गत प्रकृति की सेवाओं व प्राकृतिक पूंजी स्टॉक पर एक साथ ध्यान दिया जाता है। प्राकृतिक पूंजी स्टॉक में मिट्टी व मिट्टी के पोषक तत्व, जैव-विविधता, जल, खनिज, वन व सागर इत्यादि आते हैं। प्रकृति की सेवाओं में जल-चक्र, पोषण-चक्र कृषि-वानिकी इत्यादि आते हैं।
यथार्थ कृषि के अंतर्गत कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, कीटविज्ञान, मौसम विज्ञान, पादप क्रिया विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान व अर्थशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों के अनुसंधान कार्यों से लाभ उठाया जाता है। भविष्य में मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाये पूरा करने की दिशा में यथार्थ कृषि आशा की किरण है। वर्तमान बीज-जल-उर्वरक आधारित तकनीक संवहनीय विकास की दिशा में नहीं ले जाती है। परंतु यथार्थ तकनीक के माध्यम से संवहनीय विकास संभव है।
पीली क्रांति
खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हरित-क्रांति की अभूतपूर्व सफलता के उपरांत पीली-क्रांति कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का अग्रिम चरण है। इसके अंतर्गत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया गया है। यह मिशन तिलहन उत्पादन, उनके प्रसंस्करण तथा प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किए जाने पर दृष्टि रखेगा। पीली-क्रांति के परिणामतः आज भारत खाद्य तेलों तथा तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सका है। तिलहन उत्पादन से संबंधित इस कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले सम्मिलित हैं।
आलू क्रांति
आलू 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आया था। पुर्तगाल में इसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है; जबकि, 1949 में पटना में स्थापित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा 50 वर्ष के सतत् अनुसंधान के पश्चात आलू भारत में सर्दियों में अक्टूबर,जनवरी/फरवरी के मध्य खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। 1956 में पटना से शिमला में स्थानांतरित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा आलू की अनेक रोगरोधी किस्में, जैसे-कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना-I, कुफरी चिप्सोना II, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी स्वर्ण आदि का तथा प्रौद्योगिकी का विकास करने से भारत में आलू-क्रांति उत्पन्न हुई। भारत में आलू की प्रति हेक्टेयर औसतन उपज 19.2 टन है, जबकि शेष विश्व की प्रति हेक्टेयर औसत उपज मात्र 15.69 टन है। इस प्रकार, आलू उत्पादन में भारत विश्व में पांचवां स्थान रखता है।
शुष्क क्षेत्र कृषि
विशेषताएं: शुष्क क्षेत्र कृषि की विशेषताएं इस प्रकार हैं-
निम्न वर्षा: शुष्क भूमि क्षेत्रों में देश के 75 से 100 सेंमी. वर्षा प्राप्त करने वाले उपार्द्र क्षेत्र (जो वर्ष में लगभग 8 महीने नमी अल्पता का सामना करते हैं) तथा 30-75 सेमी. वर्षा प्राप्त करने वाले अर्द्ध-शुष्क भाग (जो वर्षभर नमी अल्पता का सामना करते हैं) शामिल हैं। ऐसे भागों का प्रतिनिधित्व पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के आंतरिक भाग (विदर्भ-मराठवाड़ा), कर्नाटक (पठारी भाग), तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश (रायलसीमा एवं तेलंगाना) द्वारा किया जाता है।
निम्न वर्षा के अलावा इन क्षेत्रों में मानसून का विलंबन तथा शीघ्र वापसी जैसी अनिश्चितताएं भी देखी जा सकती हैं। कभी-कभी दो नम चरणों के मध्य एक लंबा शुष्क चरण भी मौजूद रहता है। शुष्क क्षेत्र कृषि के अंतर्गत शुद्ध बुआई क्षेत्र (141 मिलि. हे.) का 70 प्रतिशत (99 मिलि. हे.) भाग शामिल है।
सुनिश्चित सिंचाई का अभाव
शुष्क भूमि क्षेत्रों में उगायी जाने वाली फसलें तथा फसल पद्धतियां पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती है, जो प्रायः अनियमित तथा अनिश्चित होता है। इसी कारण शुष्क क्षेत्र कृषि को वर्षाधीन कृषि भी कहा जाता है।
मुख्यतः जीविका खेती का प्रचलन
वर्षाधीन क्षेत्रों में विशेषतः छोटे एवं सीमांत किसानों का बाहुल्य होता है जो अधिशेषोन्मुखी कृषि की बजाय जीविका खेती को अपनाते हैं। जीविका खेती के मुख्य लक्षणों में निम्न उत्पादकता, निम्न आय, अनिश्चित उपज तथा निम्न पूंजी निर्माण शामिल है। ये क्षेत्र देश की सूखा ग्रस्त पेटी के अंतर्गत आते हैं तथा यहां की जनसंख्या को मानसून स्थगन या तनु मौसम के दौरान बेरोजगारी या अल्परोजगार की समस्या का सामना करना पड़ता है।
महत्व: शुष्क क्षेत्रों या वर्षाधीन परिस्थितियों में उगायी जाने वाली फसलों में दालें (प्रोटीन का एक स्रोत, कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत वर्षाधीन क्षेत्रों से प्राप्त), तिलहन (वसा का एक स्रोत, कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत वर्षाधीन क्षेत्रों से), मूंगफली, जूट व मेस्टा (इसका लगभग संपूर्ण उत्पादन शुष्क क्षेत्रों से प्राप्त); प्रमुख खाद्य जैसे-ज्वार एवं बाजरा (इसका 95 प्रतिशत शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है), मक्का (कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत वर्षाधीन कृषि से) तथा अन्य जई शामिल हैं। यदि देश में उपलब्ध संपूर्ण सिंचाई क्षमता का दोहन कर लिया जाए तो भी देश के कुल कृषित क्षेत्र का लगभग आधा भाग वर्षाधीन कृषि के अंतर्गत बना रहेगा। यह तथ्य देश की अर्थव्यवस्था में शुष्क क्षेत्र कृषि के महत्व को रेखांकित करता है।
देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में शुष्क क्षेत्र कृषि का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है। वर्षाधीन फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन में धीमी वृद्धि ने दालों व तिलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कटौती की है। इसलिए अब शुष्क क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है। यह तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि 1960-90 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि में चावल एवं गेहूं का योगदान 90 प्रतिशत था। कृषि से प्राप्त लाभों में कमी आते जाने के कारण यह परमावश्यक हो। गया कि शुष्क क्षेत्र कृषि हेतु एक समेकित रणनीति तैयार की जाय, जिसके तीन प्रमुख उद्देश्य हो-

- खाद्य सुरक्षा
- अंतरक्षेत्रीय, अंतरवैयक्तिक तथा अंतरवर्गीय असमानताओं एवं पोषकीय न्यूनता की समाप्ति
- ग्रामीण रोजगार।
उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकें एवं पद्धतियां: इन तकनीकों एवं पद्धतियों, जिनका विवेचन नीचे किया गया है, द्वारा भूमि उत्पादकता को वर्तमान स्तर से दो-तीन गुना बढ़ाया जा सकता है। ये वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं, जिनका उद्देश्य मृदा एवं नमी संरक्षण के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाना है।
समयबद्ध तैयारी तथा बीजारोपण गतिविधियां
यह मुख्यतः भंडारित मृदा नमी के संरक्षण पर जोर देती हैं। यह गहरी एवं सतही जुताईद्वारा किया जाता है। गहरी जुताई खरीफ की फसलों में सहायक होती है क्योंकि यह मृदा संस्तर के नीचे की कठोर एवं संयुक्त परत को तोड़ देती है। गहरी जुताई के परिणामस्वरूप अधिकतम वर्षा जल भूमि के अंदर रिसता है तथा बीज बोने एवं खर-पतवार को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। सतही जुताई से रबी की फसल को लाभ पहुंचता है, क्योंकि यह मृदा की नमी की संरक्षित रखने में सहायक होती है।
साथ ही, चावल एवं मूंगफली जैसी फसलों की पूर्वकालिक तथा शुष्क बुआई भी काफी लाभदायक सिद्ध हुई है। खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद रबी की फसलों को उगाना भी लाभकारी होता है।
पर्याप्त फसल समष्टि की स्थापना
खरीफ मौसम के दौरान पर्याप्त नमी उपलब्ध होती है, इसलिए थोड़ी-सी उच्च समष्टि अपेक्षित होती है। दूसरी ओर, रबी मौसम के दौरान उपलब्ध नमी एक सीमित समष्टि को कायम रखने में ही समर्थ होती है। इसीलिए चौड़ा कतार अंतराल तथा निकटवर्ती पौध अंतराल अपेक्षित होता है।
प्रभावी खर-पतवार नियंत्रण
खर-पतवार नियंत्रण उपायों के अभाव में अवशिष्ट मृदा नमी कम होती जाती है। गैर-मौसमी जुताई, समुचित बीज संस्तर निर्माण, समयबद्ध बुआई तथा खर-पतवार नाशकों के उपयोग इत्यादि उपायों से खर-पतवार को नियंत्रित किया जा सकता है।
वायु-अपरदन की रोकथाम
वायु के द्वारा होने वाला अपरदन शुष्क भूमि क्षेत्रों की एक सामान्य समस्या है। इसे पौध अवरोधों के निर्माण,रेत के टीलों के स्थिरीकरण (सतही आवरण उपलब्ध कराकर), ठूठीदार पलवार खेती तथा वनस्पति अवशिष्टों के आवरण (जो वाष्पीकरण को नियंत्रित करके मृदा की नमी को संरक्षित रखने में सहायक होता है) द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। समोच्चरेखीय जुताई तथा समोच्चों के बंध निर्माण एवं खाइयों द्वारा भी वायु अपरदन को कम किया जा सकता है।
प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग
इन किस्मों के तहत अल्पावधि वाली किस्में शामिल हैं जो विलबित बुआई तथा गहरे रोपण वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। भारत द्वारा मक्का, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा, चना, सोरघम, उड़द, सोयाबीन अरहर तथा मूंग की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है।
फसल विविधीकरण
उदाहरण के लिए, विभिन्न दलहन फसलों को अपनाकर वर्षाधीन क्षेत्रों में फसल उत्पादन को स्थिर रखा जा सकता है।
फलीदार पौधों का प्रयोग: अनाज फसलों के साथ फलीदार पौधे लगाने से कृषि जोखिम को कम किया जा सकता है, क्योंकि फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। इससे समय व स्थान की दृष्टि से भूमि का प्रभावी उपयोग संभव होता है।
वैकल्पिक भूमि उपयोग का नियोजन: गैर-मौसमी आय पैदा करने तथा खेती के जोखिम को घटाने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रतिरूपों को अपनाया जा सकता है:
- कृषि योग्य भूमि के संबंध में- कृषि वानिकी तथा फलीदार फसलों के साथ अंतर्फसलन।
- सीमांत भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के सम्बंध में- स्वतंत्र कृषि, वन चरागाह प्रबंधन तथा सामाजिक वानिकी।

ये उपाय उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि वृक्ष मिट्टी और नमी की मात्रा को बनाये रखते हैं तथा फलीदार पौधे व घासद्वारा भू-आवरण उपलब्ध कराया जाता है। शुष्क भूमि की कुछ फल किस्मों में अमरूद, बेर, फालसा तथा गुच्छसेब शामिल हैं।
भौतिक आघार संरचना का निर्माण: क्योंकि मृदा एवं नमी का संरक्षण एक स्थान केन्द्रित गतिविधि है, इसीलिए अपेक्षित आधार संरचना को स्थानीय परिस्थितियों एवं जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। इस सम्बंध में बांधों एवं समोच्च बंधों का प्रयोग, वानस्पतिक अवरोध (सतही जलप्रवाह को संगृहीत करने हेतु) जैसी आधुनिक पद्धतियों के अलावा देश के विभिन्न भागों में खादिन (khadins) तथा रेला (rela) खेती जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग भी किया जा रहा है।
अंतःस्रवणतालाबों द्वारा प्रवाहित जल के पुनर्चक्रण अथवा खादिन का प्रचलन राजस्थान के जैसलमेर जिले में सदियों से हो रहा है। इसमें जल की एक बंध की सहायता से घाटियों में संग्रहीत किया जाता है, जहां उसका अंतःस्रवण होता रहता है। अवशिष्ट नमी का उपयोग गेहूं व मटर जैसी जाड़े की फसलों द्वारा किया जाता है। खादिन द्वारा निम्न वर्षापात वाले वर्षों में भी उत्पादन को बरकरार रखने में सहायता दी जाती है। रेला कृषि के अंतर्गत मानसून के दौरान अल्पकालिक नदियों के जल को निकटवर्ती कृषि योग्य भूमि पर ले जाया जाता है और नवंबर तक उसे जमा करके रखा जाता है ताकि शीतकालीन फसलें उगायी जा सकें।
छिड़काव एवं टपक सिंचाई, बम्बा, नलकूप तथा वॉटर टरबाइन जैसी नयी तकनीकों द्वारा भी जल की हानि को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही निम्नीकृत भूमि के उद्धार हेतु भी प्रयास किये जाने चाहिए। इस उद्धारित भूमि पर कृषि वानिकी, पशुपालन, रेशम कीटपालन, कुक्कुटपालन, चरागाह विकास, चारा उत्पादन तथा घास भूमि विकास जैसी संयुक्त गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए।
शुष्क क्षेत्र कृषि के विकास हेतु सरकारी प्रयास शुष्क क्षेत्र कृषि के विकास को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों की क्षमता के दोहन हेतु अनेक कार्यक्रम एवं परियोजनाएं शुरू की गयी हैं, जिनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- बढ़ती हुईजनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करना तथा खाद्यान्नों के अलावा चारा, ईंधन लकड़ी एवं इमारती लकड़ी के उत्पादन में आने वाले उतार-चढ़ावों को न्यूनतम करना।
- सिंचित एवं वर्षाधीन क्षेत्रों के बीच मौजूद समाजार्थिक असमानताओं को समाप्त करना।
- वृक्षों, झाड़ियों एवं घासों के उपयुक्त मिश्रण द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखना।
- ग्रामीण रोजगार की स्थिति में सुधार लाना तथा इस प्रकार प्रामीण-शहरी अप्रवासन को नियंत्रित करना।
- एक लागत प्रभावी एवं संवहनीय भूमि उपयोग का विकास करना।
सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत एकीकृत व संरक्षण सहित उत्पादन वाली कृषि पद्धतियों हेतु एक साकल्यवादी उपागम को अंगीकृत किया गया है। इनमें जल विभाजक (एक भूजल वैज्ञानिक इकाई) को नियोजन की इकाई के रूप में मान्यता दी गयी है।
भारत में भूमि सुधारों का मूल्यांकन
अधिकतर राज्यों में खुद देख-रेख को स्वयं-काश्त का हिस्सा मान लिया गया। गांव में भू-स्वामी की मौजूदगी भी अनिवार्य नहीं थी। इसमें भू-स्वामी द्वारा स्वयं देख-रेख करने का प्रावधान नहीं था। भू-स्वामी के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा देख-रेख को काफी मान लिया गया। यह भूमि सुधारों के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत था। न केवल स्वयं-काश्त की परिभाषा दोषपूर्ण थी अपितु स्वयं-काश्त के लिए मध्यस्थों को बहुत बड़ी जमीन अपने पास रखने की अनुमति दी गई। इस प्रकार जमीदारों को अपने लिए बड़ी भूमि रखने की छूट मिल गई जो जमीदारी उन्मूलन के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत था।
जोतों की सीमाबंदी के कानूनों से बचने के लिए जमीदारों ने काफी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी। इस प्रकार के हस्तांतरण को रोकने के लिए किसी प्रकार के गंभीर प्रयास नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में, बंटाई के आधार पर कृषि करने वालों को काश्तकार का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि ये काफी बड़ी भूमि पर काश्त करते थे। इसलिए इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काश्त सुधार से संबंधित कानूनों का प्रयोग नहीं किया जा सका। काश्तकारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे भू-स्वामियों की शक्ति का किसी भी तरह सामना नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से भूमि त्याग दी। जैसाकि स्पष्ट है कि, कोई भी कानून काश्तकारों की मदद नहीं कर सकता यदि वे स्वयं ही अपनी भूमि का त्याग कर दें। काफी समय तक इस प्रकार की व्यवस्था रोकने का कोई कानून नहीं था।
किसी भी कानून की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि सरकार में उसे लागू करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं संकल्प हो। भूमि सुधार जैसे कानूनों की सफलता के लिए सरकार में अत्यधिक साहस व कार्यान्वयन का जोश होना चाहिए क्योंकि इन कानूनों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के संपति-संबंधों में आमूल परिवर्तन करना होता है। भारत में भूमि सुधारों के क्षेत्र में बहुत कम उपलब्धि इस बात को सिद्ध करती है की राज्य सरकारें भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए बेहद उत्सुक नहीं थी और मात्र प्रगतिवादी व समाजवादी मुखौटा पहनकर राजनैतिक लाभ अर्जित करना चाहती थीं। गौरतलब है कि भूमि सुधारों जैसे प्रगतिवादी कानूनों को बनाने और उनका सही कार्यान्वयन करने के लिए कठोर राजनैतिक निर्णयों और प्रभावी राजनैतिक समर्थन, नियंत्रण तथा दिशा-निर्देश की आवश्यकता होती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक-आर्थिक स्थितियां मौजूद हैं उन्हें देखते हुए भूमि सुधारों के क्षेत्र में तब तक कोई खास प्रगति होने की उम्मीद नहीं है जब तक कि उपयुक्त राजनैतिक इच्छा न हो।
राजनैतिक इच्छा के अभाव के साथ ही प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता पर भी विचार करना आवश्यक है। प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता राजनैतिक इच्छा के अभाव से पैदा होती है। महत्वपूर्ण है कि 1973 में पंजाब की स्थिति पर प्रकाशित हरचरण सिंह समिति की रिपोर्ट ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि हरिजनों एवं अन्य खेतिहर मजदूरों के लिए खाली की गई भूमि को प्रमुख राजनेताओं तथा सरकारी अधिकारियों ने बहुत कम कीमत देकर हड़प लिया। इससे सिद्ध होता है कि भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने की जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने स्वयं ही उसे विध्वंस कर दिया। इस प्रकार भूमि सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति के लिए ईमानदारी पूर्वक समग्र एवं समावेशी विकास करना होगा।