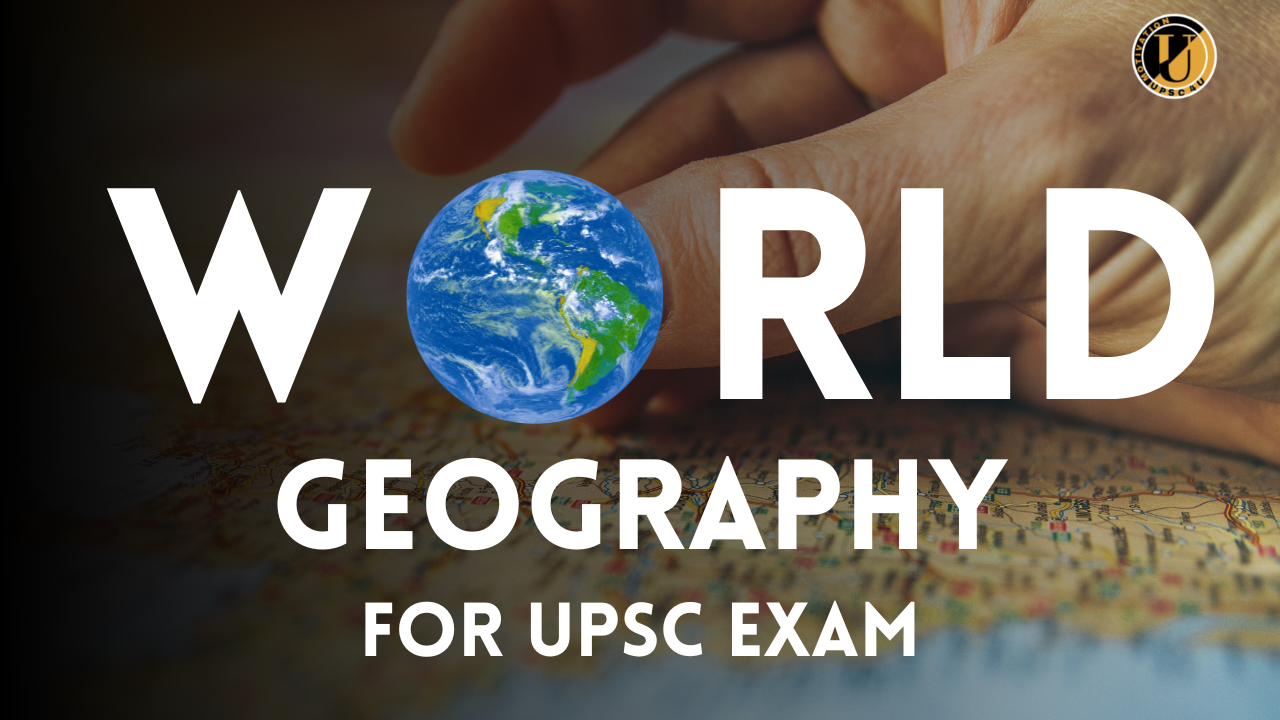किसी समाज, देश अथवा राष्ट्र में निवास करने वाले मानव समुदाय के धर्म, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप, रीति-रिवाज, खाने-पीने के तरीके, आदर्श संस्कार आदि के सामंजस्य को ही संस्कृति का नाम दिया जा सकता है या दूसरे शब्दों में मनुष्य अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है वह संस्कृति कहलाती है। रेडफील्ड के अनुसार- संस्कृति, कला और वास्तुकला में स्पष्ट होने वाले परम्परागत ज्ञान का वह संगठित रूप है, जो परम्परा के द्वारा संरक्षित होकर मानव-समूह की विशेषता बन जाता है।
भाषा और धर्म संस्कृति के एक अलग प्रकार के पहलू हैं जो सामान्यतः भौगोलिक रूप से अवगत क्षेत्रीय संदर्भ में शामिल होते हैं। भारत के अंदर व्यापक क्षेत्रीय संस्कृति है जो विभिन्न भाषाओं, बोलियों, धार्मिक प्रथाओं, आर्थिक संस्थाओं, जीवंत व्यवहारों इत्यादि से प्राप्त हुई है।
भाषा
भाषा बोली का ही विकसित रूप है। परंतु, यह तथ्य ध्यातव्य है कि भाषा और बोली में अंतर भी है। भौगोलिक दृष्टि से भाषा और बोली में यह अंतर है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित। यही कारण है कि व्यापक स्तर पर अभिव्यंजना का माध्यम भाषा ही बनती है। बोली द्वारा अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में प्रायः काम नहीं चलता।
भाषा को उसकी आधारभूत संरचना की दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये तीन वर्ग हैं- (i) एकाक्षरीय – इस प्रकार की भाषा में एक ही शब्द का वाक्य में स्थान-परिवर्तन के आधार पर अर्थ बदलता है, यथा-चीनी, वियतनामी, थाई एवं तिब्बती; (ii) योगात्मक- वह भाषा, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों का अर्थ-परिवर्तन कर देते हैं, यथा- मलय, जापानी, एवं अनेक अफ्रीकी भाषायें, तथा; (iii) श्लिस्ट योगात्मक: इस प्रकार की भाषाएं नम्य होती हैं और वांछित अर्थों के लिए ये भाषाएं अपना आधुनिकीकरण करती रहती हैं, यथा- अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच सम्मिलित हैं।
इंडो-यूरोपियन भाषा विश्व के लगभग आधे लोगों द्वारा बोली जाती है। यह समूह जर्मनी, रोमानियाई, बाल्टो-स्लाविक और इंडो-आर्यन शाखाओं से संबंध रखता है। सिंधु-तिब्बती एक अन्य भाषा परिवार है। बास्क एकमात्र भाषा है जो इंडो-यूरोपियन आक्रमण से पूर्व के समय से यूरोप में जीवित हैं। यूरोलिक और अल्टेइक भाषा परिवार भी यूरोप और एशिया में व्याप्त है। फिनिश और हंगेरियन यूरेलिक भाषाएं हैं।

विविधता एवं वितरण: भारत की भाषाओं और बोलियों में उच्च मात्रा की विविधता का कारण भारत में एशिया के पड़ोसी क्षेत्रों से आए विषमजातीय प्रजाति समूहों के मिलने में ढूंढा जा सकता है। शुरुआत में, ये भाषाएं एवं बोलियां देश के विभिन्न क्षेत्रों में एकांत अवस्था में विकसित हुई। एक खास भाषा को बोलने वाले सभी लोगों के बीच एक व्यापक सामाजिक एकात्मकता पाई जाती है। इस प्रकार भाषा और बोली क्षेत्रीय पहचान के तत्व को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतंत्रता पश्चात् राज्यों के भाषायी पुनर्गठन ने देश में भाषायी वितरण के भौगोलिक पैटर्न को एक नया राजनीतिक अर्थ प्रदान किया।
हमारे समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा 180 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 90 अप्रचलित भाषाएं 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। लगभग एक दर्जन बड़ी भाषाएं मुख्य भाषायी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये भाषाएं हैं- कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। ये बारह भाषायी क्षेत्र सामान्यतः भारतीय संघ के राज्यों के साथ बोली जाती हैं। लेकिन राज्य सीमाएं हमेशा भाषायी सीमाओं का सीमांकन नहीं करती। वास्तव में, भाषायी सीमा स्वयं एक रेखा नहीं है परंतु एक संक्रमण का क्षेत्र है, जिस पर एक भाषा धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व खो देती है और दूसरी भाषा को स्थान देती है।
भारतीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं चार भाषा परिवारों से संबद्ध हैं जिनके बारे में नीचे बताया गया है।
- ऑस्ट्रिक परिवार (निषाद): भारतीय जनसंख्या के कुल 1.38 प्रतिशत द्वारा ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अंतर्गत मध्य भारत, मेघालयकी खासी वजयतियां पहाड़ियों हैं। इस परिवार की भाषाएं बोलने वाले आधे से अधिक लोग संथाली भाषा बोलते हैं।
- चीनी-तिब्बती परिवार (किरात): इस परिवार की भाषाएं पूर्वोत्तर तथा हिमालय व उप-हिमालय क्षेत्र के उत्तरी तथा उत्तरी-पश्चिमी भाग में रहने वाली जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 0.85 प्रतिशत भाग ही इस भाषा परिवार से जुड़ा है। तिब्बती, बाल्टी, लद्दाखी, लाहुली, शेरपा, सिक्किम, भूटिया, चंबा, कनौरी, लेप्चा (सभी तिब्बती-हिमालय क्षेत्र में), अका, डाफ्ला, अबोर, मिरी, मिशमी, मिशिंग (उत्तरी असम या अरुणाचल प्रदेश), बोडी/बोरो, नागा, काचिन कुकीचिन, मणिपुरी, गारो, त्रिपुरी, मिकिर एवं लुशाई (असमी-म्यांमार शाखा) आदि इस समूह की प्रमुख भाषाएं हैं।
- द्रविड़ परिवार: भारत की जनसंख्या का 20 प्रतिशत द्रविड़ भाषा परिवार से सम्बद्ध है। इस समूह की भाषाएं पठारी प्रदेश एवं उससे संलग्न तटीय प्रदेशों में बोली जाती हैं। कन्नड़, तमिल, तेलुगू व मलयालम सबसे प्रमुख भाषाएं हैं। गोंड व उरांव जनजातियां भी द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं। तुलू, कुर्गी, कुई, येरुकला, पार्जी एवं खोंड इस परिवार से जुड़ी कुछ उप-भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषाएं अन्य भाषा समूहों की तुलना में अल्प विविधता रखती हैं। द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले लोगों का 96% चार प्रमुख भाषाओं (तमिल, तेलुगू, कन्नड़ व मलयालम) से जुड़ा है।
- भारोपीय भाषा परिवार (आर्य): भारत की जनसंख्या का 73% भाग इस भाषा परिवार से सम्बद्ध भाषाएं व उपभाषाएं बोलता है। यद्यपि इन भाषाओं का मुख्य संकेन्द्रण मैदानी भाग में है, फिर भी इनका प्रभाव प्रायद्वीपीय पठार तथा कोंकण तट तक देखा जा सकता है।
हिंदी इस भाषा परिवार की सबसे प्रमुख भाषा है, जो भारत के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्यान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली प्रमुख हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं। उर्दू उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। कच्छी एवं सिंधी बोलने वाले लोग पश्चिमी भारत में संकेन्द्रित हैं।
भारोपीय भाषा परिवार के दक्षिणी समूह की भाषाओं में सबसे प्रमुख स्थान मराठी का है। पूर्वी समूह की भाषाओं में ओडिया, बांग्ला व असमी पूर्वी भारत में बोली जाती हैं। गुजराती, मारवाड़ी व पंजाबी मध्य समूह की भाषाएं हैं। हिमालयी व उप-हिमालयी क्षेत्र के लोग उत्तरी समूह से सम्बद्ध नेपाली व पहाड़ी भाषाओं के विविध प्रकारों को अपनाते हैं।एकीकरण प्रभाव: भाषाई विविधता के ऊपर अनेक एकीकरण प्रभाव कार्य करते हैं तथा इन्हीं सामाजिक एकीकरण की शक्तियों ने एक सामान्य अखिल भारतीय शब्दावली को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। संस्कृत, फारसी एवं अंग्रेजी द्वारा इस एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभायी गई है। संस्कृत ने भारोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं के बीच तथा भारोपीय भाषा परिवार एवं द्रविड़ भाषा परिवार के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य किया है। मध्यकाल में फारसी द्वारा मराठी, कन्नड़, तेलुगू, तमिल एवं बांग्ला जैसी घरेलू भाषाओं को प्रभावित किया। आधुनिक समय में अंग्रेजी द्वारा भी ऐसी ही भूमिका निभाई गयी है। पिछले कुछ समय से हिंदी एवं उर्दू द्वारा भी भारत के भाषायी एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उदाहरणार्थ हिंदुस्तानी फिल्में देश के सभी भागों में देखी व समझी जाती हैं।
घर्म
भारत की जनसंख्या के धार्मिक संगठन पर एक दृष्टिपात विभिन्न संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण को समझने में सहायक सिद्ध होता है। हिंदू धर्म भारत के बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, किंतु यह अनेक क्षेत्रीय स्वरूप रखता है तथा प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट मान्यताओं को प्रदर्शित करता है। हिंदू धर्म पूर्व वैदिक कालीन धर्म से विकसित हुआ है, जो जनजातीय निष्ठाओं को महत्वपूर्ण स्थान देता था।
हिंदुत्व के भीतर, शैव और वैष्णव जैसे कई संप्रदाय मौजूद हैं। हिंदुत्व के अंदर विरोधी आंदोलनों ने जैन और बौद्ध जैसे नए धर्मो के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। तत्पश्चात् सिख धर्म का उदय हुआ, जो हिंदुत्व और इस्लाम के तत्व का मिश्रण लिए हुआ था।
भारतीय जनसंख्या की धार्मिक संरचना की अंतर्दृष्टि विभिन्न संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण को समझने में हमारी मदद करती है। उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के जनसंख्या की धार्मिक संरचना संबंधी आंकड़े सरकार द्वारा अभी तक प्रकट नहीं किए गए हैं। अतः जनगणना 2001 के आंकड़े ही उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में हिंदुत्ववाद अधिकतर लोगों का धर्म है। लेकिन इसके रोचक क्षेत्रीय रूप हैं और प्रत्येक सांस्कृतिक प्रदेश अपनी स्वयं की पृथक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। हिंदुत्व का जन्म पूर्व वैदिक धर्म से हुआ जिसने पूर्ववैदिक जनजाति आस्याओं के तत्वों को भी समाहित किया। भारत अन्य घर्मो के उत्तरोत्तर घुसपैठ का साक्षी रहा है जिन्हें समय-समय पर भारतीयों द्वारा अपनाया गया है। ईसाई धर्म सर्वप्रथम भारत के पश्चिम तट पर प्रकट हुआ। मुस्लिमों के भारत पर विजय प्राप्त करने से बहुत पहले, इस्लाम अरब व्यापारियों के साथ भारत के पश्चिमी तट पर आया। बौद्ध धर्म भारत का एक मुख्य धर्म रहा है, लेकिन आज यह कुछ क्षेत्र तक सीमित हो गया है। इस परिदृश्य में सिख धर्म अंत में प्रकट हुआ। इन चार मुख्य धर्मों के अतिरिक्त अन्य आस्थाएं, जैसे जैन, जुडेज्म, और जोरास्ट्रियन भी प्रतिनिधित्व करते हैं।
समायोजित आंकड़ों के अनुसार हिन्दू जनसंख्या वृद्धि दर 1981-91 के 22.8 प्रतिशत की तुलना में 1991-2001 में 20 प्रतिशत हो गई थी। इसी प्रकार की प्रवृति बौद्धों में देखी गई, जिनकी वृद्धि दर 1981-91 में 36.0 प्रतिशत की तुलना में 1991-2001 में 23.2 प्रतिशत हो गई। समायोजित आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम वृद्धि दर 1981-91 में 32.9 प्रतिशतकी तुलना में 1991-2001 मेंघटकर 29.3 प्रतिशत हो गई। जबकि ईसाइयों की वृद्धि दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 1991-2001 में 22.1 प्रतिशत हो गई। जैनियों की जनसंख्या वृद्धि दर 26 प्रतिशत ऑकत की गई जो कि 1981-1991 में 4.6 प्रतिशत के अत्यंत कम स्तर पर थी। अन्य दशकों में जैनियों की वृद्धि दर की तुलना में पिछले दशक की असामान्य रूप से निम्न वृद्धि दर एक विपथगमन प्रतीत होता है।
समायोजित आंकड़ों के अनुसार 1991-2001 में अन्य धार्मिक समूह वर्ग की वृद्धि दर 113.1 प्रतिशत के अत्यंत उच्च स्तर पर रही। इसके बाद धर्म उल्लेखित नहीं वर्ग की वृद्धि दर रही जो कि 75.1 प्रतिशत थी। अन्य धार्मिक समूह तथा विश्वास 2001 की जनगणना में एक नए तत्व के रूप में उभरा।
पारसी लोग एक अपवाद हैं लेकिन बेहद कम संख्या में होने के कारण न केवल भारत में अपितु विश्व में भी स्पष्ट उल्लेख रखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार,देश में पारसी जनसंख्या 1991 की जनगणना की जनसंख्या 76,382 (37,736 पुरुष, और 38,646 महिलाएं) के विपरीत 69,601 (33,949 पुरुष और 35,652 महिलाएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पारसी धर्म के अनुयायियों को लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार तथा पारसी समुदाय के लोगों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
0-6 आयु वर्ग की शिशु जनसंख्या से कुल जनसंख्या का प्रतिशत: 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मो को सम्मिलित कर शिशु जनसंख्या 13.58 प्रतिशत है जो 16.45 करोड़ बैठती है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 13.8 प्रतिशत (8,57,32,470) तथा महिलाओं की 13.4 प्रतिशत (7,87,45,680) है। इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ग की कुल जनसंख्या 16,44,78,150 है।
संस्कृति: संस्कृति एक जन-समूह की जीवन शैली की अभिव्यक्तियों का कुल योग है, जो वास्तुशिल्प, नृत्य, संगीत, चित्रकला, वेशभूषा, खान-पान, सामाजिक संस्थाओं एवं उनके कार्यों जैसे मूर्त तथा अमूर्त रूपों द्वारा प्रकट होती है। एक संस्कृति को किसी प्रदेश के अस्तित्व की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति माना जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष के निवासी अपने क्षेत्र की सापेक्षिक भौगोलिक पार्थक्यता, विशिष्ट जलवायु तथा अर्थव्यवस्था के आधार पर एक सुनिश्चित जीवनशैली विकसित कर लेते हैं, जो अन्य प्रदेशों से विभिन्नता रखती है। इससे विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न संस्कृतियों का उदय होता है जो पारस्परिक लेन-देन के आधार पर अंतःसम्पर्क कायम करती हैं।
उक्त कारकों के प्रभाव से ही मालवा, बुंदेलखंड, गुजराती, दक्कनी, भोजपुरी, अवध तथा कोंकणी जैसी प्रादेशिक संस्कृतियों का जन्म हुआ है। इन संस्कृतियों द्वारा विभिन्न वास्तुकला शैलियों (द्रविड़, नागर, होयसल, चोल, जौनपुरी, बंगाली आदि), चित्रकला शैलियों (राजस्थानी, पहाड़ी, अपभ्रंश आदि), नृत्य शैलियों (भरतनाट्यम, कत्थक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, गरबा, भांगड़ा आदि), नाट्य रूपों (नौटंकी, तमाशा, पांडवानी, लावणी, जात्रा, हरिकथा, नाच आदि) तथा संगीत घरानों को विकसित किया गया है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि, संस्कृति एक प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान या बाहरी रूप प्रदान करती है तथा उस सीमा तक एक प्रदेश के निर्माण में सहायक सिद्ध होती है।
भाषा, धर्म, प्रथा और परम्पराओं के आधार पर, भारत को निम्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
लद्दाखी-बौद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र: इस क्षेत्र पर बौद्ध धर्म और लद्दाखी भाषा का प्रभुत्व है। इस क्षेत्र में कई गोम्पा और बौद्ध केंद्र हैं और लेह और धर्मशाला जैसे पवित्र और सांस्कृतिक केंद्र हैं।
- कश्मीरी-मुस्लिम सांस्कृतिक क्षेत्र: इसके अंतर्गत कश्मीर घाटी और उत्तरी जम्मू के साथ-साथ लद्दाख के कुछ दक्षिणी हिस्से भी आते हैं। मुख्य धर्म इस्लाम है और भाषा कश्मीरी है। सिख और हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
- किन्नौरी-देव भूमि सांस्कृतिक क्षेत्र: इसमें पर्वतीय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड आते हैं। मुख्य भाषाएं हिन्दी (उत्तराखण्ड) और किन्नौरी (हिमाचल प्रदेश) हैं। इस क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ अन्यों के बीच प्रमुख हैं।
- सिख-गुरुमुखी सांस्कृतिक क्षेत्र: इसमें पंजाब और चंडीगढ़ शामिल हैं। यहां पर सिक्ख धर्म के लोग बहुल संख्या में हैं जो गुरुमुखी भाषा बोलते हैं। इस क्षेत्र में कई गुरुद्वारे हैं जिसमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी शामिल है जो एक तीर्थ स्थल है।
- हिन्दू-हिंदी सांस्कृतिक क्षेत्र; यह बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड के दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है। हिंदुत्व (धर्म) और हिंदी अपने कई प्रकारों सहित (भाषा) प्रभुत्व रखती है।
- उत्तर-पूर्वभारत क्षेत्र: यह भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों-असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैण्ड राज्यों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में घर्मो, भाषाओं, प्रथाओं और लोक परम्पराओं की बेहद विविधता है।
- बंगाली सांस्कृतिक क्षेत्र: यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखण्ड, बिहार, और ओडीशा में बंगाली भाषा का प्रभुत्व रखता है। यहां पर हिंदू धर्म का प्रभुत्व है।
- मराठी-हिंदू सांस्कृतिक क्षेत्र: महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, गोवा और आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हैं। यहां पर हिंदू धर्म और मराठी भाषा का प्रभुत्व है।
- जनजाति-हिन्दू सांस्कृतिक क्षेत्र: यहां जनजाति-हिन्दू मिश्रित जनसंख्या है जो छोटा-नागपुर तक आच्छादित है। यह ओडीशा और छत्तीसगढ़ तक भी फैला हुआ है।
- द्रविड़-सांस्कृतिक क्षेत्र: यह भारत के दक्षिणी राज्यों तक फैला हुआ है। तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम मुख्य भाषा हैं।