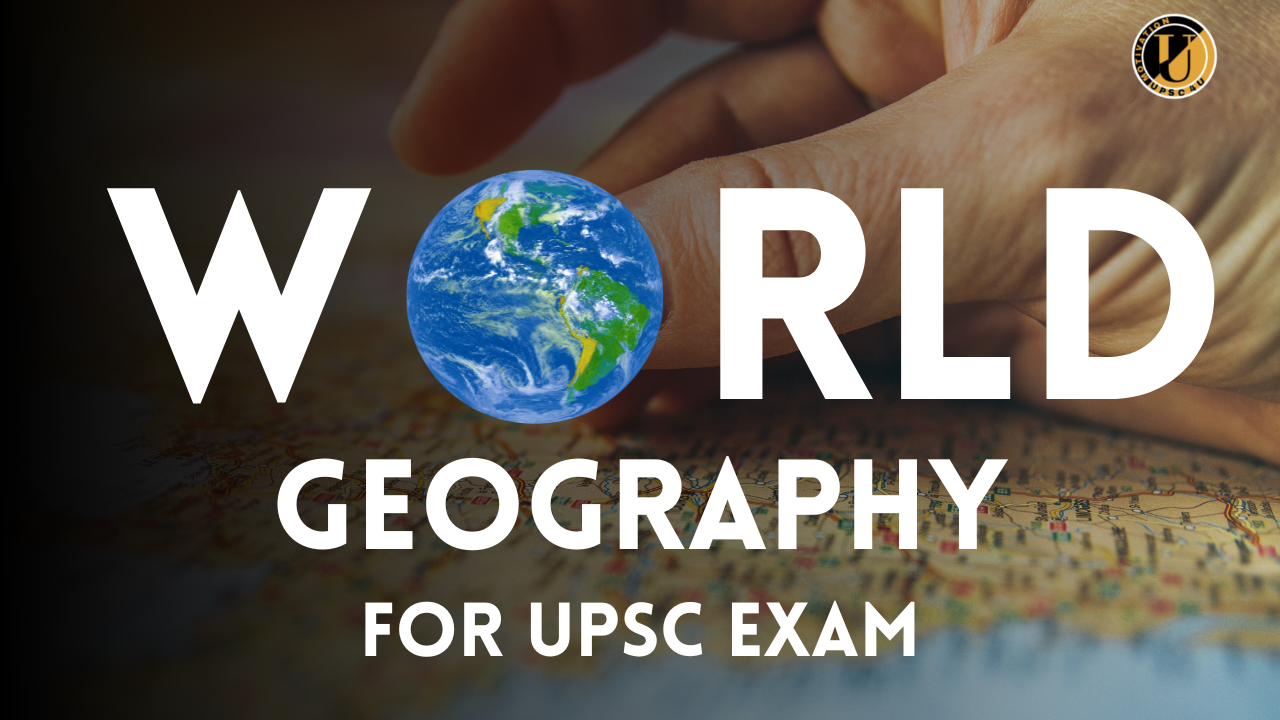मानसून की उत्पत्ति
मानसून एक भूमंडलीय प्राकृतिक घटनाक्रम है जो अभी तक पूरी तरह नहीं समझे जा सके, अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वैसे मानसून के बारे में विभिन्न संकल्पनाओं का प्रगतिशील उल्लेख किया जा चुका है।
भारतीय मानसून का परंपरागत सिद्धांत अथवा तापीय अवधारणा
इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के उत्तर की ओर होने वाले आभासी संचलन के परिणामस्वरूप भूमि एवं समुद्र की ऊष्मा की विभिन्नता के कारण भारतीय मानसूनी प्रवृत्ति का जन्म होता है। मानसून के सुदृढ़ विकास के लिए दो मुख्य कारक उत्तरदायी हैं-
- भारतीय उप-महाद्वीप एवं समुद्र का विशाल आकार
- उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला विशाल एवं ऊंचा हिमालय पर्वत तंत्र, जो उष्णकटिबंधीय एवं ध्रुवीय वायु राशियों के मध्य एक प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करता है।
दूसरा कार्य व्यापक मौसम वैज्ञानिक महत्व रखता है। शीत ऋतु के दौरान हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियां साइबेरिया से आने वाली ठंडी वायु राशियों को उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं करने देती, जबकि ग्रीष्मकाल में ये विषुवतीय सामुद्रिक वायुराशियों के हिमालय के पार जाने से रोकती है तथा उन्हें उत्तर-पश्चिमी भूभाग में चक्कर लगाने के लिए बाध्य करती हैं। हिमालय जलगतिक प्रभावों को जन्म देता है, जो भारत में वर्षण के प्रकार को निर्धारित करते हैं।
तापीय अवधारणा के अनुसार बसंत विषुव (मार्च 23) के बाद के काल में सूर्य उत्तर की ओर आभासी विस्थापन प्रारंभ करता है, जिसके परिणामस्वरूप विषुवत रेखा के उत्तर में फैले क्षेत्र सौर विकिरण की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करने लगते हैं। इस घटनाक्रम का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल उत्तरी मैदान एवं उससे जुड़े उच्च प्रदेशों में बढ़ती उष्णता के रूप में दिखाई देता है। इस कारण से पंजाब मैदान से बंगाल के डेल्टाई भाग तक एक निम्न दाब पट्टी बन जाती है। यह निम्न दाब क्षेत्र आरंभ में आसपास के क्षेत्रों की पवनों को आकर्षित करता है। किंतु मई-जून में सौर विकिरण स्तर के शीर्ष तक पहुंच जाने से इस निम्न क्षेत्र एवं समुद्री भागों के बीच की दाब प्रवणता अत्यंत उच्च हो जाती है। अब यह निम्न दाब पट्टी विषुवत रेखा के दक्षिण में प्रवाहित पवनों को भी आकर्षित करने लगती है।
इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए हिंद महासागर, अरब सागर तथा आस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ उच्च दाब केंद्रों का विकास होता है। विषुवत रेखा के दक्षिण में मौजूद पवन प्रतिरूप वास्तविक रूप से दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, जो दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये पवनें उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर स्थित निम्न दाब पट्टी द्वारा आकर्षित कर ली जाती हैं, जब ये विषुवत के उत्तर की ओर जा रही होती हैं। ये फेरेल के नियम का अनुसरण करती हुई घड़ी सूचक दिशा (या दाहिनी ओर) में मुड़ जाती हैं। दिशा का यह बदलाव पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम होता है। इस प्रकार ये दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी पवनें बन जाती हैं। इसी समय अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (आईटीसीजेड) भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। आईटीसीजेड एक परिकल्पनात्मक रेखा है, जहां पर उत्तरी गोलार्द्ध से आने वाली उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक पवनों तथा दक्षिणी गोलार्द्ध से आने वाली दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवनों का मिलन होता है। दक्षिणी-पश्चिमी पवनों को अब भारतीय प्रायद्वीप तक पहुंचने के लिए हिंद महासागर के ऊपर एक लंबी दूरी तय करनी होती है। अपनी लंबी यात्रा के दौरान ये भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं तथा भारत पहुँचते-पहुँचते अति संत्र्पित हो जाती हैं। यहाँ ये दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के रूप में जानी जाती हैं, जो प्रायद्वीप भारत के आकार के कारण अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी नामक दो शाखाओं में बंट जाती हैं। ये आर्द्रता युक्त पवनें पवनाभिमुखी दिशाओं में भारी वर्षा का कारण बनती हैं।
अरब सागर शाखा: यह शाखा सीधी पश्चिमी घाट के उच्च भू-भागों से टकराती है। पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढालें भारी पर्वतीय वर्षा ग्रहण करती हैं। यद्यपि मानसून की पश्चिमी धारा आगे जाकर भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करती है, फिर भी पवनविमुखी ढालों पर वर्षा की तीव्रता व सघनता घट जाती है। ये ढालें एक स्पष्ट वृष्टि छाया पेटी बनाती हैं जो सूखे से ग्रस्त रहती है। उदाहरण के लिए, मुंबई और पूना में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा क्रमशः 188 सेमी. एवं 50 सेमी. है, जबकि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी मात्र 160 किमी. है। पवनाभिमुखी ढालों पर वर्षा के वितरण का एक प्रमुख लक्षण यह है कि ढालों की ऊंचाई के साथ-साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। फिर भी, भारी वर्षा पश्चिमी घाट से लगी एक संकरी पट्टी में ही संकेन्द्रित होती हैं। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये वर्षायुक्त पवन धाराएं पूर्वी ढालों पर उतरती है, जहां ये रुद्धोष्म प्रभाव से गर्म हो जाती हैं। इसी कारण वृष्टि छाया प्रदेश अस्तित्व में आता है। पर्वतों की ऊंचाई के साथ वृष्टि छाया प्रदेशों के विस्तार का संबंध होता है। उत्तर की ओर, जहाँ पश्चिमी घाट अधिक ऊँचे नहीं हैं, पवंमुखी एवं पवनाविमुखी ढालों के मध्य वर्षा की मात्रा में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है।
कुछ पवन धाराएं अरब सागर शाखा से अलग होकर उत्तर में कराची एवं थार मरुस्थल की ओर मुड़ जाती है तथा कश्मीर तक बिना वर्षा किये पहुंच जाती हैं। वास्तव में, कराची के निकट एक पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गयी रेखा व्यावहारिक रूप से मानसूनी वर्षापात की सीमा को चिन्हित करती है।
बंगाल की खाड़ी शाखा: ये शाखा श्रीलंका से सुमात्रा द्वीप के बीच वाले क्षेत्र में सक्रिय रहती है। इस शाखा की मुख्य धारा के म्यांमार तट से टकराने के फलस्वरूप म्यांमार के पश्चिमी तटीय पर्वतों (अराकान एवं तेनसेरिम पर्वत) के पवनाभिमुखी ढालों पर भारी वर्षा होती है। जून-सितंबर के मध्य पश्चिमी तट पर स्थित आकयाब में 425 सेमी. तक वर्षा होती है। पवनाविमुखी ढालों पर यहां भी वृष्टि छाया क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। इस शाखा की एक उत्तरी धारा मेघालय की खासी पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा करती है। मासिनराम (चेरापूंजी के निकट खासी पहाड़ियों की दक्षिणी ढालों पर स्थित है) को विश्व का सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान माना गया है। मासिनराम एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखता है। यह चारों ओर से गारो, खासी व जयंतियां पहाड़ियों द्वारा घिरा है, जिसमें मात्र एक अंतराल है। इसी अंतराल से वर्षा पूरित पवनें अंदर प्रवेश करती हैं तथा ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है। दूसरी ओर, खासी पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित शिलांग (जो मासिनराम से मात्र 40 किमी. दूर है) में जून-सितंबर के दौरान मात्र 140 सेमी. वर्षा होती है।
बंगाल की खाड़ी शाखा की एक अन्य धारा बंगाल के डेल्टा से बायीं ओर मुड़ जाती है। यहां से यह दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम दिशा में हिमालय के अभिविन्यास के साथ-साथ प्रवाहित होती है। यह उत्तरी मैदानों में वर्षा करती है। उत्तरी मैदानों की मानसूनी वर्षा को पश्चिमी विक्षोभों का भी सहयोग प्राप्त होता है। ये बंगाल की खाड़ी में निर्मित होकर उत्तरी मैदानों के दक्षिणी छोर के साथ-साथ चलते हैं तथा चावल की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा करते हैं। उत्तरी मैदानों में वर्षा की सघनता पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिम की ओर होने वाली कमी आर्द्रता स्रोत से दूरी बढ़ते जाने के कारण होती है। जबकि दक्षिण की ओर होने वाली कमी का कारण पर्वतों से दूरी का बढ़ते जाना है, जो आर्द्रतावाही पवनों को ऊपर उठाने तथा मैदानों में (विशेषतः गिरिपादों में) पर्वतीय वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
मानसूनी पवनों की ये दोनों मुख्य शाखाएं अलग-अलग मार्गों का अनुसरण करती हैं। ये उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में निर्मित गहन निम्न वायु दाब रिक्त को भरने का कार्य करती हैं। ये दोनों शाखाएं छोटानागपुर पठार पर मिलती हैं। इन दोनों शाखाओं द्वारा वहनित कुल आर्द्रता का मात्र 20 प्रतिशत ही वर्षा के रूए में स्थल पर गिरता है। अरब सागर शाखा को बंगाल की खाड़ी शाखा से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि प्रथम, इसका आकार अधिक बड़ा है तथा द्वितीय, अरब सागरीय शाखा की अधिकांश वर्षा भारत में होती है जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा का अधिकांश भाग म्यांमार, मलेशिया एवं थाईलैंड को चला जाता है।
गतिक सिद्धांत
फ्लोन नामक विद्वान ने मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके गतिक सिद्धांत की नवीन संकल्पना का प्रतिपादन किया है, जिसमें कहा गया है की मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण (कन्वर्जेस) का आविर्भाव होता है। इसे इण्टर ट्रॉपिकल कन्वर्जेस (आई.टी.सी.) कहते हैं। उत्तरी सीमा को एनआईटीसी तथा दक्षिणी सीमा को एसआईटीसी कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति के समय एनआईटीसी 30° उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है, जिसके अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया आ जाता है। इन भागों पर डोलड्रम की विषुवत रेखीय पछुवा हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जो की गर्मी की दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाएं होती हैं। वास्तव में वायु मेखलाओं के दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तर-पूर्व व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिण-पूर्व एशिया से एनआईटीसी हट जाती है तथा उस पर उत्तर-पूर्व व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। ये ही जाड़े की मानसून हवाएं होती हैं।

नवीन सिद्धांत
वायुमंडल की ऊपरी परतों के विस्तृत अध्ययन ने मानसून की परंपरागत अवधारणा की वैधता पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिये हैं। परंपरागत अवधारणा द्वारा विश्लेषित स्थलीय व सामुद्रिक उष्णता विभेद एवं उच्च व् निम्न दाब क्षेत्रों के विपरीत नवीं सिद्धांतों द्वारा मानसून की उत्पत्ति के लिए दो कारकों को महत्वपूर्ण माना गया है-
- तिब्बती पठार का प्रभाव, तथा;
- जेट स्ट्रीम
तिब्बती पठार का प्रभाव: डॉ. पी. कोटेश्वरम् के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बती पठार का गर्म होना, मानसूनी प्रवाह की उत्पत्ति एवं नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। 1978 में आयोजित भारत-सोवियत मानसून खोज यात्रा (मोनेक्स) में भी दोनों देशों के मौसम विज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय उप-महाद्वीप के ऊपर मानसूनी प्रवाह की शुरूआत करने में तिब्बती उच्च भूमि एक निर्णायक भूमिका निभाती है।
तिब्बती पठार की लंबाई 2000 किमी. तथा चौड़ाई पश्चिम में 600 किमी. एवं पूर्व में 1000 किमी. है। इस पठार की औसत ऊंचाई 4000 मी. है। इस प्रकार यह एक वृहद भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ है।
मोंग तुन यिन के अनुसार, जून के आरंभ में ग्रीष्म मानसून के अचानक आरंभ होने का सम्बंध उपोष्ण कटिबंधीय जेट के तिब्बती पठार के दक्षिणी छोर से अचानक उत्तर की ओर विस्थापित होकर 40° उत्तरी अक्षांश के साथ पहुंच जाने से है। तिब्बती पठार जेट धारा के उत्तरी विस्थापन को विशिष्टता प्रदान करता है। साथ ही अक्टूबर के दौरान जेटधारा को सुदूर दक्षिण की ओर धकेलने में भी पठार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इस प्रकार यिन मानसूनी पवन प्रवाह उत्तर-पश्चिम में ताप प्रेरित निम्न दाब केंद्र की बजाय हिमालय के जलगतिक प्रभावों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है।
हाल ही में एक अन्य प्रक्रिया, जो गतिज प्रतिचक्रवातीय जनन कहलाती है, पर जोर दिया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान मध्य क्षोभमंडल में एक उच्च दाब वाला उष्ण क्रोड तापीय प्रतिचक्रवात उपस्थित होता है। इस प्रतिचक्रवात की दक्षिणी दिशा में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का जन्म होता है। इस धारा को तीन स्रोतों से शक्ति प्राप्त होती है-
- तिब्बती पठार के ऊपर मौजूद मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडल की सघन उष्मीयता से
- दक्षिणी-पश्चिमी मानसून द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर मुक्त की गयी गुप्त ऊष्मा की विशाल मात्रा से
- हिमालय एवं तिब्बत की उच्च सतहों द्वारा ऊपरी वायुमंडलीय प्रति चक्रवात को स्थानांतरित की गयी ऊष्मा से।
ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा मूलतः भारत के पूर्व में स्थित देशांतरों में जन्म लेती है तथा भारत को पार करके अरब सागर होती हुई पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है। ये उपरिस्तरीय पूर्वी जेट धारा तिब्बत के पठार के दक्षिण में एक वायु प्रवाह को जन्म देती है, जो उत्तरी भारत के ऊपर निचले स्तरों पर उतर आता है। यह प्रक्रिया, हिमालय के दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा के कमजोर होने तथा आईटीसीजेड के लगभग 25° उत्तरी अक्षांश पर विस्थापित होने की प्रक्रियाओं से मिलकर भारतीय उप-महाद्वीप में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के आगमन को प्रभावित करती है।
अक्टूबर में स्थितियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। तिब्बती पठार के ऊपर स्थित मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडलीय प्रतिचक्रवात विघटित हो जाता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा आलोप हो जाती है। इसके विपरीत उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा खुद को उत्तरी भारत के ऊपर स्थापित कर लेती है, जिसके फलस्वरूप ग्रीष्म मानसून का दक्षिण की ओर लौटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार वायु प्रवाह में कोई विशेष बाधा न डालने के बावजूद तिब्बती उच्च भूमि की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जेट स्ट्रीम: जेट धाराएं उच्च वेग वाली विसपी भूविक्षेपी धाराओं की संकरी एवं संकेन्द्रित पत्तियां हैं, जो निम्न गति की पवनों से परिबद्ध होती हैं तथा उपरी स्तर की पछुआ पवनों का एक भाग हैं। ये धाराएं एक ध्रुवोन्मुखी या विषुवतोन्मुखी घटक के साथ, उर्मिल व अनियमित रूप में, पछुआ पवनों की दिशा में गति करती हैं। इन्हें परिध्रुवीय अभिमुखीकरण के द्वारा पहचाना जाता है। मुख्यतः दो जेट धाराएं हैं- प्रथम, निम्न अक्षांशों पर उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा तथा द्वितीय, मध्य अक्षांशों पर ध्रुवीय वाताग्र जेट धारा। जेट धाराओं की उत्पत्ति का प्राथमिक कारक उत्तरी-दक्षिणी ताप प्रवणता है, जो एक संगत दाब प्रवणता का निर्माण करती है। यह दाब प्रवणता ऊंचाई बढ़ने के साथ बढती जाती जय तथा अधिक ऊंचाई पर वेग वाली पवनों का निर्माण करती है।
एक दृष्टिकोण के अनुसार, उपोष्ण जेट धारा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्मित होती है। विषुवत पर घूर्णन द्वारा वायुमंडल में उच्चतम वेग पैदा किया जाता है। परिणामतः उठती हुई वायु (जो उत्तर एवं दक्षिण की ओर फैलती है) अक्षांशों की तुलना में तेजी से संचलन करती है। यह उत्तरी गोलार्द्ध में दायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर विक्षेपित हो जाती है। लगभग 30° अक्षांश पर यह जेट धारा के रूप में संकेन्द्रित हो जाती है।
समतापमण्डल जलवाष्प के अभाव में शुष्क मेघ रहित होता है, किंतु इन धाराओं के प्रवेश के कारण समतापमण्डल की निचली सीमा भंग हो जाती है तथा उसमें जलवाष्प पहुंच जाती है। इस प्रकार समताप मण्डल के निचले भाग में कभी-कभी पक्षाभ मेघ दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में जेट स्ट्रीम में जहां कहीं वायुदाब प्रवणता की तुलना में वायु वेग अधिक हो जाता है, वहां उच्च वेगीय वायु अपने दायीं ओर विस्थापित हो जाती है। ऐसी वायु को उप-प्रवणता पवन कहा जाता है। जेट स्ट्रीम के दायें किनारे पर वायु के एकत्रित हो जाने के कारण पछुआ पवन की पेटी के भूमध्य रेखीय किनारे पर पृथ्वी पर उच्च वायुभार क्षेत्रों की स्थापना में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रक्रिया को एण्डीसाइक्लोजेनेसिस कहते हैं।
जेट धारा के आर-पार तापमान प्रवणता भी तीव्र होती है। यही कारण है कि इसके ध्रुवीय किनारे पर वायु अत्यधिक शीतल तथा भूमध्य रेखीय किनारे की वायु अत्यधिक गर्म होती है। यद्यपि जेट स्ट्रीम का प्रवाह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होता है, किंतु प्रायः इनमें उत्तर से दक्षिण की ओर दीर्घ तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए समभार रेखाएं सर्पाकार होती हैं। अक्षांश एवं ऊंचाई के अनुसार इस धारा में दीर्घाकार वायु कटक तथा द्रोणी पैदा होती हैं।
ध्रुवीय वाताग्र जेट का निर्माण तापीय विभेदों द्वारा होता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय जेट की तुलना में अधिक परिवर्ती अवस्थिति में होती है। ग्रीष्मकाल में इसकी अवस्थिति धुव की ओर विस्थापित हो जाती है तथा शीतकाल में विषुवत रेखा की ओर।
जेट धाराओं का औसत वेग शीतकाल में 120 किमी./घंटा तथा ग्रीष्मकाल में 50 किमी./घंटा होता है। जहां अधिकतम गति होती है, वहां जेट धाराओं में क्रोड बन जाते हैं। ये हजारों किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हैं। इनकी चौड़ाई 40 से 160 किमी. तक हो सकती है। ये दो से तीन किमी. तक की गहराई में एवं 9-12 किमी. तक की ऊंचाई पर प्रवाहित हो सकती हैं। इनकी शक्ति ताप प्रवणता (निम्न स्तरों पर) के अनुपात में बढ़ती है। जब जेट धाराएं भूसतही पवन तंत्रों में हस्तक्षेप करती हैं, तब भीषण आंधी-तूफान आते हैं। विमान चालकों द्वारा भी (यदि उन्हें जेट धाराओं के प्रवाह की दिशा में उड़ना हो) जेट धाराओं का उपयोग किया जाता है। विश्व के मौसम पर जेट धाराओं का प्रभाव इस प्रकार है:
- वायु के भारी मात्रा में विनिमय द्वारा जेट धाराएं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन को कायम रखने में सहायता करती हैं।
- ध्रुवीय वाताग्र जेट मध्य-अंक्षाशीय मौसमी विक्षोभों को प्रभावित करती हैं।
- जेट धाराएं चक्रवातों के मार्ग को भी प्रभावित करती हैं।
- शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा वे वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करती हैं।
- जेट धाराएं वायु सहतियों के संचलन पर भी प्रभाव डालती है, जो दीर्घकालिक सूखा या बाढ़ स्थितियों का कारण बन सकता है।
सोमाली जेट स्ट्रीम एवं सोमाली वायुधारा: जेट स्ट्रीम के बीच, जो भारत की ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून के विकास में सहायक होती है, सोमाली जेट है जो केन्या, सोमालिया तथा साहेल में बहती है तथा 9° उत्तर पर निम्न स्तर तथा तीव्र गति से बहते हुए अफ्रीकी तट को छोड़ देती है। ब्रिटिश मौसम विज्ञानी, जे. फिंडलेटर ने इस निम्न स्तर जेट स्ट्रीम का अध्ययन किया और पता लगाया कि यह धरातल से 1-1.5 किमी. ऊपर बहती है। यह पाया गया कि यह 3° दक्षिण में केन्या तट पर पहुंचने से पूर्व मॉरीशस तथा मेडागास्कर द्वीप के उत्तरी हिस्से में बहती है। उत्तरवर्ती रूप से दोबारा 9° उत्तर में तट पर पहुंचने से पहले यह केन्या, इथियोपिया और सोमालिया के मैदानों के ऊपर बहती है। जून माह में भारत पहुंचने से पहले इस निम्न स्तर पर बहने वाली जेट स्ट्रीम का एक बड़ा हिस्सा मई माह के दौरान पूर्वी अफ्रीका में प्रवेश करता है तथा उतरवर्ती रूप से अरब सागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। अध्ययन सुझाते हैं कि निम्न स्तर पर प्रवाहित जेट स्ट्रीम क्षेत्र में एशियाई ग्रीष्म मानसून के दौरान मजबूत विषुवतीय प्रवाह दक्षिणी से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर होता है। यह मौसम विज्ञानियों को परेशानी में डालता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वायु दक्षिणी से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर क्यों चलती है।

समुद्र विज्ञानी एक और तत्व को लेकर उत्सुक हैं, जिसका संबंध उत्तरी अफ्रीका तट से पृथक् निम्न प्रवाह वाली जेट धारा के साथ प्रतीत होता है। इस महासागरीय धारा को सोमाली वायुधारा का नाम दिया गया है, जो 9° उत्तर पर विषुवत से उत्तर की ओर बहती है, जहां यह तट से पृथक् होता है। यह साफ तौर पर एक प्रचंड वायुधारा है। सोमाली वायुधारा को हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा की एक धारा समझा जा सकता है। लेकिन इसकी अजीब विशेषता ग्रीष्म मानसून आने की विपरीत दिशा है। शीतकाल में, यह अरब तट से पूर्वी अफ्रीका तटरेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन ग्रीष्म मानसून के आगमन के साथ ही यह इसके बहने की दिशा विपरीत अर्थात् दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। यह बताता है कि इसका मानसून के लौटने के सम्बन्ध है, लेकिन वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तनों के प्रति महासागर ने प्रायः बेहद धीमा प्रत्युत्तर दिया है तथा समुद्र विज्ञानी आश्चर्यचकित हैं कि सोमाली वायुधारा क्यों अपनी दिशा बदल देती है तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की तुलना में लगभग एक माह पूर्व अपनी उच्चतम गति में होती है।
अल-नीनी एवं ला-नीनी: अल-नीनो एक उप-सतही (Sub surface) गर्म जलधारा है। यह पूर्वी महासागर में पेरू के तट के निकट 3° दक्षिणी अक्षांश से 32° दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है। यह 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होने वाली अस्थायी जलधारा है। यह संपूर्ण विश्व के मौसम को प्रभावित करती है। इसके कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा आता है। इसी तरह कहीं शीत लहर का प्रकोप छा जाता है तो कहीं गर्म हवाएं चलने लगती हैं। कुछ क्षेत्रों में भयानक तूफान भी आते हैं। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में इस जलधारा का पता चला जब पेरू के मछुआरों ने पाया कि पेरू के तट के पास कुछ वर्षों के अंतर पर एक गर्म जलधारा बहती है। यह जलधारा क्रिसमस के समय उत्पन्न होती है और इसके प्रभाव से इन महासागरीय क्षेत्रों में मछलियां विलुप्त हो जाती हैं। इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा (Corriente Del Nino) नाम दिया गया। सामान्य स्थिति में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अन्य जलधारा पेरू की ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। सतह के नीचे के ठंडे जल के तेजी से ऊपर आने के कारण यह जलधारा उत्पन्न होती है। इस ठडे जल के साथ काफी मात्रा में पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्लैंकटन बहुलता से पाए जाते हैं तथा समुद्री मछलियां भोजन के लिए इन्हीं प्लैंकटनों पर निर्भर करती हैं। अल-नीनो की उत्पत्ति के साथ ही पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में सतह के नीचे के ठंडे जल का ऊपर की ओर आना बंद हो जाता है। इसके कारण ठंडे जल का स्थानांतरण पश्चिम से आने वाली गर्म जलधारा के साथ होने लगता है और प्लैंकटन तथा मछलिय विलुप्त होने लगती हैं। इसके साथ ही इन मछलियों पर निर्भर रहने वाले पक्षी भी मरने लगते हैं। सूर्य के दक्षिणायन के समय सामान्य परिस्थितियों में आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के समीप के क्षेत्रों में निम्न दाब रहता है और पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उच्च दाब रहता है। इसके फलस्वरूप इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया में वर्षा होती है और पेरू के तटवर्ती क्षेत्र शुष्क रहते हैं। किन्तु कभी-कभी आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब और पूर्वी प्रशांत महासागर में उच्च दाब के स्थान पर निम्न दाब निर्मित हो जाता है।
गिलबर्ट वॉकर ने इस घटना को दक्षिणी दोलन (Southern oscillation) नाम दिया है। इस घटना के कारण पेरू के तट पर असाधारण रूप से काफी वर्षा होती है तथा आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का मौसम शुष्क हो जाता है। उपरोक्त घटना के पश्चात् ही अल-नीनो की उत्पत्ति होती है। इस घटना के आधार पर अल-नीनो की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए डार्विन (130° E) एवं पोलीनेशिया (150°W) के वायुदाब को सूचकांक माना गया है। अल-नीनो की उत्पत्ति के पश्चात् डार्विन पर उच्च दाब और पोलीनेशिया पर निम्न दाब पाया जाता है।
अल-नीनो के कारण पेरू, बोलिविया और कोलबिया में भयानक बाढ़ आती है तथा दक्षिणी-मध्य प्रशांत महासागर में भयानक उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जब पश्चिमी प्रशांत महासागर में निर्मित उच्च दाब का प्रभाव फिलीपींस, श्रीलंका और भारत तक होता है तो इस भाग में सूखा पड़ता है। इस प्रकार अल-नीनो का भारतीय मानसून पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अल-नीनो की घटनाओं के मध्य एक विपरीत और पूरक घटना दिखायी देती है, जिसे ला-नीनो कहा जाता है। ला-नीनो की घटना के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह के जल का तापमान न्यूनतम हो जाता है। इसके कारण इस प्रदेश में तीव्र दक्षिण-पूर्वी वाणिज्य हवाएं चलने लगती हैं। इस पवन के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का जल पश्चिम की ओर जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और नीचे का ठंडा जल ऊपर आने लगता है। ऐसा माना जाता है कि ला-नीनो का संबंध उत्तरी अमेरिका के सूखा से भी है।
ला-नीनो के बारे में: अल-नीनो लगातार विषुवतीय प्रशांत महासागर में सामान्य दशाओं के काल का अनुसरण करता है। यदाकदा, लेकिन हमेशा नहीं, अल-नीनो दशाएं अल-नीनो-दक्षिण ओसिलेशन चक्र (ईएनएसओ) का मार्ग प्रशस्त करता है। अल-नीनो के इस शीतल समकक्ष को ला-नीना कहा जाता है, स्पेनिश में जिसका अर्थ कन्या शिशु (गर्ल चाइल्ड) से होता है। शोधकर्ताओं ने इसे गैर-अल-नीनो वर्षों में खोजा। ला-नीनो वर्षों के दौरान, व्यापारिक पवनें पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के बीच वायु दाब में वृद्धि के कारण आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप, दक्षिण अमेरिका के तट के साथ-साथ उर्ध्वामुखी संचरण होता है, जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत जल की ऊपरी परत की अपेक्षाकृत अधिक ठंडा करने में योगदान करता है तथा पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत जल को सामान्य से अधिक गर्म करता है।
भारत के लिए, अक्सर एक चिंता का कारण रहा है, क्योंकि या दक्षिण-पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जैसाकि वर्ष 2009 में हुआ था। दूसरी ओर, ला-नीनो प्रायः मानसून के लिए लाभदायक होता है, विशेष रूप से मानसून के उत्तरवर्ती समय में। वर्ष 2010 में प्रशांत क्षेत्र में प्रकट हुआ ला-नीना ने संभवतः उस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के अंत में सकारात्मक परिणाम दिए। हालांकि, ला-नीनो को उत्तर-पूर्व मानसून के लिए लाभदायक नहीं माना जाता।
हिंद महासागर चुम्बकीय ध्रुव: हिंद महासागर चुम्बकीय धुव (आईओडी) समुद्री सतह तापमान का अनियमित प्रकम्पन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर वैकल्पिक रूप से महासागर के पूर्वी हिस्से के मुकाबले गर्म तथा तत्पश्चात् ठंडा होता है। इसके सकारात्मक पहलू के तहत् समुद्री सतह पर अधिक और औसत तापमान दिखाई देता है तथा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भारी वर्षण होता है; यह पूर्वी हिंद महासागर में जल को शीतलता प्रदान करता है, जिसके कारण इसके आस-पास की इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया की भूमि क्षेत्र पर सूखा प्रवृत्त होता है। आईओडी का नकारात्मक पहलू गर्म जल के साथ प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करता है तथा पूर्वी हिंद महासागर में भारी वर्षा करता है, तथा पश्चिम में शील एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न करता है। आईओडी को भी भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ताकतवर मानसून को कमजोर या प्रभावित करने वाला पक्ष समझा जाता है। एक उल्लेखनीय रूप से सकारात्म्क आईओडी 1997-98 में तथा एक अन्य 2006 में उत्पन्न हुआ था। आईओडी वैश्विक जलवायु चक्र का एक सामान्य पहलू है।
भारतीय मानसून के विशिष्ट लक्षण
भारतीय मानसून अपनी व्यापक परिवर्तनशीलता के लिए पहचाना जाता है। यद्यपि भारत में वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा 98 सेमी. है किंतु इसमें 20 सेमी. की कमी (1899 में) तथा 30 सेमी. की वृद्धि (1907 में) भी हो सकती है। विरल वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटा-सा परिवर्तन फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। ये सूखा एवं अकाल की पुनरावृत्ति वाले क्षेत्र हैं।
मानसून के आरंभ में होने वाला विलंब प्रायः उसकी शीघ्र वापसी का कारण बन जाता है।
कभी-कभी मानसूनी वर्षा, किसी एक क्षेत्र में निरंतर जारी रहने अथवा लम्बा अंतराल रखने की प्रवृत्ति रखती है। ऐसा उस समय होता है जब ग्रीष्मकालीन फसलें बढ़ रही होती हैं तथा उन्हें पर्याप्त नमी की जरूरत होती है। शीतकालीन फसलें भी इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि ये ग्रीष्म फसलों के बाद की अवशिष्ट नमी पर निर्भर होती है। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी घटित हो जाती है, जबकि एक ही राज्य के अलग-अलग भाग सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। भारत में मानसूनी वर्षण व्यापक स्थानिक असमानता रखता है। जहां पश्चिमी घाट एवं उत्तर-पूर्वी भाग वर्ष में 400 सेमी. वर्षा प्राप्त करता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेमी. से भी कम वर्षा होती है। अधिकांश भारत में 60 से 100 सेमी. के बीच वर्षा होती है।
मानसूनी वर्षा का 80 प्रतिशत भाग जून से सितंबर के दौरान, 13 प्रतिशत अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, 3 प्रतिशत जनवरी-मार्च के दौरान तथा 10 प्रतिशत मार्च से मई के दौरान (दक्षिण भारत में होने वाली आम्र वर्षा) प्राप्त होता है। भारत में मानसूनी वर्षा किसी समय हल्की तथा किसी समय मूसलाधार (जो मृदा अपरदन का कारण बनती है) रूप में होती है। देश के कुछ भागों में वर्ष के प्रत्येक महीने में होने वाली वर्षा इस प्रकार है-
- जनवरी, फरवरी-उत्तरी भारत में
- मार्च-बंगाल एवं असम में तड़ित झंझा एवं भारी वर्षा
- अप्रैल, मई-दक्षिण भारत में आम्र वर्षा
- जुलाई, अगस्त, सितंबर-दक्षिणी-पश्चिमी मानसून
- अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर-पूर्वी तट पर लौटता हुआ मानसून
मानसून का महत्व
भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर करती है और कृषि का निष्पादन मानसून पर निर्भर करता है। देश के कुल फसल क्षेत्र का 4/5 भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। मानसून के देर से आने या पहले आ जाने का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। दक्षिण की अनेक नदियां वर्षा के जल से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां अनेक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में हैं। साथ ही जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए भी वर्षा होना आवश्यक है।
भारतीय मानसून की विशेषताएं:
- वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण-पश्चिमी मानसून के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है।
- वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है।
- वर्षा की मात्रा का वितरण असमान होता है।
- भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षण का उदाहरण है।
- शीत काल में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा गंगा के मैदानों में व ग्रीष्म काल में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है।
- मानसून के देर से या शीघ्र आने का अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ता है।