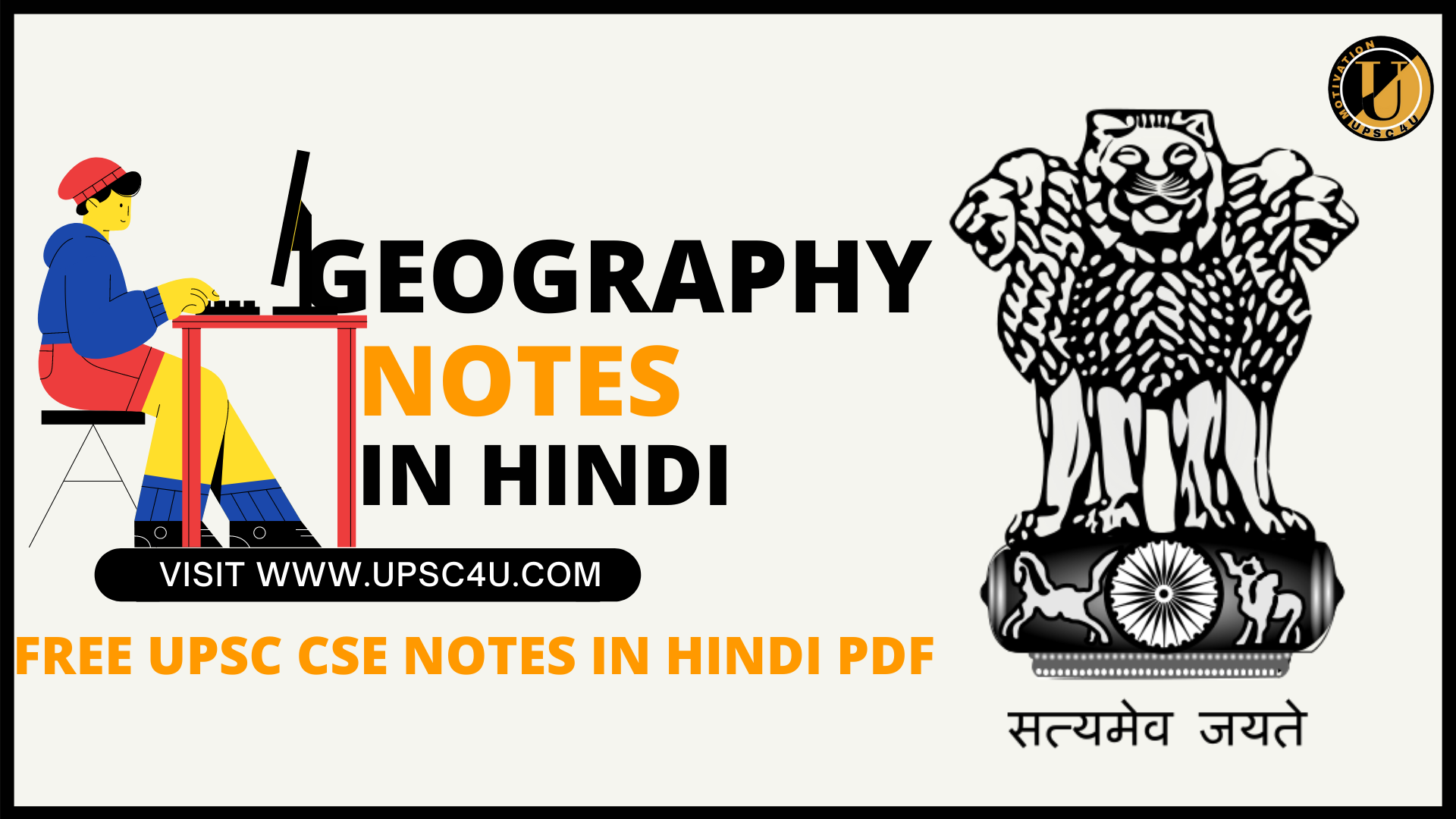भूपृष्ठ की वह उपरी सतह, जिसका विकास यांत्रिक एवं रासायनिक अपक्षय, अपरदन एवं जलवायु के तत्वों (तापमान एवं जल) के द्वारा होता है, मिट्टी कहलाती है। वस्तुतः मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट प्राकृतिक परिस्थिति में सम्पन्न होती है तथा प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूट-फूट जाने के उपरांत मिट्टी का निर्माण आरंभ होता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के निर्माण में प्राकृतिक धरातल का स्वभाव, जीव-जंतु एवं वनस्पतियां, समय, चट्टानों की स्थिति तथा जलवायु के तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी तत्व स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की जलवायु, वनस्पतियां, जीव-जंतु आदि की भिन्नताओं के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है।
प्राकृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से मिट्टी मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवीय सभ्यता के इतिहास का आरंभ ही मिट्टी से होता है। हमारी प्राचीन सभ्यता का जन्म-स्थल उपजाऊ मिट्टी वाली सिंधु नदी की घाटी ही रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी का बड़ा महत्व होता है। यदि किसी देश की मिट्टी उर्वरक होती है तो वहां की कृषि अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। इसके विपरीत अनुपजाऊ मिट्टी वाले देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या का घनत्व और जीवन-स्तर दोनों ही भिन्न होते हैं। एक ओर भारत के विशाल मैदान और तटीय मैदान दोनों की मिट्टी समृद्ध कांप मिट्टी है, जो उन्नतिशील कृषि को प्रोत्साहित करती है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की कम गहरी एवं मोटे कणों वाली मिट्टी तथा राजस्थान के शुष्क प्रदेश की मिट्टीं है, जो समृद्ध कृषि को आधार प्रदान करने में अक्षम हैं। यही कारण है कि यह प्रदेश कम घने बसे हुए हैं। मिट्टी सम्बन्धी विशिष्टताओं में पाई जाने व्काली भिन्नता के कारण दोनों क्षेत्रों के विकास के स्तर में अंतर पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रदेश के विकास स्तर में मिट्टी संबंधी विशेषताएं एक आधारभूत भूमिका निभाती हैं।

मृदा संरचना
मृदा निर्माण में पांच प्रमुख कारकों का योगदान होता है। ये कारक हैं-चट्टानें, स्थानीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्थिति तथा समय। इनमें से चट्टानें व जलवायु अति महत्वपूर्ण कारक हैं।
चट्टानें
मिट्टी के निर्माण में सहायक मूल पदार्थों की प्राप्ति, धरातल पर फैली चट्टानों के अपक्षरण से होती है। यदि चट्टानों से निर्मित मिट्टी स्थानीय रूप से मिलती है तो इसका रंग गहरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से अपनी मूल-चट्टान की विशेषताएं रखती हैं। लाल लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और वनों की भूरी मिट्टियां इस प्रकार की मिट्टियों में प्रमुख हैं। दूसरी ओर, यदि मिट्टियों का निर्माण, नदियों के निक्षेपण से होता है तो उस स्थिति में मूल चट्टान से मिट्टी का संबंध नाममात्र का ही रह जाता है। विशाल मैदानों में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, वह हिमालय की चट्टानों के अपक्षरण से प्राप्त सामग्री द्वारा निर्मित हुई हैं। नदियों द्वारा इन सामग्रियों को वहां से बहाकर मैदान में एकत्र कर दिया गया है, इसलिए ये मिट्टियां महीन कण वाली, गहरी और उपजाऊ होती हैं।
धरातलीय दशा
मिट्टी के निर्माण में धरातलीय दशा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धरातल के ढाल की भिन्नता उसके जल प्रवाह के परिमाण को तय करती है। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपरदन की मात्रा मुख्य रूप से उच्चावच एवं ढाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। इन विशेषताओं के कारण भारतीय मिट्टियों के कई रूप प्राप्त होते हैं। सम-धरातल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की परत गहरी, विशाल मैदान तथा तटीय भागों की मिट्टियों की परत मोटी होती है तथा पठारीय व पर्वतीय मिट्टियों की परत कम गहरी होती है, क्योंकि इन स्थानों में धरातल पर निक्षेपण नहीं होता है।
जलवायु
जलवायु के तत्वों की भी मिट्टियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु के तत्वों के अंतर्गत विशेष रूप से वर्षा और तापमान, मिट्टियों के प्रकार निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मिट्टी के निर्माण की स्थितियों को वर्षा की मात्र एवं रितुवत वितरण काफी हद तक प्रभावित करते हैं। यदि किसी स्थान की जलवायु ठण्डी या नम होती है तो वहां की मिट्टी में अधिक गहराई तक खनिज एवं रासायनिक पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टियों में घुले हुए पदार्थ बहकर बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि उनमें खनिज एवं रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के प्रकार को भी जलवायु ही निर्धारित करती है, जिसका प्रभाव मिट्टी की विशेषता पर भी पड़ता है।
प्राकृतिक वनस्पति
मिट्टियों के विभिन्न प्रकार के लिए प्राकृतिक वनस्पति भी उत्तरदायी होती है अर्थात् यदि कहा जाए तो मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया और इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही प्रारंभ होता है। वृक्षों के सड़े हुए पते मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं और साथ ही अत्यंत आवश्यक जीवांश तत्व प्रदान कर मिट्टी को समृद्ध भी करते हैं। भारत वर्ष के सघन वन वाले क्षेत्रों में अत्यंत उन्नत किस्म की मिट्टी पाई जाती है।
समय
मिट्टी का विकास चरणबद्ध क्रम में होता है मिट्टी शैशवास्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था की विभिन्न अवस्थाओं से गुजराती है। इस तरह मिट्टी के विकास में समय अति महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः मृदा जितनी पुरानी होती है उसमें उतना ही उपजाऊपन रहता है।
मिट्टी की विशेषताएं
मिट्टी का गठन मिट्टियों के गठन से अभिप्रायः मिट्टी का निर्माण करने वाले कणों के आकार से है। ऐसे कण जो 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले आकार के हैं, उनके गठन द्वारा मटियार चिकनी-मिट्टी मृतिका कहलाती है। कणों का आकार यदि 0.002 और 0.02 मिलीमीटर व्यास के मध्य है तो गाद अथवा रेग और 0.02 से 2 मिलीमीटर व्यास के आकार के कणों के गठन से बालू अथवा रेत का निर्माण होता है। दोमट मिट्टी विभिन्न आकार वाले कणों के गठन से निर्मित होती है।
मिट्टी का रंग
मिट्टी का रंग खाद-मिट्टी की मात्रा से प्रभावित होता हैं विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रंग की मिट्टियां मिलती हैं। मध्य-अक्षांश में काली से भूरे रंग की, आर्द्र क्षेत्रों में हल्के भूरे रंग की, अर्द्ध-शुष्क स्टैपी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में स्लेटी रंग की मिट्टी पाई जाती है।
मिट्टी का लाल रंग लोहे (रेड ऑक्साइड) के कारण होता है। पीला रंग भी लोहे की उपस्थिति के कारण ही होता है। परंतु इसमें रेड-ऑक्साइड के स्थान पर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में नीलापन या स्लेटीपन का अधिकांश अर्थ लोहे की कम मात्रा का होना है। शुष्क जलवायु क्षेत्र में मिट्टी का स्लेटीपन खाद-मिट्टी (ह्यूमस) की न्यूनता के कारण होता है व सफेद रंग मिट्टी में लवणता की अधिकता के कारण होता है।
मिट्टी की संरचना
मिट्टी की संरचना का अर्थ मिट्टी के एकाकी कणों के पिण्ड रूप में समूहन से है। मिट्टी की संरचना, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को प्रभावित करती है। साथ ही मिट्टी की जुताई और अपवर्तन को भी मिट्टी की संरचना प्रभावित करती है। मिट्टी की संरचना को आकार की दृष्टि से प्लेटी, प्रिज्मैटिक, ब्लॉकी और ग्रेनयुलर में विभाजित किया गया है।
मृदा रन्ध्रमयता
मृदा के कणों के बीच वायु एवं जल जब स्थान घेर लेते हैं तो इन्हें रन्ध्र कहते हैं। मृदा के रन्ध्रों के प्रतिशत को मृदा रन्ध्रमयता कहते हैं।
वायुमण्डलीय वायु की तरह, मृदा वायु में अधिकांशतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हालांकि, मृदा वायु में अधिक मात्रा में आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायुमण्डलीय वायु की अपेक्षा थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वास्तविक मात्रा फसलीय मौसम के दौरान बेहद परिवर्तित होती है क्योंकि इस समय मृदा में फसल की उच्च संवृद्धि दर तथा जैवकीय गतिविधियां होती हैं। अच्छी प्रकार अपवाह वाली मृदा में पर्याप्त रूप से हवा या गैस की आवाजाही होती है। लेकिन बेहद अच्छी बनावट वाली मृदा या वह मृदा जो एक लम्बे समय तक डूबी रही हो, अक्सर पर्याप्त वायु प्रवाह वाली नहीं होती है। चिकनी मिट्टी में, मृदाकण बेहद संघनता से आबद्ध होते हैं, जो मृदा में वायु के बेहतर आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। मृदा वायु जड़ के श्वसन के लिए आवश्यक होती है।

मृदा तापमान
कृषि सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों जैसे अंकुरण, वनस्पति वृद्धि, पौधों एवं मिट्टी में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के द्वारा परिवर्तित होता है। मिट्टी के तापमान का मुख्य स्रोत जैविक पदार्थों के निक्षेपण के दौरान उत्पन्न होने वाला विकिरण तथा ऊष्मा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली ऊष्मा भी मृदा ऊष्मा में योगदान करती है। मृदा का तापमान इसके रंग, संरचना, ढाल तथा जल की मात्रा द्वारा प्रभावित होता है। गहरी काली मिट्टी हल्के रंग की मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है। रेतीली मिट्टी ऊष्मा का अवशोषण एवं निष्कासन बेहतर संरचना वाली मिट्टी की तुलना में अधिक तीव्रता से करती है, क्योंकि फाईन टेक्सचर मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है तथा जल की विशेष ऊष्मा मिट्टी के कणों की ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है।
अजैविक पदार्थ
वह सभी पदार्थ जो निर्जीव स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, अजैविक पदार्थ हैं तथा सामान्य रूप से खनिजों के बने होते हैं। खनिज मृदा-मण्डल के अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं क्योंकि ये मिट्टियों के निर्माण में सहायक होते हैं। मृदामण्डल के प्रमुख खनिजों के तहत् ऑलविन, हाइपरस्थीन, आजाइट, हार्नब्लेंड, बायोटाइट, पोटाश, कैलसिक, प्लैजियोक्लेज, क्वार्टज़, फेल्सपार, मस्कोबाइट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। खनिजों के तत्वों के गठन एवं पुनर्संगठन, प्राथमिक खनिजों के टूटने, गौण खनिजों के निर्माण तथा खनिजों एवं जैविक पदार्थों के समूहन की क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं सदा कार्यरत रहती हैं। अर्थात् खनिजों का निर्माण, उनका विघटन तथा पुनः निर्माण होता रहता है। मृदामण्डल में ऊपर से नीचे जाने पर खनिजों का आकार बढ़ता जाता है।
जैविक पदार्थ
मृदा-मण्डल के जैविक पदार्थों के अंतर्गत सजीव अर्थात् पौधों तथा जंतुओं को शामिल किया जाता है। ये सामूहिक रूप में मृदा-मण्डल के समस्त संघटक में 5 से 12 प्रतिशत भाग का योगदान करते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों का आकार 20 सेंटीमीटर से लेकर 20 माइक्रो मीटर तक की लम्बाई वाला होता है। ये मृदा जीव बड़े आकार के, मध्यम आकार के तथा लघु आकार वाले होते हैं। मृदा जीवों के कुछ पक्ष-पक्षियों के गुणों तथा उनकी विशेषताओं को बढ़ाने हेतु अति आवश्यक होते हैं। इसके तहत्, जंतुओं द्वारा मृदा में व्यतीत की जाने वाली समयावधि, जंतुओं के आहार-ग्रहण की आदत, जंतुओं के निवास स्थान तथा, जंतुओं की गतिशीलता आती हैं।
सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्गत वृक्षों की जड़ों, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल तया मृदा वासी प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया जाता है। ये जीव किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की मिट्टियों के गुणों तथा विशेषताओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित तथा निर्धारित करते हैं। बैक्टीरिया तथा कवक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण, गमन तथा संचरण में सहायक होते हैं। शैवाल तथा काई मृदा-मण्डल में जैविक पदार्थों की आपूर्ति कर मिट्टी की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं।

कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात
ठोस या जैविक पदार्थ में कार्बन और नाइट्रोजन की आनुपातिक उपस्थिति को प्रायः कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात के तौर पर संदर्भित किया जाता है। कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात (सीएन) की स्थिति कृषि के लिए बेहद महत्व की है, क्योंकि इसकी स्थिति मृदा उर्वरता के बारे में एक संकेत प्रदान करती है। यह अनुपात एक सामान्य मृदा में सदैव लगभग 10:1 होता है। जैविक पदार्थों में यह अनुपात अधिक होता है। भारतीय मिट्टी में कार्बन-नाइट्रोजन का सामान्य अनुपात अधिकतर मिट्टी में निम्न होता है। कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात व्यापक रूप से, औसत मूल्य लगभग 14 के साथ, 5 से 25 के मध्य आगे-पीछे होता है।
मृदा प्रतिक्रिया
मृदा प्रतिक्रिया शब्द का इस्तेमाल मृदा की प्रकृति में अम्लीयता या क्षारीयता के संकेत के तौर पर किया जाता है। मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा का मापन लघुगुणकीय pH पैमाने पर किया जाता है जिसमें O (अत्यधिक अम्लीयता) से 14 (अत्यधिक क्षारीयता) तक बिंदु होते हैं। pH मान 7 मृदा में प्रतिक्रिया के प्रति तटस्थता दिखाता है। मृदा में, हालांकि, pH मान कभी-कभी 3 से नीचे तथा 11 से ऊपर चला जाता है।
मृदा परिच्छेदिका
मृदा परिच्छेदका में चट्टानों से प्राप्त अपक्षयित पदार्थ ही होते हैं किंतु स्तरीभूत शैल, जिस पर मिट्टी जमा होती है, स्वयं इस परिच्छेदिका का हिस्सा नहीं होती। इस परिच्छेदका में क्षेतिज पर्ते भी नहीं होती, जिन्हें क्षितिज-स्थिति (हेराइजंस) कहते हैं। वास्तविक मृदा परिच्छेदका का विकास तब होता है जब अपक्षयित पदार्थ बहुत समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहें। मृदा परिच्छेदका में क्रमशः चार क्षितिज-स्थितियां होती हैं। कृष्ट मृदा सबसे ऊपर (क्षितिज A), उसके नीचे उप-मृदा (क्षितिज B), ऋतु घर्षित शैल (क्षितिज C) और स्तरीभूत शैल (क्षितिज D) । भौतिक और रासायनिक संघटन तथा जैविक अंश के आधार पर मृदा का प्रत्येक क्षितिज दूसरों से बिल्कुल भिन्न होता है।
संस्तर ‘A’ खनिज संस्तर का जैविक संस्तर से सटा हुआ भाग होता है, इसी कारण इस संस्तर में जैविक व खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ऊपरी स्तर का रंग काला होता है आक्साइड, एल्यूमीनियम आदि खनिजों का नीचे की ओर अवक्षालन होता है। संस्तर ‘B’ का सम्पोहन संस्तर, इसमें खनिजों खासकर सिलिकेट, मृतिका और जैविक पदार्थों के अत्यधिक जमाव के कारण कहते हैं। संस्तर ‘C’ आधार शैल के गुण दोषों से प्रभावित होता है। इस संस्तर में पदार्थ ढीले एवं असंगठित होते हैं साथ ही इसमें A एवं B संस्तर के गुणों का भी अभाव रहता है।