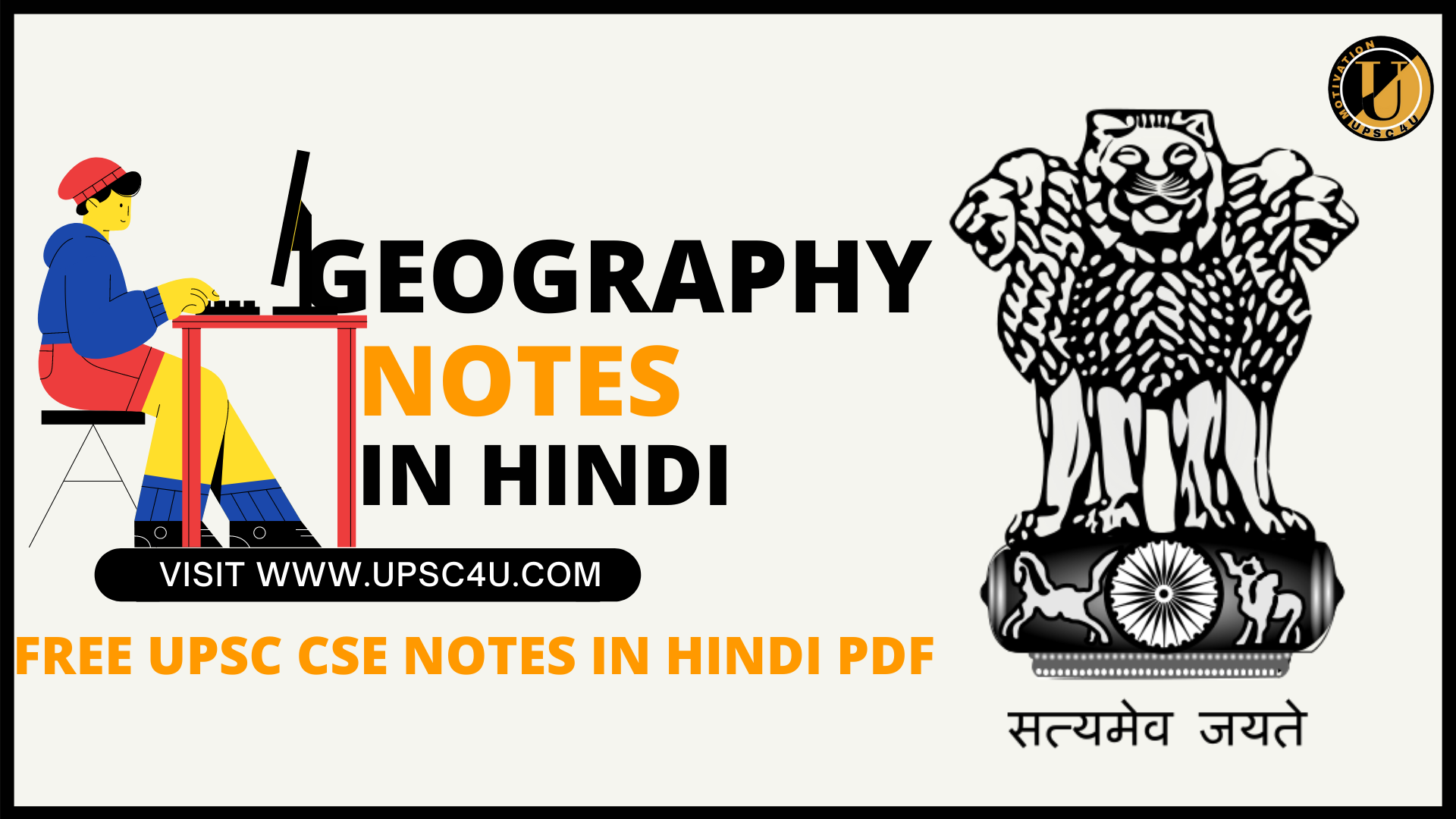यद्यपि मिट्टी के निर्माण में चट्टानों का योगदान निर्विवाद रूप से स्वीकृत है, तथापि जलवायु के तत्व, धरातलीय संरचना, जीव-जंतु, वनस्पतियां और मानव क्रियायें भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में मिट्टियों के वर्गीकरण में इन तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से भारतीय मिट्टियों का अध्ययन उनकी धरातलीय विशेषताओं को दृष्टिगत करके किया जाना चाहिए। इस आधार पर भारत की मिट्टियों को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है-
- प्रायद्वीपीय मिट्टियां
- विशाल मैदानं की मिट्टियां
- हिमालय प्रदेश की मिट्टियां
- अन्य मिट्टियां
प्रायद्वीपीय मिट्टियां
प्रायद्वीपीय मिट्टियां प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए यहां की मिट्टियां पुरानी हैं। उर्वरता, रंग और संरचना के आधार पर प्रायद्वीपीय मिट्टियों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। यथा– काली, लाल व पीली तथा लैटेराइट मिट्टी।
काली मिट्टी
दक्षिण की ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। चूंकि यह रेगुर या कपास पैदा करने वाली मिट्टी होती है, इसलिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस किस्म की मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चूना तथा जीवाष्मों की अधिकता पाई जाती है। ज्वालामुखी चट्टानों के अतिरिक्त ये मिट्टियां तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों की फेरूजिनियस, नीस और शिष्ट चट्टानों से भी निर्मित होती हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी अक्षांश में 10° से 25° तक तथा पूर्वी देशांतरों के बीच 73° से 80 तक पाई जाती है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है। यह मिट्टी विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्यप्रदेश, दक्षिण ओडीशा, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्रप्रदेश के दक्षिण और तटवर्तीय भाग, तमिलनाडु, राजस्थान के बूंदी, टोंक और झालावाड़ तथा उत्तर-प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में मिलती है।
उपर्युक्त काली मिट्टी के क्षेत्रों में बहुत से क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ हैं जबकि कुछ पठारी क्षेत्रों में मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं। ढलानों पर ये मिट्टियां कुछ रेतीली हैं और पठारी भूमि पर उपयुक्त वर्षा होने के कारण उपजाऊ हैं। पहाड़ और मैदान के बीच की मिट्टी अधिक काली गहरी और उपजाऊ होती है। पहाड़ियों से पानी के साथ बहकर आने वाली सामग्री के जमा होते रहने के कारण इनकी उर्वरता निरंतर बढती जाती है। वैसे निचले क्षेत्रों की काली मिट्टी की अपेक्षा उपरी क्षेत्रों की कलि मिट्टी की उर्वरता अपेक्षाकृत होती है।
भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेयरी मिट्टी (कपास के लिए उपयुक्त) से तथा रूस की शरजानम मिट्टी से की जा सकती है। इस काली मिट्टी की विशेषता यह है कि यह अत्यधिक काली, मटियारी और बहुत महीन कणों वाली होती है और बिना खाद के प्रयोग के भी यह हजारों वर्षों तक उपजाऊ बनी रहती है। काली मिट्टी में कैल्सियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में मिले होते हैं। ये मिट्टियां गीली हो जाने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती हैं| और सूखने पर सिकुड़ जाती हैं और इसमें बहुत लम्बी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में अघुलनशील अंश 68.71 प्रतिशत, फेरिक ऑक्साइड 11.24 प्रतिशत, एलुमिना 9.39 प्रतिशत, जल और जीवांश 5.83 प्रतिशत, चूना 1.81 प्रतिशत तथा मैग्नीशियम 1.79 प्रतिशत पाये जाते हैं। ध्यातव्य है कि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा तम्बाकू, ज्वार-बाजरा और मूंगफली आदि फसलें भी इस मिट्टी में उगाई जाती हैं।
लाल व पीली मिट्टियां
यह मिट्टी दक्षिण भारत के अधिकांश भू-भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्र लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट जैसी पुरानी चट्टानों के टुकड़ों से हुआ है। यह हल्की कंकरीली और प्रवेश योग्य होती है। कहीं-कहीं इसका रंग पीला, भूरा, चाकलेटी और काला भी पाया जाता है। रंग की विभिन्नता का कारण लोहे के अंश की विभिन्नता है। यह मिट्टी दक्षिण भारत के अलावा बिहार के संथाल परगना और छोटानागपुर पठार, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिले (बांकुरा, वीरभूमि, मिदनापुर), कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण-पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी-दक्षिणी आंध्रप्रदेश, मेघालय, ओडीशा, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है।
काली मिट्टी की अपेक्षा इसमें चूना, फेरस ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा कम होती है। सामान्यतया इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सड़े-गले जीवाष्म की भी कमी होती है। स्थानों के आधार पर मिट्टियों के प्रकार में थोड़ा-बहुत फर्क पड़ता है। पठारी भागों में ये मिट्टियां कमजोर, कंकरीली और हल्के रंग की होती हैं, जबकि निचले मैदानों और घाटियों में पाई जाने वाली लाल मिट्टियां अधिक उपजाऊ, गहरी और गहरे रंग की होती है।
लाल मिट्टी साधारण किस्म की मिट्टी होने के कारण विविध फसलें उत्पन्न करती है। यथा- ज्वार, बाजरा कपास, गेगुन मोटे अनाज, दलहन, रागी, तम्बाकू और साग सब्जियां आदि। निम्न क्षेत्रों की गहरे लाल रंग की मिट्टी अधिक गहरी उअर उपजाऊ’ होती है, जिसमें सिंचाई द्वारा गन्ना भी उगाया जाता है। उच्च भागों की लाल मिट्टी पर मूंगफली और आलू का उत्पादन किया जाता है।
लैटेराइट मिट्टी: इस मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु की विशिष्ट स्थितियों में होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इसका स्वरूप चट्टानों की तरह होता है। गीली होने पर यह मिट्टी कांप बन जाती है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडीशा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय और बिहार के संथाल परगना जिले में मिलती है। लैटेराइट मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में लौह फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। निम्न भाग की लैटेराइट मिट्टियों पर खाद की सहायता से गन्ना, रागी और धान का उत्पादन होता है। ऊपरी भाग की मिट्टियों में पशुओं के लिए चारे का उत्पादन होता है।

हिमालय पर्वत की मिट्टियां
इस पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हिमालय पर्वत की मिट्टियों का निर्माण अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अभी यह मिट्टी बाल्यावस्था में है और पतली, दलदली, तथा छिद्रयुक्त है। इसकी गहराई नदियों की घाटियों, और पहाड़ी ढालों पर अधिक होती है। पहाड़ी ढालों पर सामान्यतया हल्की बलुई, छिछली व छिद्रयुक्त मिट्टियां पाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय के ढालों पर भारी बलुई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय की मिट्टियों में वनस्पति के अंश की अधिकता है, जिसके कारण यह अधिक उपजाऊ है। वैसे पर्वतीय मिट्टियों का विकास अन्य मिट्टियों की अपेक्षा कम हुआ है। इन पर्वतीय मिट्टियों को उनकी संरचना, कणों के आकार और फसल उत्पादन की विशेषता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है-
आग्नेय मिट्टी: आग्नेय मिट्टी का निर्माण हिमालय में पाई जाने वाली ग्रेनाइट और डायोराइट नामक आग्नेय चट्टानों द्वारा हुआ है। चूंकि इन मिट्टियों में नमी बनाए रखने की शक्ति मौजूद रहती है, इसलिए इन पर खेती करना सरल होता है।
चूना व डोलोमाइट निर्मित मिट्टी: हिमालय के कई भागों में चूना व डोलोमाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों के निकटवर्ती भागों में ही चूनायुक्त मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्षा होने पर चूने का अधिकांश भाग इस मिट्टी में से बहकर निकल जाता है, थोड़ा-बहुत अंश धरती पर रह जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार की भूमि अनुपजाऊ या बीहड़ बन जाती है। इस मिट्टी में चीड़, साल आदि के वृक्ष उगते हैं और कहीं-कहीं तो घाटियों में चावल भी उगाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से नैनीताल, मसूरी और चकराता के निकट पाई जाती है।
पथरीली मिट्टी: इसका क्षेत्र हिमालय का दक्षिणी भाग है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए पत्थरों को निचले ढालों पर इकट्ठा करने के उपरांत होता है। पथरीली मिट्टी की विशेषता यह है की इसके कण मोटे होते हैं, क्योंकि इसमें कंकड़-पठार के टुकड़े मिले हुए होते हैं।
चाय की मिट्टी: मध्य हिमालय के पर्वतीय ढाल वाली मिट्टी में वनस्पति के अंश की प्रचुरता होती है और लोहे की मात्रा अधिक तथा चूने की मात्रा कम होती है। चूंकि इस प्रकार की मिट्टी चाय उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है, इसलिए इसे चाय मिट्टी कहा जाता है। चाय मिट्टी प्रमुख रूप से देहरादून, कांगड़ा, दार्जिलिंग तथा असम राज्य के पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है।
टरशियरी मिट्टी: इस मिट्टी का निर्माण हिमालय प्रदेश की घाटियों में होता है। यद्यपि इन मिट्टियों की गहराई कम होती है, तथापि यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। टरशियरी मिट्टी मुख्य रूप से दून तथा कश्मीर की घाटी में पाई जाती है। इस मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें हैं- चावल, आलू और चाय।
विशाल मैदान की मिट्टियां
भारत के विशाल क्षेत्र में नदियों की घाटियों में मैदानों का निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा अपने मार्ग-परिवर्तन के द्वारा अलग-अलग मैदान का निर्माण किया गया है। नदियों द्वारा बाढ़ में लायी गयी कांप के इन क्षेत्रों में बिछाने से जलोढ़ मिट्टी का विशाल क्षेत्र निर्मित हो गया है और नदियों ने जैसे-तैसे अपना मार्ग परिवर्तित किया है, वैसे-वैसे जलोढ़ और पुरानी-जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण हो गया है। विशाल मैदान में अधिकांश जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है।
जलोढ़ मिट्टी: इसप्रकार मिट्टी स्थानांतरित होती है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रवाली है। इस मिट्टी की प्रकृति अन्य मिट्टियों से सर्वथा भिन्न होती है। जलोढ़ मिट्टी अपनी ऊपरी परत को हमेशा परिवर्तित करती रहती है। जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं- खादर और बांगर। खादर मिट्टी हल्के रंग की होती है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है तथा नए जलोढ़ द्वारा बिछाई जाती है। दूसरी ओर, बांगर मिट्टी गहरे रंग की होती है और इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है तथा इस प्रकार की मिट्टी में कांप की अधिकता होती है। यदि स्थूल रूप से देखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिन क्षेत्रों में नदियों द्वारा बाढ़ में बहाकर लायी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी अब नहीं पहुंच पाती, वहां मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है और उसे ही बांगर मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात्, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है।
फिर, जिन क्षेत्रों में वर्तमान में नदियों द्वारा बाढ़ के साथ नयी जलोढ़ मिट्टी को बिछाया जा रहा है, वहां की मिट्टी को खादर की संज्ञा दी जाती है। साधारणतः, जलोढ़ मिट्टी के प्रकारों में कोई स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता। जलोढ़ मिट्टी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्वरूप लिए हुए है और इसका कारण जलवायु, वनस्पतियां तथा सतही परिस्थितियां हैं। जलोढ़ मिट्टियां नाइट्रोजन और खाद (ह्यूमस) के लिए विशिष्ट हैं।
जलोढ़ मिट्टी गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और खेडा जिले, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियों में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की भूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24 प्रतिशत है। यह मिट्टी मोटे अनाजों, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। भारतीय मैदान के पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी जूट के उत्पादन के लिए भी अनुकूल है।
अन्य मिट्टियां
वन्य मिट्टी: इस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। ये मिट्टियां उन क्षेत्रों को घेरती हैं, जहां या तो पर्वतीय ढाल हों या वन्य क्षेत्रों में घाटियां हों। इस मिट्टी की संरचना और प्रकृति, भू-संरचना, पारिस्थितिकी, जलवायु, पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पतियों एवं अन्य कारकों से नियंत्रित होती है। वन्य मिट्टी में जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है और ये मिट्टियां रासायनिक एवं यांत्रिक सम्मिश्रण को प्रदर्शित करती हैं। वन्य मिट्टियां पोटाश, फॉस्फोरस और चूना पत्थर (लाइम) की उपलब्धता की दृष्टि से विशिष्ट हैं। अच्छे उत्पादन के लिए इस प्रकार की मिट्टी का उर्वरण अत्यावश्यक है।
वन्य मिट्टी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मद्रास (वर्तमान चेन्नई) के नीलाम्बर टीक वन, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर आदि में मिलती हैं।

चाय, कहवा, उष्णकटिबंधीय फल और मसालों का उत्पादन दक्षिणी भारत की वन्य मिट्टी में होता है। कुछ राज्यों में गेहूं, मक्का, जौ आदि का भी उत्पादन वन्य मिट्टी में होता है।
मरुस्थलीय मिट्टी: इस प्रकार की मिट्टी सिंधु और अरावली के बीच (पंजाब और राजस्थान में) उड़ती हुई रेत की भांति मिलती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील नमक की मात्रा उच्च होती है, परंतु इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है। ये मिट्टियां फॉस्फेट की उपलब्धता की दृष्टि से तो धनी हैं, किंतु नाइट्रोजन की उपलब्धता की दृष्टि से निर्धन हैं।
हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है। कुल मिलाकर 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है।
अनेक प्रकार की फसलों की कृषि इस मिट्टी में होती है। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग के बाद मरुस्थलीय मिट्टी कपास और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मिट्टी के रूप में पहचानी गयी है।
लवणीय एव क्षारीय मिट्टी: ये अनुर्वर एवं अनुत्पादक मिट्टियां रेह, ऊसर एवं कल्लर के रूप में भी जानी जाती हैं तथा ये एक प्रमुख मिट्टी समूह हैं। लवण, लवणीय मृदा का निर्माण क्लोराइड सम्मिश्रित होता है। ये मिट्टियां अपने में मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्सियम लवण समाहित करती हैं।
उत्तरी भारत के सूखे एवं अर्द्ध सूखे क्षेत्रों, यथा- पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में इस मिट्टी का विस्तार है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी भारत में लगभग 170 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलती है।
पीट एव अन्य जैविक मिट्टी: उच्च घुलनशील लवण एवं जैविक पदार्थों से युक्त पीट मिट्टी केरल के अलप्पी और कोट्टायम जिले, बिहार के पूर्वोत्तर भाग, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इन मिट्टियों में पोटाश और फॉस्फेट की कमी होती है। कच्ची या दलदली मिट्टी में वानस्पतिक पदार्थ की मात्रा उच्च होती है तथा यह उत्तरी एवं मध्य बिहार, ओडीशा के तटीय भागों, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिलती है।
दलदली मिट्टियां: अधिक दिनों तक पानी जमा रहने और वनस्पतियों के सड़ने के बाद जो मिट्टी बनती है, वह दलदली मिट्टी कहलाती है। ये मिट्टियां सामान्यतः नीले रंग की होती है, क्योंकि इसमें जीवांश और लोहे का अंश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये मिट्टी मुख्य रूप से ओडीशा के समुद्रतटवर्ती प्रदेश, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर पाई जाती है।