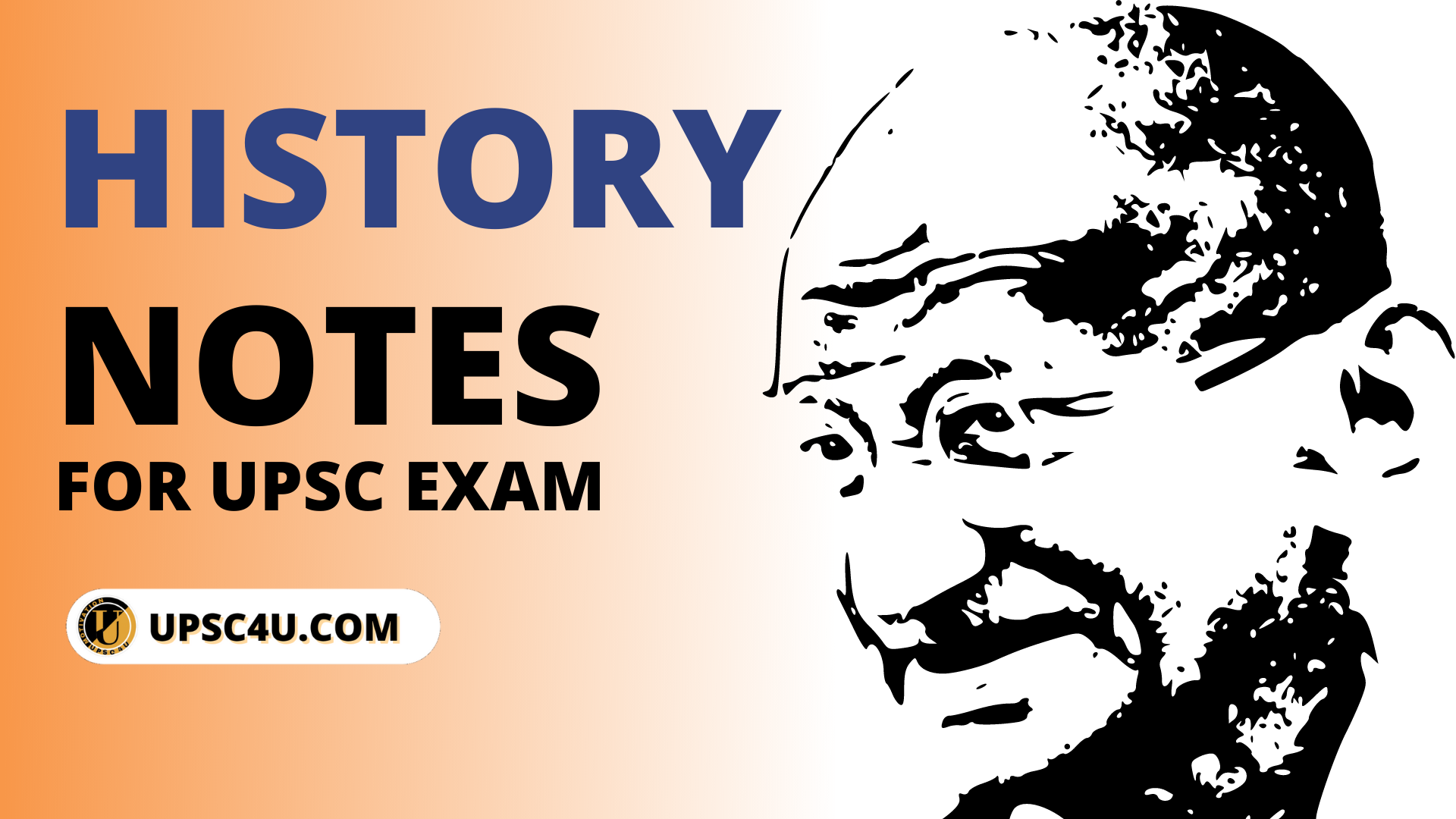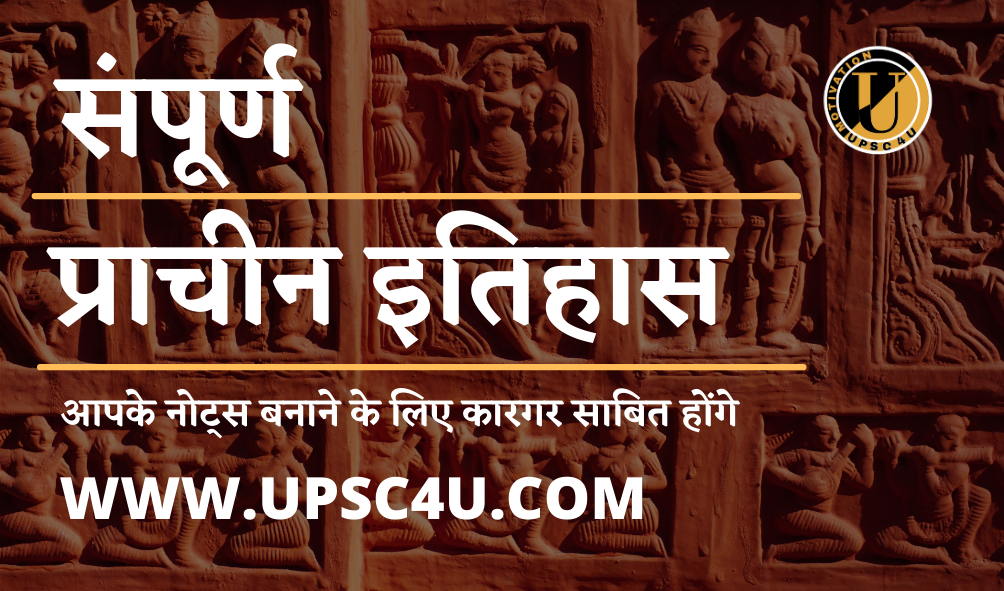मुगलकाल में औद्योगिक विकास की क्या स्थिति थी, इस विषय में विदेशी यात्रियों और तत्कालीन इतिहासकारों के विवरणों से महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
कारखाना का शब्दिक अर्थ है, वह स्थान जहाँ लोगों के प्रयोग के लिए कार्यशालाएँ हों। परन्तु मध्ययुग में इस शब्द की ध्वनि नितान्त भिन्न थी। मध्ययुगीन इतिहासकारों ने इसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है जिसके अनुसार कारखाना के अंतर्गत कार्यशालाओं के अतिरिक्त अन्य चीजे भी सम्मिलित थीं जैसे कि भंडार, शाही दरबार, सुल्तान की निजी सेवाएँ एवं पशुओं के बाडे इत्यादि। मुगल इसके लिए बयूतात शब्द का प्रयोग करते थे जो कि अरबी भाषा के शब्द बैत का द्विवचन/बहुवचन है। बैत का अर्थ है घर। अत: घरबार के संदर्भ में बयूतात का अर्थ मुगल प्रशासकों के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट था। कारखानों या बयूतात जैसा कि इस विभाग का नाम था, के अंतर्गत वे कारखाने और भंडार आते थे जिनका रखरखाव सरकार राज्य के इस्तेमाल के लिए करती थी। मोती और हीरे-जवाहरात से लेकर तलवारों, तेगों, तोप-बंदूकों और भारी गोला बारूद तक की खरीद-फरोख्त और रखरखाव इसी विभाग की जिम्मेदारी थी। सेना के लिए घोडे और हाथी, सामान ढोने वाले टट्टू, जानवर और शाही शिकार के लिए अन्य पशुओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भी बयूतात की ही थी। यह विभाग न केवल सब प्रकार की वस्तुओं की खरीद और भंडारण करता था अपितु युद्ध के लिए अस्त्र-शस्त्र एवं विलास-सामग्रियों के निर्माण का सबसे बड़ा अभिकरण भी था। यद्यपि बयूतात का स्वामित्व एवं प्रबंध राज्य के हाथ में था फिर भी इसे पूर्णत: व्यापारिक ढंग से चलाया जाता था। कारखानों की भूमिका न केवल घरेलू अपितु साम्राज्य के सैन्य एवं वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त राज्य की औद्योगिक प्रगति को भी ये प्रभावित करते थे।
मध्ययुगीन शासकों के विलास, उनके दरबारों, अंत:पुरों की साज-सज्जा एवं शानशौकत के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उनका निर्माण सामान्य बाजार में होना कठिन था। अत: शासकों को बाध्य होकर इनके निर्माण के लिए सरकारी कारखाने लगवाने पड़े। कारखानों की व्यवस्था कदाचित् फारस से ली गई हैं किन्तु वास्तव में कारखानों का प्रसंग मौर्य शासकों, अलाउद्दीन खलजी एवं फिरोज तुगलक के समय में भी आता है। मिस्र में भी सरकारी और निजी उद्यमों के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाया गया है। सरकारी उद्यम शाही परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की पोशाके बनाते थे।
सल्तनत काल के सभी कारखानों को उचित रूप से कारखाने या कार्यशालाएँ नहीं कहा जा सकता। इनमें से कुछ तो कारखाने थे जबकि अन्य शाही विभागों एवं सुल्तान की निजी सेवाओं और पशुओं के बाड़ों से सम्बन्धित थे।
कारखानों का एक महानिदेशक होता था। जब सुल्तान कोई चीज बनवाना चाहता तो सबसे पहले शाही हुक्म तश्तदारखाना और ख्वाजा जहाँ-ए-सल्तनत के पास भेजा जाता था। मुगल साम्राज्य में सरकारी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ शासन स्वयं उपलब्ध कराता था। इसके लिए स्वयं सरकार लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन करती थी। इसके अतिरिक्त बेहतरीन किस्म की चीजें भी वहीं बनाती थीं।
बड़े स्तर पर उत्पादन न होने के कारण सामान्य बाजार सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। आज जो सरकार बाजार से तैयार वस्तुएँ खरीदती है या ठेकेदारों को बड़ी मात्रा में वस्तुएँ उपलब्ध कराने का आदेश देती है, वह कुटीर उद्योगों के उस काल में सम्भव नहीं था। साथ ही पूँजीपति बिक्री को दृष्टि में रखकर बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करवाते थे। अत: सरकार के पास इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था कि अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करे। राज्य की वस्तुओं की आवश्यकता कितनी बड़ी होती थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल में दो बार, सर्दियों और बरसात के मौसम में, पोशाके तैयार रखनी पड़ती थीं। राज्य स्वयं अनेक कारखाने चलाकर इन वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता था। ये कारखाने साम्राज्य के प्रमुख शहरों में लगाए गए थे जहाँ कुशल कारीगरों को (कभी-कभी तो दूर-दूर से) लाकर रखा जाता था। ये कारीगर एक सरकारी दरोगा की निगरानी में कार्य करते थे और उन्हें दैनिक मजदूरी दी जाती थी। इनके द्वारा तैयार की गई हस्तशिल्प की वस्तुओं के भंडारण की उचित व्यवस्था की जाती थी। शाही घराने के लिए आवश्यक उपभोक्ता एवं विलास वस्तुओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए ऐसी ही व्यवस्था की जाती थी। इसमें संदेह नहीं कि मुगल बादशाह कारखानों में विशेष रुचि लेते थे। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि शासकीय कारखाने न केवल केद्रीय अपितु प्रान्तीय मुख्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में भी लगाए जाएँ।दरबारी इतिहासकारों एवं विदेशी यात्रियों की टिप्पणियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल सम्राट् कारखानों एवं कार्यशालाओं में कितनी रुचि लेते थे- कुशल विशेषज्ञों और कारीगरों को देश में बसाया गया था ताकि वे लोगों को उत्पादन के सुधरे हुए तरीके सिखा सके। लाहौर, आगरा, फतेहपुर, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित शाही कार्यशालाएँ कारीगरी के अनेक अनुपम नमूने बनाती हैं, कारीगरों की अच्छी देखभाल की जाती है और इस कारण यहाँ के चतुर कारीगर शीघ्र ही अपने काम में कुशल हो गए हैं- शाही कार्यशालाएँ वे सब वस्तुएँ उपलब्ध कराती हैं जो दूसरे देशों में बनाई जाती हैं। बढ़िया वस्तुओं के प्रति रुचि आम हो गई है और दावतों के समय प्रयुक्त वस्त्रों का तो वर्णन करना कठिन है। अकबर अपने कारखानों एवं उनमें विभिन्न देशों के कारीगरों को भर्ती करने में और स्थानीय लोगों को कला में प्रशिक्षित करने में रूचि लेता था इसका विवरण आइन-ए-अकबरी में मिलता है। फादर मंसरात ने भी इसका उल्लेख किया है। मंसरात का कहना है कि अकबर स्वयं खड़े होकर आम कारीगर को काम करते हुए देखता था और कभी-कभी तो मनबहलाव के लिए स्वयं भी करने से नहीं हिचकिचाता था। जहाँगीर और शाहजहाँ भी कारखानों प्रश्रय देते रहे। जहाँगीर के समय में अनूठी वस्तुएँ बनाने एवं कुशल कारीगरों पारितोषिक दिए जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इनमें से सर्वोत्तम उदाहरण एक छुरी का है जिसकी मूठ काले धब्बों वाले दंदार-ए-माही (मछली दाँत) की बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त जहाँगीर ने एक सौ तोले उल्का पत्थर और सामान्य लोहे के मिश्रण से उस्ताद दाऊद द्वारा एक तलवार, एक छुरी और एक चाकू बनवाया था। इस तलवार की धार इतनी तेज थी कि सर्वोत्तम पानीदार तलवार से मुकाबला कर सकती थी। बंगाल का मुगल सूबेदार इस्लाम खान जब राजधानी राजमहल से ढाका ले गया तो उसने बढ़इयों, लुहारों, शस्त्र ढालने वालों एवं अन्य कारीगरों की सहायता से सरकारी जहाजघाटों, भंडारघरों और कारखानों का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के काल में कश्मीर और लाहौर का कालीन उद्योग श्रेष्ठता की ऐसी ऊँचाइयों पर पहुँचा कि सौ रुपए प्रति गज के से बनने वाले ऊनी कालीनों की तुलना में ईरान के शाही कारखानों में वाले ऊनी कालीन टाट प्रतीत होती थी। गृह-उद्योगों की ओर शाहजहाँ और कितना प्रश्रय देता था संयोगवश उसके एक दान के उदाहरण है। गद्दी पर बैठने से पहले जब उसकी लाडली बेटी बेगम साहिबा तो उसने पाँच लाख रुपए मक्का भेजने की मन्नत माँगी। जब वह गद्दी पर बैठा और उसकी बेटी ठीक हो गई तो उसने अपनी मन्नत पूरी की। किंतु और जहाँगीर की भाँति उसने रुपया नकद न भेजकर निर्देश दिया कि अहमदाबाद से उतनी धनराशि का माल खरीद कर हेजाज भेजा जाए और उसकी बिक्री से जो राशि प्राप्त हो उसे लाभांश सहित गरीबों और जरुरतमंदों में बाँट दिया जाए। उसने एक तृणमणि निर्मित दीपाधार शाही कारीगरों द्वारा तैयार करवा कर मक्का के पवित्र तीर्थ में भेजा। यह दीपाधार स्वर्णजाली के भीतर बना हुआ था और इसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उसकी लागत ढाई लाख रुपए थी।
दक्षिण में अपने उपराजत्व काल में औरंगजेब निरंतर इस प्रयास में रहता था कि मसुलीपट्टम के कुशल कपड़ा-छपाई करने वालों को दिल्ली या आगरा लाकर सरकार कारखानों में कार्य करने के लिए राजी किया जा सके। इसके लिए उन्हें लगभग बाध्य किया जाता था।
प्रांतों में लाहौर, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर और कश्मीर में सरकारी कारखाने थे। यहाँ के गवर्नर स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देते थे क्योंकि उन्हें अपने-अपने प्रांतों की अनूठी चीजें सम्राट् को भेजनी होती थीं। मनूची के अनुसार पादशाह और शहजादे इनमें से प्रत्येक प्रांत में अपने कारिंदे रखते थे जिनका कार्य था इन स्थानों की सर्वोत्तम वस्तुएँ लाकर उन्हें देना। वे निरंतर निगरानी रखते थे कि इस दिशा में इन प्रांतों के शासक क्या प्रयास करते हैं।
गोलकुंडा के सुल्तान की एक कार्यशाला थी। मुगल साम्राज्य के अनेक गवर्नरों के अपने निजी कारखाने थे, जहाँ कुशल कारीगर विलास की वस्तुएँ बनाते थे। यह बात मोरलैंड की धारणा से मेल खाती है कि कुछ लोगों के निजी कारखाने होते थे। कुछ स्थानीय शासकों जैसे कि बनारस के महाराजा की रामनगर में अपनी कार्यशाला थी।
कभी-कभी यूरोपीय कपनियों को भी केंद्रीकृत उत्पादन एवं नियंत्रण की आवश्यकता प्रतीत होती थी और उन्होंने भी अपने कारखाने स्थापित करने के प्रयास किए।
सरकारी कारखानों में बनने वाली वस्तुओं में खिलत विशेष उल्लेखनीय है। खिलत सम्मान की पोशाक होती थी जिसे विशेष अवसरों पर पादशाह विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान करता था। ये अवसर होते थे राज्यारोहण की वर्षगाँठ, दोनों ईदें, उत्सव का कोई भी अवसर इत्यादि।
कारखानेशाही वस्त्रागार के लिए पोशाके भी तैयार करते थे। साथ ही आभूषण, श्रेष्ठ नक्काशीदार वस्तुएँ जिनमें अत्यन्त कुशल कारीगरी होती थी। विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं भारी बंदूके एवं तोपें भी बनाई जाती थीं। तात्पर्य यह कि शाही परिवार के प्रयोग की अधिकांश वस्तुएँ विभिन्न सरकारी कारखानों में ही बनाई जाती थीं।
ये सरकारी कारखाने यद्यपि बड़े पैमाने के उद्योगों के ढरें पर ही चलाए जाते थे जिनमें कच्चा माल, औजार और कर्मशालाएँ सरकार ही मुहैया कराती थी। कारीगर का, जो कि वास्तव में उत्पादन करता था, सम्बन्ध केवल पारिश्रमिक पाने तक ही सीमित था। इन वस्तुओं के उपभोग का वह अधिकारी नहीं था। फिर भी ये उद्योग वास्तविक वाणिज्यिक कारखाने का रूप नहीं ले सके। इन कारखानों में पादशाहों की रूचि के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन होता था और उनमें कारीगरी का कमाल दिखाई देता था। इन वस्तुओं के उत्पादन लागत का भी ठीक-ठीक हिसाब रखा जाता था कितु वह उत्पादन निर्णायक पहलू नहीं होता था। सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं पादशाहों की श्रेष्ठ रूचि और कल्पनाशीलता की भी कोई सीमा न थी। परिस्थितियों में कारखानों का वाणिज्यिक उद्योगों के रूप में विकास सम्भव नहीं था। इसके विपरीत ये कारखाने पादशाहों की रूचियों, पसंद अं सरकारी आवश्यकताओं पर ही निर्भर थे। इसका निश्चित परिणाम मुगल साम्राज्य के पतन के साथ इन कारखानों का भी पतन हो गया। कारखानों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि व्यवस्था में कारीगर कला को परिष्कृत करने के लिए अत्याधिक प्रोत्साहन मिलता था।
वस्तुओं की गुणवत्ता पादशाहों की परिष्कृत रूचि पर आधारित होती थी और कारीगरों के लिए प्रतिमान स्थापित करती थी। इससे कुशल आदान-प्रदान हुआ। कारीगरी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती थी। इसी कारण जब मुगल साम्राज्य और उसके कारखाने न रहे तब भी देश में कारीगरी बची रही और चलती रही।
ये कारखाने किस प्रकार कार्य करते थे, इसकी जानकारी हमें उन विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है जो मुगल दरबार में आते थे। अकबर के समय में कारखानों के सम्बन्ध में दीवान-ए-बयूतात बहुत महत्वपूर्ण था। आगे चलकर सारे विभाग का दायित्व ही उसे सौंप दिया गया और प्रशासनिक मशीनरी में उसकी स्थिति स्थिर हो गई। अब उसे मीर-ए-सामान कहा जाने लगा। जहाँगीर के काल में उसके दायित्वों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है और उसे मीर-ए-सामान कहा गया है, न कि खान-ए-सामान।
जहाँ तक इस विभाग के अधिकारियों का सम्बन्ध है मीर-ए-सामान इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था जिस पर विभाग को सुचारू रूप से चलाने और इसकी निगरानी का दायित्व था। अन्य अधिकारी थे-
1. दीवान-ए-बयूतात- जो कि ऊँचे ओहदे का अधिकारी था और मुख्यत: विभाग का वित्तीय दायित्व सँभालता था।
2. मुशनिफ-ए-कुल-ओ-जुज (जिसका शब्दिक अर्थ है अंश का और सारे का लेखापाल) विभाग का मुख्य लेखापाल होता था। विभाग की प्रत्येक शाखा में उसका एक लेखापाल (मुशरिफ) होता था।
3. दरोगा- कारखाने की प्रत्येक शाखा में एक दरोगा होता था जिसका काम अपनी शाखा के कारीगरों से सीधा सम्बन्ध होता था। वही कारीगरों को प्रतिदिन काम बाँटता था और उन्हें दिए जाने वाले कच्चे माल के लिए उत्तरदायी होता था।
4. तहसीलदार- प्रत्येक कारखाने में दरोगा की ही भाँति एक तहसीलदार भी होता था जो अपनी शाखा के लिए आवश्यक माल और रोकड़ का प्रभारी होता था।
5. मुस्तौफी- यह कारखानों के लेखा का परीक्षण करता था, व्यय का मिलान व्यययंत्रों से करता था, वक्तव्य तैयार करके उस पर अपने हस्ताक्षर करता था, उसे विभाग के दीवान के समक्ष प्रस्तुत करता था और अंत में उस पर मीर-ए-सामान की मुहर लगवाता था।
6. दरोगा-ए-कचहरी- उस पर कार्यालय की सामान्य देखरेख का भार था। उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि कागजात और रजिस्टर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास उचित रूप से पहुँचे। वह यह भी देखता था कि कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कोई आपत्तिजनक व्यवहार न करे। वह सम्बंधित अधिकारी की मुहर सहित द्वारों पर ताला लगाता था और उस पर अपनी मुहर भी लगाता था।
7. नजीर– इसका ओहदा विभागीय दीवान सेनीचे होता था। वह पुन:रीक्षण अधिकारी होता था जो यह सुनिश्चित करता था कि कार्य अधिक कुशलतापूर्वक और सहीं ढंग से हो सके। जहाँ तक विभाग के वास्तविक कार्य का प्रश्न था, नजीर का सम्बन्ध विभाग के कार्यकारी पक्ष की अपेक्षा वित्तीय पक्ष से ही अधिक था। उसका पद निश्चित रूप से दीवान से नीचे था और भी किसी रूप में वह दीवान का समकक्ष नहीं था। जहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल में दरोगाओं और तहसीलदारों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। जब भी आवश्यकता होती, दरोगा और तहसीलदारों को अपने कारखानों में निर्मित वस्तुएं लेकर पादशाह के सामने जाने का अवसर मिलता था, किन्तु कार्यालय के रोजमर्रा के कामकाज को देखने वाले नजीर का उल्लेख नहीं मिलता, न तो उसके दायित्व ही दरोगा और तहसीलदार की भाँति महत्वपूर्ण थे और न ही उसका पद मीर-ए-सामान या दीवान की भाँति महत्वपूर्ण था।
जहाँ तक इन अधिकारियों के कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है विभागाध्यक्ष की हैसियत से मीर-ए-सामान का कार्य था कार्यकारी पक्ष का दायित्व सँभालना। वह प्रत्येक शाखा के आंतरिक कार्य पर आम निगरानी रखता था। दरोगाओं, मुशरिफों और तहसीलदारों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में उसे पहल करने का अधिकार था। उसे यह भी अधिकार था कि आवश्यकता पड़ने पर अपने किसी भी मातहत अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके। वह विभाग के सभी मामलों को देखता था और कारखानों को प्रांतों से मिलने वाले आदेशों को ग्रहण करता था। अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले या बड़े सौदे वह पादशाह के सामने रखता था और रोजमर्रा के मामले स्वयं ही निपटाता था। दीवान का कार्य था, विभाग का वित्तीय दायित्व सँभालना। इस रूप में उसे नजीर मुस्तौफी और मुशरिफ से कार्य लेना होता था। अन्य मामलों में भी वह कारखानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता था, किन्तु प्रत्येक मामले की जानकारी पहले वह मीर-ए-सामान को देता था। नियमानुसार उसे मीर-ए-सामान की सलाह पर ही कार्य करना होता था। जिस प्रकार दीवान और मुस्तौफी के जरिए अपने पास आने वाले वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कागजात पर मीर-ए-सामान विवरण पढे बिना अपनी मुहर लगा देता था, उसी प्रकार अन्य मामलों में दीवान मीर-ए-सामान के निर्णयों पर भरोसा करता था। नजीर के कोई स्पष्ट अधिकार और दायित्व नहीं होते थे और वह दीवान के साथ मिलकर ही कार्य करता था। उसकी उपस्थिति से लेखों का केंद्रीय लेखा-परीक्षा विभाग के सामने प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा के पुन:रीक्षण का कार्य सरल हो जाता था। मुस्तौफी सभी आवश्यक कागजात जुटाता था, विशेष रूप से प्रत्येक शाखा के तहसीलदारों एवं मुशरिफों से दैनिक प्रविष्टि पुस्तिका और दैनिक नगर रसीदों और वितरण का विवरण। वह लेखा में उल्लिखित प्रत्येक विवरण को एक-एक करके मिलाता था और उन पर दीवान के हस्ताक्षर करवाता था। यदि दीवान किसी बात का स्पष्टीकरण चाहता तो मुस्तौफी उसे स्वयं अपनी कलम से लिख लेता था। लेखा के स्वीकृत हो जाने पर वह धन का माँग-पत्र तैयार करता था, उस पर दीवान के हस्ताक्षर लेकर उसे कचहरी के दरोगा को सौंप देता था ताकि धनराशि प्राप्त की जा सके। यह देखना दीवान का दायित्व था कि उसके विभाग में किसी को भी कठिनाई न हो। अपने हाथ से गुजरने वाले सभी सौदों और लेखों के लिए वह उत्तरदायी होता था। प्रत्येक तहसीलदार के अंतर्गत आने वाले विभाग की आय एवं व्यय का विवरण और प्रत्येक कारखाने के आम हालात एवं लेखों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भी वह तैयार करता था।
शाखा की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक धन तहसीलदार के पास रहता था। शाखा विशेष में होने वाले कार्य के लिए आवश्यक कच्चे माल का भंडार भी वही रखता था। उसी से धन या माल लेकर दरोगा अपने मातहत कार्य करने वाले कारीगरों को बाँटता था। शाम के समय दरोगा कारीगरों से वस्तुओं को, वे निर्माण की जिस भी अवस्था में होतीं, वापस ले लेता था और प्रत्येक कारीगर के कार्य की मात्रा का हिसाब लिखकर वस्तुओं को तहसीलदार के पास जमा करवा देता था। अधबनी वस्तुओं को दरोगा अगले दिन फिर जारी करवा कर कारीगरों को दे देता था। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती रहती थी जब तक कि वह वस्तु पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जाती थी। कार्य समाप्त हो जाने पर इन नियमित प्रविष्टियों के आधार पर कार्य के कुल दिनों के पारिश्रमिक का और कच्चे माल पर होने वाले व्यय का भी हिसाब लगाया जाता था जिसके आधार पर उस वस्तु की लागत का निर्धारण किया जाता था। अंत में बनने वाली रिपोर्ट में उस वस्तु का लागत मूल्य, कारीगर का नाम और उस दरोगा का नाम भी अंकित होता था जिसकी निगरानी में यह कार्य हुआ था।
प्रत्येक शाखा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी, भले ही वह रसोई का विभाग हो जहाँ अनाज इत्यादि की आपूर्ति की जाती थी या भवन-निर्माण का विभाग हो जहाँ ईंटों की संख्या, पत्थरों का आकार एवं उस क्षेत्र में प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाली अन्य सभी सामग्रियों का विवरण रखा जाता था।
इस प्रकार तहसीलदार और दरोगा का कारीगरों से सीधा सम्पर्क रहता था। तहसीलदार आवश्यक धन और कच्चे माल का भंडार अपने पास रखता था। दरोगा उसे कारीगरों में बाँटता था और कार्य की निगरानी करता था। उसी शाखा का मुशरिफ प्रतिदिन का हिसाब रखता था, प्रतिदिन अग्रिम दिए जाने वाले धन, कच्चे माल और किए गए कार्य की प्रविष्टियाँ करके हिसाब मुस्तौफी को सौंप दिया जाता था और तहसीलदार, दरोगा और मुशरिफ इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते थे।
कचहरी का दरोगा इसके एवं अन्य उच्च अधिकारियों के बीच कडी का कार्य करता था। सभी आवश्यक कागजात को प्रत्येक चरण या उनके गतव्यों तक भेजना उसी का उत्तरदायित्व था।
मीर-ए-सामान और दीवान-ए-बयूतात कारखानों के प्रबंध के लिए और सुचारू कार्य-संपादन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते थे किंतु इसके बावजूद अंदरूनी कामकाज और प्रक्रियागत बारीकियों से ज्ञात होता है कि मीर-ए-सामान की स्थिति विभाग के दीवान से थोड़ी ऊँची थी, किंतु दीवान को उसका मातहत नहीं कहा जा सकता था।
दोनों को ही दरबार में जाने और पादशाह के सामने अपने-अपने दायित्वों से संबंधित मामलों को रखने का अधिकार था, किंतु मीर-ए-सामान को वरीयता प्राप्त थी और उसे यह अधिकार भी था कि अपने विभाग की आवश्यकताओं को पादशाह के सामने रख सके, जबकि प्रतीत होता है कि दीवान का अधिकार पादशाह के सामने आवश्यक कागजात रखने भर तक सीमित था।
मीर-ए-सामान का ओहदा इस कारण भी दीवान से ऊँचा था कि वह फरमानों पर मुहर लगाता था। विभाग के प्रकायाँ एवं कार्यों के विभाजन से भी यही अंतर स्पष्ट होता है। सभी महत्वपूर्ण कागजात पर मीर-ए-सामान के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक थे। पद के अनुसार उनकी हैसियत के सम्बन्ध में अकबर के काल में बहुत कम जानकारी मिलती है, किंतु जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों के समय में मीर-ए-सामान पद और हैसियत में निश्चित रूप से दीवान से ऊँचा था।
कारखानों की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण मीर-ए-सामान अर्धवार्षिक आधार पर तैयार करता था और उसे पादशाह की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता था। शाही स्वीकृति एक फरमान के रूप में मिलती थी जिसे बरत/बारात कहते थे। रोकड़, बाकी, भंडारों में वस्तुओं की मात्रा की संख्या, उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न कार्य, उन पर होने वाले व्यय, इन सब का लेखा लेखाकारों को रखना होता था, जो समय-समय पर पादशाह के सामने परीक्षण के लिए रखा जाता था। इसी लेखे में अचानक आ पड़ने वाले व्यय की स्वीकृति के लिए भी व्यवस्था होती थी जो अर्धवार्षिक बजट में पहले स्वीकृत न हुआ हो। ऐसे अवसरों पर पादशाह अपनी रुचि की किसी भी वस्तु के निर्माण की आज्ञा देता था और अन्य विभागों द्वारा या शहजादे और अमीरों द्वारा दी गई आज्ञाओं पर भी स्वीकृति देता था और कारखानों के लेखा विभाग द्वारा वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों का अनुमोदन भी करता था।
पादशाह की आज्ञा यह भी होती थी कि राजधानी के प्रांतीय कारखानों में निर्मित बहुमूल्य एवं कलात्मक वस्तुओं को दीवान-ए-आम में उसके सामने पेश किया जाए और प्रदर्शित वस्तु के साथ उसे बनाने वाले कारीगर को भी। युद्ध के शस्त्रास्त्र, विलास या उपभोग की वस्तुएँ ऐसी थीं जो अपने महत्व या कारीगरी के कारण पादशाह की रुचि का विषय हो सकती थीं सामने पेश की जाती थीं। इस व्यवस्था से पादशाह को अपने कारीगरों को व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर मिलता था, ताकि वे सरकारी नौकरी पा सके और पादशाह के सामने पेश होने का फ़ख्र हासिल कर जिसे वे सबसे बड़ा सम्मान समझते थे। इस प्रकार प्रत्येक उपलब्धि का केवल विभाग और इसके उच्चाधिकारियों को ही नहीं अपितु कारीगरों को मिलता था। कभी-कभी तो इन्हें मौलिक नमूनों, श्रेष्ठ काम और अनूठी कारीगरी के लिए इनामो-इकराम से मालामाल कर दिया जाता था।
केंद्रीय सरकार की कारखानों की इस व्यवस्था से न केवल उचित मूल्यों पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी अपितु इससे देश के विभिन्न भागों के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता था। इन कारखानों की सुधरी हुई कार्य-पद्धति एवं यहाँ निर्मित वस्तुओं को स्थानीय कारीगर अपना आदर्श बनाते थे।
लोगों के आर्थिक जीवन पर इन कारखानों का जो प्रभाव पड़ा उसे नगण्य नहीं का जा सकता। शाही कर्मशालाओं में उत्पादन की श्रेष्ठता के मानक स्थापित होते थे जिनकी नकल की जाती थी। इस प्रकार अन्य कारीगरों की कारीगरी में भी सुधार होता था। शाही कर्मशालाओं में कार्य करने वाले कारीगर बड़ी लगन और मेहनत से कार्य करते थे ताकि वे पादशाह से प्रशंसा और इनाम प्राप्त कर सके।
सोने और चाँदी के काम, ताँबे के पात्र बनाने, कपड़ा और कालीन उद्योग, लुगदी और हाथीदाँत के काम में जो मानक मुगल काल में स्थापित हुए उनकी मिसाल नहीं मिलती। इनमें से कुछ शिल्प तो समाप्त ही हो गया है। ढाका की पारदर्शी मलमल और कश्मीर के हल्के-फुल्के शालों को बनाने का रहस्य सदा के लिए लुप्त हो गया। मुगल काल के थोडे बहुत अवशेषों से ही इन वस्तुओं की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। विदेशी शासन के काम आने वाली अराजकता ने परंपराओं को नष्ट कर दिया। जीवन का आर्थिक ढर्रा ही बदल गया। कोई प्रोत्साहन देने वाला न रहा और बाहर से आने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा ने परंपराओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथापि मुगल काल में ये हस्तशिल्प देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और शाही घराने से जुड़ी कर्मशालाओं ने इनके पोषण में बड़ा योगदान किया। कई अन्य क्षेत्रों में भी कारखानों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। शाही फल भंडार, फलों की सुधरी किस्मों की खेती को प्रोत्साहन देता था, शाही बागीचों में फलों की किस्में सुधारने और विदेशों से नई किस्में मंगाकर अपने यहाँ उगाने के प्रयास निरन्तर होते रहते थे, शाही कुतुब खानों में सर्वोत्तम सुलेखकारों और चित्रकारों को नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार इन कलाओं और जिल्द बाँधने की कला में नए-नए प्रयोग किए गए।
कारीगर सरकारी कारखानों में कार्य पाने को बड़े लालायित रहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह थ की अपने बलबूते पर कम करने वालों की स्थिति बड़ी दयनीय रहती थी। मजदूर की अच्छी स्थिति नहीं थी और न ही देहस के सच्चे आर्ह्तिक विकास में सहायक। राजधानी, जो की देश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध नगर था, एक भी ऐसा निजी कारखाना या कर्मशाला नहीं थी जिनका प्रबंध कुशल शिल्पी स्वयं करते हों। बर्नियर की टिप्पणी उचित ही है- यदि कारीगरों और उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाए तो उपयोगी कलाएं और ललित कलाएं फले-फुलेंगी, किन्तु ये अभागे तो तिरस्कृत हैं, इनके साथ बड़ा रुखा रुखा व्यवहार किया जाता है और इन्हें इनके काम का उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता अमीरों को प्रत्येक वस्तु सस्ती दर पर मिलती है। जब किसी उमरा या मनसबदार को किसी कारीगर की आवश्यकता होती है तो वह उसे बाजार से बलपूर्वक बुला भेजता है। उसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है औए जब कार्य पूरा हो जाता है, तो हृदयहीन मालिक उसे श्रम के हिसाब से नहीं अपनी इच्छानुसार थोड़ा बहुत पारिश्रमिक दे देता है। कारीगर तो इसी में खैर मनाता है कि उसे मजदूरी के बदले कोड़े नहीं खाने पड़े…….। फिर ऐसी आशा कैसे की जा सकती है कि कारीगर या उत्पादक प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित हो…….। केवल वे ही कारीगर अपनी कला के क्षेत्र में कुछ नाम कमा सकते हैं जो या तो पादशाह या किसी बड़े उमरा की सेवा में हों और केवल अपने आश्रयदाता के लिए कार्य करते हों। इस कारण कारीगर यही अच्छा समझते थे कि वे किसी सरकारी कारखाने में नौकरी पा जाएँ ताकि कार्य के अनुसार, दैनिक या मासिक आय सुनिश्चित हो और उन्हें अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सके। जबाबित-ए-आलमगीरी के अनुसार सत्रहवीं शती के अंत तक शाही कारखानों की संख्या 69 थी किन्तु अठारहवीं शती के मध्य शकीर खान के संस्मरणों के अनुसार केवल 36 ही रह गई थी। इससे ज्ञात होता है कि मुगल साम्राज्य के उत्तरार्ध में कारखानों में गिरावट आ गई थी। ये 18वीं शती के आठवें दशक तक चलते रहे।
कारखानों ने शहरी जीवन और गाँवों एवं कस्बों के सम्बन्धों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। ये श्रमिकों की गाँवों से शहर की ओर गतिशीलता में सहायक हुए। ग्रामीण क्षेत्रों के जाने माने कारीगरों को स्वेच्छा से या बलपूर्वक राज्य के कारखानों में लाया जाता था (जैसा कि दक्षिण में औरंगजेब के काल में मसुलीपतनम नगर के कपडा छपाई करने वालों के साथ हुआ था)। इस प्रकार अपने व्यवसाय में विशेष योग्यता के कारण कारीगरों को हैसियत मिलती थी। इसके अतिरिक्त कारखानों ने जातियों एवं शिल्प संघों के संघटन को सुदृढ़ किया।
शिल्पकला की दृष्टि से अट्टालिकाओं के निर्माण में स्वाभाविक रूप से संगतराशों, शिल्पियों और बढ़ईयों को प्रोत्साहन दिया, साथ ही यह एक मध्यवर्ग का भी उद्यम होने लगा जिसमें दुकानदार, व्यापारी, दलाल, जहाज बनाने वाले जैसे वर्ग सम्मिलित थे। पेलसर्ट का कहना है कि- कर्मकार की तुलना में दुकानदार को अधिक आदर की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे खाते-पीते भी हैं किन्तु वे इस तथ्य को प्रकट नहीं होने देते। प्रांतीय गवर्नर और अमीर भी स्थानीय कारीगरों और कर्मकारों को बढ़ावा देते थे…..या तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के देने के लिए या अपने से बड़े लोगों को उपहार देने के लिए।
कारीगरों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में कुछ छुट-पुट जानकारी बाबर के संस्मरणों, आइन-ए-अकबरी और विदेशी यात्रियों की टिप्पणियों में मिलती है, किन्तु तत्कालीन विवरणों में इसका कोई क्रमबद्ध वर्णन नहीं मिलता। अपने संस्मरणों में बाबर हर तरह के असंख्य कर्मकारों का उल्लेख करता है। उसके अनुसार, विभिन्न शिल्पों और उद्योगों में असंख्य कारीगरों का होना हिन्दुस्तान में लाभप्रद था। अबुल फजल उस्तादों और कारीगरों के देश में बसने की बात कहता है। वह विभिन्न श्रेणी के कुशल और अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक का भी उल्लेख करता है। दिल्ली में कुशल शिल्पियों की कोई अपनी स्वतंत्र कर्मशाला नहीं थी। अधिकांश कारीगर राजकीय कारखानों में नौकरी पा जाने पर अपने आपको भाग्यवान समझते थे। प्रतीत होता है कि राजकीय कारखानों की व्यवस्था के अंतर्गत कारीगर स्वतंत्रता के बदले सुरक्षा पाते थे। उन्हें दिन भर सामान्य श्रमिकों की भाँति कडी निगरानी में और निरीक्षक के निर्देशों पर काम करना पड़ता था, जैसा कि पेलसर्ट और डीलायट के विवरण में इस बात का उल्लेख है कि एक यूरोपीय कर्मकार तीन या चार भारतीय कर्मकारों के बराबर कार्य करता है, दो सम्भावनों को दर्शाता है…….या तो भारतीय कर्मकार बहुत सुस्त थे या यहाँ की विशेषत: अत्यन्त बढ़ी-चढ़ी थी। सत्रहवीं शती में कारीगरों के निजी कारखानों के अभाव का कारण प्रतिभा का अभाव नहीं था, जैसा कि बर्नियर का कथन है इंडीज के हर भाग में कुशल लोग थे। कारीगरों के सामने अनेक गम्भीर समस्याएँ थीं…….सबसे बड़ी तो यह कि उनका पारिश्रमिक बहुत कम था। पेलसार्ट जो कि आगरा में डच कारखाने का प्रमुख था, अपने सात वर्षों (1620-1627) के अनुभव के आधार पर कहता है कि तीन वर्गों के लोग ऐसे थे जो नाम के लिए तो स्वतंत्र थे किन्तु जिनकी हैसियत वस्तुतः स्वैच्छिक दासता से अधिक भिन्न नहीं थी-कर्मकार, सेवक और छोटे दुकानदार। इनमें भी कर्मकार दोहरे अभिशप्त थे……स्वर्णकार, चित्रकार, कशीदाकार, कालीन बनाने वाले इत्यादि ——-एक तो इनका पारिश्रमिक बहुत कम था, सुबह से रात तक कार्य करने पर केवल 5 या 6 टके या 5 रुपया ही कमा सकते थे। इसकी पुष्टि डीलायट एवं अन्य विदेशी यात्रियों ने भी की है। सत्रहवीं शती में श्रमिकों की स्थिति का अनुमान आइन-ए-अकबरी में दी गई दैनिक पारिश्रमिक की दर से लगाया जा सकता है। मोरलैंड ने आधुनिक मुद्रा (1920) से इसका मिलान किया है- आम मजदूरों को 2 दाम/5आने, थोडे ऊँचे कर्मकारों को 3-4 दाम/8.5 आने, बढ़इयों को 3-7 दाम/8.5 आने-1.5 रुपये, दरबार के गुलामों (निम्म श्रेणी) को बारह आने प्रतिमाह मिलता था। किन्तु महत्व पारिश्रमिक रूप में मिलने वाले पैसे का नहीं अपितु उसकी क्रयशक्ति का था…….जो अनिवार्यतः जीवन स्तर से जुड़ी थी। यूरोपीय कारखानों के अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि मुगलकालीन भारत में कुशल और अकुशल श्रमिकों पर किस हद तक सरकारी और गैर-सरकारी दबाव थे। पेलसर्ट लिखता है दूसरा (अभिशाप) था गवर्नर, अमीरों, कोतवाल, बक्शी और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार। जब कभी इनमें से किसी को, किसी कर्मकार की सेवाओं की आवश्यकता होती थी तो उससे यह नहीं पूछा जाता था कि वह काम करना चाहता है या नहीं, उसे घर या बाजार से पकड़ कर मंगाया जाता था और यदि वह विरोध करने का प्रयास करता तो उसकी पिटाई की जाती थी और काम करवाने के बाद शाम को आधी मजदूरी या कुछ भी देकर भगा दिया जाता था। मसुलीपतनम के दक्ष कपड़ा छपाई करने वाले कारीगरों को दिल्ली या आगरा में आकर कार्य करने के लिए बाध्य करना लगभग जबरन काम करवाने का एक उदाहरण है। गुजरात प्रान्त के गाँवों और शहरों के कारीगरों को सरकारी अधिकारियों द्वारा जबरन काम लेने से कितना कष्ट होता था इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इसे समाप्त करने के लिए 1665 में औरंगजेब को एक फरमान निकालना पडा।
कुछ यूरोपीय कपनियाँ न केवल दास श्रमिक ही रखती थीं अपितु जबरन श्रम करवाने जैसे हथकडों का प्रयोग भी करती थीं। एक और बात जो कर्मकारों के विरुद्ध जाती थी वह थी दलाली। मैंडेल्सलो (1638) के अनुसार कारीगरों को अपने लाभांश का पर्याप्त भाग दलालों को देना पड़ता था क्योंकि उपभोक्ता और कारीगर के बीच अनेक स्तरों पर दलाल होते थे। इस बात की पुष्टि बर्नियन ने भी की है- वह धनवान् तो कभी हो नहीं सकता और पेट की भूख मिटाना और मोटे-मोटे कपड़ों से तन ढक सकने का प्रबन्ध कर लेना भी उसके लिए बड़ी बात है। पैसा किसी को मिलता है तो व्यापारी को, कर्मकार को नहीं।
ऐसी परिस्थिति में कारीगरों में गैर-आर्थिक रवैये का होना स्वाभाविक ही था। अधिकांश जनता गरीब थी। अत: उसके बीच उत्तम कारीगरी की वस्तुओं की माँग का तो प्रश्न ही नहीं था। उसको जीवन-यापन के लिए सस्ती वस्तुओं की आवश्यकता थी। दमन के भय से लोग अपना थोड़ा बहुत धन भी छिपाते थे और निम्न कोटि का जीवन बिताने के आदि हो गए थे। आम जनता का निम्नस्तरीय जीवन (जिसकी पुष्टि पेलसर्ट, डीलायट एवं अन्य लेखकों ने की है) और कारीगरों का गैर-आर्थिक दृष्टिकोण कार्य-कारण रूप में परस्पर जुड़े हुए थे। अत: आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से अतिरिक्त काम करने के लिए कोई अभिप्रेरणा नहीं थी।
आकांक्षाओं के अभाव के आशिक कारण हिन्दू और मुसलमानों दोनों में ही, श्रम का विभाजन और कड़े जाति-सम्बन्धी नियम भी थे। पेलसर्ट, डीलायट और बर्नियर इसकी पुष्टि करते हैं। जाति का शिकंजा इतना कठोर था कि व्यक्ति या समूहों को आर्थिक गतिशीलता की छूट नहीं थी। श्रमिकों की गतिशीलता भी अत्यन्त सीमित थी। मुगलकालीन भारत में कारीगरों की कुछ भी गतिशीलता नहीं थी क्योंकि इसके लिए व्यापारिक लाभ का कोई प्रोत्साहन नहीं था।
कच्चे माल की कीमत अधिक होती थी और कर्मकार के पास इतनी पूँजी नहीं होती थी कि स्वयं अपना काम आरम्भ कर सके। उसे दलालों या महाजनों पर आश्रित रहना पड़ता था। जिससे शोषण को बढ़ावा मिलता था। कभी-कभी अकबर, जहाँगीर और औरंगजेब द्वारा करों को माफ या कम करने के उल्लेख मिलते हैं। अकबर ने अनेक प्रकार के करों में छूट देकर कर्मकारों को राहत पहुँचाने का प्रयास किया, उदाहरण के लिए चमड़ा बनाने और चूना उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्योगों पर। मीरात-ए-अहमदी में उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के लाइसेंस करों को समाप्त किया। इसके पूर्व कारीगरों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती थी।
ऐसी विषम परिस्थितियों में अनेक शिल्पी ऊँचे मानदंड स्थापित करते थे। इस सम्बन्ध में बर्नियर का कहना है- ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ कारीगरों ने सुन्दर शिल्पों की रचना की है और ये कारीगर ऐसे हैं जिनके पास न तो अपने औजार होते हैं और न ही यह कहा जा सकता है कि उन्हें किसी उस्ताद ने प्रशिक्षण दिया है। कभी-कभी तो वे यूरोपीय वस्तुओं की इतनी नकल कर लेते हैं कि असल और नकल में भेद करना कठिन हो जाता है। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त भारतीय कारीगर बढ़िया बंदूकें, शिकारी बंदूकें और ऐसे सुन्दर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि यूरोपीय स्वर्णकारों के लिए इनकी कारीगरी को मात देना सम्भव प्रतीत नहीं होता। मुझे तो इनकी चित्रकृतियाँ एवं सूक्ष्य कलाकृतियाँ प्राय: मुग्ध करती हैं, विशेष रूप से एक ढाल पर चित्रित अकबर के अभियानों को देखकर तो मैं चकित रह गया। कहा जाता है कि इसे बनाने में एक प्रसिद्ध चित्रकार को 7 वर्ष लगे। मेरे विचार से यह अनूठी कारीगरी है। भारतीय चित्रकारों की कृतियों में मुख्य दोष यह है की उसमे समानुपात का आभाव होता है और चेहरे भावशून्य होते हैं, किन्तु इन दोषों को सरलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें ऐसे गुरू मिल जाएँ जो उन्हें कला सम्बन्धी नियमों का ज्ञान करा सके। यह धारणा उचित ही है कि यदि परिस्थितियाँ अनुकूल होती तो कला का स्तर और ऊँचा हो सकता था। यह स्तर कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित न रहकर, भारतीय कला का आम स्तर हो सकता था।
वस्तुत: कारीगरों के लिए कतिपय अनुकूल परिस्थितियाँ भी थीं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि उन्हें पादशाह की ओर से प्रोत्साहन मिलता था। अकबर ने अपने अमीरों की कुछ श्रेणियों को निर्देश दे रखा था कि वे विशेष प्रकार के स्थानीय कपडे ही पहनें। उसने फारस के कालीन बुनकरों को भी आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में आकर बसने के लिए राजी किया था। इस प्रकार के प्रश्रय से देश में रेशम, कालीन और शाल उद्योगों का बड़ा विकास हुआ और इन कार्यों में लगे कारीगरों की स्थिति में भी सुधार हुआ। अकबर ने होशियार कारीगरों को गोवा भेजा ताकि वे वहाँ के तत्कालीन विभन्न कला-कौशलों की प्राप्त करें और उनके सम्बन्ध में पादशाह को बता सके। वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लौटने वाले कारीगरों के हुनर की तारीफ होती थी।
दूसरी अनुकूल बात थी कुछ शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अमीर वर्ग द्वारा कारीगरों को प्रोत्साहन देना। किन्तु यह प्रतिकूल परिस्थितियों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बर्नियर का कथन है कि कलात्मक हस्तशिल्पों का पतन दो कारणों से धीमा रहा- एक तो शाही कर्मशालाओं के कारण और दूसरे कुछ शक्तिशाली आश्रयदाताओं के प्रभाव के कारण, जो कारीगरों को अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक दिलाने में सहायक हुआ। इसकी पुष्टि अन्य लेखकों ने भी की है।
शाही कर्मशालाएँ प्रतिभा का प्रसार करने एवं देश के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध हुई। सभी दक्ष और प्रशिक्षित कारीगरों या नवशिक्षुओं जैसे कि चित्रकार एवं संगीतज्ञ को इन कर्मशालाओं में स्थान नहीं मिलता था। बचे हुए लोगों को अमीर और राजा अपने पास रख लेते थे। इससे कला एवं शिल्प को बढ़ावा मिलता था।
कुल मिलाकर सोलहवीं और सत्रहवीं शती के सूत्रों में तत्कालीन शिल्पियों, कारीगरों और औद्योगिक कर्मकारों की स्थिति को खराब चित्रित किया गया है। मोरलैंड के अनुसार सत्रहवीं शती के मध्य में इन लोगों की स्थिति खराब थी। ये मुख्य रूप से व्यापारियों, खरीदारों और दलालों के फायदे के लिए काम करते थे और अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए उन पर आश्रित रहते थे। आड़े वक्त के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। उनकी एकमात्र आशा थी कि कोई शक्तिशाली एवं धनी आश्रयदाता उन्हें प्रश्रय दे दे। किन्तु ऐसा सुअवसर कुछ ही भाग्यशालियों को मिल पाता था। अधिकांश कर्मकार तो बडी कठिनाई से जीवनयापन के साधन जुटा पाते थे।